जब भारतीय डॉक्टर ने मिट्टी से निकाली कैंसर की दवा
डॉक्टर सुरेन्द्रनाथ सहगल ने रापामाइसिन की खोज की जो आज लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के काम आती है .यह दवा अंग प्रत्यर्पण के वक्त दी जाती है, इसके अलावा ऑटो-इम्यून डिसऑर्डर्स और कैंसर के इलाज में भी इसका उपयोग होता है.
Advertisement
Comment Section
वीडियो देखें-ये भारतीय न होता तो दुनिया के नक़्शे पर तिब्बत न दिखाई देता

.webp?width=120)




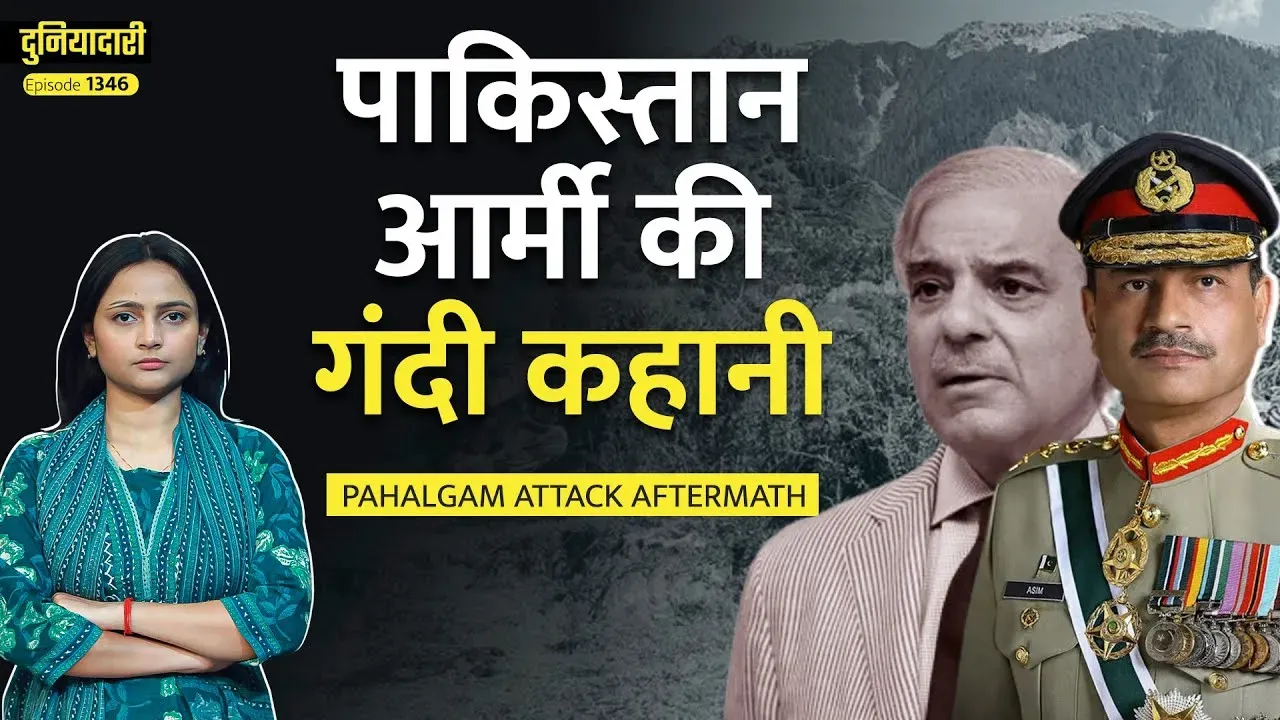



.webp)
