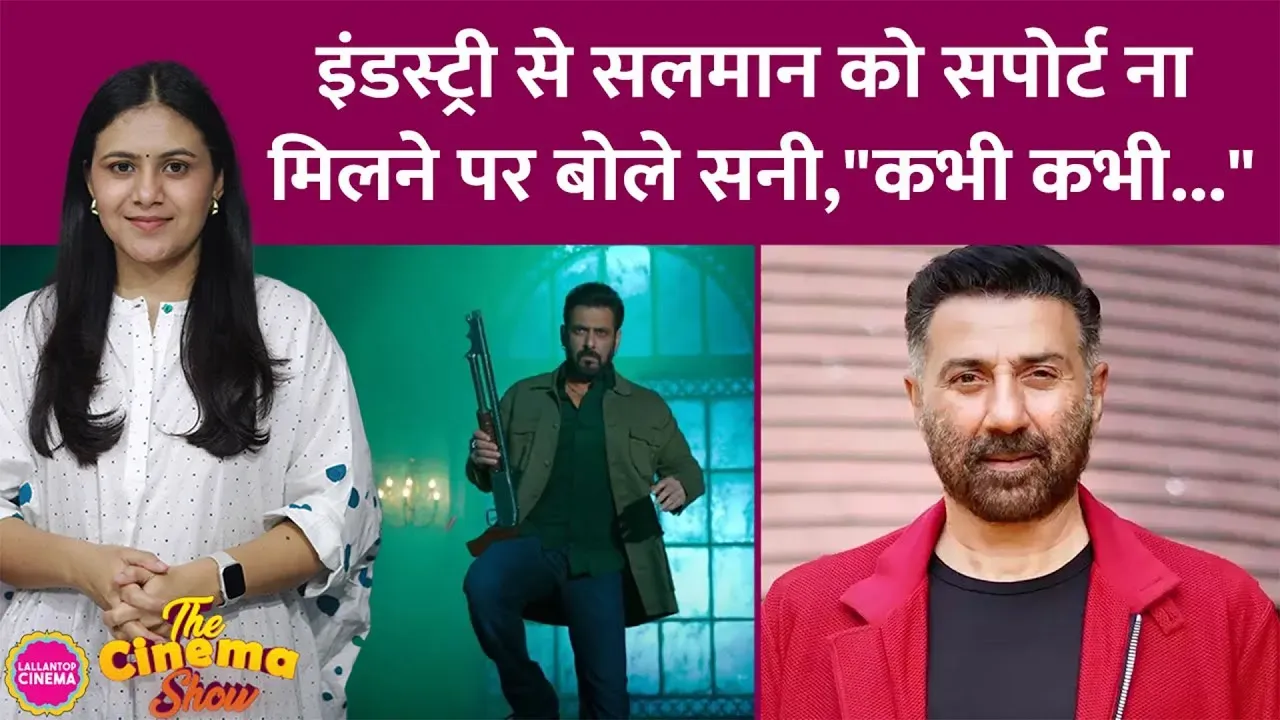वे चार्ली चैपलिन के लैवल की आर्टिस्ट थीं. बस दोनों की विषय-वस्तु में फर्क था. लेकिन बुनियादी लोगों पर पड़ने वाला टुनटुन का असर भी उतना ही था. हिंदी न बोल सकने वाले जो करोड़ों, ग्रामीण-कस्बाई दर्शक हिंदी फिल्मों के डायलॉग नहीं समझते थे, वे चैपलिन के दीवाने थे. वे टुनटुन के भी दीवाने थे. क्योंकि दर्शक को जोड़ने के लिए वे महज भाषा पर निर्भर नहीं रहती थीं.
उनकी फिल्में कैसी थीं? टुनटुन की कॉमेडी कैसी थी?वे हमेशा एक मोटी लड़की के रोल में होती थीं जिसका कनेक्टिंग पॉइंट उसका मोटापा होता था. ऐसी औरत जो किसी भी मर्द का बुरा सपना होगी. पुरुषों की फैंटेसी जबकि पतली, मांसल, गोरी, हिरणी जैसी आंखों वाली, लाल होठों वाली, रेशमी जुल्फों वाली, पढ़ी-लिखी, शर्माने वाली, सिल्की कपड़े पहनने वाली, खनकती आवाज वाली, नज़ाकत की प्रतिमूर्ति, रसखान की कविताओं की नायिका होती थीं/हैं. टुनटुन के रोल ठीक उलट थे. फूहड़, गंवार, मोटी, सांवली, अजीब कपड़े पहनने वाली, डराने वाली, उत्तेजना भगा देने वाली, मर्दों के पीछे भागने वाली, उसके साथ सेक्स की हसरत रखने वाली, जिसे कोई पसंद नहीं करता था, राह देखने वाली कि कोई उससे शादी कर ले, बच्चों जैसी, बद्तमीज, भद्दे जिस्म वाली.
मगर जो भी कह लो थीं बहुत कमाल की, इसी वीडियो को टाइम निकाल के देख लीजिए. कसम से मारक मजा मिलेगा:https://youtu.be/NQX-0-fW6Fk
तब ऐसी ही कॉमेडी होती थी जिसमें कोई फिसलकर गिर जाए तो हम हंसते थे. मोटी लड़की की शादी नहीं होती थी तो हम हंसते थे. हालांकि आज भी दर्शकों का स्तर बिलकुल वैसा ही बना हुआ है. टीवी और यूट्यूब पर 2016 में ऐसे कॉमेडी शो की व्यूअरशिप बेहिसाब है.
टुनटुन जिनका पूरा नाम उमा देवी खत्री था, उन्हें हिंदी फिल्मों ने स्टीरियोटाइप्स से भरे रोल दिए. जिनकी बहुत आलोचना की जा सकती है. जो औरतों को नीचा करने वाले थे. इसमें चर्चा का विषय नहीं है. लेकिन इसमें उमा का कोई दोष नहीं था. वे हास्य कलाकार थीं, कंटेंट प्रगतिशील होता तो वैसा कर लेतीं, पेट पालने के लिए वो करती गईं जो स्क्रिप्ट वाले ने लिखा और निर्माताओं ने लिखवाया. 'बाबुल' (1950), 'हाफ टिकट' (1962), 'सुहागरात' (1968), 'पंडित और पठान' (1977) जैसी फिल्मों में तब वे वही कर रही थीं जो आज मेलिसा मेकार्थी 'ब्राइड्समेड्स', 'हैंगओवर-3', 'द हीट', 'टैमी' में कर रही हैं और ऐसा करके टॉप फीमेल कॉमेडी/एक्टर हैं.
उमा से टुनटुन नाम रखने के बाद वे इतनी लोकप्रिय हुई थीं कि टुनटुन का पर्यायवाची शब्द ही मोटी औरत हो गया. इसे उन्होंने अच्छे रूप में ही लिया. एक्ट्रेस के अलावा उमा की बड़ी पहचान गायिका की भी थी. उनके जीवन का पहला ही गाना था 'अफसाना लिख रही हूं दिल-ए-बेक़रार का'. 1947 में रिलीज हुई 'दर्द' फिल्म से ये गाना बहुत हिट हुआ था. आज भी सुना जाता है. फिल्म में उनके गाए बाकी गाने भी बहुत अच्छे थे. उन्होंने तब की बाकी गायिकाओं के मुताबिक क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली थी इसलिए उनकी सीमाएं थीं. लेकिन वे वाकई में बहुत ही विशेष गायिका थीं. उनके गानों में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं थे, वे बहुत अच्छे थे.
जरा इस गाने पे भी ठुमक लीजिए-https://youtu.be/3G9uGb_PEuY
उनकी सब पहचानों को फीका करने वाला था उनका व्यक्तित्व. उनकी उपस्थिति बहुत ही dominating और ताकतवर थी. जहां वे मौजूद होती थीं, हर मर्द तमीज़ सीख जाता था. उन जैसी तेज-तर्रार, वाकपटु, बेधड़क और चतुर communicator दुर्लभ हैं. वो भी तब, जब वे पढ़ी लिखी नहीं थीं. बचपन त्रासदियों में बीता. एक के बाद एक दुख मिलते रहे. म्यूजिक, एक्टिंग, सम्मान हर चीज उन्होंने अपने हौसले से प्राप्त की, नसीब से नहीं. पुरुषों के वर्चस्व वाली दुनिया में वे चट्टान की तरह न हिलाई जा सकने वाली थीं.
 अपने समय के साथी मेल कॉमेडियन्स के बीच टुनटुन/उमा.
अपने समय के साथी मेल कॉमेडियन्स के बीच टुनटुन/उमा.उत्तर प्रदेश के एक गांव में 1923 में उनका जन्म हुआ था. दिन था 11 जुलाई. अस्सी बरस जिंदा रहीं. सही मायनों में ज़िंदादिली के साथ. 24 नवंबर, 2003 को उन्होंने आखिरी सांसें ली. उनका आखिरी इंटरव्यू 27 अक्टूबर को फिल्म लेखक और इतिहासकार शिशिर कृष्ण शर्मा ने लिया था. वे सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने आ रही थीं. शिशिर बताते हैं, "मैं तय समय पर उस मीटिंग में पहुंचा. मंच पर बैठी दुबली-पतली, बुज़ुर्ग टुनटुन को सामने देखते ही उनकी वो इमेज भरभराकर ढह पड़ी जिसे मैं अभी तक सिनेमा के परदे पर देखता आया था. मंच पर मौजूद दिलीप कुमार, चन्द्रशेखरजी, धर्मेन्द्र, अमरीश पुरी और दारासिंह जैसे वरिष्ठ कलाकारों को उनके साथ बेहद अदब से पेश आते देखा. इतनी उम्र हो जाने के बावजूद टुनटुन की चुहलबाज़ी, गर्मजोशी और चुटीली बातों में कोई कमी नहीं आई थी. मैंने उन्हें अपना परिचय देते हुए उनका इंटरव्यू करने की इच्छा बताई तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी. शाम 6 बजे मैं अपने फोटोग्राफर साथी अनिल मुरारका के साथ टुनटुन के पाली विलेज स्थित घर पर पहुंचा. मस्तमौला स्वभाव, चुटीली बातें, बात-बात पर हंसना-हंसाना भले ही उनके व्यक्तित्व का जगज़ाहिर पहलू था लेकिन वास्तव में उसके पीछे अथाह दर्द छुपा हुआ था. ज़िन्दगी में उन्होंने शायद ही कभी कोई सुख देखा हो."
टुनटुन के गुजरने से दो दिन पहले ये इंटरव्यू छपा था. शिशिर लिखते हैं, "मैंने उन्हें फोन करके बताया कि अखबार की प्रति उन्हें कुरियर से भिजवा रहा हूं. इस पर उन्होंने अपनी चिरपरिचित स्टाइल में कहा, 'अखबार कुरियर से भेज रहा है तो फिर इंटरव्यू भी फोन पर ही ले लेना था'. क़रीब आधा घंटे बाद उन्होंने फोन तब बंद किया जब मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्द ही उनसे मिलने आऊंगा. लेकिन मैं वादा निभा नहीं पाया. वो अपना ये आखिरी इंटरव्यू भी नहीं पढ़ पाईं. अगली ही सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें बांद्रा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां 24 नवंबर 2003 की सुबह क़रीब 5 बजे उनका देहांत हो गया."
ये बातचीत शिशिर जी के बेहद दुर्लभ ब्लॉग बीते हुए दिन
से बड़े आभार के साथ यहां प्रस्तुत कर रहे हैं.
उमा देवी / टुनटुन

' मुझे याद नहीं कि मेरे माता-पिता कौन थे और कैसे दिखते थे. मैं दो-ढाई बरस की रही होऊंगी जब वो गुजरे थे. घर में मुझसे आठ-नौ साल बड़ा एक भाई था जिसका नाम हरी था. मुझे बस इतना याद था कि हम लोग अलीपुर नाम के गांव में रहते थे. गांव के बीच में एक तालाब था जिसमें बत्तखें तैरती रहती थीं'.
मेरा भाई गांव की रामलीला में भाग लेता था. एक रोज़ मैं किसी घर की छत पर बैठी रामलीला देख रही थी कि मुझे नींद आ गयी और मैं लुढ़ककर नीचे गिर पड़ी. भाई मेरा इतना ख्याल रखता था कि वो रामलीला के बीच में ही मंच छोड़कर मुझे उठाने के लिए दौड़ पड़ा था. उस वक़्त मैं तीन-चार बरस की और भाई बारह-तेरह बरस का रहा होगा.
लेकिन एक रोज़ भाई भी ग़ुज़र गया और दो वक़्त की रोटी के एवज़ में रिश्तेदारों के लिए चौबीस घंटे की नौकरानी छोड़ गया. अब रिश्तेदारी-बिरादरी में जहां कहीं भी शादी-ब्याह-जीना-मरना हो काम के लिए मुझे भेजा जाने लगा. मेरा अन्दाज़ है कि अलीपुर शायद दिल्ली के आसपास कहीं था क्योंकि अक्सर घरेलू काम के सिलसिले में मुझे दिल्ली के दरियागंज इलाक़े में किसी रिश्तेदार के घर आते-जाते रहना पड़ता था.
उसी दौरान एक रोज़ पड़ोसियों से पता चला था कि अलीपुर में हमारी काफी ज़मीनें थीं जिन्हें हड़पने के लिए पहले मेरे माता-पिता का और फिर भाई का क़त्ल कर दिया गया था.
गाने का शौक़ मुझे बचपन से था. लेकिन गुनगुनाते हुए भी डर लगता था क्योंकि उन लोगों में से अगर कोई गाते हुए सुन लेता, तो मार पड़ती थी. उन्हीं दिनों दिल्ली में मेरी मुलाक़ात एक्साइज़ विभाग में इंस्पेक्टर अख्तर अब्बास काज़ी से हुई.
उन्होंने मुझे सहारा दिया तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा. लेकिन तभी मुल्क़ का बंटवारा हुआ और काज़ी साहब लाहौर चले गए. इधर हालात से तंग आकर फिल्मों में गाने का ख्वाब लिए मैं एक रोज़ चुपचाप बंबई भाग आयी. दिल्ली में किसी ने निर्देशक नितिन बोस के असिस्टेंट जव्वाद हुसैन का पता दिया था, सो उनसे आकर मिली और उन्होंने मुझे अपने यहां पनाह दे दी. उस वक़्त मेरी उम्र बहुत कम थी. काज़ी साहब का मन लाहौर में नहीं लगा इसलिए मौक़ा पाते ही वो भी बंबई चले आए और फिर हमने शादी कर ली. ये सन् 1947 का वाक़या है.
मैं काम की तलाश में थी. डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार उन दिनों फिल्म 'दर्द' बना रहे थे. एक रोज़ उनके स्टूडियो में पहुंची और बेरोक-टोक उनके कमरे में घुसकर बेझिझक उन्हीं से पूछ बैठी, 'कारदार कहां मिलेंगे, मुझे गाना गाना है!' दरअसल मैं न तो कारदार को पहचानती थी और न ही फिल्मी तौर-तरीक़ों से वाक़िफ थी. शायद मेरा यही बेतक़ल्लुफी भरा अंदाज़ कारदार को पसन्द आया जो बिना नानुकुर किए उन्होंने नौशाद साहब के असिस्टेंट ग़ुलाम मोहम्मद को बुलाया और मेरा टेस्ट लेने को कहा.
ग़ुलाम मोहम्मद ढोलक लेकर बैठे तो मैंने उनसे ठीक से बजाने को कहा. मेरे बेलाग तरीकों से वो भी हक्के-बक्के थे. बहरहाल मैंने फिल्म 'ज़ीनत' का नूरजहां का गाया गीत 'आंधियां ग़म की यूं चलीं' गाकर सुनाया जो सबको इतना पसन्द आया कि मुझे पांच सौ रुपए महीने की नौकरी पर रख लिया गया.
पहला गीत जो मेरी आवाज़ में रेकॉर्ड हुआ, वो था 1947 में बनी फिल्म 'दर्द' का 'अफसाना लिख रही हूं दिल-ऐ-बेक़रार का'. ये गीत इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि मुझे आज तक इसी से पहचाना जाता है.
इस फिल्म में मेरे गाए बाक़ी तीनों गीत 'आज मची है धूम', 'ये कौन चला' और सुरैया के साथ 'बेताब है दिल' भी काफी पसन्द किए गए. उसी साल बनी फिल्म 'नाटक' में मैंने 'दिलवाले, जल कर ही मर जाना' गाया. साल 1948 में बनी फिल्म 'अनोखी अदा' में मेरे दो सोलो गीत 'काहे जिया डोले हो कहा नहीं जाए' और 'दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया' थे. 1948 में प्रदर्शित हुई 'चांदनी रात' में मुझे उस फिल्म का शीर्षक गीत 'चांदनी रात है, हाए क्या बात है' गाने का मौक़ा मिला था.
उसी साल बनी फिल्म 'दुलारी' में मैंने शमशाद बेगम के साथ मिलकर गाया था - 'मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग'. इन सभी फिल्मों के संगीतकार नौशाद साहब थे. इसके अलावा मैंने 'चन्द्रलेखा', 'हीर रांझा' (1948), 'भिखारी', 'भक्त पुण्डलिक', 'प्यार की रात, 'सुमित्रा', 'रूपलेखा', 'जियो राजा', 'हमारी किस्मत' (1949), 'भगवान श्री कृष्ण' (1950), 'सौदामिनी' (1950), 'दीपक' (1951), 'जंगल का जवाहर' (1952) और 'राजमहल' (1953) जैसी फिल्मों में भी गीत गाए.
चूंकि संगीत और गायन की मैंने विधिवत शिक्षा नहीं ली थी और उधर बच्चों के जन्म के साथ घरेलू ज़िम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थीं इसलिए बतौर गायिका मेरा करियर ज़्यादा नहीं चल पाया. मेरे गाए गीतों की कुल संख्या क़रीब 45 होगी. यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि मुझे सिंदूर खिलाकर मेरी आवाज़ खराब कर देने वाली जो बात अक्सर कही-सुनी जाती है, वो महज़ अफवाह है. उसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है.
कुछ समय मैं फिल्मों से दूर रहकर अपने परिवार में उलझी रही. पति नौकरी करते थे लेकिन परिवार बढ़ने के साथ उनका वेतन कम पड़ने लगा तो मजबूरन मुझे एक बार फिर से काम की तलाश में निकलना पड़ा. मैं नौशाद साहब से मिली जो उन दिनों फिल्म 'बाबुल' बना रहे थे. उन्होंने मुझे उस फिल्म में एक हास्य भूमिका करने को कहा जिसे मैंने स्वीकार कर लिया. हालांकि इससे पहले फिल्म 'दर्द' में भी वो मुझे एक रोल ऑफर कर चुके थे लेकिन तब मैं अभिनय के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं थी.
उमादेवी की जगह टुनटुन नाम भी मुझे फिल्म 'बाबुल' में नौशाद साहब ने ही दिया था.
आगे चलकर यही नाम मेरी पहचान बन गया. मेरा ये रूप दर्शकों को बेहद पसन्द आया और देखते ही देखते मैं हिन्दी फिल्मों की अतिव्यस्त हास्य अभिनेत्री बन गयी. फिर तो 'उड़न खटोला', 'बाज़', 'आरपार', 'मिस कोकाकोला', 'मि. एंड मिसेज़ 55', 'राजहठ', 'बेगुनाह', 'उजाला', 'कोहिनूर', 'नया अंदाज़', '12 ओ क्लॉक', 'दिल अपना और प्रीत पराई', 'कभी अन्धेरा कभी उजाला', 'मुजरिम', 'जाली नोट', 'एक फूल चार कांटे', 'कश्मीर की कली', 'अक़लमन्द', 'सीआईडी 909', 'दिल और मोहब्बत', 'एक बार मुस्कुरा दो' और 'अन्दाज़' जैसी दर्जनों फिल्में मैंने कीं.
'सत्तर के दशक में मेरी सक्रियता में कमी आनी शुरू हुई और फिर 'क़ुर्बानी' और 'नमक हलाल' जैसी फिल्में करने के बाद मैंने खुद को अभिनय से दूर कर लिया. नब्बे के दशक की शुरुआत में काज़ी साहब गुज़रे. अब दोनों बेटों और दोनों बेटियों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद होने के बाद पिछले क़रीब बीस बरस से मैं घर पर ही रहकर आराम कर रही हूं'.
*** **** ***
जितना ज्यादा आदर किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, वो उमा देवी के लिए हमेशा रहेगा.
टॉम ऑल्टर के साथ उनका ये इंटरव्यू भी उनके आखिरी दिनों का है. इसमें उनकी सत्ता साक्षात देखी जा सकती है.
https://youtu.be/xg-MoJmdKRg
वीडियो देखें: सलमान की हिरोइन बनने पर ट्रोल हुई आलिया ने दिया करारा जवाब 










.webp)