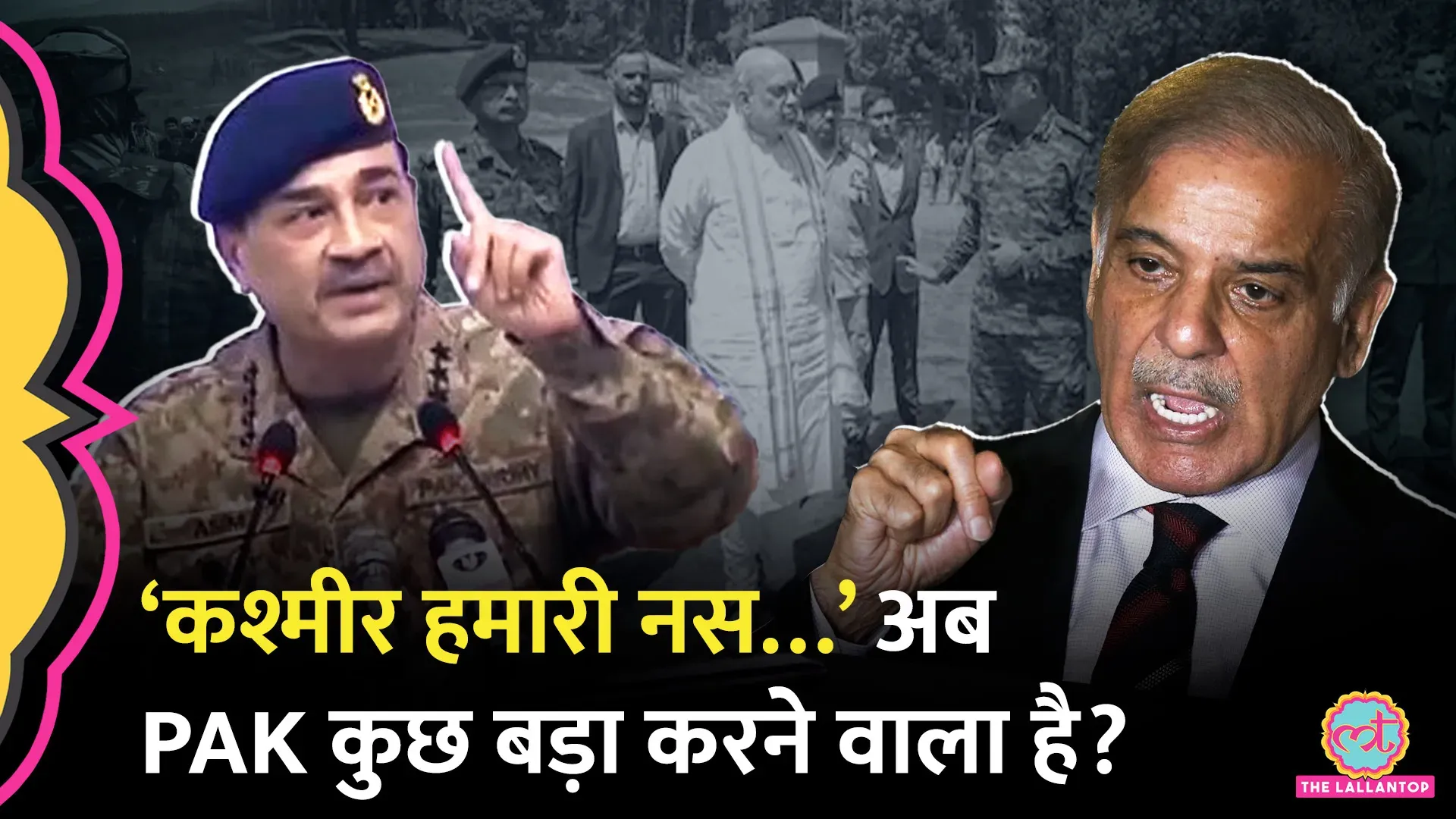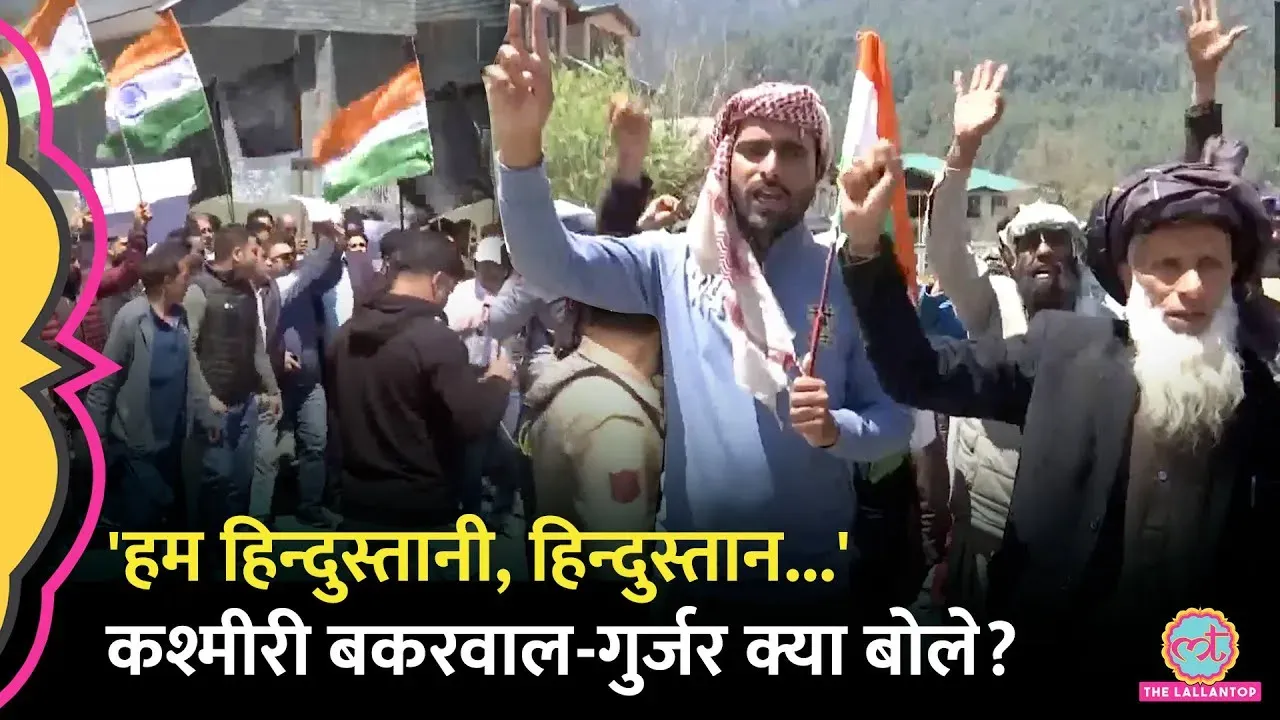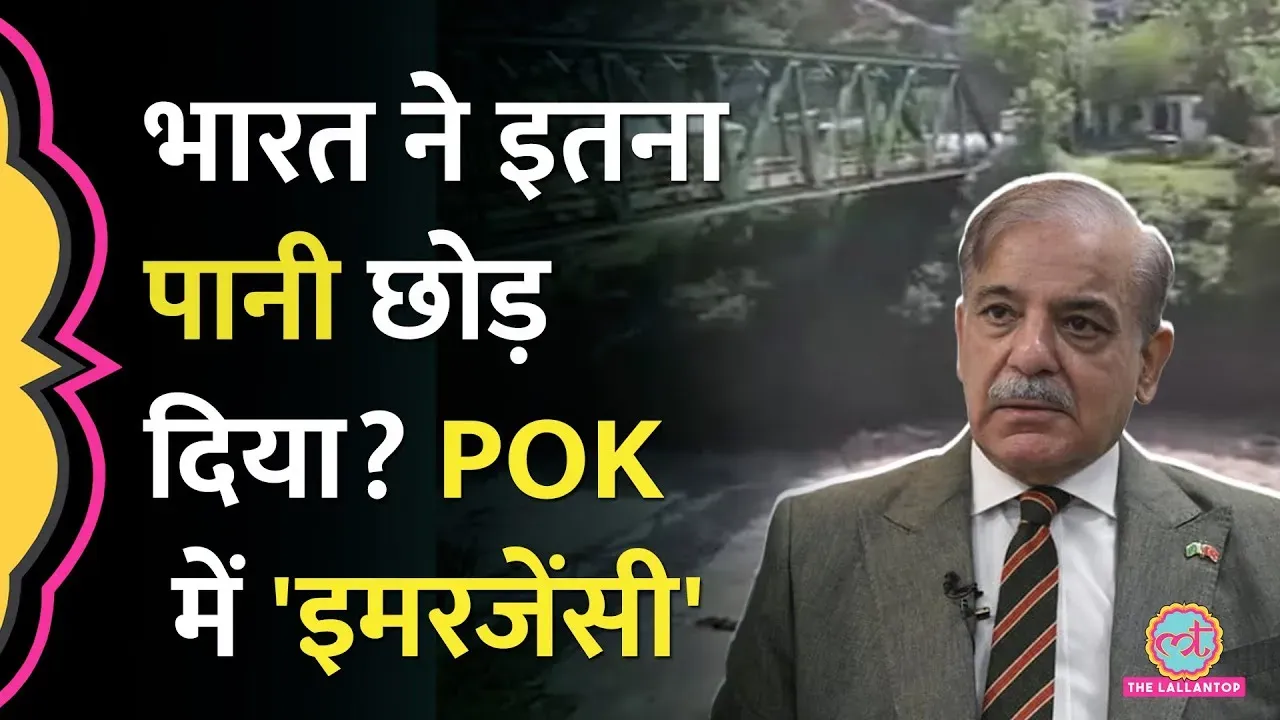आज 6 दिसंबर है. भारत के वर्तमान को गढ़ने वाली दो घटनाओं का संबंध इस तारीख से है. एक, जिसके बारे में आपमें से ज़्यादातर लोग जानते ही हैं - बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद. और दूसरी घटना, या कहें फेनोमिना थे - डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहब भी कहा जाता है. एक नामी स्कॉलर, नौकरशाह, कानूनविद, समाज सुधारक और राजनेता - जिन्होंने आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. और ये करते हुए वो किसी धारा के बंधक नहीं हुए. उन्होंने एक अलहदा और स्पष्ट लकीर खींची. आज ही के दिन, साल 1956 में उनका देहांत हो गया था. इस घटना को डॉ आंबेडकर का महापरिनिर्वाण कहा जाता है. महापरिनिर्वाण क्यों? क्योंकि डॉ आंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था. इसीलिए उनका अंतिम संस्कार भी बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही किया गया.
डॉ आंबेडकर का महापरिनिर्वाण कहा जाता है. लेकिन क्यों?
डॉ आंबेडकर ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में ढेर सारे ऐसे काम किए, जिनपर लंबी बहस की जा सकती है.

डॉ आंबेडकर ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में ढेर सारे ऐसे काम किए, जिनपर लंबी बहस की जा सकती है. पक्ष और विपक्ष में तर्क दिये जा सकते हैं. आज दी लल्लनटॉप शो में हम इनमें से एक काम को चुन रहे हैं - धर्म परिवर्तन. डॉ आंबेडकर अपने अनुभवों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, कि वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं बने रह सकते. इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया. और उन्हें देखते हुए उनके अनुयायियों ने भी. भारत में धर्म परिवर्तन को लेकर जो बहस है, उसके इतिहास में ये घटना एक मील का पत्थर थी. फिर हमारे सामने धर्म के विषय पर संविधान सभा और उसके बाद आई संसद में हुई बहसें हैं. और वो राजनीति है, जो बात को कब कहां से कहां पहुंचा दे, कहा नहीं जा सकता. आज जब धर्म परिवर्तन की बात होती है, तो उसका संदर्भ बदला हुआ है. डॉ आंबेडकर समाज सुधार की बात कर रहे थे, उसी को लेकर उनकी स्कॉलरशिप और राजनीति रही. लेकिन आज की राजनीति जनसंख्या के अनुपात, धर्मरक्षा, लव जिहाद आदि कीवर्ड्स पर चल रही है. ये विरोधाभास ही है कि ये सब करते हुए भी भारत का कोई राजनैतिक दल डॉ आंबेडकर को पीठ दिखाने की कोशिश नहीं करता. इन सब से इतर संसद से पास कानून हैं और सर्वोच्च न्यायालय में चल रही जिरह भी. सो आज दिन की बड़ी खबर में हम इसी विषय के पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे.
हम ये स्पष्ट कर दें कि न डॉ आंबेडकर और न ही धर्म परिवर्तन ऐसे विषय हैं कि एक एपिसोड में समा सकें. इसीलिए ये संभव है कि कुछ चीज़ों का उल्लेख छूट भी जाए. यहां मकसद ये है कि आप धर्म परिवर्तन पर बहस के प्रमुख पहलुओं से वाकिफ हो जाएं. एक और बात. आज के विषय में दो शब्दों का बार बार इस्तेमाल होगा - दलित और अछूत. दलित का अर्थ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं. एक समय था, जब दलितों को अछूत समझा जाता था. तब इस विषय पर बात करते हुए अछूत शब्द का ही इस्तेमाल होता था. इसीलिए जहां ऐतिहासिक संदर्भ होगा, हम इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे ताकि मूल भावना बरकरार रहे. ये बाद दर्ज की जाये कि भारत के कानून के तहत अस्पृश्यता या अनटचेबिलेटी, तथा जातीय आधार पर भेदभाव कानूनन अपराध है और इसके लिए सज़ा का प्रावधान भी है.
सबसे पहले ये जानें कि डॉ आंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला क्यों और कैसे लिया. इसके लिए हम इतिहास पर हमारी खास पेशकश तारीख के एक एपिसोड का सहारा लेंगे. ये 6 दिसंबर 2021 को हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था. इसमें हमारे साथी कमल भट लिखते हैं - बचपन से जाति प्रथा का दंश झेल चुके आंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक में एक घोषणा की. जिसमें उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं. इसके अगले साल यानी 1936 में उन्होंने महार सम्मेलन के दौरान एक और भाषण दिया. जो ‘मुक्ति कोण पथे’नाम से इतिहास में दर्ज है. इसका मराठी से हिंदी में तर्जुमा करने पर बनता है - ‘मुक्ति का मार्ग क्या है’. इस भाषण में उन्होंने सिलसिलेवार रूप से तर्क दिए कि दलितों को अपना धर्म बदलने की ज़रूरत क्यों है. डॉ साहब कहते हैं,
“यह दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच का संघर्ष नहीं बल्कि दो वर्गों के बीच का संघर्ष है. यह एक आदमी पर दूसरे के प्रभुत्व या अन्याय का सवाल नहीं. यह एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व का, एक वर्ग द्वारा दूसरे के साथ किए गए अन्याय का प्रश्न है.''
इसी बात को डॉ आंबेडकर अपने दूसरे भाषणों में और विस्तार देते हैं. सुनिए डॉ अरविंद अरविंद कुमार को. आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के Centre for the Study of Social Exclusion and Inclusive Policy में पढ़ाते हैं और दलित मामलों के जानकार हैं.
ऐसे तर्कों के आधार पर डॉ आंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने का इरादा पक्का किया. अब प्रश्न था कि ये धर्म छोड़ें, तो पकड़ें कौनसा. एक बार फिर हम आपको कमल द्वारा लिखे तारीख के एपिसोड पर ले जाना चाहते हैं. इस एपिसोड में दर्ज है -
डॉ आंबेडकर का मानना था कि दलितों में संगठन का अभाव है. इसलिए उन्हें एक ऐसे धर्म को चुनना होगा जो संख्या में अधिक हों और अन्याय का विरोध कर सके. तो आंबेडकर के शुरुआती लेखों और भाषणों में उनका झुकाव इस्लाम की ओर दिखता है. 1929 में ‘बहिष्कारी भारत’ के एडिटोरियल लेख ‘नोटिस टू हिंदूइज़्म’ में वो लिखते हैं,
‘धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो’
तब हिंदुत्ववादी संगठनों को इससे ख़तरा लगा तो उन्होंने डॉ आंबेडकर के सामने आर्य समाज या सिख धर्म चुनने का प्रस्ताव रखा. लेकिन कुछ ही सालों में आंबेडकर को समझ आया कि सिख धर्म भी जाति प्रथा से अनछुआ नहीं है. इसलिए उन्होंने इसका विचार त्याग दिया. 1936 में अपनी घोषणा के अगले 20 सालों तक आंबेडकर सही धर्म के सवाल पर जूझते रहे.
उनके हिसाब से एक व्यक्ति के विकास के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है- करुणा, समानता और स्वतंत्रता. उनके मतानुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में इन तीनों का ही अभाव था. सांसारिक पक्ष के लिए आंबेडकर को इस्लाम और ईसाई धर्म में ये तीनों चीज़ें दिखाई दी. लेकिन उनके लिए धर्म का आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत ज़रूरी था. धर्म के आध्यात्मिक पक्ष के बारे में लिखते हुए वो चारों धर्मों की तुलना करते हैं. उनका कहना था, ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की है जो खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं. और ऐसा माने बिना कोई भी ईश्वर के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता. इस्लाम के संस्थापक मुहम्मद ना सिर्फ़ खुद को पैग़म्बर घोषित करते हैं, बल्कि जन्नत में जाने के लिए ये मानना भी ज़रूरी है कि वो आख़िरी पैग़म्बर हैं. उनके बाद और कोई पैग़म्बर नहीं पैदा हो सकता. हिंदू धर्म के बारे में डॉ आंबेडकर कहते हैं, हिंदू धर्म में कृष्ण ने ईसा मसीह और मुहम्मद से भी आगे जाकर खुद को ईश्वर घोषित कर दिया.
अंत में डॉ आंबेडकर इन तीनों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हैं. बुद्ध एक साधारण इंसान थे. उन्होंने कभी भी ईश्वर होने का दावा नहीं किया. कोई चमत्कार नहीं किया. उन्होंने खुद को मुक्ति देने वाला ना कहकर मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला कहा. तर्क और विज्ञान के विद्यार्थी रहे आंबेडकर के लिए धर्म पारलौकिक नहीं हो सकता था. उनका कहना था कि धर्म इंसान के लिए हैं ना कि भगवान के लिए. और जाति का सवाल ही जब बराबरी का सवाल था, तो ऐसी किसी धर्म की जगह कहां बचती थी, जिसमें एक व्यक्ति बाक़ियों से ऊपर हो जाए. तो देखा आपने, धर्म परिवर्तन को लेकर आंबेडकर ने क्षणिक आवेष में फैसला नहीं लिया. उन्होंने साइंटिफिक तरीके से प्रयोग किए. और नतीजों के आधार पर तय किया कि किस राह जाना है. वो स्वयं इस राह पर चले और दूसरों को भी प्रेरित किया. दलितों के उत्थान के लिए डॉ आंबेडकर ने जो रास्ता चुना, उसके लिए उन्होंने विरोध या आलोचना नहीं झेली, ऐसा नहीं है. स्वयं महात्मा गांधी और उनके बीच पूना पैक्ट को लेकर एक लंबी बहस हुई. बात ये थी, कि 16 अगस्त 1932 के कम्यूनल अवार्ड में अंग्रेज़ सरकार ने मुस्लिम, यूरोपीयन, सिख, एंगलो-इंडियन व भारतीय ईसाइयों के साथ-साथ अछूतों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की. माने केंद्रीय व प्रांतीय विधान-मंडल में अछूत, अछूतों के लिए ही वोट डालते. गांधी का मानना था कि यह हिंदुओं को बाँटने का प्रयास है और वे अलग निर्वाचन क्षेत्र हटाने तक आमरण अनशन करेंगे.
तब महात्मा गांधी और डॉ आम्बेडकर के बीच में बातचीत कराई गई. और बातचीत में ये सामने आया कि अछूतों को लेकर गांधी और अंबेडकर के दृष्टिकोण में अंतर था. अंतर ये, कि गांधी कम्यूनल अवार्ड को संदेह की नज़र से देखते थे. उन्हें डर था यह कि ये सवर्णों को अछूतों से अलगाव की दिशा में ले जाएगा. वहीं दूसरी ओर आम्बेडकर इस तर्क पर दृढ़ थे कि सवर्ण हिंदू, अछूत समूहों को हिंदू धर्म का हिस्सा ही नहीं मानते हैं. गांधी विद्या केंद्र कोलकाता के निदेशक सुपर्णा गोप्तु मानते हैं कि आम्बेडकर ने अधिकारों माने राइट्स पर आधारित रास्ता चुना, तो वहीं गांधी की राह विश्वास व आध्यात्म की रही.
पूना पैक्ट दो विचारों के द्वन्द को प्रदर्शित करता है, जाति और नागरिकता का. गांधी और अम्बेडकर के बीच का मंथन जाति को समझने के तरीक़े पर ही है. आधुनिक भारत के इतिहास में आम्बेडकर ही पहले हैं जो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जाति एक राजनैतिक सवाल है, जिसके उत्तर केवल सामाजिक सुधारों में नहीं खोजे जा सकते. यहीं पर आप धर्म परिवर्तन के लिए एक तर्क को आकार लेते हुए देखते हैं. लेकिन क्या इसने किसी तरह का अलगाव पैदा किया? आइए इतिहास पर गौर करें.
1932 के पूना पैक्ट से पहले न तो गांधी ही आम्बेडकर को अच्छी तरह जानते थे न ही उनके सहयोगियों ने उन्हें आंबेडकर के बारे में पर्याप्त सूचनाएँ दी थी. इतिहासकारों का मानना है कि यदि ऐसा हुआ होता तो गांधी और आम्बेडकर के सम्बन्धों में कड़वाहट की गुंजाइश कम होती। बावजूद इसके, आंबेडकर और गांधी जैसे दो महारथियों के बीच टकराव का नतीजा विध्वंस नहीं था. पूना पैक्ट को भारत के राजनैतिक और संवैधानिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण माना जाता है, इसने अछूतों और दूसरे हिंदू समूहों के बीच के तनाव को काफ़ी हद तक कम किया. अन्यथा इसका प्रतिकूल असर आज़ादी के आंदोलन व भारत व ब्रिटिश सरकार के बीच वार्ता पर पड़ सकता था। इस पैक्ट ने इस बात को मज़बूती से स्थापित कर दिया कि अछूत एक राजनैतिक अल्पसंख्यक समूह हैं जिनकी माँगों को भारत का संविधान बनाते हुए नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता.
यहां तक आते आते आपने देखा कि धर्म परिवर्तन को लेकर डॉ आंबेडकर ने कितने गहन विचार और संघर्ष के बाद कदम उठाए थे. तब धर्म परिवर्तन की वोकैबलरी आधुनिक भारत में इतनी बदल कैसे गई? समाज सुधार से चली बात जनसंख्या के अनुपात, प्रलोभन से धर्मपरिवर्तन और लव जिहाद जैसे विषयों तक कैसे पहुंची?
जिन चिंताओं का उल्लेख डॉ पाठक ने अभी अभी किया, उन्हीं से धर्म परिवर्तन की मौजूदा राजनीति का उदय होता है. और इसी राजनीति ने वो कानून जने हैं, जिनके तहत भारत में धर्म परिवर्त वैध या अवैध माना जाता है. ये आंबेडकर के विचार पर कितना फिट बैठता है. डॉ आंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर किसी भी दूसरे विचारक को आलोचना से परे कतई नहीं माना जा सकता. डॉ आंबेडकर की भी स्वस्थ आलोचना मौजूद है. लेकिन भारतीय राजनीति का मौजूदा गणित इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आंबेडकर के विचारों से कोई परे दिखे. अब यहां एक द्वंद्व है. आंबेडकर ने जो रास्ता दिखा दिया, उसपर चलने लायक ईमादारी सभी के पास है नहीं. इसीलिए आंबेडकर की तस्वीर लगाने वाली पार्टी आंबेडकर की प्रतिज्ञा का बचाव नहीं कर पाती. और जिस पार्टी के तमाम बड़े नेता आंबेडकर की कसमें खाते नहीं थकते, पिछड़ों के उत्थान को अपना USP बताते हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं के पाठ पर आपत्ति ले लेते हैं. इस बात क्या ही फर्क पड़ता है कि उनके गठबंधन का एक नेता बाद में कह देता है कि प्रतिज्ञाओं पर गर्व है. खैर, नेताओं का क्या, वो तो पार्टी लाइन से बंधे हैं. हम अब अदालतों की बात कर लेते हैं. जहां धर्म परिवर्तन पर सुनवाई चल रही है.
पूरा केस लॉ समझने जितना वक्त अभी नहीं हैं. हम हाल में चल रही एक सुनवाई का ही ज़िक्र करेंगे, जिसकी जानकारी आपको बताएगी कि कानून के रास्ते धर्म परिवर्तन के मोर्चे पर कैसे प्रश्नों पर विचार हो रहा है. और वो कौन कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका पर सुनवाई चल रही है. याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने धमकी, गिफ्ट और रुपए-पैसे के लालच के जरिए धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की थी. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान 28 नवंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि धार्मिक स्वतंत्रता में किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है और यह किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, जबरदस्ती, या लालच के जरिए धर्म परिवर्तन के अधिकार को शामिल नहीं करता है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस तरह की चीजों को रोकने के लिए कानून जरूरी हैं. ताकि समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछले वर्गों के अधिकारों की रक्षा हो सके. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह धर्म परिवर्तन के खिलाफ नहीं बल्कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है. बेंच ने केंद्र से इस मामले में राज्यों से जानकारी लेकर एक डिटेल्ड एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा था. 5 दिसंबर 2022 को एक बार फिर से मामले पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है. चैरिटी का उद्देश्य धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए. यह हमारे संविधान के खिलाफ है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है. मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.
दी लल्लनटॉप शो: डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करते हुए इस्लाम और ईसाइयत को क्यों नहीं अपनाया?











_(1).webp)