(ये स्टोरी हमारे साथी अतुल ने लिखी है.)
टेलीमेडिसिन का लाभ लेने से पहले इसकी इन कमियों पर जरूर गौर कर लेना
महामारी के इस दौर में चर्चा में आई इस सर्विस की चुनौतियों से निपटना बहुत जरूरी है.

फोटो क्रेडिट- Pixabay.com
स्कूल के दिनों में हम में से कइयों ने एक निबंध लिखा और पढ़ा है, ‛विज्ञान वरदान या अभिशाप’. कोरोना महामारी के इस न्यू नॉर्मल दौर में इस शीर्षक को बदल कर ‛टेलीमेडिसिन’ कर देते हैं. क्योंकि रहन-सहन, नौकरी, दफ्तर और पढ़ाई के साथ यह हेल्थ केयर सिस्टम में भी परिवर्तन का दौर है. कोविड-19 महामारी के दौरान इस एक शब्द की काफी चर्चा हुई है- टेलीमेडिसिन. तो टेलीमेडिसिन क्या है, बदलते हेल्थकेयर सिस्टम में इसकी भूमिका कितनी प्रभावी है, आइए समझते हैं. साथ ही इसके नफ़ा नफा-नुकसान को भी टटोलते हैं.
पहले बात टेलीहेल्थ की?
टेलीमेडिसिन पर बात करने से पहले टेलीहेल्थ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ‛टेलीमेडिसिन’ और ‛टेलीहेल्थ’ अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है. हम समझाते हैं. ऐसे समझिए कि ‛टेलीहेल्थ’ एक पेड़ है जिसकी कई शाखाएं हैं. टेलीमेडिसिन उसी एक शाखा का नाम है. टेलीहेल्थ माने सम्पूर्ण प्रणाली. उसी का एक पार्ट है टेलीमेडिसिन. ‛टेलीहेल्थ’ की व्यापक परिभाषा में क्लिनिकल सेवाओं के अलावा रिमोट एरियाज़ में नॉन-क्लिनिकल सेवाएं भी समाहित हैं. मसलन, प्रोवाइडर की ट्रेनिंग, प्रशासनिक बैठक और मेडिकल एजुकेशन उपलब्ध कराना. विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिखित ब्यौरे के अनुसार टेलीहेल्थ सर्विलांस, हेल्थकेयर प्रमोशन और पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल को टेलीकम्युनिकेशन के जरिये दुरुस्त रखने के सिस्टम का नाम है.
अब बात टेलीमेडिसिन की
‛टेलीमेडिसिन’ ग्रीक शब्द ‛टेली’ और लैटिन शब्द ‛मेडेरी’ से मिल कर बना है. टेली का अर्थ ‘दूरी’ और ‛मेडेरी’ का अर्थ है हीलिंग. माने दूरदराज में रह रहे रोगियों और चिकित्सकों के बीच की दूरी को पाट कर उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को वर्चुअली सुलभ बनाना. इस व्यवस्था में स्वास्थ्य सम्बंधित समस्याएं होने पर मरीज डॉक्टर के सामने फिजिकली अपीयर होने के बजाय वीडियो कॉल, फोन कॉल, चैटिंग और ईमेल के जरिये सलाह लेता है. टाइम मैगजीन ने इसे ‛हीलिंग बाई वायर’ (healing by wire) का नाम दिया है. तो आधी बात तो यहीं समझ गए होंगे. अब थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं. वैसे तो टेलीमेडिसिन का उदय इंटरनेट के दौर से पहले हो गया था, लेकिन इस विधा को असल विस्तार इंटरनेट युग में ही मिला. इसने रोगियों को घर बैठे स्वास्थ्य सेवा देने की तमाम सम्भावनाओं को खोल दिया और टेलीमेडिसिन की विधा में कई परिवर्तन भी किए. टेलीमेडिसिन को शुरू किया था अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने. 1960 के दशक में स्पेस में जाने वाले अपने अंतरिक्ष यात्रियों और स्पेसक्रॉफ्ट के हेल्थ का हाल-चाल जानने के लिए. बाद में ग्रामीण इलाकों में इसे उपयोगी बनाने के लिए 1971 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा अलास्का के 26 गांवों में इसे टेस्ट किया गया. उसके बाद NASA ने बकायदा कम्प्यूटर, इंटरनेट समेत तमाम तकनीकी सुविधाओं के साथ 1989 में आर्मेनिया के येरेवान शहर में एक टेलीमेडिसिन सेंटर को ऑफिशियली स्थापित किया. वहीं भारत में इसकी शुरूआत अपनी स्पेस एजेंसी इसरो ने 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की. प्रोजेक्ट की सफलता के बाद भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन टास्क फोर्स का गठन किया और इससे संबंधित गाइडलाइंस भी जारी कीं. कोरोना वायरस से महामारी फैलने के दौरान टेलिकन्सल्टेशन की बढ़ती मांग को देखते हुए 25 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस में कई बदलाव किए और टेलीमेडिसिन का एक व्यवस्थित रोडमैप तैयार कर रोगियों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जरूरी प्रोटोकॉल तय किया.
फायदे
COVID-19 महामारी के दौरान टेलीमेडिसिन को सामाजिक दूरी के साथ प्रभावी उपचार देने वाला सबसे सुरक्षित संवाद प्रणाली माना गया. अस्पताल के चक्कर काटने में पूरा दिन खर्च कर देने की तुलना में यह टाइम फ्लेक्सिबल है. साथ ही अस्पताल आने-जाने के खर्चों को कम करने और वहां के बीमारू संक्रामक माहौल से लेकर मानसिक रूप से बीमार करने वाली हेल्थ गॉसिपिंग से भी दूर रखता है. जो मरीज अस्पताल जाने में असहज महसूस करते हैं, उनके लिए यह प्रणाली रामबाण साबित हुई. कुछ विशेष आपातकालीन स्थितियों में भी टेलीमेडिसिन मददगार साबित हुई और डिजिटल निगरानी से मरीज के स्वास्थ्य देखभाल की लागत भी कम हुई है. लॉकडाउन में घरों में कैद रहने के कारण लोगों में डिप्रेशन के मामले बढ़े हैं. उन मरीज़ों के लिए टेली काउंसलिंग खूब कारगर साबित हुई है. कोरोना महामारी के दौर में जब अधिकांश अस्पताल मरीजों से ठसाठस भरे हुए थे, तब लाखों लोग टेलीमेडिसिन के सहारे स्वस्थ हुए. कुलमिलाकर टेलीमेडिसिन ने दुनियाभर के डॉक्टरों और मरीज़ों के बीच के ट्रैवल डिस्टेंस को समाप्त कर इलाज के नए अवसर खोले.
चुनौतियां
इतिहास-भूगोल और नियम कानून तो आपने समझ लिए. अब समझते हैं टेलीमेडिसिन की चुनौतियों को. इससे जुड़े जोखिमों और इसकी बाधाओं को. सबसे पहले यह समझना होगा कि टेलीमेडिसिन हर व्यक्ति या स्थिति के लिए अनुकूल नहीं है. ट्रेडिशनल देखभाल की विधियों में टेलीमेडिसिन उपयोग करने के कुछ संभावित नुकसान भी हैं. जिन रिमोट एरियाज़ में रह रहे मरीजों के लिए यह सबसे कारगर बताई जा रही है, वहां कम इंटरनेट स्पीड या सर्वर की समस्या के कारण वर्चुअल कम्युनिकेशन को जोड़ने में इस प्रणाली को जूझना पड़ रहा है. इसके साथ ही मरीज बढ़ते साइबर अपराध के कारण अपनी गोपनीयता को लेकर आशंकित भी हैं. कई लोग टेलीमेडिसिन पर पूरी तरह निर्भर हो रहे हैं, ऐसे में किसी व्यक्ति को यदि आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता होती है तो अस्पताल पहुंचने के बजाय पहले टेलीमेडिसिन का रुख करना घातक हो सकता है. टेलीमेडिसिन में मरीज की हेल्थ हिस्ट्री की जानकारी जुटाने में डॉक्टरों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है. डॉक्टर मरीज के बताए लक्षणों के आधार पर ही जांच और दवाएं सुनिश्चित करता है. डॉक्टर के सामने होने पर मरीज अगर अपने लक्षणों को ठीक ढंग से नहीं बता पाता है तो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिये बीमारी को समझने की कोशिश करता है. दूसरी तरफ टेलीमेडिसिन में यदि कोई रोगी एक भी महत्वपूर्ण लक्षण छोड़ देता है तो पूरा इलाज कोम्प्रोमाइज़ होने का खतरा रहता है. वर्चुअल कम्युनिकेशन में डॉक्टर आपके दिल की धड़कन या सांस को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग नहीं कर सकते. आपका बीपी या शुगर नहीं जांच सकते. इसके लिए उन्हें विजुअल असेसमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है. उदाहरण के तौर पर, अगर आपको आंखों में परेशानी है तो वह टॉर्च जलाकर नहीं देख सकता. आपके बताए लक्षणों पर ही उपचार शुरू करना पड़ता है. दूसरी समस्या भाषा और तकनीकी की है. भारत में कम पढ़े-लिखे लोग आज भी अपने लक्षणों को सही भाषा और सटीक शब्दावली में नहीं समझा पाते. इस सेवा का लाभ लेने के लिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क, कम्प्यूटर या मोबाइल के कुशल जानकारों जरूरत है. जिसकी भारी कमी है.
टेलीमेडिसिन प्रोवाइडर्स को कैसे खोजें?
यह इतना सरल है कि एक गूगल सर्च पर उपलब्ध है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-संजीवनी के नाम से निःशुल्क राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की है. यह सेवा ई-संजीवनी मोबाइल एप्लिकेशन, और वेबसाइट के रूप में उपलब्ध है. इसके अलावा कुछ पेड ऐप भी हैं जिनका इस्तेमाल भारत में प्रमुखता से किया जा रहा है. Practo, 1 mg, Apollo 24/7, Docs App, Tata health और Lybrate जैसे एप्लीकेशन्स का इस्तेमाल लोग ई-ओपीडी के लिए कर रहे हैं. टेलीफोनिक कन्सल्टेशन के लिए मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल द्वारा हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किए जा रहे हैं. आमतौर पर यह कॉन्टैक्ट नम्बर्स जिला प्रशासन की वेबसाइट पर मिल जाते हैं. इसके साथ ही कई प्रदेशों में राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण इलाकों में टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र भी स्थापित किए गए हैं. आप वहां जाकर भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं.












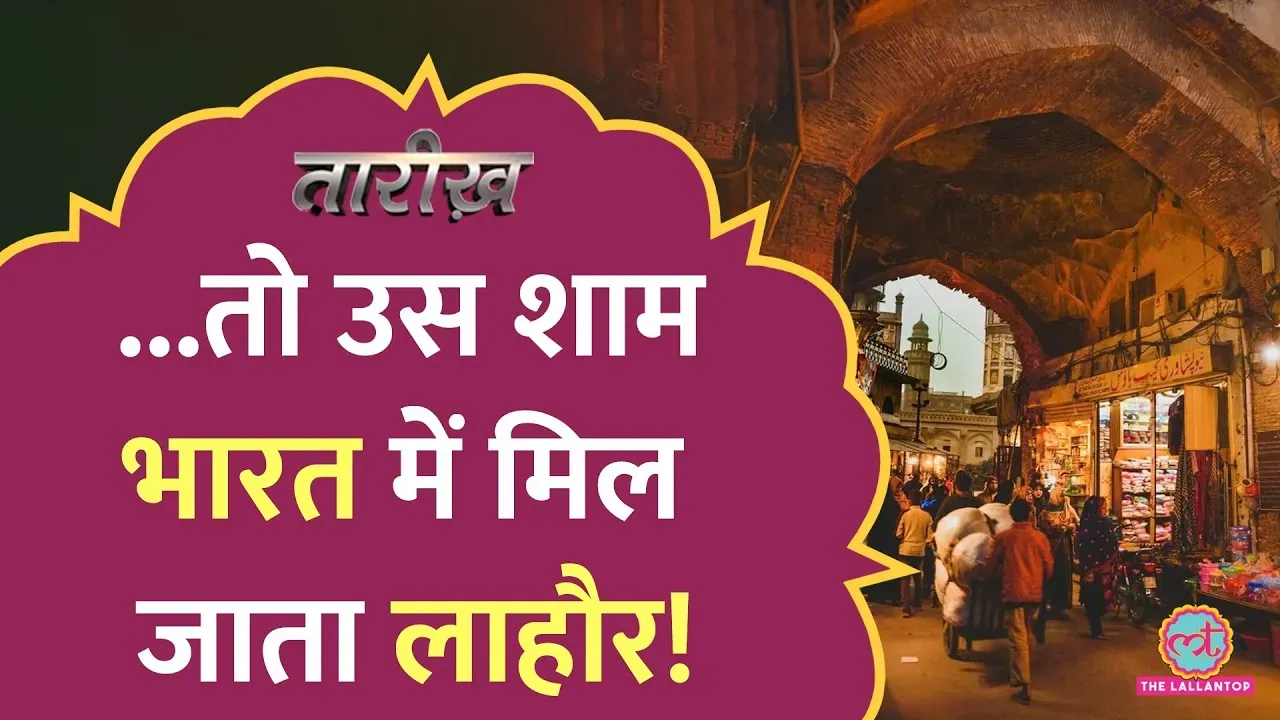

.webp)



.webp)