इस बीच आप ये जान लीजिए कि ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, जिसमें ‘हार’ जाने पर सरकार गिर जाती है. आगे हम लोकसभा के संदर्भ में भी बात करेंगे.
अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत मोटा-माटी एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके रास्ते सरकारें सदन में ये साबित करती हैं कि उनके पास सत्ता में बने रहने लायक सांसद (या विधायक) हैं. सत्ता में बने रहने लायक माने 50 फीसदी से ज़्यादा. ये साबित करने के लिए विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही होती है. ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं. बस एक फर्क है. विश्वास मत सरकार खुद लाती है. अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टियां लाती हैं.
भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत का ज़िक्र नहीं है. लेकिन अनुच्छेद 75 के मुताबिक, कैबिनेट सामूहिक रूप से पूरे सदन (लोकसभा/विधानसभा) के प्रति ज़िम्मेदार होता है. इसका मतलब ये हुआ कि सदन में मौजूद ज़्यादातर (कम से कम 50 फीसदी से एक सांसद ज़्यादा) सांसद कैबिनेट और उसके लीडर (PM/CM) के पाले में हों. इसीलिए आप भले 2% वोट के साथ चुनाव जीत लें लेकिन 50% सांसदों से कम के साथ सरकार नहीं बना सकते. बना भी ली, तो आपको सरकार बनाने के तय समय के भीतर बहुमत साबित करना ही पड़ेगा (जैसे 1991 में नरसिम्हा राव को करना पड़ा था.)
एक बात का गोदना बना लीजिए. विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है. राज्यसभा में नहीं. वैसे ही राज्यों में ये दोनों प्रस्ताव सिर्फ विधानसभा में लाए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं.तो अविश्वास प्रस्ताव आया कहां से?
संविधान के अनुच्छेद 118 के मुताबिक, संसद के दोनों सदन कार्यवाही के लिए अपने-अपने नियम बना सकते हैं. इसी के तहत लोकसभा में नियम 198 है. नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव की लाने की व्यवस्था की गई. ये बड़ी आसान सी प्रक्रिया होती है. पहले कोई सांसद एक लिखित नोटिस स्पीकर को देता है. फिर स्पीकर को इसे सदन में पढ़कर पूछना होता है कि कितने सांसद अविश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हैं. अगर 50 सांसद कह दें कि वो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हैं, तो स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मंज़ूरी देनी होती है और इसके लिए एक तारीख तय कर दी जाती है. इस तारीख पर चर्चा के बाद वोटिंग होती है.

नरसिम्हा राव उन प्रधानमंत्रियों में से हैं, जिन्हें सरकार बनाने के बाद बहुमत साबित करना पड़ा था.
इससे थोड़ा ही अलग होता है विश्वास मत
विश्वास मत के लिए अलग से नियम नहीं है. इसे सरकारें नियम 184 के तहत करवा लेती हैं. 184 के तहत लाए जाने वाले प्रस्तावों पर वोटिंग करवाई जा सकती है. और इस वोटिंग से मालूम चल जाता है कि कितने सांसद सरकार के पक्ष में हैं और कितने खिलाफ.
जब कोई भी पार्टी सदन में सरकार बनाने लायक बहुमत साबित न कर पाए, तो राष्ट्रपति (राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल) किसी ऐसी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनने का न्योता देते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा सांसद हों और वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने का जुगाड़ कर सके. इस पार्टी का नेता सरकार पहले बना लेता है, बहुमत बाद में साबित करता है. और बहुमत साबित किया जाता है 184 के तहत विश्वास मत लाकर. 1998 में राष्ट्रपति के आर नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता ऐसे ही दिया था. तब वाजपेयी को बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन मिले थे.
विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव साथ आ जाएं तो?
सदन में आमतौर पर सरकार द्वारा शुरू की कार्यवाही पर पहले अमल होता है. तो साथ-साथ आने पर भी पहले चर्चा विश्वास मत पर ही होगी. 1990 में वीपी सिंह के समय ऐसा हुआ भी था. तब स्पीकर ने वीपी सिंह के लाए विश्वास मत पर पहले चर्चा करवाई थी.
अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक सीधा मकसद होता है, सरकार को सदन में अकेला साबित करना और हो सके तो उसे गिरा देना. लेकिन विपक्ष कई बार ऐसी स्थिति में भी अविश्वास प्रस्ताव लाता है, जब उसे मालूम होता है कि वो सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता (जैसी की हाल में राजस्थान की स्थिति है). इसके पीछे विपक्ष की कोशिश रहती है किसी तरह अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन को चर्चा के लिए राज़ी कर लेना. अविश्वास प्रस्ताव पर अमूमन दो दिन चर्चा होती है. तो विपक्ष को सरकार की लानत मलानत के लिए लाइव टीवी पर 48 घंटे मिल जाते हैं. विपक्ष इसके ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता है.
विश्वास मत का मामला थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है. ये वैसा ही है कि क्लास खुद ही कह दे कि मैडम आज पढ़ाइए मत, टेस्ट ले लीजिए. मतलब विश्वास मत लाने के पीछे हमेशा सरकार चलाने के दावे के अलावा एक छुपा हुआ एजेंडा भी होता है. ये अमूमन इन दो में से एक होता है –
1. अगर सरकार से कुछ सांसद/विधायक (या पार्टियां) अलग हो जाएं और सरकार ये साबित करना चाहे कि वो अब भी टिकी रह सकती है और बड़े फैसले ले सकती है.
2. विश्वास मत से सरकार अपने कुनबे की मज़बूती चेक करती है. विश्वास मत परीक्षा की घड़ी होती है. पार्टी के भीतर जो सांसद थोड़ा बहुत नाराज़ रहता भी है, वो भी मॉरल प्रेशर के चलते इस वक्त साथ आ जाता है. यही बात सरकार के सहयोगी दलों पर भी लागू होती है. विश्वास मत में जो दल सरकार के साथ टिके, उसे भरोसे के काबिल माना जाता है, भले उनकी कुछ मांगों से सरकार इत्तेफाक न रखती हो.

मनमोहन सिंह जब विश्वास मत लाए थे, तो वो यूपीए सरकार की मज़बूती साबित करने के लिए था.
कोई सरकार विश्वास मत जीते या अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए (जो सरकार की जीत ही हुआ) तो नतीजा साधारण सा होता है. सरकार बनी रहती है. झोल होता है जब सरकारें इसमें हारती हैं. विश्वास मत हार जाने या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार के पास कोई चारा नहीं बचता है. ये मान लिया जाता है कि सरकार सदन का भरोसा खो चुकी है. उसके पूरे कैबिनेट (प्रधानमंत्री भी कैबिनेट का हिस्सा होते हैं) को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है.
एक ऐसा प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री जिसे अविश्वास प्रस्ताव हारने का डर हो, बस एक काम कर सकता है. वो चाहे तो इस्तीफा देने से पहले सदन भंग करने की मांग कर सकता है. ऐसे में दोबारा चुनाव होते हैं. लेकिन ये मांग वो पद पर रहते हुए ही कर सकता है. माने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही.
ऐसा नहीं है कि ये मांग हमेशा मान ली जाती है. ये राष्ट्रपति/राज्यपाल के विवेक पर होता है कि ऐसी स्थिति में सदन भंग किया जाए या नहीं. अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो सदन भंग करने की मांग नामंज़ूर कर किसी और दल को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं. राष्ट्रपति पर सरकार की अनुशंसा बाध्यकारी होती है, लेकिन तभी, जब ये साफ हो कि अनुशंसा करने वाली सरकार के पास सदन में बहुमत है. इसलिए जिन सरकारों का गणित बहुमत के आंकड़े के करीब रहता है, उनकी जेबों में एक कैलकुलेटर हमेशा पड़ा रहता है.
जयललिता की एआईएडीएमके ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और मायावती की बसपा ने कह दिया था कि वो विश्वास मत में वोट नहीं डालेगी. तो वोटिंग का नतीजा रहा एनडीए – 269 और विपक्ष – 270. ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि कम रह गया ये एक वोट गिरधर गमांग का था. लेकिन एनडीए एक और वोट से महरूम रह गई थी. ये वोट था स्पीकर बालयोगी का. बालयोगी टीडीपी से थे जो एनडीए का हिस्सा थी. लेकिन वो अपनी पार्टी का गठबंधन बचाने के लिए वोट नहीं डाल सकते थे, क्योंकि स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे.
स्पीकर बस एक स्थिति में वोट डाल सकते हैं – अगर वोटिंग टाइ हो जाए, तो बतौर टाई ब्रेकर. लेकिन सदन में टाई विरले ही होता है.
अशोक गहलोत के खेमे के विधायकों की बाड़ेबंदी खत्म, सचिन भी लौटे मगर बयान नहीं रुके


















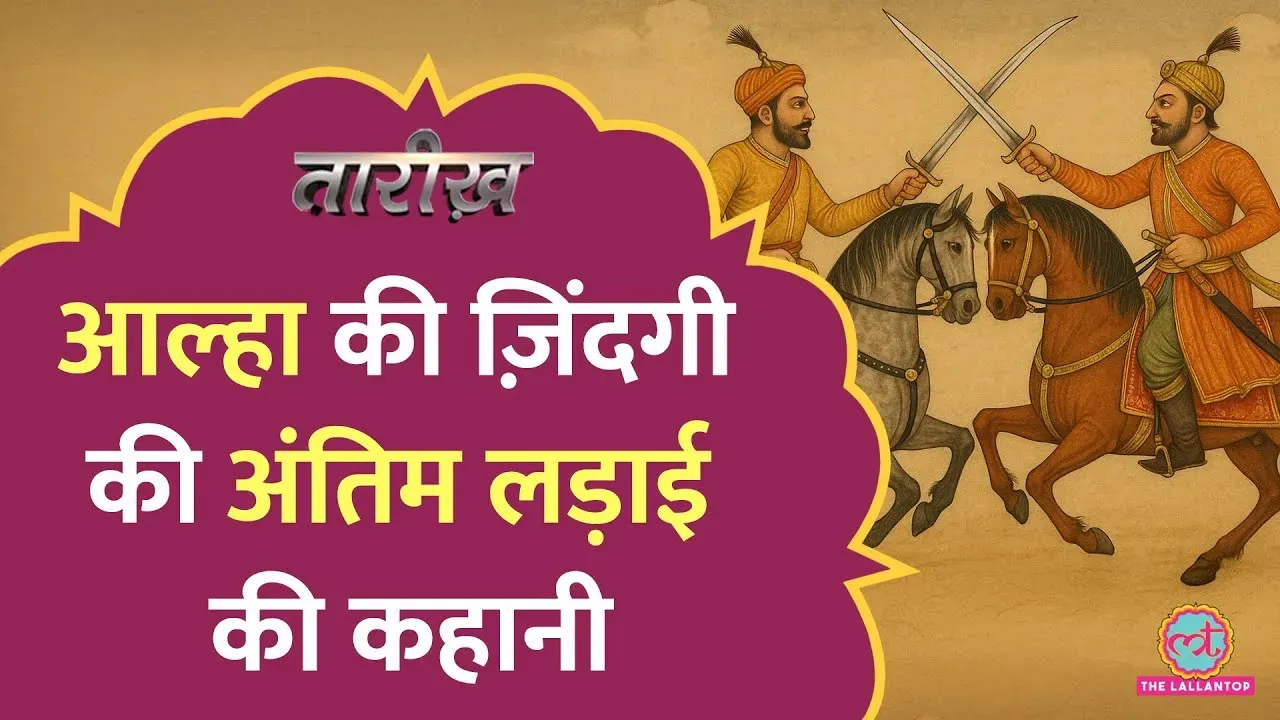


.webp)
_(1).webp)
