हालांकि ऐसा ही प्रयोग पहले भी किया गया था. 1957 में बेल लेबोरेटरीज में. तब गाना था -‘डेज़ी बेल’ (Daisy Bell). कंप्यूटर पर प्ले किया जाने वाला पहला गाना भी यही था. बाद में 1972 में इसे द ट्रिपल ईको नाम की फ़िल्म के लिए ओलिवर रीड (Oliver Reed) ने गाया भी.
लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से उपजे इन गानों का हमारे इस एक्स्प्लेनर के टाइटल से क्या लेना देना?
भरपूर लेना-देना है. आगे समझेंगे. फ्रीक्वेंसी का एक और खेल आपको समझाते हुए. # फ्रीक्वेंसी का खेल एक बार हमारे एक दोस्त की कॉल आई. हमने जैसे ही फोन उठाया, उधर से जनाब ने सवाल दाग दिया. बोले, “कॉल क्यूं कर रहे थे.” हमने जवाब दिया, “भाई कॉल तो की. लेकिन याद आया तुम ऑफिस में होगे तो फ़ौरन काट दी.”
कितना फ़ौरन? तत्काल, यानी कॉल जाने से पहले ही. उसकी कॉलरट्यून बजने से भी पहले. तब उसने बताया कि तुम्हारी कॉल तो नहीं आई, लेकिन ट्रूकॉलर (Truecaller) पर मैसेज आया, तुम्हारी मिसकॉल का. इसलिए पूछ लिया.
लेकिन ये हुआ कैसे? कॉल जाने से पहले ही ट्रूकॉलर को कैसे पता चल गया कि मैं फलां नंबर पर कॉल कर रहा हूं और उसने उस नंबर पर मेरी कॉल का एडवांस पॉपअप नोटिफ़िकेशन भी भेज दिया.
ये एडवांस फ़ीचर वाली पहेली सिर्फ ट्रूकॉलर के साथ नहीं है, बाकी ऐप्स के साथ भी है. ऐप्स पर अपना फ़ोन-नंबर रजिस्टर करने के लिए हमें ओटीपी (OTP) डालना होता है. लेकिन कई बार ओटीपी का टेक्स्ट मैसेज आने से कुछ सेकंड पहले ही ओटीपी ऑटोफिल हो जाता है.
कॉल से पहले ही ट्रूकॉलर का एडवांस मैसेज आ जाना, या ओटीपी का मैसेज आने से पहले ही किसी ऐप में उसका एडवांस ऑटोफिल हो जाना, या फ़ोन के बगल में रखे किसी और गैजेट का आवाज़ करने लगना, ये कोई तकनीकी फ़ीचर नहीं है. बल्कि सेल्युलर नेटवर्क और इंटरनेट नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी और स्पीड में फर्क की वजह से होने वाली एक टेक्निकल रेस का नतीजा है.
 ओटीपी का टेक्स्ट मैसेज आने से कुछ सेकंड पहले ही ओटीपी ऑटोफिल हो जाना (पिक्चर क्रेडिट - आज तक)
ओटीपी का टेक्स्ट मैसेज आने से कुछ सेकंड पहले ही ओटीपी ऑटोफिल हो जाना (पिक्चर क्रेडिट - आज तक)# सेल्युलर नेटवर्क और Wi-Fi नेटवर्क की रेस ट्रूकॉलर का जो एडवांस नोटिफिकेशन आता है. यानी असल कॉल से पहले कॉल का पॉपअप मैसेज. इसे ट्रूकॉलर अपना एक एडवांस फ़ीचर बताता है. और इसे नाम देता है 'Caller alert before calls connect' फ़ीचर. यहां तक कि इस फ़ीचर के बूते ट्रूकॉलर आपको इसका प्रीमियम वर्ज़न लेने के लिए भी पुश करता है. लेकिन यूज़र्स जब इस फ़ीचर में इंवॉल्व सिक्योरिटी रिस्क की बात करते हैं तो ट्रूकॉलर का जवाब होता है कि नहीं इस्तेमाल करना है, तो फ़ीचर को डिसेबल कर दो. ये नहीं बताता कि वो इसे चाह के भी ख़ुद रोक नहीं सकता.
क्यूं नहीं रोक सकता?
दरअसल ये एक रेस है जो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के नेटवर्क्स के बीच चलती रहती है. सेल्युलर नेटवर्क यानी वो नेटवर्क जिसका सिम हमारे फ़ोन में पड़ा होता है. ये नेटवर्क्स (चाहे Airtel के हों या Jio के या किसी और टेलिकॉम कम्पनी के.) एक तय फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं. आपने GSM यानी 2G नेटवर्क और UMTS यानी 3G नेटवर्क के बारे में सुना ही होगा. पहले हम इन्हीं नेटवर्क पर फ़ोन चलाते थे. अब हमारे फ़ोन में LTE यानी 4G नेटवर्क रहता है. हालांकि हमारे फ़ोन में 3G का भी ऑप्शन रहता है. लेकिन हम अच्छी इन्टरनेट स्पीड और बढ़िया कॉलिंग एक्सपीरियंस के लिए 4G मोड का ही इस्तेमाल करते हैं.
 4G और 3G अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं (फ़ोटो सोर्स - आजतक)
4G और 3G अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं (फ़ोटो सोर्स - आजतक)नेटवर्क 3G हो या 4G. फ़ोन कॉल करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 450 मेगाहर्ट्ज़ (MHz) से 2700 मेगाहर्ट्ज़ (MHz) है. लेकिन ये तो रही हमारे फ़ोन की बात. हमारा मोबाइल नेटवर्क जो भी हो, ट्रूकॉलर फ़ोनकॉल की फ्रीक्वेंसी पर नहीं, बल्कि इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. ठीक से कहें तो हमारे मोबाइल डेटा नेटवर्क या WiFi नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी पर. 4G मोबाइल डेटा नेटवर्क के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड है -2 गीगाहर्ट्ज़ से 8 गीगाहर्ट्ज़ (2GHz – 8 GHz). इंटरनेट पर डेटा एक्सचेंज इन्हीं रेडियो वेव्स पर होता है. फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो जाहिर है बैंडविथ भी ज्यादा. जिसके चलते इंटरनेट की सुविधा देने वाली इन रेडियो वेव्स की स्पीड, कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली फ्रीक्वेंसी वेव्स से कहीं ज्यादा होती है.
ऐसे में मान लीजिये कि हमने किसी को कॉल करने के लिए नंबर लगाया. और अगले ही सेकंड हमने कॉल काट दी. माने कॉल जाती उसके पहले ही डिसकनेक्ट कर दी. चूंकि हमारे फ़ोन में और जिसे हमने कॉल की है उसके फ़ोन में ट्रूकॉलर इनस्टॉल है. सो अब ट्रूकॉलर अपना काम करेगा. चूंकि ये रेडियो वेव्स की स्पीड से काम करता है जोकि कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किये गए सेल्युलर नेटवर्क की स्पीड से कहीं ज्यादा है, ऐसे में होगा ये कि कॉल तो पहुंचने के पहले भले कट गयी हो, लेकिन ट्रूकॉलर मिसकॉल अलर्ट का मैसेज दूसरी तरफ भेज देगा.
इसीलिये कॉल जाने के कुछ सेकंड पहले ही ट्रूकॉलर का पॉपअप मैसेज आ जाता है. जिसमें कॉल करने वाले का नंबर, और नाम शो होता है. अगर वॉयस कॉल की जा रही है तो कुछ सेकंड बाद कॉल भी आ जाती है. अगर किसी वजह से कॉल नहीं लगी या कॉलर ने फ़ोन मिलाते ही डिसकनेक्ट कर दिया तो पॉपअप में मिसकॉल का मैसेज आता है.
 ट्रूकॉलर रेडियो वेव्स की स्पीड से काम करता है जोकि कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ( पिक्चर क्रेडिट - इंडिया टुडे)
ट्रूकॉलर रेडियो वेव्स की स्पीड से काम करता है जोकि कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ( पिक्चर क्रेडिट - इंडिया टुडे)इसका एक फायदा भी है. मान लीजिये हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहां मोबाइल नेटवर्क बहुत स्लो है. लेकिन वहां डेटा सर्फिंग के लिए कोई लोकल WiFi नेटवर्क मौजूद है. ऐसे में अगर हमें कोई कॉल करता है तो, भले कॉल न आए लेकिन उस WiFi नेटवर्क की मदद से हमें ट्रूकॉलर का नोटिफिकेशन मिल जाता है कि फलां नंबर से कॉल करने की कोशिश की गई है.
शुरू में हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI से जुड़ी एक दास्तान बताई थी. कि कैसे एक कंप्यूटर से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी तरंगों से रेडियो पर गाना बज गया. ट्रूकॉलर के मैसेज और ओटीपी की ऑटोफिलिंग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और स्पीड से कनेक्शन तो हमने समझ लिया, लेकिन इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से और भी तमाम तरह का खेला हो जाता है.
सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस बात पर बड़े डिस्कशन हुए कि किस तरह रेडियो वेव्स से पैदा होने वाला करेंट इतना ज्यादा हो सकता है कि आपके इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के तारों को पिघला दे. हैकर्स तो कंप्यूटर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करके ये तक पता लगा लेते हैं कि कंप्यूटर पर इस वक़्त काम क्या चल रहा है. कीबोर्ड पर दबाई जाने वाली Keys का सीक्वेंस क्या है.
 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा हैकर्स पता करते है आपके कंप्यूटर पे इस वक़्त क्या काम चल रहा है (पिक्चर क्रेडिट - आजतक)
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा हैकर्स पता करते है आपके कंप्यूटर पे इस वक़्त क्या काम चल रहा है (पिक्चर क्रेडिट - आजतक)लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI नाम की एक और मजेदार चीज़ है. असल ज़िन्दगी में EMI आप भी महसूस कर सकते हैं. कभी अपने फ़ोन को कंप्यूटर या रेडियो के आस पास रखियेगा. हो सकता है आपका फ़ोन या रेडियो घरघरा उठे. माने कुछ असामान्य सा शोर करने लगे. कैसे? चलते चलते इसे भी समझ लेते हैं. # जानिए क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI SCIENTIFIC AMERICAN नाम की एक साइंस वेबसाइट पर डेविड ग्रिएर का एक आर्टिकल है. डेविड ग्रिएर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं. उनके मुताबिक़, दरअसल सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट चाहे-अनचाहे रेडियो ट्रांसमीटर की तरह ही काम करते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इन डिवाइसेज़ में तेजी से चेंज हो रहे इलेक्ट्रिक करेंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड्यूस होती हैं. ऐसा समझ लीजिये कि ये वेव्स बाई-प्रोडक्ट हैं. इलेक्ट्रिक डिवाइसेज़ पर काम करना है तो ये होगा ही. वो कहते हैं न कि आग लगेगी तो धुआं उठना लाज़िम है.
कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. मान लीजिये कंप्यूटर ऑन है, हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं, तो जाहिर है इसमें इलेक्ट्रिक करेंट भी तेज़ी से चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एंड्यूस हो रही हैं. ऐसे में कई बार कंप्यूटर अनचाहे ही ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कर देता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 800 मेगाहर्ट्ज़ के आस-पास होती है. ये फ्रीक्वेंसी की वो रेंज है जिसके आस-पास हमारा फ़ोन काम करता है. यानी रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी रेंज. यही रेंज हमारे फ़ोन के कम्युनिकेशन के लिए रिजर्व्ड होती है.
अब अगर हमारे कंप्यूटर से आने वाले सिग्नल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारा फ़ोन इसे पकड़ सके तो फ़ोन एक गलती कर देगा. वो समझ लेगा कि ये सिग्नल सेलफ़ोन ट्रांसमिशन वाले हैं. लेकिन, हमारे फ़ोन का ऑनबोर्ड कंप्यूटर जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, वो इस तरह प्रोग्राम्ड ही नहीं होता कि कंप्यूटर से आ रहे सिग्नल्स को समझ सके. सो कंप्यूटर और फ़ोन के बीच का ये कम्युनिकेशन एक तरह से फ़ेल साबित होता है, और रिजल्ट के तौर पर हमारा फ़ोन हमें बस एक शोर सा सुनाता है. शोर माने कई तरह के ऑडियो अलर्ट्स की एक सीरीज़.
कंप्यूटर की बजाय आप रेडियो को अपने फ़ोन के पास रखते तो भी संभव है कि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से घरघरा उठता. सवाल ये भी है कि कई बार फ़ोन पर कॉल आने से पहले ही रेडियो घरघराहट की आवाज़ करने लगता है. पहले कैसे? जवाब वही है, रेडियो वेव्स की स्पीड. फ़ोन जिस नेटवर्क पर काम करता है वो नेटवर्क भी रेडियो वेव्स पर बेस्ड होते हैं, और रेडियो में तो रेडियो वेव्स ही मेन डिपेंडेंस है. ऐसे में फ़ोन की रेडियो वेव्स के सिग्नल को जब आपका रेडियो पकड़ लेगा, तो रिएक्ट करेगा. कैसे? शोर करके.
आपकी दो डिवाइसेज़ के बीच ये जो शोर वाला कम्युनिकेशन हो रहा है, इसकी एक वजह और भी है. हालांकि इसका भी लेना-देना रेडियो वेव्स से ही है. दरअसल एक फ़ोन में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं. उनमें से एक है ऑडियो एम्प्लीफायर. इसी के बूते हमारे फ़ोन के स्पीकर काम करते हैं. जब कंप्यूटर रेडियो वेव्स निकालता है तो ये वेव्स फ़ोन के एम्पलीफायर की वायरिंग में भी करेंट पैदा कर सकती हैं. जिसकी वजह से फ़ोन का एम्प्लीफायर एक ऑडियो आउटपुट देता है.
दरअसल ये ऑडियो और कुछ नहीं बल्कि वो काम होता है जो हमारे कंप्यूटर पर उस वक़्त चल रहा है. लेकिन हमें और आपको ये ऑडियो सिर्फ एक शोर या चीखने जैसा लगेगा. वजह? वही जो हमने आपको पहले बताई कि हमारा फ़ोन इस तरह प्रोग्राम्ड ही नहीं होता कि वो कंप्यूटर के सिग्नल्स को इन्टरप्रेट कर सके. यानी समझ सके.
अब हम स्टीव डॉम्पियर जितने समझदार होते तो बेशक इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को शोर की बजाय गानों में बदलने की कोशिश करते. लेकिन हमारा काम है आसान भाषा में मुश्किल चीज़ें आपको बताना. फिर किसी दिन ऐसी ही कोई मुश्किल शय जिसका लेना-देना हमारी-आपकी आम जिंदगी से होगा, आपके लिए लेकर आएंगे.















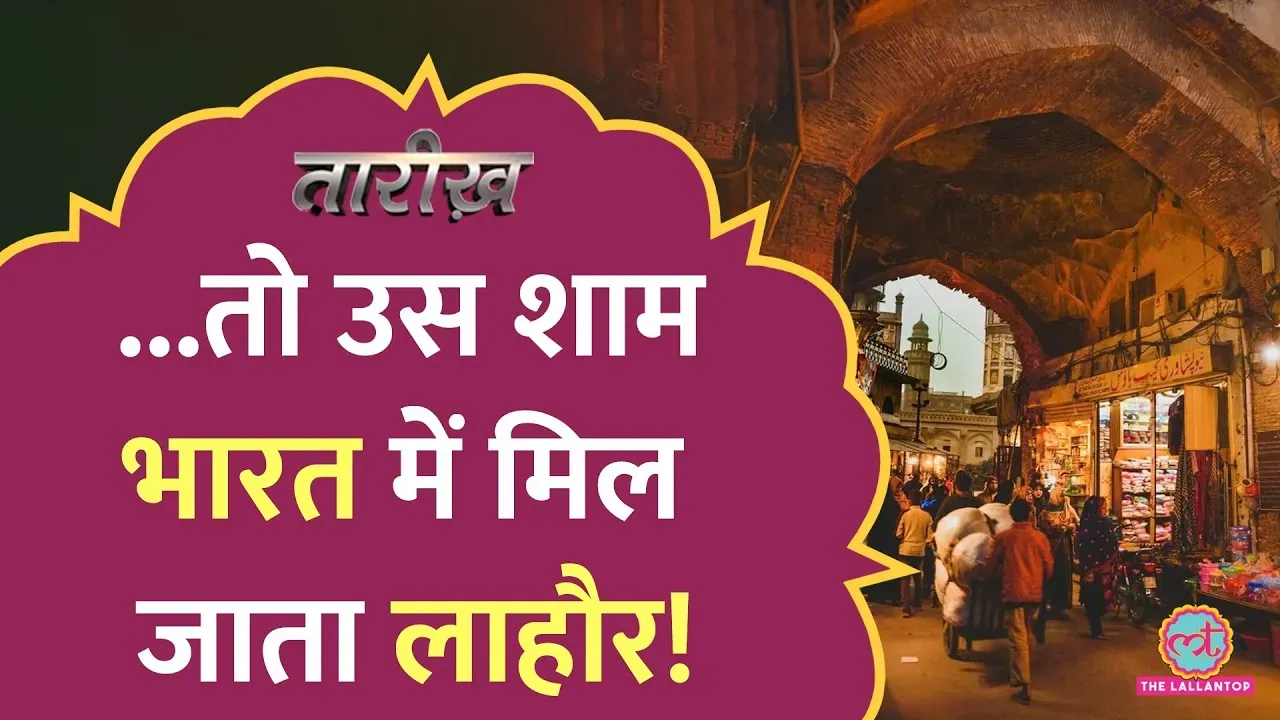

.webp)

