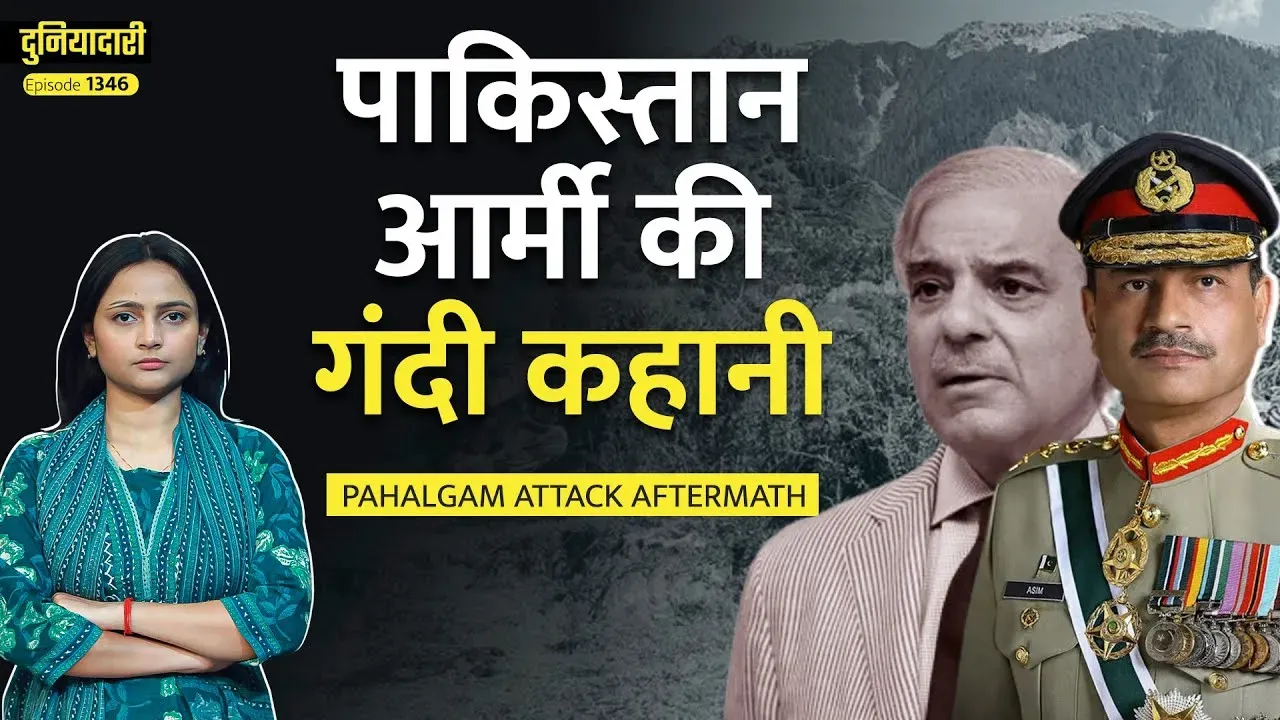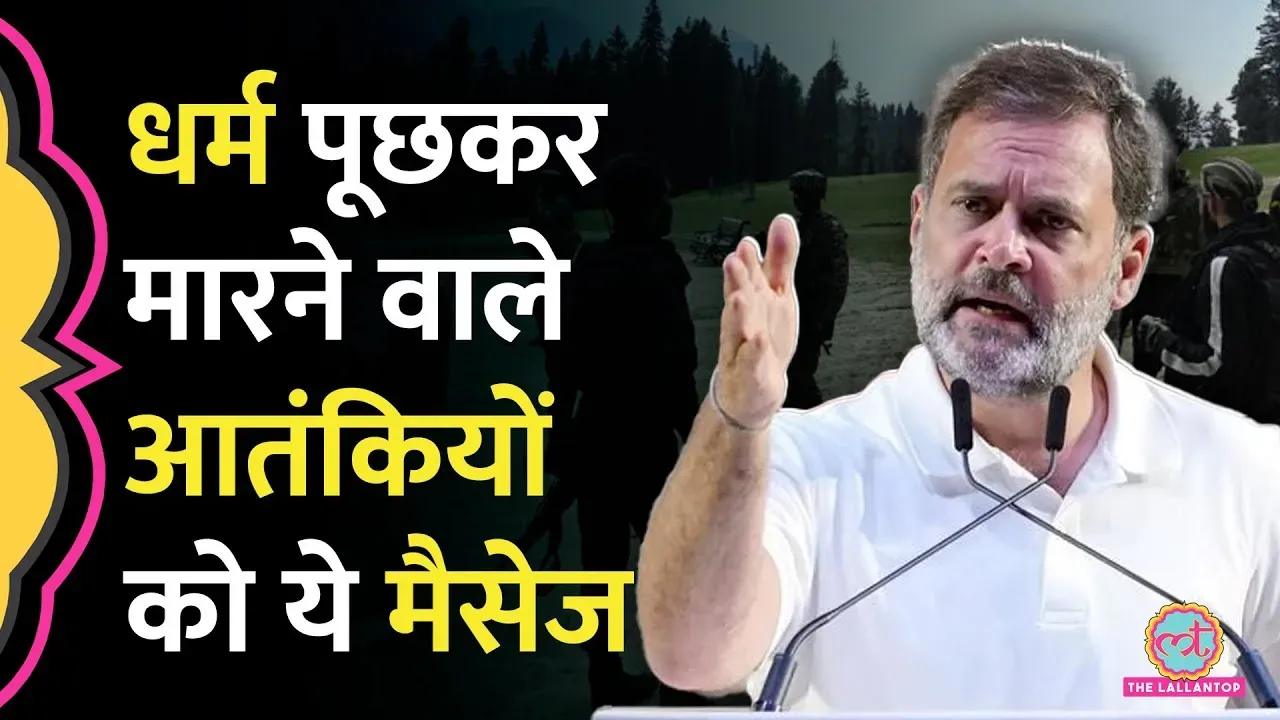एडवर्ड आठवें नाम के ब्रिटेन के एक राजा हुए जिन्होंने अपने प्यार के लिए शाही मुकुट को त्याग दिया. उन्हें वॉलिस सिम्पसन नाम की एक विधवा से प्यार हो गया था. जब शाही परिवार इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का ऐलान कर दिया. 22 जनवरी 1939 की न्यू यॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि जब एडर्वड ने गद्दी छोड़ने का ऐलान किया, तो उनकी होने वाली पत्नी वॉलिस सिम्पसन ने उनसे कहा, “तुम इंग्लैंड के राजा न भी रहो तो क्या भारत के राजा नहीं बने रह सकते?”
भारत को 15 अगस्त को नहीं मिली थी आजादी?
भारत को आजादी मिली साल 1947 में. इसके बावजूद भारत 1950 तक डोमिनियन रूल के अंदर रहा और किंग जॉर्ज भारत के राजा बने रहे. जानिए क्या थी वजह.

एडवर्ड के बाद राजा बने जॉर्ज छठे. क्वीन एलिज़ाबेथ के पिता. एडवर्ड अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड के राजा रहे लेकिन जब भारत की गद्दी छोड़नी पड़ी तो उन्हें भी बड़ा दुःख हुआ. एडवर्ड को हमेशा ये गम सालता रहा कि उन्हें कभी दिल्ली दरबार के आगे खड़े होने का मौका नहीं मिला, जैसे कि उनके पिता जॉर्ज पंचम को मिला था. और भारत के हाथ से निकल जाने के बाद शाही महफ़िलों में वो रौनक भी नहीं रही जो भारतीय राजाओं के होने से होती थी.
जॉर्ज छठे ने 1948 में भारत की गद्दी छोड़ी थी. ये इसलिए रोचक है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था. इसी के चलते कुछ लोगों का मानना है कि 15 अगस्त को आजादी का दिन मानना तर्क संगत नहीं. इस मामले में एक और तर्क दिया जाता है कि अगर 15 अगस्त को आजादी मिल गयी थी तो 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटेन का डोमिनियन क्यों था?
माउंटबेटन अगले 10 महीने तक भारत के गवर्नर जनरल क्यों बने रहे?
और क्यों 1950 तक भारत, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहा?
टेक्निकली देखें तो ये सभी बातें सच है. लेकिन उसी तरह जिस तरह ये वाक्य सच है कि मैं चेस में कभी नहीं हारा. ये बात पूर्णतया सत्य है. लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक चेस का एक भी गेम नहीं खेला. तो भी क्या ये बात उतनी ही सच होगी?
ये सच है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक डोमिनियन रहा. जबकि 1930 में ही कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा कर चुकी थी. इसलिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये डोमिनियन स्टेटस की बात आई कहां से.
कैबिनेट मिशन प्लानशुरुआत 1945 से. वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो ब्रिटेन के सामने भारत का सवाल खड़ा हुआ. वाइसरॉय आर्किबाल्ड वेवल ब्रिटिश कैबिनेट के आगे पेश हुए और उन्होंने बताया कि भारत में हालत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं. जनवरी 1946 में सूबों में हुए चुनाव हुए और हालात और तेज़ी से बिगड़ने लगे. मुहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के बीच सुलह का कोई रास्ता न देखते हुए ब्रिटिश PM क्लीमेंट एटली ने मार्च 1946 में भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा.

कैबिनेट मिशन ने भारत में एक तीन-स्तरीय प्रशासन का प्रस्ताव रखा. जिसमें सबसे ऊपर एक संघीय सरकार होती, जिसके पास केवल नाम भर की शक्तियां होती. दूसरे स्तर पर अलग-अलग प्रांतो के समूह होते, जैसे पूर्व भारत के प्रांतो का एक समूह, मध्य भारत के प्रांतों का एक समूह और उत्तर पश्चिम प्रांतों का एक समूह.
इसके बाद तीसरे स्तर पर प्रांतों की भी अपनी अलग-अलग सरकार होती. आसान भाषा में समझें इस प्लान के तहत भारत तीन हिस्सों में बंट जाता. कैबिनेट मिशन वार्ता के दौरान ये भी तय हुआ कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी. जिसके मेंबर सूबे के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे. मुस्लिग लीग ने पहले तो इसे बनने से रोकने का प्रयास किया. और जब वो इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया.
2 सितम्बर 1946 को इसी संविधान सभा से एक अंतरिम सरकार का चयन किया गया. और इसके तहत कार्यपालिका का काम देखने के लिए वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव कॉउन्सिल बनाई गई. इस कॉउन्सिल के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए. और इसी तरह वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी बन गए. अक्टूबर में अंतरिम सरकार में कुछ फेरबदल हुए और मुस्लिम लीग भी इससे जुड़ गई. इसके बाद पावर ट्रांसफर कैसे हो, इसके लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस में टसल चलती रही.
कैबिनेट मिशन प्लान पर कांग्रेस तैयार नहीं थी और पाकिस्तान से कम किसी समझौते पर जिन्ना राजी नहीं थे. ब्रिटेन के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही थी. सेना में विद्रोह पनपने लगा था और ब्रिटेन के पास यहां ट्रुप्स भेजने के संसाधन नहीं थे. द्वितीय विश्व युद्ध ने उनकी कमर तोड़ के रख दी थी. इसलिए वो इस झमेले को किसी भी तरह निपटाना चाहते थे.
फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि जून 1948 तक भारत आजाद हो जाएगा. वक्त तय हो चुका था. अब जरुरत थी एक ऐसे आदमी की जो इस काम को अंजाम दे सके. इस काम को पूरा करने के लिए क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय बनाकर भेजा. क्लीमेंट ने उनसे कहा था, “हो सके यो भारत को एक रखना, अगर ये संभव न हुआ तो कोशिश करना इस तबाही को जितना कम कर सको, और चाहे कुछ भी हो ब्रिटेन को इस मुसीबत से बाहर निकाल लेना.“

22 मार्च को माउंटबेटन भारत पहुंचते हैं और अपने काम लग जाते हैं. 4 अप्रैल को उनकी मुलाक़ात महात्मा गांधी से होती है. गांधी एक नई अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखते हैं. जिसमें जिन्ना अपनी मर्जी से सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे. प्रस्ताव के अनुसार यही सरकार पावर ट्रांसफर के बाद भारत की पूर्ण सरकार बन जाती. विभाजन को रोकने के लिए ये गांधी की अंतिम कोशिश थी.
माउंटबेटन गांधी से कहते हैं कि वो इस प्रस्ताव को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब कांग्रेस की पूर्ण सहमति हो. इसी बीच एंट्री होती है VP मेनन की. मेनन माउंटबेटन के सलाहकार थे. और उनसे पहले के दो वाइसरॉय के सलाहकार भी रह चुके थे.
मेनन को मालूम था जिन्ना, गांधी के प्लान पर सहमत नहीं होने वाले. इसलिए उन्होंने माउंटबेटन को सलाह दी कि वो कांग्रेस को कैबिनेट मिशन प्लान पर सहमत करने की कोशिश करें. मेनन का मानना था कि अगर कांग्रेस कैबिनेट मिशन प्लान पर ना मानी तो पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा. हालांकि मेनन जिस पाकिस्तान की बात कर रहे थे, उसमें दोनों देशों के डिफेन्स, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन का एक साझा लिंक होता. 11 अप्रैल के दिन गांधी माउंटबेटन को एक खत लिखकर बताते हैं कि वो कांग्रेस का समर्थन नहीं ले पाए, इसलिए अपना प्रस्ताव वापिस लेते हैं.
डोमिनियन रूल की जरुरत क्यों पड़ी?इधर माउंटबेटन की परेशानियां बढ़ते जा रही थीं. कैबनेट मिशन प्लान कहीं नहीं जा रहा था, इसलिए माउंटबेटन ने एक अलग प्लान बनाने का निर्णय लिया. इस नए प्लान के तहत सूबों के समूहों को स्वायत्ता दी जाती, और बाद में वो खुद तय करते कि किसे भारत में रहना है, किसे पाकिस्तान में. नए प्लान में सभी सूबों के डिफेन्स मामलों के लिए एक सेन्ट्रल अथॉरिटी का प्रस्ताव भी शामिल था. 2 मई को ये प्लान लन्दन भेजा गया.

मेनन इस प्लान के सख्त खिलाफ थे. उन्होंने तब इस्तीफे की धमकी तक दे डाली. जब ये बात एडविना माउंटबेटन तक पहुंची तो उन्होंने मेनन को मिलने के लिए बुलाया. मेनन ने उनके सामने अपनी आपत्तियां रखी. तब एडविना ने मेनन को शिमला आने का न्योता दिया, जहां माउंटबेटन दंपति कुछ दिन आराम के लिए जाने वाले थे. इस दौरे ने नेहरू भी उनके साथ थे.
शिमला में मेनन ने पहली बार माउंटबेटन के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज़ की. उन्होंने सूबों को सत्ता देने का प्लान बिलकुल इमप्रॅक्टिकल बताते हुए कहा कि इस तरह तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा. यहीं पहली बार डोमिनियन स्टेटस की बात भी आई. मेनन ने माउंटबेटन को सलाह दी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर उन्हें डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए. मेनन के अनुसार इसके तीन फायदे थे.
पहला पावर ट्रांसफर शांतिपूर्ण तरीके से होता. दूसरा इसके लिए मुस्लिम लीग और ब्रिटेन भी आसानी से तैयार हो जाते. तीसरा फायदा ये होता कि ट्रांजिशन के दौरान ब्रिटिश सिविल सेवकों और ब्रिटिश अफसरों से काम निकलवाया जा सकता था. एक फायदा ये भी होता कि डोमिनियम स्टेटस के रहते रियासतों के साथ नेगोशिएशन में आसानी रहती.
मेनन के इस प्लान को सरदार पटेल का समर्थन भी हासिल था. उन्होंने मेनन से कहा था कि वो कांग्रेस में इसके लिए समर्थन जुटा सकते हैं. इसके कुछ दिन बाद यानी 8 मई को नेहरू शिमला पहुंचते हैं. और मेनन उन्हें अपने प्लान के बारे में बताते हैं. इस मुद्दे पर बात आगे बढ़ती, इससे पहले ही मेनन से जो प्लान लन्दन भेजा था उसे ब्रिटिश कैबिनेट पास कर देती है. माउंटबेटन नेहरू को वो प्लान दिखाते हैं लेकिन नेहरू देखते ही इंकार कर देते हैं. अब माउंटबेटन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था.
संविधान की जरुरतइसके बाद माउंटबेटन मेनन के प्लान के आधार पर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं. जिसके तहत दोनों देशों को डोमिनियन स्टेटस मिलना था. इस फैसले के पीछे एक वजह और थी, और वो वजह थी, संविधान. देश तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार चल रहा था, जिसमें शक्तियां अंग्रेज़ों के पास थीं, इसलिए नया संविधान बने बिना ये तय होना मुश्किल था कि देश काम कैसे करेगा, नए संविधान के बिना सत्ता किसे दी जाएगी, ये तय करना भी मुश्किल था. ब्रिटिश सिविल सेवकों का काम किसे सौंपा जाएगा. सेना का कार्यभार कौन संभालेगा, ये सब तय करना भी बहुत मुश्किल था.

माउंटबेटन को 1948 से पहले सब कुछ समेटकर निकलना था, और तब तक संविधान बनाना असंभव था. इसीलिए डोमोनियन स्टेटस का रास्ता चुना गया. डोमिनियन स्टेटस से ये काम कुछ ही दिनों में हो सकता था क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक एक्ट बनाने की देर थी. 3 जून को माउंटबेटन ने एक मीटिंग बुलाकर ऐतिहासक माउंटबेटन प्लान रखा. सबकी सहमति के बाद मेनन की देखरेख में नए बिल का मसौदा तैयार किया गया. 15 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित कर दिया और 18 जुलाई को इस एक्ट पर शाही मुहर भी लग गयी.
15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडपेंडेन्स एक्ट लागू हुआ, जिसके तहत संविधान सभा आजाद भारत की पहली विधायिका बनी. और नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने रहे. चूंकि भारत डोमिनियन स्टेटस के तहत था इसलिए वाइसरॉय का पद भंग कर दिया गया. और ब्रिटिश शासन के रिप्रेजेन्टेटिव के रूप में माउंटबेटन गवर्नर जनरल नियुक्त हुए. 21 जून, 1948 तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और सी. राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए. 22 जून, 1948 यानी आज ही के दिन जॉर्ज सिक्स्थ ने भी भारत के एम्परर का पद त्याग दिया.
डोमिनियन रूल हटा कैसे?अब सवाल ये कि अगले तीन साल यानी 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटेन का डोमिनियन क्यों बना रहा. इसका कारण था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट. जिसके तहत डोमोनियन स्टेटस मिला था. उसे हटाने के लिए नए क़ानून की जरुरत थी. इसलिए 1950 में नया संविधान बनते ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट रद्द हो गया और इसी के साथ डोमिनियन स्टेटस भी.

एक बात और भी. इस दौरान भारत उस तरह डोमिनियन नहीं था, जिस तरह न्यू जीलैंड या ऑस्ट्रेलिया थे. ऑस्ट्रेलिया और न्यू जीलैंड, स्टेचू ऑफ वेस्टमिनिस्टर क़ानून के तहत डोमिनियन स्टेटस रखते थे. जिसे 1931 में ब्रिटिश संसद से पास किया था. जबकि भारत का डोमिनियन स्टेटस इंडिपेंडेंस ऑफ़ इंडिया एक्ट के तहत था.
1947 में डोमिनियन स्टेटस मिलने का यह मतलब नहीं था कि भारत तब आजाद नहीं हुआ. ये एक कानूनी समझौता था, ताकि जल्द से जल्द सत्ता का ट्रांसफर हो सके. टेक्निकली ये बात सच है कि पूर्ण आजादी 1950 में मिली, लेकिन सिर्फ टेक्नीकली ही. तुलना के लिए समझिए की टेक्निकली क्वीन एलिज़ाबेथ 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया की महारानी हैं, लेकिन सिर्फ टेक्निकली ही. अब अंत में एक किस्सा सुनिए, जिससे आपको भारत की स्वायत्ता का इशारा मिलेगा.
1961 में क्वीन एलिज़ाबेथ ने भारत का दौरा किया. भव्य स्वागत हुआ. रानी की हर मांग पूरी की गई सिवाय एक के. एलिज़ाबेथ लाल किले के दीवान-ए-ख़ास में रिसेप्शन होस्ट करना चाहती थीं लेकिन इसके प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने इसकी इजाजत नहीं दी. ऐसा ही एक वाकया 1983 में भी हुआ. एलिज़ाबेथ मदर टेरेसा को सम्मानित करने वाली थीं, और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में कार्यक्रम की इच्छा जताई, तब इंडिरा ने भी इसकी इजाजत देने से इंकार कर दिया था.
अंत में इतना ही कि आजादी मुश्किल से मिलती है. इसलिए सिर्फ 15 अगस्त को ही क्यों, रोज़ मनाइए, और सहेज कर भी रखिए. आज के लिए..














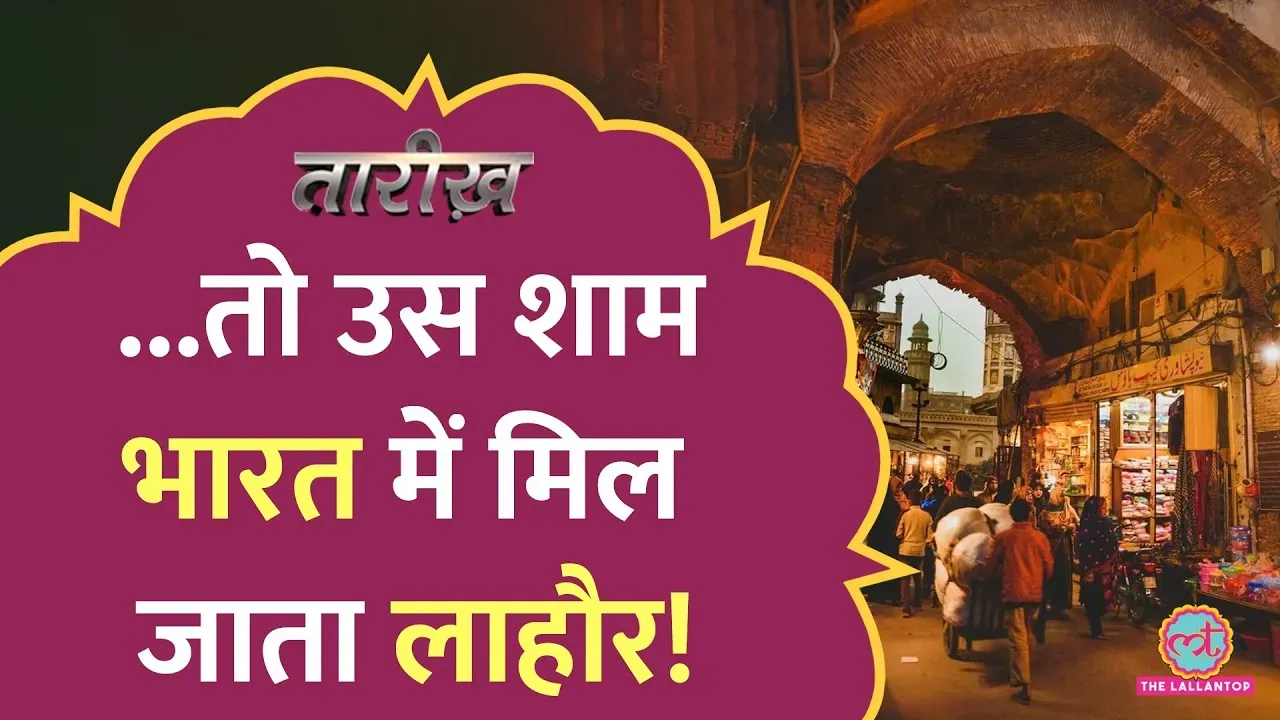

.webp)
.webp)
.webp)