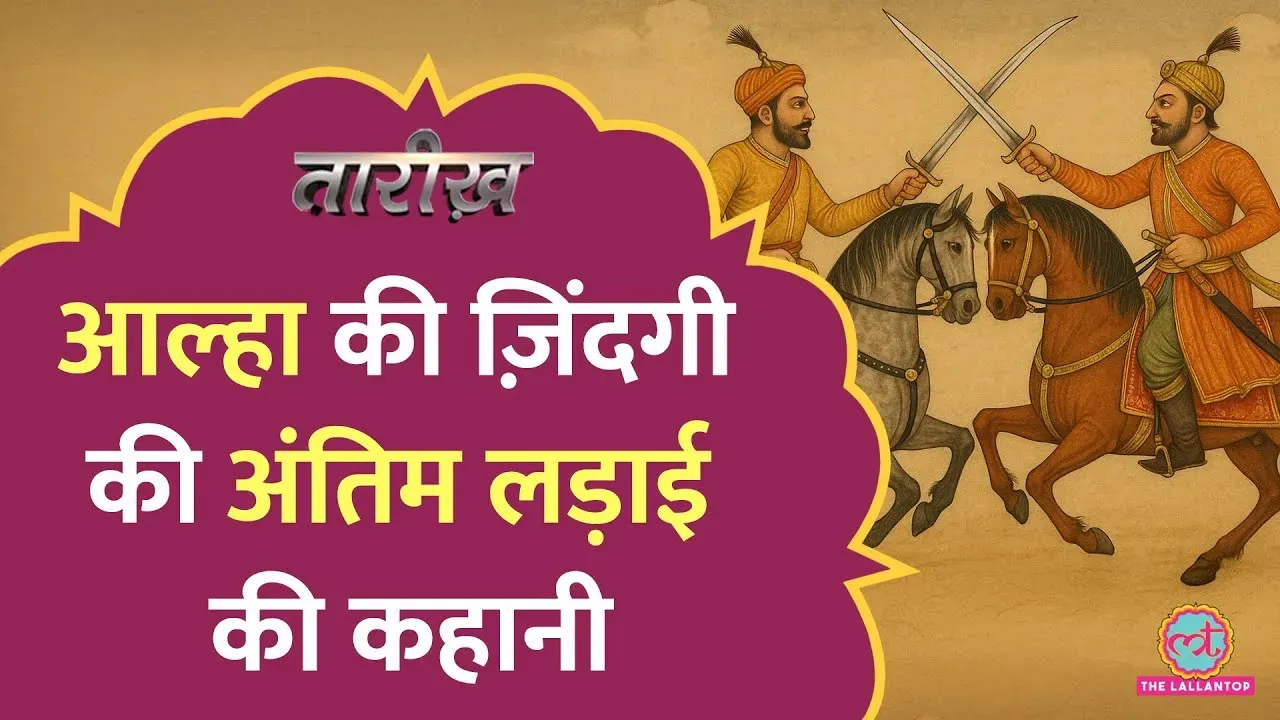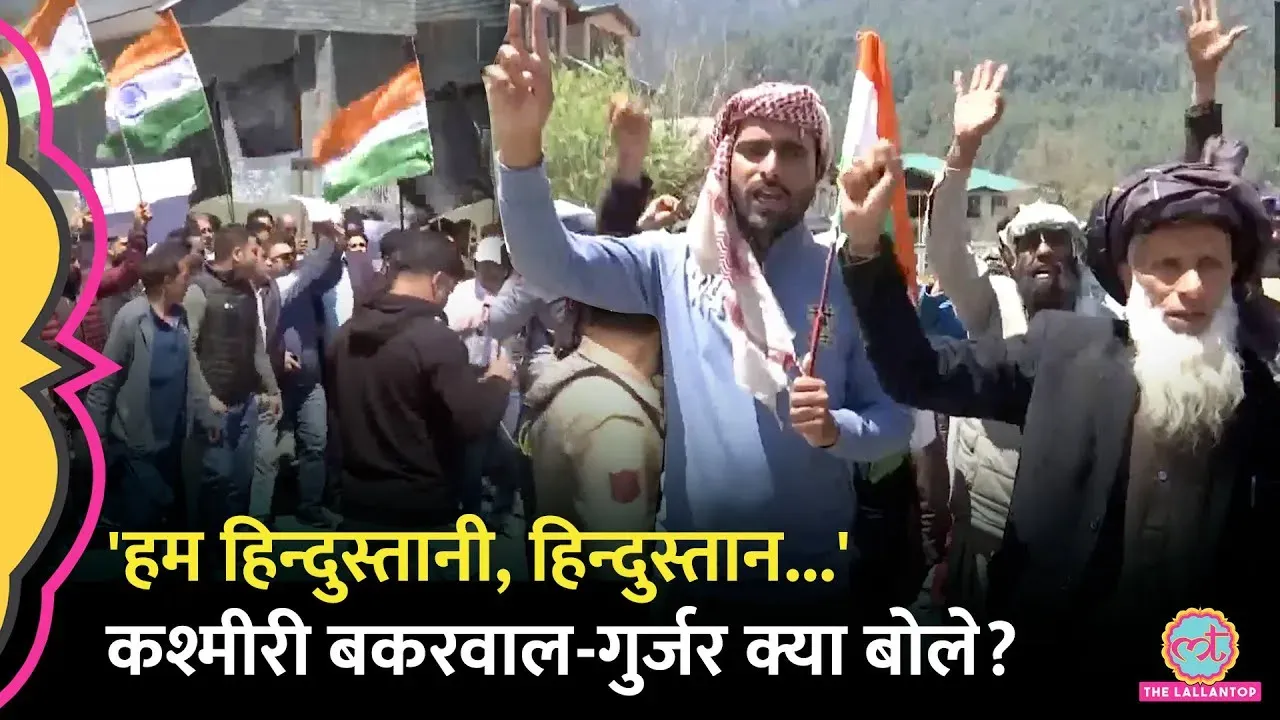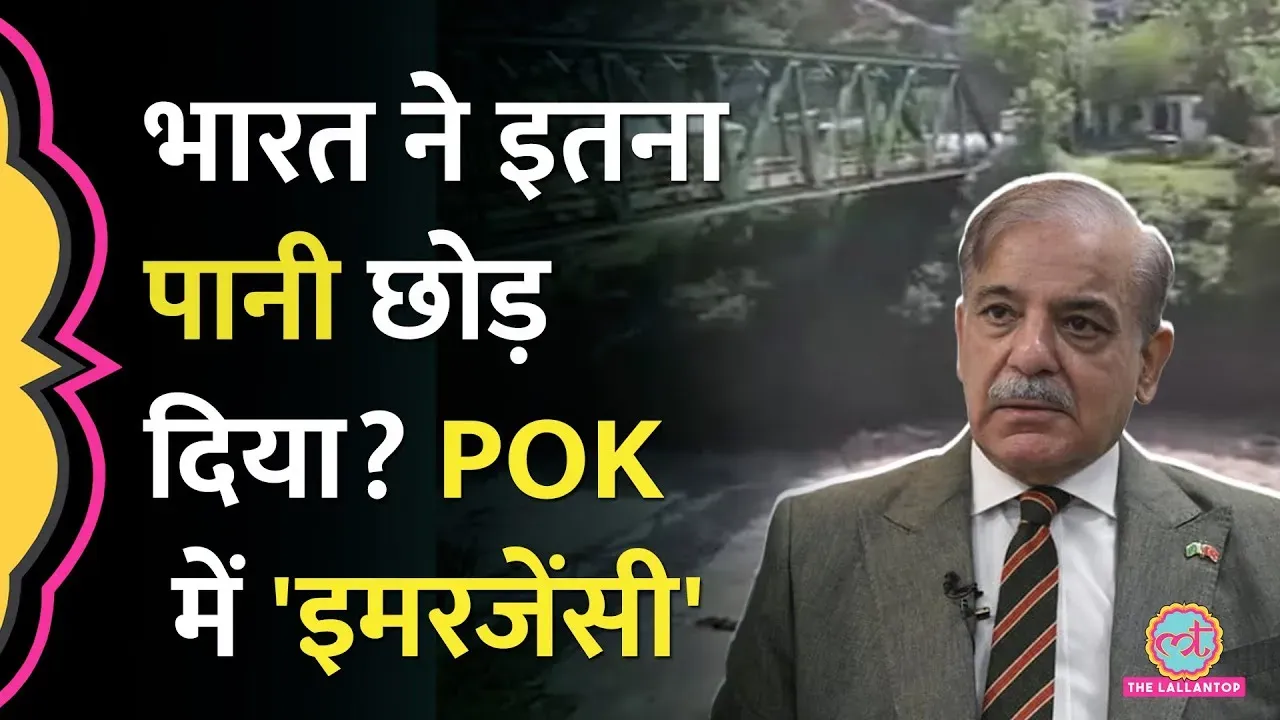सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on land acquisition) ने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए एक आदेश दिया. इस आदेश के अनुसार, सरकारों के पास लोगों की संपत्तियों का अधिग्रहण करने का अधिकार तो है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा. यानी अगर सरकार को जरूरत पड़ी तो किसी भी वक्त आपकी संपत्ति सरकार की हो सकती है. लेकिन इससे पहले आपके पास कुछ अधिकार हैं. ये अधिकार और शर्तें नए नहीं हैं. संविधान में इसका जिक्र है. और इसको जानना भी जरूरी है.
अगर कभी सरकार आपकी संपत्ति का अधिग्रहण करने आए तो ये संवैधानिक अधिकार बहुत काम आएंगे
संपत्तियों के अधिग्रहण के दौरान सरकार को आर्टिकल 300A के 7 उप-अधिकारों का पालन करना होता है.
.webp?width=360)
लाइव लॉ की एक रिपोर्टे के मुताबिक, 16 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अनुच्छेद 300 (A) पर प्रकाश डाला. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि आर्टिकल 300 (A) के मानकों को पूरा किए बिना किया गया अधिग्रहण असंवैधानिक माना जाएगा.
आर्टिकल 300 (A) में क्या है?आर्टिकल 300 (A) कहता है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. उच्चतम न्यायालय ने इस आर्टिकल के 7 उप-अधिकारों का जिक्र किया. इसमें अधिग्रहण के पहले से लेकर अधिग्रहण के बाद तक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया. ये 7 उप-अधिकार इस प्रकार हैं-
- नोटिस का अधिकार: राज्य का कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को सूचित करे कि सरकार उसकी संपत्ति अर्जित करने का इरादा रखती है.
- सुनवाई का अधिकार: जिस व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण होना है, सरकार को उसकी आपत्तियों को सुनना होगा.
- तर्कसंगत निर्णय का अधिकार: सरकार को इस बात की सूचना देनी होगी कि उन्होंने किसी व्यक्ति की संपत्ति के अधिग्रहण का निर्णय ले लिया है.
- केवल सार्वजनिक जरूरतों के लिए अधिग्रहण: सरकार को ये बताना होगा कि अधिग्रहण 'पब्लिक पर्पस' यानी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है.
- पुनर्वास या उचित मुआवजा: सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि अधिग्रहण के लिए व्यक्ति को उचित मुआवजा मिले. या उसके पुनर्वास की उचित व्यवस्था हो.
- कुशल और समयसीमा के अंदर होने वाली प्रक्रिया: अधिग्रहण कुशलतापूर्वक हो. और अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर हो. ये सुनिश्चित करना भी सरकार काम है.
- निष्कर्ष का अधिकार: सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है कि ये पूरी प्रक्रिया अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचे.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि ये 7 अधिकार अनुच्छेद 300 (A) के मूलभूत तत्व हैं. इनमें से एक या कुछ को नजरअंदाज करना कानून को चुनौती देने जैसा है. इसका पालन नहीं करना कानून के अधिकार का उल्लंघन होगा.
इन अधिकारों को अधिग्रहण से जुड़े कई अन्य अधिनियमों में भी शामिल किया गया है. जैसे- 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम. इन अधिनियमों में भी उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की बात की गई है.
इससे पहले का कानून क्या था?साल 1978 में भारत के संविधान का 44वां संशोधन हुआ. इसके जरिए अनुच्छेद 31 में बदलाव किया गया. अनुच्छेद 31 के तहत 'संपत्ति का अधिकार' मौलिक अधिकार हुआ करता था. भूमि अधिग्रहण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था. इसलिए सरकार ने संविधान के 44वें संशोधन के जरिए कहा कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहेगा. संविधान का भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 (मौलिक अधिकार) से अनुच्छेद 31 को पूरी तरह से हटा दिया गया.
(ये स्टोरी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे तेजस ने लिखी है.)
वीडियो: नेता नगरी: देश की आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग होने के बाद क्या सूरत-ए-हाल है, हवा का रुख किस ओर?