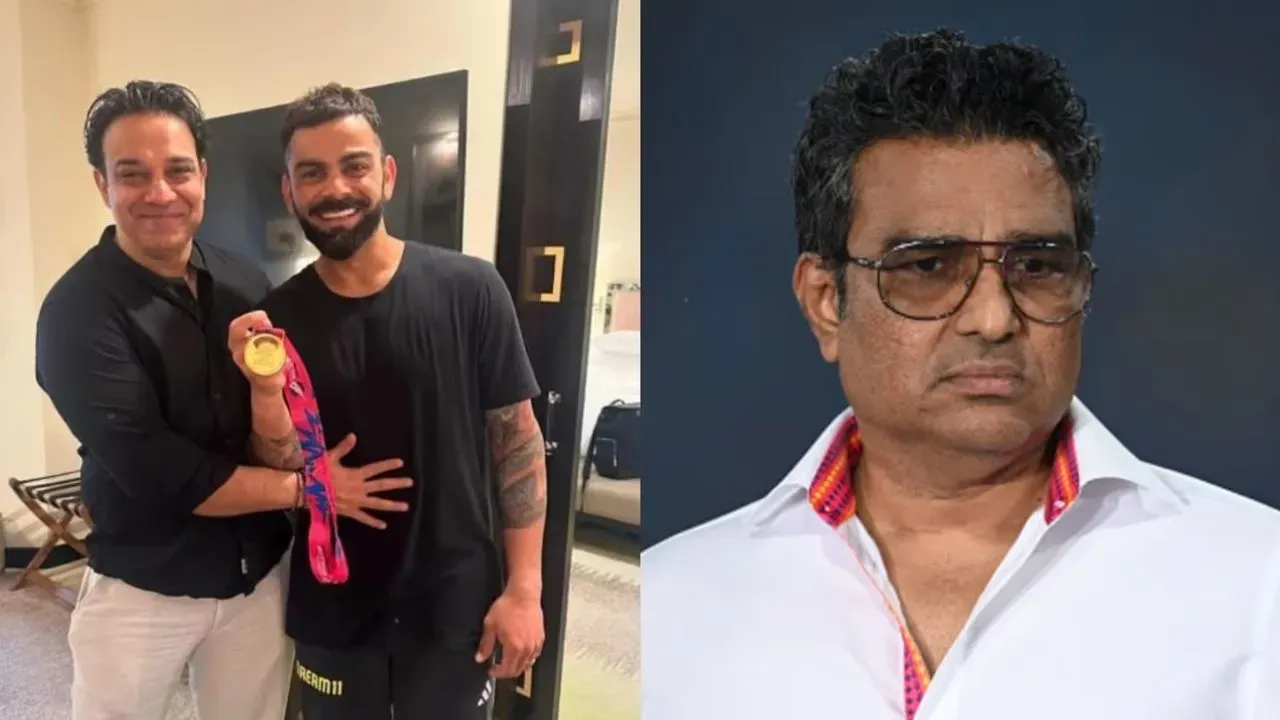इसके अनुसार, जिस किसी रियासतदार या शासक के औलाद न हो, उसे किसी उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार न था. मने जब शासक की मृत्यु हो जाए तो उसकी रियासत पर अंग्रेजों का कब्ज़ा हो जाता था. लॉर्ड डलहौज़ी ने हमेशा वफादार रही अवध की रियासत को भी इसी नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया. अवध में हज़ारों लोग और सैनिक बेरोज़गार हो गए. यही उस विद्रोह की पहली वजह थी, जो आज की तारीख़ का मेन सब्जेक्ट है.
इस विद्रोह की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी, अंग्रेजों के पश्चिमी तौर तरीके और भारतीयों का धार्मिक अपमान. 1850 में एक एक्ट लाकर उत्तराधिकार के हिन्दू कानून को बदल दिया गया था. ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों को प्रमोशन मिलता था. एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया गया था जो हिन्दू और मुसलमान दोनों के पुराने तरीकों को सीधे चैलेन्ज करता था. लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज़ भारतीयों को इसाई बनाने में जुटे हुए हैं.
 तोपों से उड़ा दिए गए क्रांतिकारी (तस्वीर: विकीमीडिया)
तोपों से उड़ा दिए गए क्रांतिकारी (तस्वीर: विकीमीडिया)विद्रोह की तीसरी वजह आर्थिक थी. किसानों पर भारी-भरकम लगान लगाया जा रहा था. सख्ती से वसूली की जा रही थी. क़र्ज़ न चुकता होने की वजह से किसानों के हाथों से ज़मीनें हड़पी जा रही थीं. सिपाही भी ज्यादातर किसानों के ही परिवारों से थे. कपड़ा उद्योग भी बर्बाद हो चुका था क्यूंकि हाथ के कामगारों की टक्कर अब ब्रिटिश मशीनों से थी.
ये तीन तो वो कारण थे जो सुलग तो रहे थे पर धरती के अंदर. लेकिन विद्रोह का ज्वालामुखी अंततः फूटा सैनिकों के असंतोष के चलते. मतलब ये कि विद्रोह तो पहले से तय था, और उसमें सैनिक भी शामिल होंगे ये भी तय था. सवाल था कब और कैसे.
आगे बढ़ने से पहले ज़रा विद्रोह शब्द पर भी ग़ौर कर लें. विद्रोह माने बग़ावत. लेकिन बग़ावत हमेशा बुरी नहीं होती. अप्रैल 1857 में मंगल पांडेय की बंदूक से अंग्रेजों के खिलाफ़ विद्रोह की पहली गोली चली थी. लंबे समय तक ब्रिटिश सेना में बागी सिपाहियों को पांडे कहकर बुलाया जाने लगा था. और बाग़ी भी हमेशा बुरे नहीं होते. होंगे मंगल पांडे उनके लिए बाग़ी का सिनोनिम हमारे लिए तो वो आज़ादी के महानायक थे. हैं और रहेंगे. # बैरकपुर छावनी- कोलकाता से थोड़ी दूर हुगली नदी के हरे-भरे किनारे पर है बैरकपुर. ये भारत में अंग्रेज़ों की बसाई पहली छावनी है. साल 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में पाँव जमाने की जगह मिली. यहीं अंग्रेजों ने साल 1765 में अपना फ़ौजी अड्डा बनाया. और यहीं से 1857 में अंग्रेज़ी राज़ के खात्मे की इबारत भी लिखी गयी. वो पोएटिक जस्टिस के मुरीद लोग कहते हैं न कि कहानी जहां से शुरू होती है, ख़त्म भी वहीं होनी चाहिए.
 बैरकपुर
बैरकपुरहालांकि बैरकपुर कैंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट बताती है कि बैरकपुर छावनी में 1824 में भी विद्रोह हुआ था. जिसके लीडर बने थे सिपाही बन्दा तिवारी. एंग्लो-बर्मन वॉर के दौरान बन्दा की लीडरशिप में सैनिकों ने नाव पर चढ़ने से मना कर दिया था. बदले में इन सभी सैनिकों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया था. और ये विद्रोह वहीं दब गया था. लेकिन आज बात 1857 की. # गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने एक रिपोर्ट में लिखा था-
एक हथियारखाने में काम करने वाले खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने को कहा. सिपाही ने नीची जाति का हवाला देते हुए अपना लोटा देने से मना कर दिया. इस पर खलासी ने जवाब दिया कि जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है. क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से खींचना होगा.इस रिपोर्ट में कमांडेंट राइट ने जो कुछ कहा वो कितना सच होगा, ये आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि ‘डिवाइड एंड रूल’ का ज़िक्र जहां कहीं भी आता है, वहां अंग्रेजों का भी ज़िक्र आता है. लेकिन कैप्टन राइट की इस रिपोर्ट से एक बात क्लियर थी कि चर्बी वाली बात छावनी में फैलनी शुरू हो चुकी थी. और एक बार जब ये चर्बी वाली बात फैलनी शुरू हो गयी तो अंग्रेजों के लाख समझाने पर भी सैनिक नहीं माने कि कारतूसों में चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया गया है.
एक और अफवाह ये भी थी कि धर्म भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का आटा मिलना शुरु कर दिया है. छावनियों में सिपाही और आम लोगों ने आटा छूने तक से इनकार कर दिया था.
 तस्वीर: विकीमीडिया
तस्वीर: विकीमीडियाकहते है न कि कुछ बड़ा होने को हो तो वैसा ही माहौल बनने लगता है. उत्तर भारत के आम लोगों के दिमाग में एक तत्कालीन भविष्यवाणी भी तैर रही थी. इसके मुताबिक़ प्लासी के युद्ध के सौ साल पूरे होते ही यानी 23 जून, 1857 को अंग्रेज़ी राज़ ख़त्म हो जाएगा. # निकलि आव पलटुन, निकलि आव हमार साथ नई इनफील्ड राइफल में गोली दागने के लिए परकशन कैप का इस्तेमाल करना होता था. लेकिन राइफल में गोली भरने के लिए तरीका वही पुराना. बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था. गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों की ख़बर यहाँ भी फ़ैल चुकी थी. हिन्दू और मुसलमान सैनिकों को ये गवारा नहीं था.
29 मार्च का दिन था. बीबीसी की एक स्टोरी के मुताबिक़, इतिहासकार किम ए वैगनर अपनी क़िताब द ग्रेट फियर ऑफ 1857 - रयूमर्स, कॉन्सपिरेसीज़ एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन अपराइज़िंग में 29 मार्च की घटना के बारे में लिखते हैं-
शाम के 4 बजे थे. मंगल पांडे अपने तंबू में बंदूक साफ कर रहे थे. सिपाहियों के बीच बेचैनी थी. अपनी जैकेट, टोपी और धोती पहने मंगल पांडे अपनी तलवार और बंदूक लेकर क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग के करीब परेड ग्राउंड की ओर दौड़ पड़े.मंगल पांडे चिल्ला रहे थे-
निकलि आव पलटुन, निकलि आव हमार साथ. फिरंगी मारो.मंगल पांडे को पकड़ने गये मेजर जनरल ह्वीसन और अडज्यूटेंट लेफ्टिनेंट बेंपदे बाग पर मंगल ने गोली चला दी. हालांकि गोली चली नहीं. सिर्फ एक हवलदार शेख पलटू के अलावा सभी सैनिकों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया. इस दौरान मंगल पांडे ने ख़ुद को मारने का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें सफल होने से पहले ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया.
इसके बाद मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया. 6 अप्रैल, 1857 को कोर्ट मार्शल हुआ और 8 अप्रैल को फांसी. हालांकि कोर्ट ने फांसी देने की तारीख 18 अप्रैल 1857 तय की थी. लेकिन उठते विद्रोह को दबाने के लिए फांसी दस दिन पहले ही दे दी गयी. मंगल पांडे को फांसी देने से बैरकपुर जेल के जल्लादों ने इनकार कर दिया था. इसके बाद अंग्रेज़ अफसरों को कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाने पड़े. मंगल पांडे के बाद एक और सिपाही ईश्वरी प्रसाद पांडे को फांसी दी गई. ईश्वरी प्रसाद ने पल्टू से कहा था कि अगर मंगल को भागने नहीं दिया गया वो गोली चला देगा.
मंगल पांडे की फांसी के बाद भारतीय सिपाहियों में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत और बढ़ गई. 23 अप्रैल को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने गंगाजल और कुरान हाथ में लेकर कसम ली कि वो चर्बी वाली गोली की ख़िलाफ़त करेंगे. 24 अप्रैल को मेरठ के परेड ग्राउंड में 90 में से 85 सिपाहियों ने नई कार्टेज के इस्तेमाल से इनकार कर दिया.
30 अप्रैल से 7 मई के बीच मेरठ के कई इलाकों में आग लगा दी गई. रात के वक़्त कई सरकारी दफ्तरों के छप्पर जला दिये गए. 9 मई को मेरठ के परेड ग्राउंड में सिपाहियों की वर्दी उतार ली गई और जंजीरों में जकड़कर जेल भेज दिया गया.
 1857 की क्रांति की शुरुआत (तस्वीर: विकीमीडिया)
1857 की क्रांति की शुरुआत (तस्वीर: विकीमीडिया)सर चार्ल्स नेपियर के इस बयान ने भी आग में घी का काम किया कि ''अगर वो गवर्नर जनरल बने तो ईसाई धर्म को राज्य धर्म बना देंगे क्योंकि भारत अब इंग्लैंड के अधीन है.’'
इसके विरोध में मौलवी अहमदुल्लाह ने हिन्दू और मुसलमानों से अपील की. कहा कि सब मिलकर अपने पूर्वजों के भरोसे को बचाओ. यही वक़्त है. मेरठ के सिपाहियों में मौलवी की इस अपील ने जोश भर दिया. 10 मई. रविवार का दिन था. अंग्रेज छुट्टी के मूड में थे. या तो बाज़ार में खरीदारी कर रहे थे या चर्च गए हुए थे. सिपाही 'मारो फ़िरंगियों को' चिल्लाते हुए छावनी की तरफ़ बढ़े और अंग्रेजों के बंगलों में जा घुसे. सवा छ: बजे तक मेरठ की दो जेलें तोड़ दी गईं. जंजीरों में कैद सैनिकों को आज़ाद करा लिया गया. कर्नल जॉन फीनिस ने जब सिपाहियों को रोकने की कोशिश की तो उनके सिर में गोली मार दी गई, अगले दिन सोमवार को भी कई अंग्रेज़ मारे गए. मरने वालों में जॉन पहले थे. 10 मई की शाम 7 बजे तक पूरा छावनी इलाका जला दिया गया था. शाम 7.30 के आसपास सैनिक रिठानी गांव के पास इकट्ठे हुए और दिल्ली की तरफ कूच का निर्णय हुआ. सोमवार सुबह सैनिक यमुना किनारे लाल किले के बाहर इकट्ठा हो गए. # बहादुरशाह ज़फर और बाकी क्रांतिकारी- उस दौरान की एक कहानी बड़ी प्रचलित है. कहा जाता है बहादुर शाह ज़फ़र बगावती सिपाहियों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं थे. लेकिन उन्हें एक सपना आया. बहादुर शाह ज़फ़र के निजी सचिव जीवन लाल के मुताबिक़ बादशाह को सपने में उनके दादा शाह आलम ने कहा कि वक्त आ गया है कि 100 साल पहले की प्लासी की लड़ाई का बदला लिया जाए. इसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र सिपाहियों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए. सिपाहियों ने 82 साल के बुज़ुर्ग बहादुरशाह ज़फर द्वितीय को दिल्ली का शहंशाह घोषित कर दिया.
कहते ये भी हैं कि बहादुरशाह ज़फ़र के पास क्रांतिकारी सैनिकों की लीडरशिप कबूल करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था. सैनिक किले में घुस गए थे. जो भी अंग्रेज़ जहां मिल रहा था उसे मार रहे थे. इतनी मारकाट हुई कि ज़फ़र ने लिखा-
दिल्ली के अलावा विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान तक फैल चुका था. विद्रोह के मुख्य सेंटर थे - कानपुर, लखनऊ, बरेली, झाँसी, ग्वालियर और बिहार का आरा ज़िला. कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब कर रहे थे. झाँसी में 22 साल की रानी लक्ष्मी बाई अंग्रेजों से लोहा ले रही थीं. ग्वालियर पर लक्ष्मी बाई ने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर कब्ज़ा कर लिया था.
उधर लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून, 1857 को हुई थी. यहां क्रांतिकारी सैनिकों ने ब्रिटिश रेजिडेंसी का घेराव किया और रेजिडेंट 'हेनरी लॉरेन्स' को मार दिया. हैवलॉक और आउट्रम नाम के अंग्रेज़ अधिकारियों ने लखनऊ का विद्रोह कुचलने की कोशिश की. लेकिन सफ़ल नहीं हुए. लखनऊ में अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हज़रत महल ने विद्रोह की कमान संभाल रखी थी. # विरोध का कुचला जाना- 20 सितंबर, 1857 यानी आज ही की तारीख़ थी जब अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर दिल्ली पर पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया था. एक किस्सा जाने कितना सच कितना झूठ, पर है रोचक. जब मेजर हडसन मुगल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा तो उसने बहादुर शाह ज़फ़र से कहा:
दमदमे में दम नहीं है ख़ैर मांगो जान की, ऐ ज़फर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की.
 बहादुर शाह ज़फ़र (तस्वीर: विकीमीडिया)
बहादुर शाह ज़फ़र (तस्वीर: विकीमीडिया)हडसन या बाकी अंग्रेजों को भी हिंदी उर्दू का ज्ञान हो चला था. क्यूंकि उन्हें यहीं रहना और यहीं की अवाम पर राज करना था. बहरहाल बहादुर शाह ज़फ़र, जो न केवल शेरो-शायरी को एप्रीशिएट करते थे, बल्कि खुद भी काफ़ी अच्छे शायर थे, ने मेजर हडसन को जवाब दिया-
ग़ज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख़्त ऐ लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की.तो, इस विद्रोह के नेताओं को या तो मार दिया गया या निर्वासित कर दिया गया. कुछ ने आत्मसमर्पण भी कर दिया. 22 साल की लक्ष्मी बाई खूब लड़ीं लेकिन आखिरकार अंग्रेज़ों से हार गईं. और ये कहानी तो बुंदेलों हरबोलों के मुंह से हमने सुनी ही है. ग्वालियर पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था. इधर हडसन ने धोखे से बहादुरशाह द्वितीय के दो बेटे 'मिर्ज मुगल' और 'मिर्ज ख्वाजा सुल्तान' और एक पोते 'मिर्जा अबूबकर' को गोली मरवा दी. कॉलिन कैंपवेल ने गोरखा रेजिमेंट को लखनऊ का मोर्चा दे दिया और मार्च 1858 में लखनऊ भी दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया. 1857 का स्वाधीनता संग्राम एक साल से ज्यादा वक़्त तक चला. अँग्रेज़ पूरी तरह जुलाई 1858 में इस विद्रोह को दबा पाए. 8 जुलाई, 1858 को आखिरकार कैनिंग ने घोषणा कर दी कि विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया है. # क्यूं फेल हो गया विद्रोह- हालाँकि विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अछूता रहा. बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर और राजपूताना के लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए. दक्षिणी क्षेत्रों ने भी इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था.
इसके अलावा विद्रोहियों में एक मेन लीडरशिप की कमी थी. बहादुरशाह ज़फ़र को लेकर बाकी क्रांतिकारी नेता दिल्ली के बाहर आश्वस्त नहीं थे. हालाँकि नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने छिटपुट नेतृत्व किया भी लेकिन वे पूरे विद्रोह को रास्ता नहीं दिखा पाए.
एक और पॉईंट जो इस क्रांति या बग़ावत की असफलता का कारण बना वो था कम्यूनिकेशन गैप. रेल, डाक, तार और परिवहन अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था. क्रांतिकारी खबरें भेजने के लिए हरकारों पर निर्भर थे. जबकि अंग्रेजों के पास गोला बारूद और बंदूकों के अलावा सबसे बड़ा हथियार था- तार, जो मिनटों में सैकड़ों मील की दूरी तय करता था.
 ये लड़ाई टेलीग्राम और हरकारों के बीच भी थी. (तस्वीर: विकीमीडिया)
ये लड़ाई टेलीग्राम और हरकारों के बीच भी थी. (तस्वीर: विकीमीडिया)हालांकि अंग्रेज़ों का टेलीग्राफ़ विभाग सलामत नहीं रहा. क्रांतिकारियों ने कई तार लाइनें नष्ट कर दीं और काम कर रहे अंग्रेज़ कर्मचारियों को मार डाला. लेकिन कुल मिलाकर अंग्रेज़ों की, उस वक्त के हिसाब से, कटिंग एज़ टेक्नॉलजी विद्रोहियों पर भारी पड़ी.
विद्रोहियों के पास हथियारों और बाकी रसद की भी कमी थी. ऊपर से अंग्रेजी एजुकेशन पाने वाले मिडिल क्लास लोग और बंगाल के अमीर व्यापारियों और ज़मींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों की भरपूर मदद भी की थी.
बेशक विद्रोह कुचल दिया गया लेकिन इसमें इस विद्रोह से एक बात साफ़ हो गई थी कि अंग्रेज़ अपराजेय नहीं हैं, उन्हें घुटनों पर लाया जा सकता है. और इसलिए ही ठीक नौ दशकों बाद यानी 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजों के लिए बहादुर शाह ज़फ़र का एक और शे’र मौज़ूं हो गया था-












.webp?width=60)


.webp)