अगर मैं गलती से भी उका को छू लेता तो मुझे शुद्धिकरण के लिए कहा जाता. मैं यह सब चुपचाप मान लेता. यह सब बिना मुस्कुराए एक विरोध था, जो मैं यह जानते हुए कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि छुआछूत का धर्म में कोई स्थान नहीं है. मैं अपनी मां को यह बात बता चुका था कि उका के साथ छुआछूत का बर्ताव पूरी तरह से गलत है. - महात्मा गांधी ( द कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी सेयह बात उस वक्त की है जब महात्मा गांधी सिर्फ 12 साल के थे. उनके घर पर उका नाम की महिला सफाई का काम करने आती थी. उसके साथ हुए छुआछूत का व्यवहार महात्मा गांधी को ताउम्र याद रहा. यह घटना भले ही 19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों की व्यवस्था की झलक देती है, लेकिन भारत की सामाजिक व्यवस्था में छुआछूता का वर्णन इससे काफी पहले मिलता है. ह्वेंनसांग ने ऐसे देखी छुआछूत इतिहासकार साइमन बील अपनी किताब 'द लाइफ ऑफ ह्वेंनसांग
)
' में चीनी यात्री ह्वेंनसाग की नजरों से भारत का वर्णन लिखते हैं. बता दें कि ह्वेंनसांग भारत की यात्रा पर 7वीं शताब्दी में आया था. ह्वेंनसांग ने भारत को कुछ ऐसा देखा,
भारत का समाज अपने कामों के आधार पर चार भागों में बंटा है. इनमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर और सम्मानित माना गया है. इनकी ख्याति ऐसी है कि भारत को ब्राह्मणों का देश कहा जाता है. इसके बाद क्षत्रिय और वैश्यों का क्रम आता है. सबसे नीचे कृषक आते हैं. इनसे अलग कसाई, मछुआ, जल्लाद और चांडाल आदि लोग आते हैं. इनकी बस्तियां बाकियों की बस्तियों से अलग बसाई जाती हैं. दूर बसी बस्तियों से ही इन्हें पहचान लिया जाता है. जब वह सड़क पर चलते हैं, तो डरते हुए बाईं तरफ ही रहते हैं, जिससे बाकी लोग उनसे छू न जाएं.इस वर्णन से पता चलता है कि छुआछूत की जड़ें भारतीय समाज में सैकड़ों बरस गहरी हैं. वक्त-वक्त पर कुछ शूद्र राजाओं और योद्धाओं का वर्णन छोड़ दें तो छुआछूत को व्यवस्था के हिस्से की तरह ही माना गया था. पुणे का 'सत्यशोधक' ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक माली परिवार में जन्मे ज्योतिबा फुले को रचनात्मक आंदोलनकारी कहा जाए तो गलत नहीं होगा. उन्होंने छुआछूत के खिलाफ खड़े होने का नयाबा तरीका चुना. इस तरीके ने पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लोगों तक पैठ बनाई. उन्होंने अपने हथियार के तौर पर पढ़ाई-लिखाई को चुना. दलित समाज से जुड़े लोगों और खासकर महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. उनका साथ उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने दिया.
सावित्रीबाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की नौ छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए एक स्कूल की स्थापना की. एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले पांच नए विद्यालय खोलने में सफल हुए.
ज्योतिबा फुले ने लोगों की भाषा में उनसे बात की. किताबें ऐसी लिखीं कि दलित चिंतन जैसी गंभीर बात लोगों के दिमाग तक सीधे पहुंचे. बानगी देखिए तृतीय रत्न (नाटक, 1855), छत्रपति राजा शिवाजी का पंवड़ा (1869), ब्राह्मणों की चालाकी( 1869), ग़ुलामगिरी (1873), किसान का कोड़ा (1883) जैसी रचनाओं में सीधे-सीधे दलित अत्याचार और व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे. इसमें ‘गुलामगिरी’ तो बहुत खास है. इसमें दो पात्रों (धोंडिराव और ज्योतिराव) के सवाल-जवाबों के जरिए जाति और धर्म की तार्किक व्याख्या करने की कोशिश दिखती है. सटीक सवाल और उनके नुकीले और तार्किक जवाब. इस किताब को दलित चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है.

महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने लेखन के जरिए दलित चेतना पर गहरा प्रभाव डाला.
फिर आया 24 दिसंबर 1873 का दिन. ज्योतिबा फुले ने 'सत्यशोधक समाज' की नीव रखी. इस संगठन ने समाज सुधार का ऐसा घोषणा पत्र जारी किया कि आजतक दलितों की लड़ाई में यह हथियार बना हुआ है. सत्यशोधक के प्रमुख उद्देश्य में शूद्रों-अतिशूद्रों को पुजारी, पुरोहित, सूदखोर आदि की दासता से मुक्ति दिलाना, धार्मिक-सांस्कृतिक कामों में पुरोहितों की जरूरत को खत्म करना, शूद्रों-अतिशूद्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वे उन धर्मग्रंथों को खुद पढ़-समझ सकें, जिन्हें उनके शोषण के लिए ही रचा गया है, पढ़े-लिखे शूद्र युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आदि शामिल थे.
इस संगठन की सदस्यता सभी के लिए खुली थी, फिर भी मांग, महार, मातंग, कुनबी, माली जैसी अस्पृश्य और अतिपिछड़ी जातियां तेजी से उससे जुड़ने लगीं. सत्यशोधक समाज ने निचली जातियों को बड़ी संख्या में एक जुट करने का काम किया. ज्योतिबा फुले आज भी दलित आंदोलन और चिंतन के स्तंभ पुरुष के तौर पर जाने जाते हैं. उनके इस संगठन ने आधुनिक भारत में दलित चिंतन की एक रचनात्मक आवाज बुलंद की. छत्रपति शाहूजी महाराजः देश में पहली बार रिजर्वेशन लागू करने वाले राजा वक्त- उन्नीसवीं शताब्दी के आखिरी साल जगह - कोल्हापुर, महाराष्ट्र.
दलित गंगाराम कांबले की चाय की दुकान पर लोगों की भारी भीड़ जमा है. इसका कारण यह है कि महाराजा खुद एक दलित की दुकान पर चाय पीने आ रहे हैं. महाराजा चाय पीने पहुंचे और उन्होंने गंगाराम कांबले से पूछा,
तुमने अपनी दुकान के बोर्ड पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा है?महाराजा ने भारी भीड़ की मौजूदगी में मुस्कुराते हुए कांबले की चाय का आनंद लिया, उनमें से कई लोगों को शायद मालूम नहीं था कि चाय की दुकान खोलने के लिए कांबले को खुद महाराजा ने ही पैसे दिए थे.
कांबले -दुकान के बाहर दुकानदार का नाम और जाति लिखना कोई ज़रूरी तो नहीं.
महाराजा ने चुटकी ली - ऐसा लगता है कि तुमने पूरे शहर का धर्म भ्रष्ट कर दिया है.
आखिर कौन थे ये महाराज? ये महाराज छत्रपति शाहू जी महाराज थे. 26 जून 1874 को पैदा हुए शाहूजी कोई मामूली राजा नहीं थे, बल्कि महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वशंज थे. इस घटना का जिक्र इतिहासकार डॉक्टर मंजुश्री पवार अपनी किताब Rajarshi Shahu And British Paramountcy में किया हैं.
साल 1902 में शाहूजी महाराज ने अपने राज्य में एक और क्रांतिकारी कदम उठाया. 26 जुलाई 1902 में एक आदेश के तहत कोल्हापुर स्टेट गैजेट में एक व्यवस्था बनाई गई. इसने भारत पर राज कर रहे अंग्रेजों को भी बेचैन कर दिया. इस ऑर्डर में लिखा था,
‘हिज हाइनेस को यह बताते खुशी हो रही है कि इस ऑर्डर की तारीख से राजा के सभी ऑफिसों में पिछड़ों* के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी. जिन ऑफिसों में अभी पिछड़ों का प्रतिनिधित्व 50 फीसदी से कम है वहां पर अगली भर्ती में पिछड़े वर्ग को भर्ती किया जाए.*यहां पर पिछड़ों से मतलब गैर ब्राह्मण जातियों से है. यह वह वक्त था जब 90 फीसदी से ज्यादा प्रशासनिक पदों पर ब्राह्मण होते थे.
यह एक ऐसा फ़ैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की राह दिखाई. उन्होंने अपने शासन क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के छूआछूत पर क़ानूनन रोक लगा दी थी.

देश में नौकरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था का प्रावधान सबसे पहले कोल्हापुर के राजा शाहूजी महाराज ने किया था. (फोटो-विकिपीडिया)
आंदोलन जिन्होंने रास्ता दिखाया महात्मा गांधी और आंबेडकर तक दलित चेतना के पहुंचने से पहले भारत की जमीन पर छुआछूत के खिलाफ कई बार आवाजें बुलंद हुईं. दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय ने इन कुरीतियों पर बात की. इससे समाज में सुगबुगाहट जरूर हुई. हालांकि उनके प्रयासों में वह धार नहीं थी, जिससे दलित चेतना उठ खड़ी होती. ऐसे वक्त में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इस दंश से रूबरू हो रहे थे. उस वक्त भारत भी छुआछूत के खिलाफ जनआंदोलन का इंतजार कर रहा था. तीन बड़े आंदोलनों ने छुआछूत के खिलाफ समाज में तगड़ी चेतना का विस्तार किया. इसमें से एक आंदोलन पश्चिम में महाराष्ट्र से उठा, तो दूसरा सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु से, वहीं तीसरी आवाज भी दक्षिण से ही थी. तीनों ही आंदोलनों में छुआछूत के खिलाफ आग थी. तीनों ही बड़े बदलाव चाहते थे. इन तीनों आंदोलनों ने भारत में दलित आंदोलनों की राह प्रशस्त कर दी. तमिलनाडु में पेरियार का संघर्ष एक तरफ जहां महाराष्ट्र में पिछड़ों और दलितों को पढ़ने-लिखने और अलग से रिजर्वेशन देने जैसे कदम उठाए जा रहे थे, वहीं दक्षिण में इस आंदोलन का स्वरूप कुछ अलग था. तमिलनाडु में दलित आंदोलन की जड़ में ब्राह्मणों के खिलाफ पनप रहा गुस्सा था. दलितों में बरसों का गुस्सा दबा था. दक्षिण में छुआछूत की जड़ें बहुत गहरी थीं. मंदिरों से लेकर राजा के दरबार तक में ब्राह्मणों का बोलबाला था. छुआछूत का आलम यह था कि धार्मिक स्थलों में जाति विशेष के लोगों का प्रवेश तो दूर, नजदीक तक नहीं आने दिया जाता था. यह गुस्सा पेरियार यानी ई.वी रामास्वामी के नेतृत्व में बरस पड़ा. पेरियार ने 1919 में अपना राजनीतिक सफ़र कट्टर गांधीवादी और कांग्रेसी के रूप में शुरू किया. वो गांधी की नीतियों जैसे शराब बंदी, खादी और छुआछूत मिटाने की ओर आकर्षित थे. लेकिन एक घटना से नाराज होकर 1916 में वह कांग्रेस से नाराज हुए और जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने. इस पार्टी ने बाद में बड़े दलित आंदोलन का रास्ता खोला.

पेरियार यानी ईवी रामास्वामी का दक्षिण भारत में दलित आंदोलन में बड़ा योगदान है.
असल में पेरियार हमेशा से कांग्रेस में जातीय आरक्षण के प्रस्ताव को पास करने का प्रयास करते रहते थे. उनका कहना था कि कॉलेज से लेकर नौकरियों में दलितों को सही प्रतिनिधित्व और प्रोत्साहन मिले. इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई जिससे उन्हें बहुत धक्का लगा. असल में चेरनमादेवी शहर में कांग्रेस पार्टी के अनुदान से चलाए जा रहे एक स्कूल से दलित छात्रों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया था. यह स्कूल सुब्रह्मण्यम अय्यर का था. उस स्कूल में ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण छात्रों के साथ खाना परोसते समय अलग तरह का बर्ताव किया जाता था. पेरियार ने ब्राह्मण अय्यर से सभी छात्रों से एक जैसा बर्ताव करने की गुजारिश की. लेकिन न तो वो अय्यर को इसके लिए राजी कर सके और न ही कांग्रेस के अनुदान को रोक पाने में कामयाब हुए. उन्होंने खीज कर कांग्रेस ही छोड़ दी.
कांग्रेस छोड़ने कर उन्होंने 'आत्म-सम्मान आंदोलन' शुरू किया, जिसका लक्ष्य गैर-ब्राह्मणों (जिन्हें वो द्रविड़ कहते थे) में आत्म-सम्मान पैदा करना था. बाद में वो 1916 में शुरू हुए एक गैर-ब्राह्मण संगठन दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन (जस्टिस पार्टी के रूप में विख्यात) के अध्यक्ष बने. पेरियार घोर नास्तिक थे और बाकी लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे. पेरियार का मानना था कि समाज में बसे अंधविश्वास और भेदभाव की जड़ें वैदिक हिंदू धर्म में हैं. यही समाज को जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटता है, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है. इसलिए, वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ने पर आमादा थे. एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की धारणा के विरोध में प्रचार किया. केरल का वायकोम सत्याग्रह यहां पर दक्षिण के एक और सत्याग्रह की चर्चा भी करना जरूरी हो जाता है. इसे वायकोम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है. साल 1924 में वायकोम गांव में दलितों के समर्थन में बड़ा आंदोलन हुआ, जिसकी देशभर में चर्चा हुई. केरल में त्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था. केरल में पहले ही छुआछूत का बुरा हाल था. कुछ जातियों को 16-32 फुट की दूरी बना कर चलना होता था. ऐझवा और पुलैया जाति का बहुत ही बुरा हाल था. 30 मार्च, 1924 को केरल के कांग्रेसियों के एक दल ने मंदिर की बाड़ को तोड़कर मंदिर में प्रवेश किया. इनका नेतृत्व एझवाओं के कांग्रेसी नेता टीके माधवन ने किया. मंदिर में प्रवेश का समाचार फैलते ही ब्राह्मणों ने उग्र विरोध किया. सभी सत्याग्रहियों को गिरफ़्तार किया गया. इस सत्याग्रह के समर्थन में पूरे देश से स्वयंसेवक वायकोम पहुंचने लगे. पूरे देश का ध्यान वायकोम की तरफ गया. मार्च 1925 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में त्रावणकोर की महारानी के साथ मंदिर में प्रवेश को लेकर आंदोलनकारियों का समझौता हुआ. मंदिर के आसपास जाने के आदेशों को बदला गया. इसे दक्षिण भारत में एक बड़े आंदोलन की जीत की तरह देखा जाता है आंबेडकर का महाड सत्याग्रह डॉ भीमराव आंबेडकर आधुनिक भारत की दलित चेतना का सबसे बड़ा चेहरा हैं. उनके राजनीतिक जीवन की सबसे निर्णायक घटना 20 मार्च 1927 को घटी. यह घटना महाड़ के चवदार तलै (यानी मीठे पानी का तालाब) में हुई थी. इस कार्यक्रम में जाति से कायस्थ विनायक चित्रे नाम के सज्जन को धन्यवाद ज्ञापन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उन्होंने अपने भाषण में यह सुझाव दिया कि बंबई विधान परिषद के कानून के मुताबिक महाड़ की नगरपालिका ने यहां की चवदार तालाब को सभी जातियों के लिए खोल तो दिया है. लेकिन अभी भी किसी दलित की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह तालाब से पानी भर लाएं. इसलिए यदि हम अध्यक्ष (आंबेडकर) के साथ तालाब पर चलें और इस परंपरा को तोड़ें ताकि इस कानून की असल परीक्षा हो जाए.
फिर क्या था, इस सभा में दूर-दूर से भाग लेने आए तकरीबन 1500 दलित अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब की ओर चल पड़े. खुद उस इलाके के पुलिस इंस्टपेक्टर भी स्थिति की गंभीरता नहीं समझ पाए. वह भी उनके साथ-साथ ही चल दिए. यह तालाब ब्राह्मणों के मोहल्ले के ठीक बीच में था. चूंकि किसी को पता नहीं था कि दलितों की यह भीड़ तालाब पर पानी पीने जा रही है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई. सैकड़ो दलित तालाब में घुस गए और हर-हर महादेव का घोष करते हुए अपनी प्यास बुझाने लगे. सैकड़ों वर्षों से चली आ रही एक भेदभावपूर्ण परंपरा टूट चुकी थी.
इस नजारे को जब सवर्णों ने देखा, तो उनके भीतर गुस्सा भर गया. किसी ने झूठी अफवाह फैलाई कि अब ये अछूत वीरेश्वर मंदिर में घुसने वाले हैं. देखते ही देखते 400-500 लोग लाठी-डंडे लेकर निकल पड़े और रास्ते में जो भी दलित उन्हें दिखा, उसे बेतहाशा पीटा. दलितों को झोपड़ियों से निकाल-निकाल कर बेदम होने तक पीटा गया. घटना की जानकारी जब महात्मा गांधी को भी लगी, तो उन्होंने घटना का विरोध किया और आंबेडकर के कदम को सही बताया. हालांकि इस घटना ने भीमराव आंबेडकर के दिल में छुआछूत को लेकर खास नजरिए को मजबूत कर दिया. वह मानने लगे कि हिंदू धर्म में रहकर दलितों के अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती.

डॉ. भीमराव आंबेडकर के जीवन में महाड़ की घटना ने बड़ा असर छोड़ा. इस घटना के बाद उनकी दलित और हिंदू समाज के बीच रिश्तों को देखने का नजरिया बदला.
पूना पैक्ट समझौता 1931-32 के दौरान हुए गोलमेज सम्मेलन में आंबेडकर ने अंग्रेजों को दलितों के लिए खास इलेक्टोरेट के लिए राजी करने की कोशिश की. ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसके लिए राजी भी हो गए. जिसके तहत बाबासाहेब द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को दो वोटों का अधिकार मिला. एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तथा दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे. इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाना था. दूसरे शब्दों में उम्मीदवार भी दलित वर्ग का तथा मतदाता भी केवल दलित वर्ग के ही. लेकिन महात्मा गांधी को यह कतई मंजूर नहीं था. 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने पुणे की यरवडा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया.
24 सितम्बर 1932 को शाम पांच बजे यरवडा जेल पूना में गांधी और डॉ. आम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ. इस समझौते में डॉ. आम्बेडकर को कम्युनल अवॉर्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन (जैसा कि आजकल है) पद्धति को स्वीकार करना पडा, लेकिन इसके साथ हीं उन्होंने कम्युनल अवार्ड से मिली 71 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली. साथ ही दलितों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि तय करवाईं और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया.
इस समझौते पर हस्ताक्षर करके आंबेडकर ने महात्मा गांधी का अनशन तुड़वाया. हालांकि आंबेडकर इस समझौते से खुश नहीं थे. उन्होंने गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दवाब डालने के लिए खेला गया एक नाटक करार दिया.
अब गोलमेज सम्मेलन के बाद जब ब्रिटिश शासकों ने उस वक्त की अछूत जातियों के लिए अलग से एक अनुसूची बनाई. इसमें इन जातियों का नाम डाला गया. इसे एक खास व्यवस्था के तौर पर बनाया गया. इन्हें प्रशासनिक सुविधा के लिए अनुसूचित जातियां कहा गया. आज़ादी के बाद के भारतीय संविधान में भी इस व्यवस्था को बनाए रखा गया. इसके लिए संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जारी किया गया. इसमें भारत के 29 राज्यों की 1108 जातियों के नाम शामिल किये गए थे.
इस व्यवस्था पर ही आधुनिक रिजर्वेशन सिस्टम को जामा पहनाने की कोशिश बरसों से हो रही है. लेकिन आलोचकों का मानना है कि फिर भी अनुसूचित जातियों की इस संख्या से दलितों की असल तादाद का अंदाज़ा नहीं होता. क्योंकि ये जातियां भी, समाज में ऊंच-नीच के दर्जे के हिसाब से तमाम उप-जातियों में बंटी हुई हैं.












.webp)

.webp)

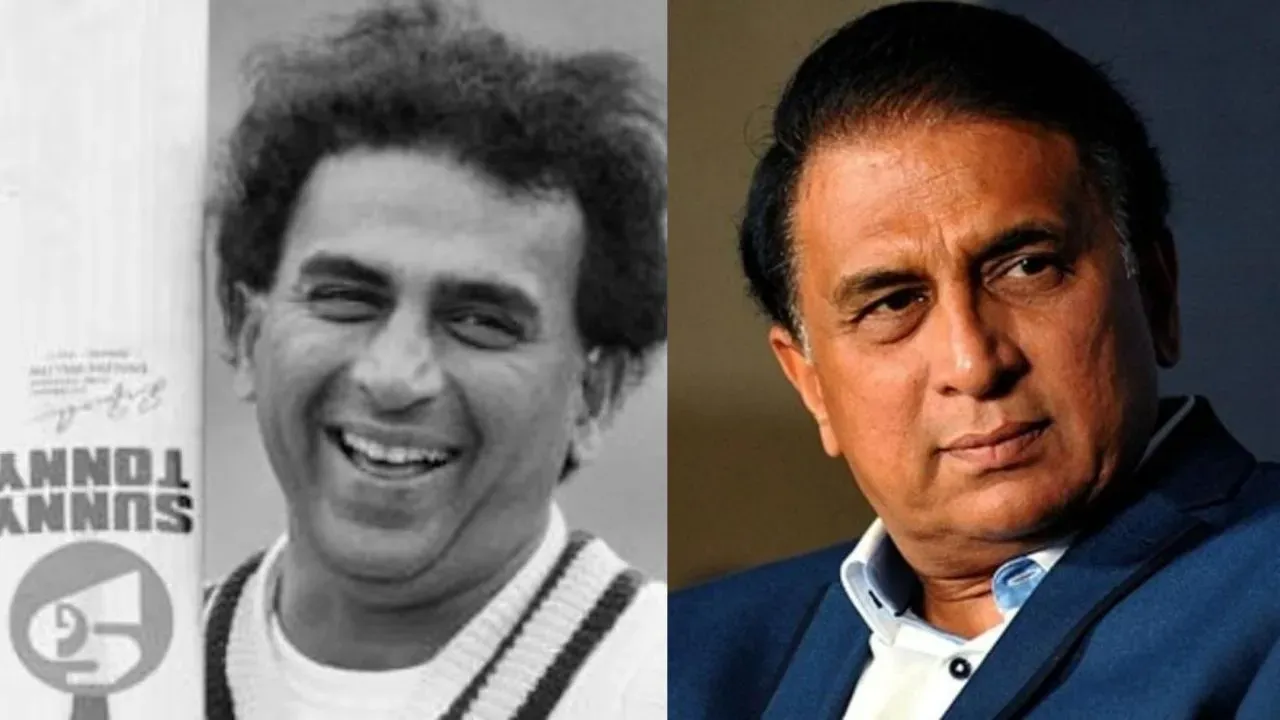
.webp)

