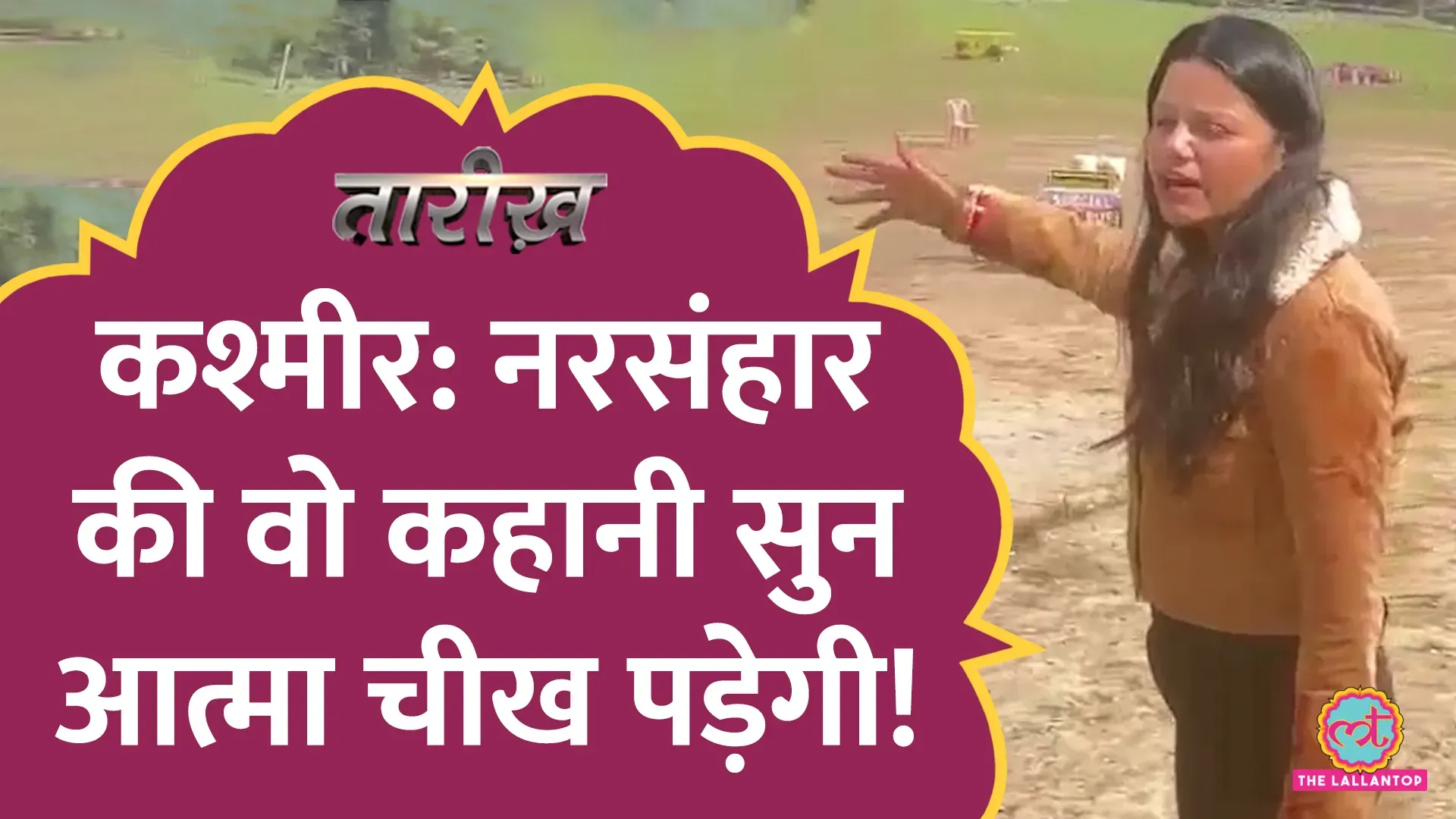प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर ट्वीट किया,
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून के निधन से काफी दुखी हूं. उन्होंने समर्पण भाव से देश की सेवा की और हमारे राष्ट्र को मजबूत और सुरक्षित बनाने का काम किया. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं.
साल था 1929. देश का विभाजन नहीं हुआ था. इस अविभाजित भारत के एबोटाबाद में एक लड़के का जन्म हुआ. इस लड़के का घर कांग्रेस का हेडक्वार्टर हुआ करता था. आज़ादी की लड़ाई और उनके लीडरों से काफी नजदीकी रही. 18 साल की उम्र में उसने देहरादून की इंडियन मिलिटरी एकेडमी में दाखिला लिया. उसी साल देश की आज़ादी और बंटवारा एकसाथ हुआ था.
दो साल बाद उस लड़के को सिख रेजिमेंट में कमीशन किया गया. उसने 1962 के भारत-चीन और 1965 के भारत-पाक युद्ध में भी हिस्सा लिया. इंडियन आर्मी में कई बड़े पदों पर काम किया. कई रणनीतिक लड़ाइयों में देश का नाम ऊंचा किया.

लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून का जन्म एबोटाबाद (अब पाकिस्तान) में हुआ था.
सबसे खास मुकाम आया 1984 में, जब इंडियन आर्मी ने 'ऑपरेशन मेघदूत' चलाकर सियाचिन पर कब्ज़ा किया था. 'ऑपरेशन मेघदूत' एक कोड नेम था. लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून उस वक्त श्रीनगर के 15 कॉर्प्स के कमांडर हुआ करते थे. उन्होंने 'ऑपरेशन मेघदूत' में काफी अहम भूमिका निभाई थी.
सियाचिन का महत्व
NJ 9842 पॉइंट से काराकोरम पास तक का इलाका. ये जमीन रहने के लिए तो किसी मतलब की नहीं थी, लेकिन इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था. अगर सियाचिन का इलाका पाकिस्तान के कब्ज़े में आ जाता, तो पाकिस्तान और चीन एकदम पास हो जाते. ये सुरक्षा के नजरिए से भारत के लिए बहुत बड़े खतरे वाली बात थी.
कराची समझौता और NJ 9842
1947 में अंग्रेज भारत से गए. जाने से पहले एक लफड़ा लगाकर गए. देश को दो हिस्सों में बांट दिया. हिन्दुस्तान और पाकिस्तान. घर के लोग पड़ोसी हो गए थे. और पड़ोसी ऐसे, जिनको एक-दूसरे की शक्ल फूटी आंख नहीं सुहाती थी. आज़ादी के फौरन बाद पहली लड़ाई शुरू हुई. जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान ने अपने कबाइली लड़ाके भेजे. महाराजा हरिसिंह के दस्तखत के बाद इंडियन आर्मी कश्मीर में गई और लड़ाई को अपने हाथों में ले लिया. पाकिस्तानी लड़ाकों को आगे बढ़ने से रोका. ये दोनों पड़ोसी देशों के बीच हुआ पहला टकराव था.

महाराजा हरिसिंह ने भारत में शामिल होने के कागजातों पर दस्तखत किए, उसके बाद ही इंडियन आर्मी कश्मीर में गई. फोटो में महाराजा हरिसिंह और सरदार पटेल नजर आ रहे हैं. (फोटो: PIB)
भारत-पाकिस्तान की इस पहली लड़ाई पर लगाम लगी संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर. 1 जनवरी, 1949 को दोनों देशों के बीच सीजफ़ायर हो गया था. UN ने अपनी मौजूदगी में दोनों देशों के बीच एक समझौता करवाया. कराची में. 27 जुलाई 1949 के दिन. इस समझौते ने एक लकीर खींची. सीजफायर लाइन. ये लकीर जिस पॉइंट पर खत्म होती थी, उस पॉइंट को NJ 9842 का नाम दिया गया. इस पॉइंट के नॉर्थ में काफी बड़ा हिस्सा ग्लेशियरों का था, जहां किसी भी देश का दावा नहीं था. किसी भी देश को उस हिस्से में पोस्ट या आर्मी कैंप बनाने की मनाही थी. वहां कोई लकीर नहीं थी. ये एक बड़े विवाद को जन्म देने वाला था.
भारत-चीन की लड़ाई
1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ. लड़ाई में चीन बीस साबित हुआ. इसके बाद हालात में बदलाव होना शुरू हो गया. पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े वाले कश्मीर का बड़ा हिस्सा चीन को दे दिया. अक्साई चिन पर पहले ही चीन ने अपना दावा ठोक दिया था.
1960 के दशक के बाद के बरसों में ये स्थिति और भी खराब होती गई. NJ 9842 से आगे के इलाके में पाकिस्तान ने विदेशियों को ट्रेकिंग की परमिट देनी शुरू कर दी. ये उस बंजर हिस्से पर दावा ठोकने की शुरुआत थी. माउंटेनियरिंग के नक्शों में इस हिस्से को पाकिस्तान का दिखाया जाने लगा. पाकिस्तान की तरफ से लाइजन ऑफिसर भी इन ट्रेकिंग्स में साथ में जाने लगे थे.
LoC की लकीर
1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ. इस युद्ध का अंत 1972 के शिमला समझौते के बाद हुआ. इंदिरा गांधी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच. शिमला समझौते के तहत दोनों देशों के मिलिटरी डेलीगेशन के बीच 9 मुलाकातें हुईं. वाघा और सुचेतगढ़ में. सुचेतगढ़ में समझौते पर दोनों पक्षों ने साइन किए. और, NJ 9842 को लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) का नाम दे दिया गया. ये स्थिति तब तक बरकरार रहनी थी, जब तक कि दोनों देशों के बीच जम्मू-कश्मीर का मसला सुलझ नहीं जाता.

1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध ने इंदिरा गांधी को राजनीति की आयरन लेडी बना दिया था.
शिमला समझौते के पांच साल बाद. दोनों देशों में सरकार बदल चुकी थी. भारत में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर चुकी थी. मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बने. पाकिस्तान में जनरल ज़िया उल हक़ ने भुट्टो को गद्दी से उतारकर फ़ांसी पर लटका दिया था.
एक नक्शे ने पूरी कहानी बदल दी
इसी बीच खुफिया एजेंसी RAW को एक टिप मिली. किससे? लंदन की एक कंपनी से. ये कंपनी आर्कटिक गियर बनाती थी. आर्कटिक गियर उन कपड़ों को कहा जाता है, जो अत्यंत बर्फीले इलाकों के लिए जरूरी होते हैं. इंडियन आर्मी अपने लिए आर्कटिक गियर उसी कंपनी से खरीदती थी. RAW को ये पता चला कि पाकिस्तान भी उसी कंपनी से यही आर्किटक गियर खरीद रहा है. RAW ने ये टिप इंडियन आर्मी तक पहुंचाई.
1977 में जर्मनी से पर्वतारोहियों की एक टीम आई थी. इंडिया की तरफ से साल्टोरो रेंज पर ट्रेकिंग की इजाज़त लेने के लिए. ये लोग कर्नल बुल्ल कुमार से मिले. कर्नल कुमार High Altitude Warfare School के कमांडिंग ऑफिसर थे. जर्मनों के पास जो नक्शा था, उसमें NJ 9842 से काराकोरम पास तक का हिस्सा पाकिस्तान का बताया जा रहा था. इसमें सियाचिन का हिस्सा भी शामिल था.

सियाचिन दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है.
कर्नल बुल्ल कुमार नई दिल्ली में पहुंचे. उन्होंने वो जर्मन नक्शा डायरेक्टर ऑफ़ मिलिटरी ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छिब्बर को दिखाया. कई और विदेशी जर्नलो में छपे नक्शे दिखाए गए. हड़कंप मच गया. लेफ्टिनेंट जनरल छिब्बर ने कर्नल बुल्ल कुमार को असल स्थिति की जानकारी लाने की इजाजत दे दी.
कर्नल नरेद्र बुल्ल कुमार ने ट्रेकिंग के लिए गई एक टीम को लीड किया. ये लोग बिलाफ़ोंड ला पहुंचे, तो उनको कुछ जापानी लेबल वाले टिन के डिब्बे मिले. एक समय पाकिस्तानी हेलिकॉप्टर की गश्त भी नजर आई. ग्राउंड पर कोई पाकिस्तानी हरकत नहीं दिखी. कर्नल कुमार ने लौटकर रिपोर्ट सौंपी. इसमें कहा गया था कि इंडिया को सियाचिन के इलाकों में गश्त तेज कर देनी चाहिए. एक पोस्ट बनानी चाहिए, जिसे गर्मी के महीनों में सैनिकों की तैनाती के लिए इस्तेमाल में लाया जाए.
पोस्ट बनाने की बात तो नकार दी गई. लेकिन पेट्रोलिंग की फ़्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई.
Attack is the Best defence
पेट्रोलिंग के दौरान इंडियन आर्मी को पर्चा दिखा. इसमें पाकिस्तान का संदेश था. पाकिस्तान ने साफ-साफ कहा कि इंडिया को उसके इलाके में दखल नहीं देनी चाहिए. संकेत था कि सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान अपनी जमीन मान चुका है.
1982 में लेफ्टिनेंट जनरल छिब्बर नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने. उसी दौरान उनके पास पाकिस्तान का एक प्रोटेस्ट नोट आया था. इंडिया की तरफ से भी विरोध दर्ज कराया गया. लेकिन पाकिस्तान सियाचिन पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था.
21 अगस्त, 1983 को पाकिस्तान के नॉर्दर्न सेक्टर कमांडर ने इंडिया के नॉर्दर्न सेक्टर कमांडर को एक नोट भेजा. इसमें लिखा था,
आग्रह, अपने सैनिकों को निर्देश दें कि वे जल्द-से-जल्द NJ 9842 और काराकोरम पास को जोड़ने वाली NJ 9842 से बाहर निकल जाएं. मैंने अपने जवानों को संयम रखने के लिए कहा है, लेकिन हमारी जमीन खाली करने में देरी हुई तो स्थिति गंभीर हो सकती है. LoC पर शांति बनाए रखने में मेरा पूरा सहयोग रहेगा.29 अगस्त, 1983 को इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट नोट भेजा गया. कहा गया कि अपने जवानों को सीमा में रखें और बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश न करें. सितंबर-अक्टूबर, 1983 में इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान सियाचिन में अपनी आर्मी भेजने की तैयारी कर रहा है. उसने Burzil Forces के नाम से एक टुकड़ी तैयार की थी, जिसे सियाचिन पर कब्जे के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी.
अब एक ही रास्ता बचा था. इंडिया को अपनी तैयारी से दुश्मन के वार को बेअसर कर देना था. बर्फ की हुकूमत वाले उन इलाकों के लिए जरूरी सामान चाहिए था. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून को इन इक्विपमेंट के लिए यूरोप भेजा. वे एक सप्लायर से मिले. लेकिन उसने दूसरे सप्लायर का नंबर दिया. पहले सप्लायर के पास 150 इक्विपमेंट का ऑर्डर था. ये ऑर्डर पाकिस्तान का था.
अब लड़ाई आर-पार की थी. ब्रिगेडियर चन्ना की रणनीति थी कि दुश्मन को मौका देने से पहले कार्रवाई कर देनी चाहिए. अप्रैल के महीने में भारी बर्फबारी होती है. उस मौसम का सामना करना आम इंसानों के बस की बात नहीं है. आर्मी ने ऑपरेशन के लिए वही वक्त चुना.

ऑपरेशन मेघदूत में हल्के चीता हेलिकॉप्टरों ने खास भूमिका निभाई थी.
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने अपनी किताब 'इन दी लाइन ऑफ़ फ़ायर' में लिखा,
इंडिया ने हमें हैरान कर दिया था. हमें इस कदम की कतई उम्मीद नहीं थी.इधर कर्नल कुमार के नेतृत्व में जवानों की ट्रेनिंग चल रही थी. लद्दाख स्काउट्स और कुमाऊं रेजिमेंट के जवान इस अभियान के लिए तैयार किए जा रहे थे. जब इक्विपमेंट आने में देरी हो रही थी, उस वक्त जवानों से पूछा गया था,
क्या आप बिना सही कपड़ों के ऊंचाई वाले इलाकों में जाएंगे?सबने एक स्वर में कहा था,
यस सर.12 अप्रैल 1984. शाम 5 बजे. MI-17 हेलिकॉप्टर उतरा. हेलिकॉप्टर में थे लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून द्वारा लाए गए इक्विपमेंट. ये सामान पहुंचते ही ऑपरेशन को हरी झंडी दिखा दी गई. चार टीमें सियाचिन को अपने कब्जे में लेेने के मिशन के लिए तैयार थीं. इंदिरा कॉल, सिया ला, बिलाफोंड ला और ग्योंग ला.
अगला दिन बैसाखी का था. पाकिस्तान को इस दिन इंडिया के ऑपरेशन की कोई उम्मीद नहीं थी. 13 अप्रैल, 1984 की सुबह चीता हेलिकॉप्टरों ने जवानों को ऊंचाई वाले इलाकों पर पहुंचाना शुरू कर दिया. 30 जवानों ने बिलाफोंड ला को आराम से कब्जे में ले लिया गया. उसके बाद बर्फबारी और तेज हो गई. दो दिनों के बाद मौसम साफ हुआ. 16 अप्रैल, 1984 को सिया ला भारत के कब्जे में था.
पाकिस्तान ने जून के महीने में 'ऑपरेशन अबाबील' लॉन्च किया था. दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड में गोलियां और मोर्टार दागे गए. पाकिस्तान को बार-बार मुंह की खानी पड़ी. अगस्त आते-आते ग्योंग ला पर इंडियन आर्मी ने तिरंगा फहरा दिया था. अब पूरा सियाचिन कब्जे में था. लेकिन ये लड़ाई का अंत नहीं था.
कारगिल का ब्लूप्रिंट
'ऑपरेशन मेघदूत' को 1999 के कारगिल वॉर का ब्लूप्रिंट कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि सियाचिन पर कब्जे की लड़ाई ने ही कारगिल वॉर की बुनियाद रखी थी.

परवेज मुशर्रफ़ ने अपनी किताब 'In the Line of Fire' में सियाचिन विवाद का किस्सा बयान किया है. (फोटो : गेट्टी इमेजेज)
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ 1987 में सियाचिन के पास की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप (SSG) के ब्रिगेड कमांडर बने. उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति जनरल ज़िया उल हक़ को एक डिटेल प्लान पेश किया. प्लान था इंडियन आर्मी को सियाचिन ग्लेशियर से हटाने का. इसके लिए उन्होंने NH-1A को कब्ज़े में लेने की राय दी. ताकि इंडियन आर्मी सियाचिन तक सप्लाई पहुंचा न सके. इस प्लान को ज़िया उल हक़ ने रिजेक्ट कर दिया. 1988 में प्लेन क्रैश में ज़िय़ा उल हक़ की मौत हो गई. मुशर्रफ़ ने ये प्लान बेनज़ीर भुट्टो के सामने भी पेश किया. उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया.
लेकिन सियाचिन में पाकिस्तान की हार मुशर्रफ़ के दिमाग से नहीं निकली. 1999 में जब मुशर्रफ़ पाकिस्तान के DGMO(Director General of Military Operations) बने, तब उन्होंने ये प्लान बाहर निकाला और कारगिल पर कब्जा किया. कारगिल में जो हुआ, वो एक अलग इतिहास है.
वीडियो : भारत का सबसे ज़्यादा मेडल वाला वॉर हीरो मर गया, न फूल चढ़े, न 'ट्वीट' हुआ