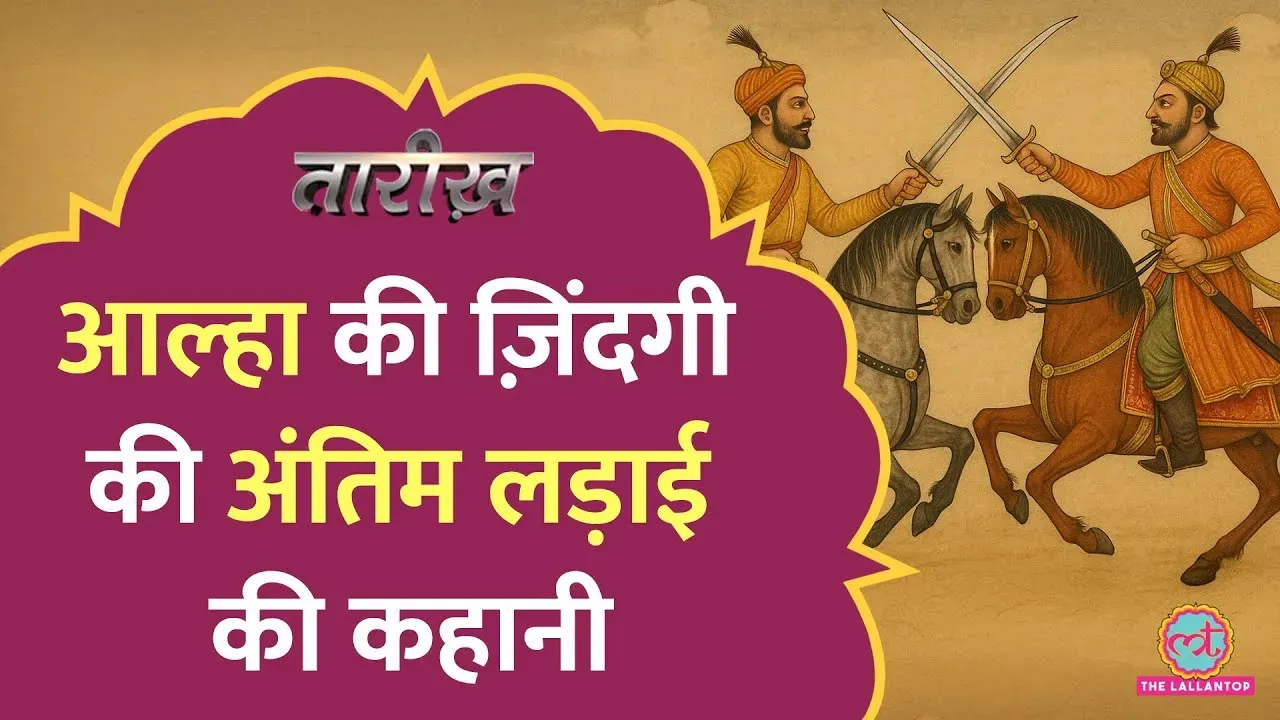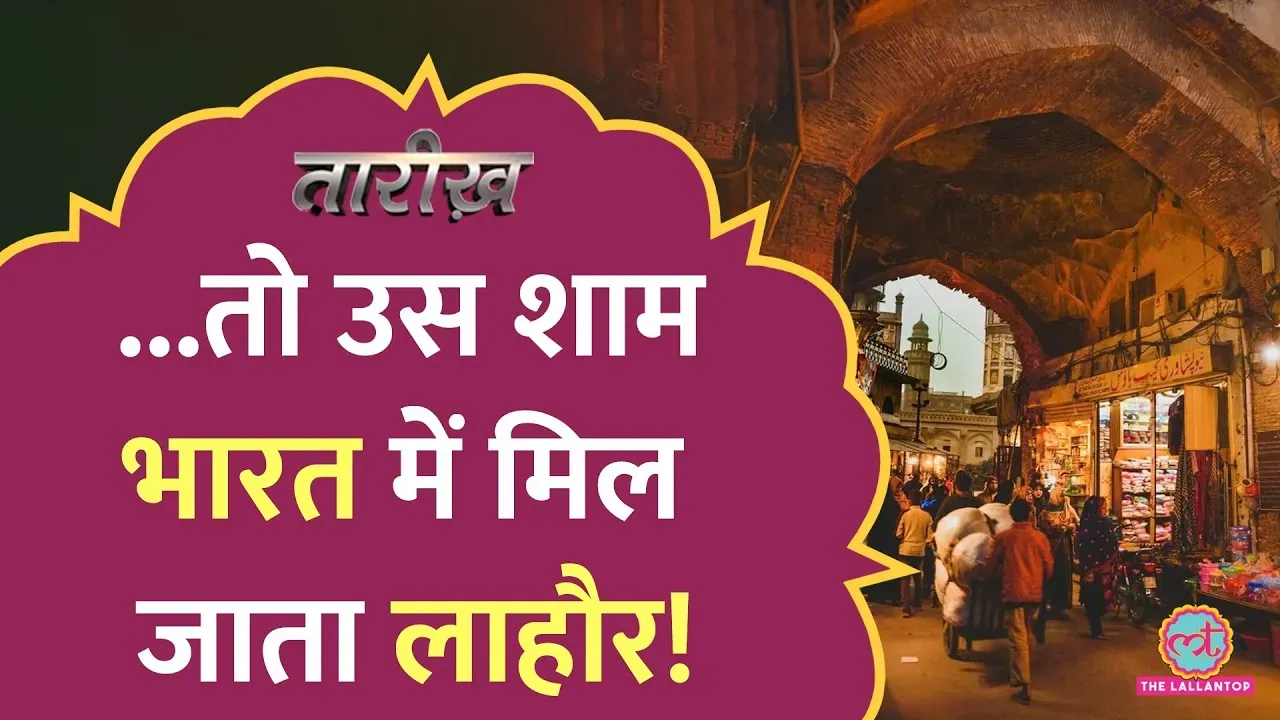उत्तर भारत के लोगों को भले ही कैम्पेगौड़ा नाम अजनबी सा सुनाई देता हो, कर्नाटक में ये नाम सुनकर कई लोगों का सिर श्रद्धा से झुक जाता है. बंगलौर में कैम्पेगौड़ा के नाम पर हवाई अड्डा है. कुछ ही दूर पर कैम्पेगौड़ा की 108 फ़ीट की विशाल मूर्ति है. इस नाम की राजनीतिक अहमियत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बख़ूबी समझा. उन्होंने पिछले साल यानी 11 नवंबर 2022 को इस मूर्ति का अनावरण किया. उसी दिन मोदी ने कैम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का उद्घाटन किया. टर्मिनल बनाने का कुल ख़र्च – 5 हज़ार करोड़ रुपए!!
कहानी कर्नाटक के वोक्कलिगा समाज की जो हर बार देवगौड़ा को किंगमेकर बना देता है
कर्नाटक के जातीय समीकरण का पूरा तियां पांचा.


कर्नाटक की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले जानते हैं कि बीजेपी के लिए लिंगायत समाज की कितनी अहमियत है. कर्नाटक की सत्ता में बीजेपी की एंट्री का जरिया ही पार्टी के बड़े नेता येदियुरप्पा थे. और डिस्क्लेमर ये कि येदियुरप्पा लिंगायत समाज से आते हैं. लेकिन जिन कैम्पेगौड़ा का ज़िक्र पहले हमने किया वो वोक्कलिगा समाज के आराध्य हैं. उनके प्रतीक पुरुष. उत्तर भारत में जैसे हर पार्टी जातीय गणित लगाती है, कर्नाटक में राजनीति की कल्पना वोक्कलिगा और लिंगायत पंथों के बिना नहीं की जा सकती. बीजेपी को दोनों समुदायों को एक साथ साधना है. पर पेच ये है कि लिंगायत और वोक्कलिगा राजनीतिक रूप से कभी पास ना आने वाले दो ध्रुव हैं. बीजेपी की निर्भरता लिंगायत वोटों पर रहती है लेकिन बावजूद इसके वोक्कलिगा के हीरो कैंपेगौड़ा को महत्व देना, राज्य में वोक्कलिगा समाज के महत्व को बयां करता है. लिंगायत के साथ-साथ कर्नाटक में सभी राजनीतिक पार्टियां वोक्कलिगा समाज के वोट पाने के लिए नतमस्तक रहती है.
कौन हैं वोक्कलिगा?वोक्कलिगा शब्द बना है वोक्कलु से. वोक्कलु का मतलब होता है खेती करना. यानी वोक्कलिगा खेतिहर लोग हैं. बेंगलुरु की ISEC यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चंदन गौड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वोक्कलिगा शब्द का पहली बार इस्तेमाल दसवीं शताब्दी में हुआ था. जब शिवाकोटिआचार्य ने जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ वड्डाराधने में खेतिहर लोगों के लिए वोक्कलिगा शब्द लिखा. उन्होंने खेती करने वालों को वोक्कलिगा कहा. इसका जाति से कोई लेना देना नहीं था.
बाद में मैसूर पर हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने राज किया. 1799 में टीपू सुलतान की मौत के बाद वहां अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया. 19 शताब्दी के अंत में जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई तो खेती-किसानी करने वालों को वोक्कलिगा कह दिया. इसमें वो लोग भी शामिल थे जो खेती के साथ साथ लोहे या लकड़ी का काम भी करते थे.
पर पहली बार 1906 में वोक्कलिगा समाज को एक समुदाय के तौर पर एकजुट करने की कोशिश की गई. इस बरस वोक्कलिगारा संघ की स्थापना हुई. संघ का पहला लक्ष्य था छात्रों के लिए हॉस्टल बनाना. मैसूर के तब के महाराजा इस संघ के संरक्षक बने. तभी से वोक्कलिगा समाज खुद को एकजुट करने, राजनीतिक रूप से खुद को सशक्त करने की कोशिश में जुटा हुआ है. आज कर्नाटक की राजनीति में इस समुदाय को एक ख़ास मक़ाम हासिल हो चुका है.
कैम्पेगौड़ाकैम्पेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य में प्रभावशाली मुखिया थे. उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था. कैम्पेगौड़ा का परिवार तमिलनाडु के कांची से कर्नाटक आया था और उसके बाद उन्होंने विजयनगर में कामकाज संभाला. बताया जाता है कैम्पेगौड़ा ने बहुत कम उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद पद संभाला. और इसी दौरान उन्होंने बेंगलुरु शहर की स्थापना की. आज ये एक मॉडर्न शहर है -- कर्नाटक की राजधानी और देश का एक प्रमुख IT हब.

वोक्कलिगा समाज कैम्पेगौड़ा पर उसी तरह गर्व करता है जैसे मराठा समाज छत्रपति शिवाजी पर. यही वजह थी कि लिंगायत समाज की सबसे करीबी माने जाने वाली बीजेपी ने भी कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई.
वोक्कलिगा समाज का राजनीतिक प्रभावइस बात में आज कोई विवाद नहीं है कि कर्नाटक में वोक्कलिगा समाज का एकमुश्त वोट जनता दल सेक्यूलर यानी JDS के हिस्से जाता है. और इसकी एक मात्र वजह हैं एचडी देवगौड़ा. देवगौड़ा ने ये विश्वास एकाएक नहीं हासिल किया. और न ही ऐसा उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ. प्रधानमंत्री बनने से देवगौड़ा का कद बढ़ा और उन पर समाज की जिम्मेदारियां बढ़ीं लेकिन समाज का ये विश्वास उन्होंने दशकों में हासिल किया है. कर्नाटक की राजनीति की समझ रखने वाले बताते हैं कि देवगौड़ा अपने समाज के प्रभावशाली लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं. उन्होंने घर-घर जाकर अपने लोगों का भरोसा जीता है.
देवगौड़ा वोक्कलिगा समाज के इकलौते नेता नहीं हैं, लेकिन फिलहाल वो इस समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं.
कर्नाटक बना 1973 में. उससे पहले इसे मैसूर स्टेट के नाम से जाना जाता था. आज़ादी के बाद कर्नाटक वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है. मैसूर स्टेट में मैसूर रीजन तक ही सीमित था.1956 में राज्य का पुनर्गठन किया गया. पुनर्गठन में मुंबई-कर्नाटक रीजन और हैदराबाद-कर्नाटक रीजन को भी इसमें शामिल किया.
1956 में जब मैसूर स्टेट का पुनर्गठन हुआ तब राज्य के मुख्यमंत्री थे केंगल हनुमंथइया. वो वोक्कलिगा थे और तब सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे. न सिर्फ वोक्कलिगा बल्कि मैसूर राज्य के बड़े नेता. बताया जाता है कि जब मैसूर राज्य का पुनर्गठन हो रहा था तब लोग इसके समर्थन में नहीं थे. लोगों का कहना था कि महाराजा का मैसूर तो पहले से ही विकसित और संपन्न है. लेकिन अगर मुंबई कर्नाटक रीज़न और हैदराबाद कर्नाटक रीज़न को जोड़ दिया जाएगा तो मैसूर स्टेट के हिस्से आने वाला मैसूर उतना संपन्न नहीं रहेगा. क्योंकि ये दोनों रीज़न मैसूर के मुकाबले आर्थिक रूप से कमजोर थे.
विरोध के पीछे की एक और वजह थी. मैसूर रीज़न में वोक्कलिगा समाज का वर्चस्व है. वो वर्चस्व आज भी कायम है. लेकिन ये जानते थे कि अगर उत्तर कर्नाटक का लिंगायत समाज भी राज्य में शामिल हो जाएगा तो संख्या बल में वोक्कलिगा कमजोर हो जाएंगे.
कहा जाता है कि जब मैसूर के पुनर्गठन का विरोध हुआ तो केंगल हनुमंथइया ने ही लोगों को समझाया कि अगर पुनर्गठन नहीं हुआ को वोक्कलिगा समाज पर बड़ा इल्जाम आएगा. हालांकि लोगों डर जायज़ था. और हुआ भी कुछ ऐसा ही. पुनर्गठन के बाद से वोक्कलिगा कमजोर पड़ते गए. और लिंगायत मजबूत होते गए.
1956 में राज्य विधानसभा चुनाव हुए और वोक्कलिगा हनुमंथइया की जगह इस बार कांग्रेस ने लिंगायत एस निजलिंगप्पा को मुख्यमंत्री बनाया. यहां से कर्नाटक में शुरू हुआ लिंगायतों का वर्चस्व. 1956 से 1973 तक यानी मैसूर के कर्नाटक बनने तक राज्य में चार मुख्यमंत्री बने और चारों लिंगायत थे.
सत्ता में वोक्कलिगा नेता की वापसी लगभग 50 बरस बाद हुई जब 1994 में हरधनहल्ली दौड्डेगौडा देवगौड़ा मुख्यमंत्री बने. सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले देवगौड़ा पढ़ाई के बाद राजनीति में आ गए. वो 1953 में कांग्रेस में शामिल हुए. ये वो दौर था जब सूबे के मुख्यमंत्री थे हनुमंथइया. देवगौड़ा 1962 तक तो कांग्रेस में रहे. उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी. यहीं से उनकी चुनावी राजनीति की शुरुआत भी हो गई. 1962 से 89 तक देवगौड़ा सात बार होलेनरसीपुरा से विधायक चुनकर आए. कभी निर्दलीय तो कभी अन्य पार्टियों से. जब जनता पार्टी बना तो देवगौड़ा उसमें शामिल हो गए. फिर 1989 में उन्होंने जनता दल ज्वाइन कर लिया.

समय बीतने के साथ ही देवगौड़ा वोक्कलिगा समाज पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे. अपने समाज में वो पॉपुलर लीडर थे. और दशकों की चुनावी राजनीति ने उन्हें दक्षिण कर्नाटक के घर-घर तक पहुंचा दिया था.
1990 में राजीव गांधी ने लिंगायत सीएम वीरेंद्र पाटिल को अचानक हटा दिया. पाटिल बीमार थे. उन्हें हटाना कांग्रेस को भारी पड़ा. लेकिन यहीं से पहली बार देवगौड़ा बिग पिक्चर में आए. जनता दल को 1994 के चुनाव में बहुमत मिला और कुर्सी देवगौड़ा को मिली. हनुमंथइया के बाद कोई वोक्कलिगा पहली बार कर्नाटक का मुख्यमंत्री बन रहा था.
लेकिन कर्नाटक की कुर्सी पर बैठने के बाद देवगौड़ा ने ख़्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर बैठना होगा. और वो भी जनादेश के बिना. 1996 के लोकसभा चुनाव में जनादेश बिखरा हुआ था. गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस दलों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बनाया. सरकार कांग्रेस के समर्थन से बननी थी. सभी पार्टियां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमत थीं. लेकिन खुद ज्योति बसु की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भाँजी मार दी. पार्टी ने कहा बसु प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे. लेफ्ट के हैरान करने वाले इस फैसले ने ज्योति बसु को बंगाल तक ही सीमित कर दिया.
फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. इस चुनाव में कर्नाटक में जनता दल को 16 सीटें मिली थी. वहां के मुख्यमंत्री थे देवगौड़ा. कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनती है और देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं एचडी देवगौड़ा. धान की खेती करने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना था. वोक्कलिगा समाज इससे ज्यादा उत्साहित पहले नहीं हुआ था. देवेगौड़ा ख़ुद को बार-बार ‘हम्बळ फ़ार्मर’ कहते थे.
देवगौड़ा के बाद वोक्कलिगा समाज से आने वाले एसएम कृष्णा को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया. 1999 से 2004 तक कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे. बाद में वो कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय विदेश मंत्री भी रहे. हालांकि 2017 में वो बीजेपी में शामिल हो गए.
मौजूदा दौर में कर्नाटक की जमीनी राजनीति के एक मज़बूत नेता हैं एचडी कुमारस्वामी हैं. एचडी देवेगौड़ा के बेटे. कुमारस्वामी दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं. हालांकि दोनों बार गठबंधन के सहारे ही सत्ता तक पहुंचे. कुमारस्वामी के वोक्कलिगा समाज के नेता होने के पीछे बड़ी वजह देवगौड़ा ही हैं. देवगौड़ा के बेटे होने के नाते राजनीति और वोक्कलिगा समाज का समर्थन उन्हें विरासत में मिला है.
वोक्कलिगा समाज को साधना क्यों जरूरी?जैसे उत्तर कर्नाटक को लिंगायतों का गढ़ माना जाता है वैसे ही दक्षिण कर्नाटक वोक्कलिगा समाज का गढ़ है. खास तौर पर ओल्ड मैसूर रीजन. दक्षिण कर्नाटक के जिले जैसे मंड्या, हसन, मैसूर, बैंगलोर (ग्रामीण), टुमकुर, चिकबल्लापुर, कोलार और चिकमगलूर इलाकों वोक्कलिगा वोट विधायक चुनने की क्षमता रखता है.
सूबे में इनकी आबादी करीब 11 प्रतिशत बताई जाती है. और 48 सीटें ऐसी हैं जहां वोक्कलिगा अहम भूमिका निभाते हैं. मौजूदा विधानसभा में 42 विधायक वोक्कलिगा समाज के हैं. जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा वोक्कलिगा विधायक जेडीएस के थे. जेडीएस के 23 विधायक वोक्कलिगा समाज से आते हैं. कांग्रेस के 11 विधायक और बीजेपी के 8 विधायक वोक्कलिगा हैं.
यही वजह है कि बीजेपी वोक्कलिगा समाज को अपनी तरफ खींचने की भरसक कोशिश कर रही है. कैम्पेगौड़ा की मूर्ति लगाना हो या एसएम कृष्णा को चुनावी साल में पद्म विभूषण से सम्मानित करना, वोक्कलिगा वोट को लुभाने के लिए बीजेपी कोई प्रतीकात्मक कसर नहीं छोड़ना चाह रही. लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि पार्टी के पास वोक्कलिगा समाज का कोई बड़ा नेता नहीं है. 90 साल की उम्र में एसएम कृष्णा को बीजेपी न तो वोक्कलिगा नेता के तौर पर पेश कर पा रही है न ही वोटों के लिए अपील करवा पा रही. ऐसे में पार्टी ने उन्हें सम्मानित करने के लिए पद्म विभूषण दे दिया.

कांग्रेस भले ही वोक्कलिगा वोटों को जेडीएस की तरह अपने पाले में नहीं ला पा रही हो, लेकिन पार्टी के पास डीके शिवकुमार के जैसा कद्दावर नेता तो है ही. डीके वोक्कलिगा समाज से आते हैं. मौजूदा समय में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष है और सरकार बनने पर मुख्यमंत्री की रेस में भी शामिल हैं.
कर्नाटक की अन्य जातियांदलितलिंगायत और वोक्कलिगा समाज की तरह दलितों की भी कर्नाटक की राजनीति में बड़ी अहमियत है. वजह है कर्नाटक की सबड़े बड़ी आबादी. राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या दलित समुदाय की है. हालांकि बावजूद इसके ज्यादा रसूख लिंगायत और वोक्कलिगा समाज का है. राज्य में दलितों की आबादी की करीब 19.5 फीसदी बताई जाती है.
कर्नाटक में अनुसूचित जाति के लिए 36 सीटें आरक्षित हैं. हालांकि दलित जातियों का प्रभाव इससे कहीं ज्यादा सीटों पर है. कांग्रेस के पास मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा दलित नेता होने के बावजूद राज्य में बीजेपी दलितों के बीच ज्यादा मजबूत रही है. पिछले चुनाव में 36 में से 17 आरक्षित सीटें बीजेपी के खाते में गईं. जबकि कांग्रेस के 12 विधायक आरक्षित सीट से चुनकर आए. दलित समाज में जेडीएस का कोई खास दबदबा नहीं दिखता. पिछले चुनाव में जेडीएस ने 6 आरक्षित सीटें जीतीं जबकि बसपा के खाते में एक सीट गई. मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं. एक दलित नेता कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना है. इस बात को पार्टी कर्नाटक चुनाव में कितना भुना पाती है, ये देखना होगा.
अनुसूचित जनजाति
कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति के लिए 15 सीटें रिज़र्व की गई हैं. इनकी आबादी करीब 7 फीसदी है. ये मुख्यत: मध्य कर्नाटक और उत्तर कर्नाटक में बसे हुए हैं. पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सात-सात सीटें मिलीं थीं. और जेडीएस के हिस्से में एक सीट आई थी.
मुस्लिम
कर्नाटक में मुस्लिम आबादी भी करीब 13 फीसदी है. लेकिन राज्य की करीब 40 सीटों पर मुस्लिम समाज सीधा प्रभाव रखता है. गुलबर्गा, मेंगलुरु, भटकल, उडुपी मुरुदेश्वर बिदर, बीजापुर, रायचुर और धारवाड़ जैसे इलाकों में मुस्लिम चुनाव का रुख पलटने की हैसियत रखते हैं. दक्षिण कन्नड़, धारवाड़, गुलबर्गा में 20 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं. साथ ही गांवों के मुकाबले मुस्लिमों की ज्यादा आबादी शहरों में रहती है. आबादी और प्रभाव के मुकाबले मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम ही है. पिछले चुनाव में पूरे राज्य में सिर्फ 7 मुस्लिम विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे. और सातों कांग्रेस के हैं.
ब्राह्मण
राज्य में ब्राह्मण हैं तो सिर्फ दो फीसदी, लेकिन राजनीतिक रसूख अच्छा खासा है. राज्य में इनके प्रभाव का समझने के लिए पिछले चुनाव का नतीजा देखा जा सकता है. सिर्फ 2 फीसदी आबादी होने के बाद भी 14 ब्राह्मण विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे. परंपरागत तौर पर ये बीजेपी के वोटर हैं. 14 में 10 विधायक बीजेपी के थे जबकि 4 कांग्रेस से चुनकर आए थे.
ओबीसी
कर्नाटक में ओबीसी 16 फीसदी हैं और उनका प्रभाव 24 सीटों पर है. पिछली बार 22 विधायक ओबीसी कैटेगरी के चुने गए. इनमें 13 बीजेपी, 8 कांग्रेस और 1 विधायक जेडीएस से था.
कुरुबा
कुरुबा समाज की आबादी 7 फीसदी है. लेकिन इनका प्रभाव 20 से ज्यादा सीटों पर माना जाता है. राजनीतिक रूप से इनका प्रभाव तब और ज्यादा बढ़ा जब सिद्दारमैया सत्ता के केंद्र में आए. सिद्दा कुरुबा समाज से आते हैं. उनकी वजह से फिलहाल कुरुबा समाज कांग्रेस के पीछे लामबंद है. पिछले चुनाव में 12 विधायक कुरुबा समाज से चुने गए. इनमें 9 कांग्रेस के थे, 2 जेडीएस और एक विधायक बीजेपी से चुना गया.
स्थानीय भाषा के मुताबिक कुरुबा का मतलब चरवाहों से होता है. इस समाज कर्नाटक के अलग-अलग जगहों पर फैला हुआ है. लेकिन दक्षिण कर्नाटक में इनकी आबादी खासा प्रभाव रखती है.
यानी कर्नाटक की राजनीति में जातियों का जाल ही राजनीतिक दलों को सत्ता तक पहुंचाता आया है. जो इस जाल से बचकर निकल गया, सत्ता उसकी. और जो फंस गया, उसके हिस्से आता है पांच साल का इंतजार. इस बार क्या कुछ घटने वाला है कर्नाटक की सियासत में, सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए दी लल्लनटॉप.
वीडियो: कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर बड़ा दावा कर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से क्या पूछा?