डॉनाल्ड लू. अमेरिका की सरकार में दक्षिण और मध्य एशिया के सहायक सचिव हैं. दस दिन पहले, उनका एक बयान ख़बरों में था. 22 अप्रैल को उन्होंने भारत की प्रेस की तारीफ़ की थी. कहा था कि भारत एक लोकतंत्र है क्योंकि भारत के पास एक स्वतंत्र प्रेस है, जो असल में काम करती है. आज एक और बयान आया है. पत्रकारों के ख़िलाफ़ हिंसा, पक्षपाती मीडिया और मीडिया संस्थानों का स्वामित्व मुठ्ठी भर लोगों के हाथ में जाना यही दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी संकट में है. किसने कहा? एक अंतर्रराष्ट्रीय NGO ने, जिसका मक़सद है समाचार और सूचना की आज़ादी के अधिकार को बढ़ावा देना.
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 11 पायदान नीचे फिसला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहां पर हैं?
2002 से हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरी है.

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 आ गया है. इसमें भारत की रैंकिंग है, 161. कितने में. 180 देशों में. पिछले साल भारत 150वें स्थान पर था. उससे पिछले साल, यानी 2021 में 142वें स्थान पर. थोड़ा और पीछे जाएं, तो 2012 में 131वां स्थान था और 2002 में, जिस साल इस इंडेक्स का उद्घाटन हुआ था भारत 80वें स्थान पर था. यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक़ तो भारत में प्रेस की आज़ादी में लगातार गिरावट हो रही है.
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था तैयार करती है. शॉर्ट फॉर्म में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को RSF कहते हैं. हमने बताया ही कि ये एक अंतरराष्ट्रीय NGO है, जिसका मक़सद मीडिया की आजादी को बढ़ावा देना है. इसे यूनाइटेड नेशन्स और यूनेस्को ने कंसल्टेटिव स्टेटस दे रखा है. इस संस्था का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है. RSF दुनिया भर के 180 देशों में मीडिया को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर का मूल्यांकन करती है और फिर इसके आधार पर रैंकिंग तैयार करती है. इसी तरह इन 180 देशों में पत्रकारों और मीडिया को मिलने वाली स्वतंत्रता के स्तर की तुलना हो जाती है. RSF के मुताबिक़ -
> प्रेस की आज़ादी का मतलब किसी राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और सामाजिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहते हुए और बिना किसी शारीरिक या मानसिक खतरे के पत्रकारों का इंडिविजुअल या सामूहिक रूप से सार्वजनिक हित में खबरों को सेलेक्ट करना, प्रोड्यूस करना और प्रसार करना.
ये रिपोर्ट किन आधारों पर तैयार होती है, हम इस पर आएं. इससे पहले ये बता देते हैं कि इस संगठन ने भारत की प्रेस की स्थिति पर क्या टिप्पणियां की हैं. RSF ने कहा है कि,
''पत्रकारों के ख़िलाफ़ हिंसा, राजनीतिक रूप से पक्षपाती मीडिया, कुछ लोगों के हाथ में मीडिया का स्वामित्व ये दिखाता है कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रवादी हिंदू विचारधारा से जुड़े नरेंद्र मोदी शासित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी ख़तरे में है.''
इसके अलावा RSF ने अपने रिपोर्ट में कैटेगरी वाइज़ भी कमेंट किए हैं. वो भी समझ लेते हैं.
पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में RSF ने लिखा है कि भारतीय मीडिया को मूल रूप से एंटी-कोलोनियल मूवमेंट का प्रोग्रेसिव प्रोडक्ट समझा जाता रहा है. लेकिन पिछले दशक में चीजें बदली, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने. RSF ने मुकेश अंबानी को पीएम मोदी का दोस्त बताते हुए कहा है कि उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज मीडिया इंडस्ट्री पर हावी है. इसी तरह PM के एक और दोस्त अडानी के NDTV अधिग्रहण को मीडिया इंड्स्ट्री में बहुलतावाद के अंत का संकेत बताया गया है. RSF ने कहा है कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को मोदी समर्थक(जिन्हें भक्त बताया गया है) द्वारा चौतरफा निशाना बनाया जाता है.
>दूसरी कैटेगरी है लीगल फ्रेमवर्क.
RSF ने कहा है कि थियरी में तो भारतीय कानून प्रोटेक्टिव है लेकिन मानहानि, राजद्रोह, अदालत की अवमानना और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप सरकार की ओर से अकसर भारतीय पत्रकारों पर लगाए जाते हैं और इन्हें राष्ट्र विरोधी कहा जाता है. सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों को कवर करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों को अक्सर गिरफ्तार किया जाता है और कभी-कभी मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है.
> आर्थिक संदर्भ में RSF का कहना है कि बड़े पैमाने पर भारतीय मीडिया स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों के विज्ञापनों पर निर्भर है. अकसर बिजनेस और एडिटोरियल पॉलिसी के बीच एक निश्चित सीमा का अभाव होता है, और व्यावसायिक जरूरतों के हिसाब से खबरें एडजस्ट की जाती हैं. जिसका फायदा उठाकर सरकारें अपना नैरेटिव थोप सकती हैं.
> सोशियो-इकॉनमिक संदर्भ में RSF के मुताबिक भारतीय समाज की विशाल डायवर्सिटी मेनस्ट्रीम मीडिया में बड़ी मुश्किल से दिखाई देती है. अधिकतर पदों पर कथित ऊंची जाति के हिंदू पुरुष पत्रकारिता में हैं. जब कोविड-19 संकट चरम पर था तो कुछ टीवी एंकर्स ने इसके लिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोषी बताया. लेकिन यही मीडिया वैकल्पिक उदाहरणों से स्मृद्ध भी है. जैसे- खबर लहरिया, जिसे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यक महिला पत्रकार चलाती हैं.
> सुरक्षा के लिहाज़ से RSF ने भारत को मीडिया के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है. RSF का कहना है कि हर साल औसतन तीन या चार पत्रकारों को उनके काम की वजह से मार दिया जाता है. पत्रकारों को सभी प्रकार की शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिसमें पुलिस हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा की जाने वाली हिंसा, आपराधिक समूहों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों के द्वारा भी. सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी पत्रकारों खासतौर पर महिला पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है. RSF ने कश्मीर में भी स्थिति को चिंताजनक बताया है. और कहा है कि सुरक्षा बलों की ओर से अक्सर पत्रकारों को परेशान किया जाता है.
ये तो हुई टिप्पणियां. और, आपने सुनी ही कि ये सरकार के लिए तल्ख़ हैं. बुलेटिन के लिखे जाने तक तो सराकार की कोई टिप्पणी नहीं आई, लेकिन इससे पहले सरकार ने इस रिपोर्ट को ख़ारिज किया था. सरकार ने साफ़ कहा था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग की और निष्कर्षों से वो सहमत नहीं है.
इससे पहले कि इस रिपोर्ट को भी ख़ारिज कर दिया जाए, ये जान लेते हैं कि ये कैसे तय होता है कि किस देश की प्रेस कितनी आज़ाद है.
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तैयार करने के लिए RSF ने पांच कैटेगरी बनाई है.
1. पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट
2. लीगल फ्रेमवर्क
3. इकॉनमिक कॉन्टेक्स्ट
4. सोशियो-कल्चरल कॉन्टेक्स्ट
5. सेफ्टी
इन्हीं पांच चीजों पर एक क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली तैयार की जाती है. इसके साथ-साथ इसमें दो चीजें और होती हैं.
> पहला, मीडिया और पत्रकारों से उनके काम काम की वजह से होने वाला दुर्व्यवहार.
> और दूसरा, RSF क्वेश्चनेयर पर प्रेस फ्रीडम से जुड़े विशेषज्ञों - पत्रकार, रिसर्चर, एकेडमीशियन, और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर उस क्षेत्र या देश में स्थिति का विश्लेषण.
आप पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चनेयर में किस तरह के सवाल होते हैं? हम बताते हैं.
> एडिटोरियल बोर्ड में सरकार का कितना एन्फु्लुएंस होता है ?
> लाइसेंस प्रोसेस कितनी ट्रांसपैरेंट है?
> सरकार के लिए किसी पत्रकार का डिसमिसल कितना आसान है?
> क्या सभी तरह के पॉलिटिकल व्यूज को मीडिया में जगह मिलती है?
> क्या ओनर्स या पॉलिटिकल अथॉरिटीज के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से एडिटोरियल बोर्ड सार्वजनिक रूप से अपना ओपिनियन दे सकता है?
> क्या कोर्ट या अथॉरिटीज के ऑर्डर पर डिजिटल मीडिया को जर्नलिस्टिक कंटेंट सेंसर करना पड़ता है, जो एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय मानकों के उलट है?
ये सवाल कुछ नमूने हैं. इसी तरह के 117 सवाल पांचों कैटेगरी में पूछे जाते हैं. आप समझ ही पा रहे होंगे, कि इन सवालों का जवाब सब्जेक्टिव होगा. यानी व्यक्तिपरक. अलग-अलग लोगों के अलग-अलग अनुभव होंगे और धारणाएं होंगी. तो इसकी क्वॉलिटेटिव एनालिसिस की जाती है. इसके अलावा क्वॉन्टिटेटिव ऐनालिसिस भी की जाती है -- पत्रकारों के ख़िलाफ़ उनके काम के संबंध में और मीडिया आउटलेट्स के ख़िलाफ़ हिंसाओं के आंकड़ों की. इन्हीं दोनों समीक्षाओं के आधार पर 0 से 100 के बीच हर देश को स्कोर दिया जाता है और इसी आधार पर रैंकिंग तय की जाती है.
मीडिया वन चैनल के लाइसेंस रीन्यूवल की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,
"एक मज़बूत लोकतांत्रिक गणराज्य के कामकाज के लिए एक आज़ाद प्रेस चाहिए. लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की भूमिका अहम है. राज्य काम कैसा कर रहा है, प्रेस इसपर रोशनी डालती है. प्रेस का कर्तव्य है कि वो सच बोले और नागरिकों के सामने तथ्य रखे. ताकि लोकतंत्र सही दिशा में चले. प्रेस की आज़ादी पर अगर प्रतिबंध लग जाए, तो नागरिक एक ही तरह से सोचने लगेंगे. और अगर समाज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर एक ही तरह की विचारधारा रखने लगे, तो इससे प्रजातंत्र को गंभीर ख़तरे पैदा होंगे."
पूर्व राजनयिक और राज्य सभा सांसद पवन कुमार वर्मा ने इस पूरे मसले पर एक कॉलम लिखा है. क्या लिखा है? लिखा -
"मीडिया प्लेटफॉर्म्स को धमकाना, उन पर दबाव बनाना, उन्हें दंडित करना, विज्ञापन न देना लोकतंत्र की सीमारेखा को लांघने वाली गतिविधि कहलाएगी. तो क्या सरकार ने यह सीमारेखा लांघी है? हां और ना, दोनों. यह तो कोई भी नहीं कह सकता कि भारत में स्वतंत्र मीडिया नहीं है. लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि उस पर अंकुश लगाने की कोशिशें नहीं हुई हैं. हाल के समय में कुछ परेशान कर देने वाले ट्रेंड्स उभरे हैं, जिनकी अनेदखी नहीं की जा सकती. पहला तो यही, कि सरकार की किसी भी तरह की आलोचना को तुरंत राष्ट्रविरोधी या राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध क़रार दिया जाता है."
हालांकि, जब भी इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं. अक्सर इनके बरक्स एक तर्क दिया जाता है कि इनकी मेथेडोलॉजी या तरीका ठीक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान जैसे देश इंडेक्स में हमसे ऊपर होते हैं हालांकि हम इन देशों की स्थिति देख ही रहे हैं.













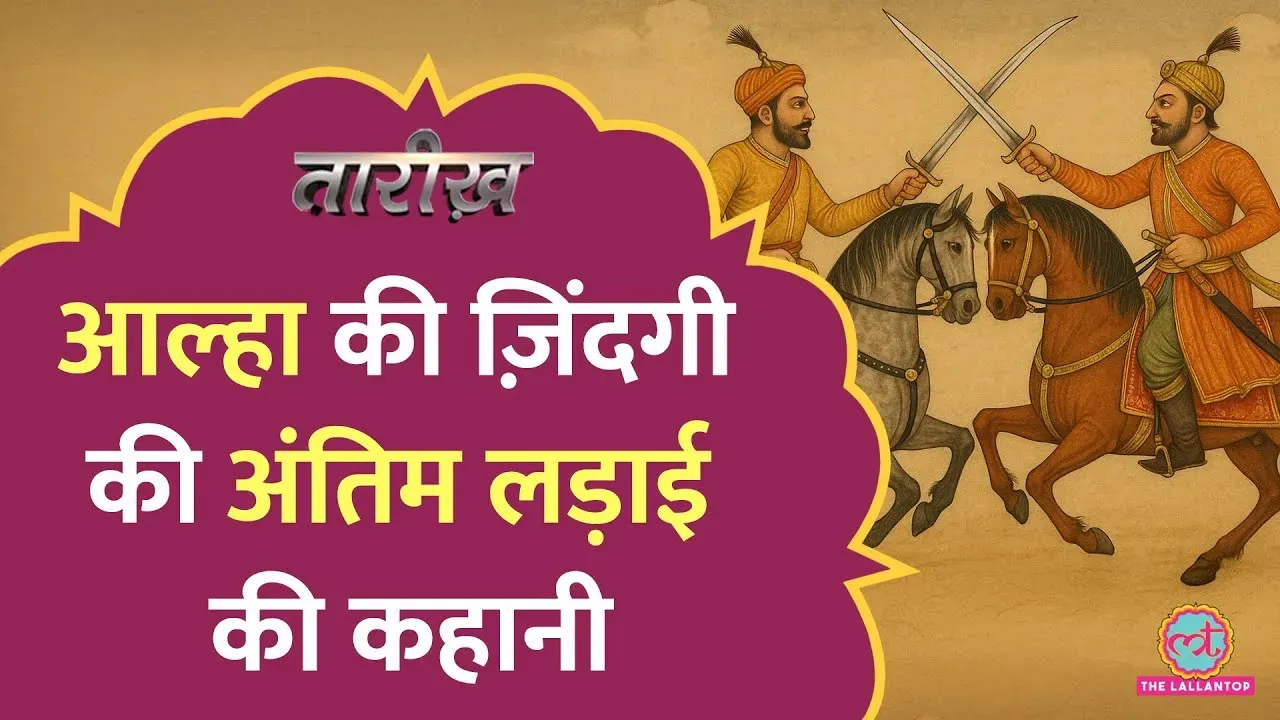
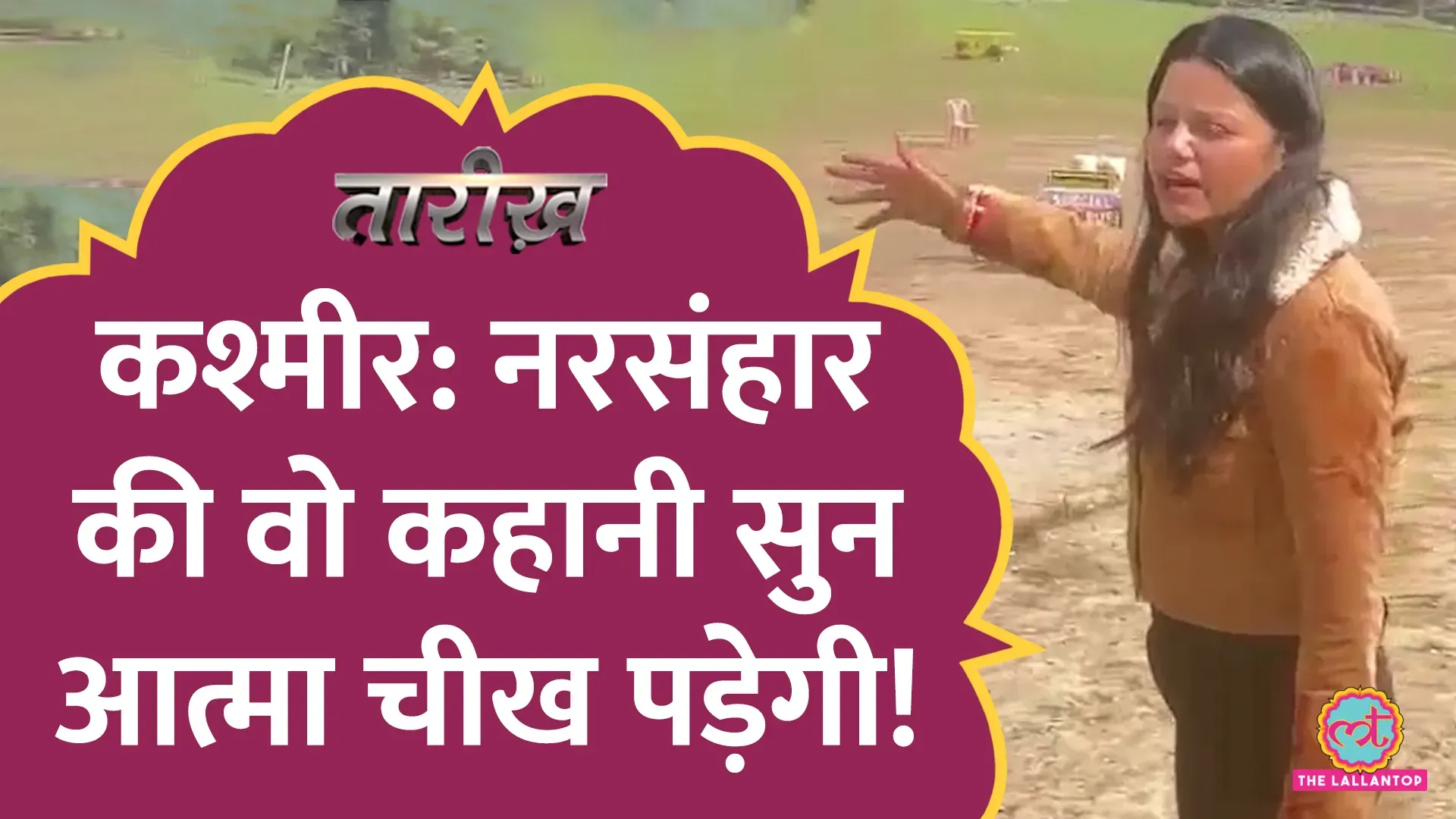
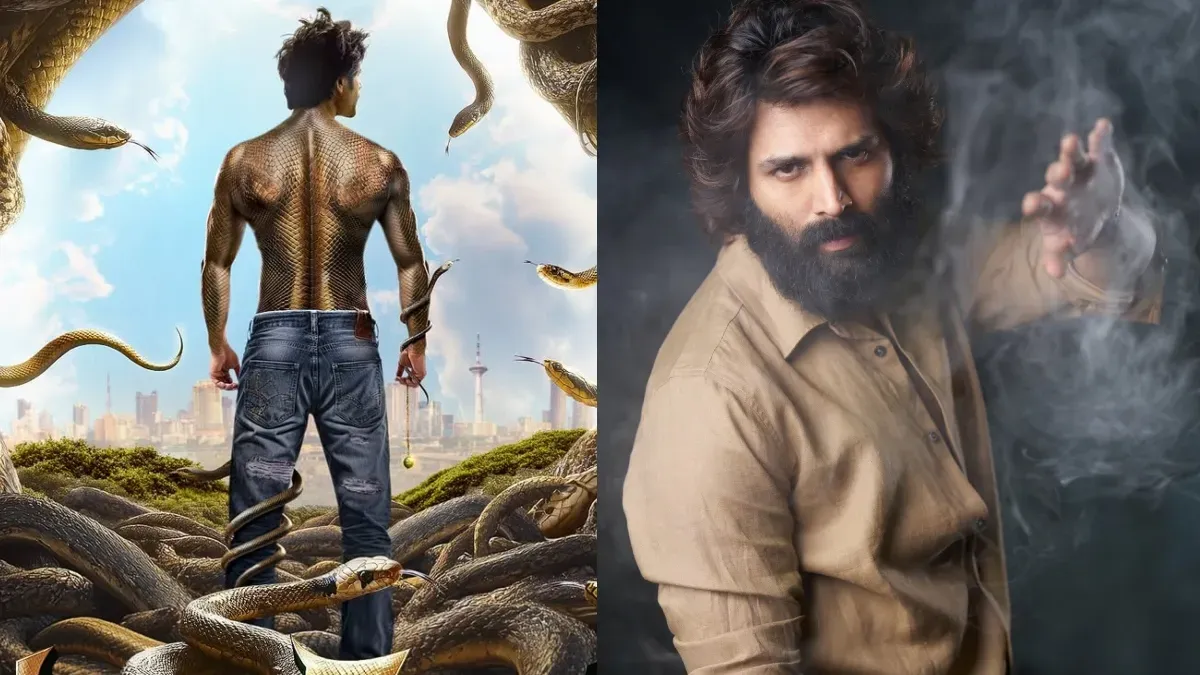


.webp)
