तीनों बीकानेर की बेकलू (रेत) में जन्मे. तीनों के कंठों में मीठे संगीत का शीतल झरना बहता था. ऐसे कंठ इन्हें कैसे मिले, तीनों की कहानियां विरली हैं. इन्हें सुनना और सोचना बड़ी वैज्ञानिक और दार्शनिक तृप्तियों को पाने जैसा है. पश्चिम में आज आप लिल वेन, जस्टिन बीबर जैसे पॉप आर्टिस्टों के फैन हैं, तो इन तीनों का अतीत में इन सिंगर्स से भी ज्यादा क्रेज़ होता था. दुनियाभर में लोग, सेलेब्रिटी, राजनेता, कारोबारी, राजे-रजवाड़े, फिल्म स्टार और कई तरह के पावरफुल लोग इन्हे सुनने के लिए हाथ-पैर मारते थे. अपने घरों में इनकी महफिल काबिल करवा पाना, इन सुपर लोगों के जीवन के बड़े मौकों में से होता था.अल्लाह जिलाई बाई, मेहदी हसन और रेशमा - इन तीनों में कॉमन क्या है?
बाईजी
और मेहदी हसन
के बारे में हम पहले यहां पढ़ चुके हैं. आज बात रेशमा की. आज ही के दिन 3 नवंबर, 2013 को लाहौर, पाकिस्तान में उनका इंतकाल हो गया था. आज उनकी याद हो आई है.

बलवंत गार्गी
पंजाबी भाषा के नाटककार, रंगकर्मी और शिक्षाविद् बलवंत गार्गी ने कोई तीन दशक पहले रेशमा से मुलाकात की थी जब वे भारत आई थीं. इस पर एक बहुत ही दुर्लभ लेख उन्होंने लिखा था. जो उनकी किताब 'हसीन चेहरे' में छपा था जो संभवत: गार्गी की मृत्यु के बाद 2006 में छपी. इसमें कई अन्य क्षेत्रों की हस्तियों के बारे में भी आलेख थे.
गार्गी की पंजाबी किताब में से 'रेशमा' शीर्षक के लेख को हिंदी में नीलम शर्मा 'अंशु' ने ट्रांसलेट किया. इसे 2013 में उन्होंने अपने ब्लॉग संस्कृति सेतु पर
लगाया. उनके आभार के साथ हम इसे यहां उपलब्ध करवा रहे हैं.
अब भी इसे पढ़ते हुए आप एक ऐसी रेशमा से मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिलेगी. कह सकते हैं कि ये संस्मरण आपको पूरी उम्र याद रहेगा.
*** **** ***










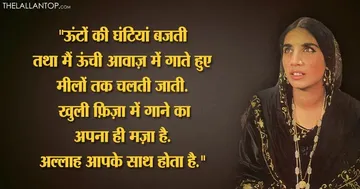



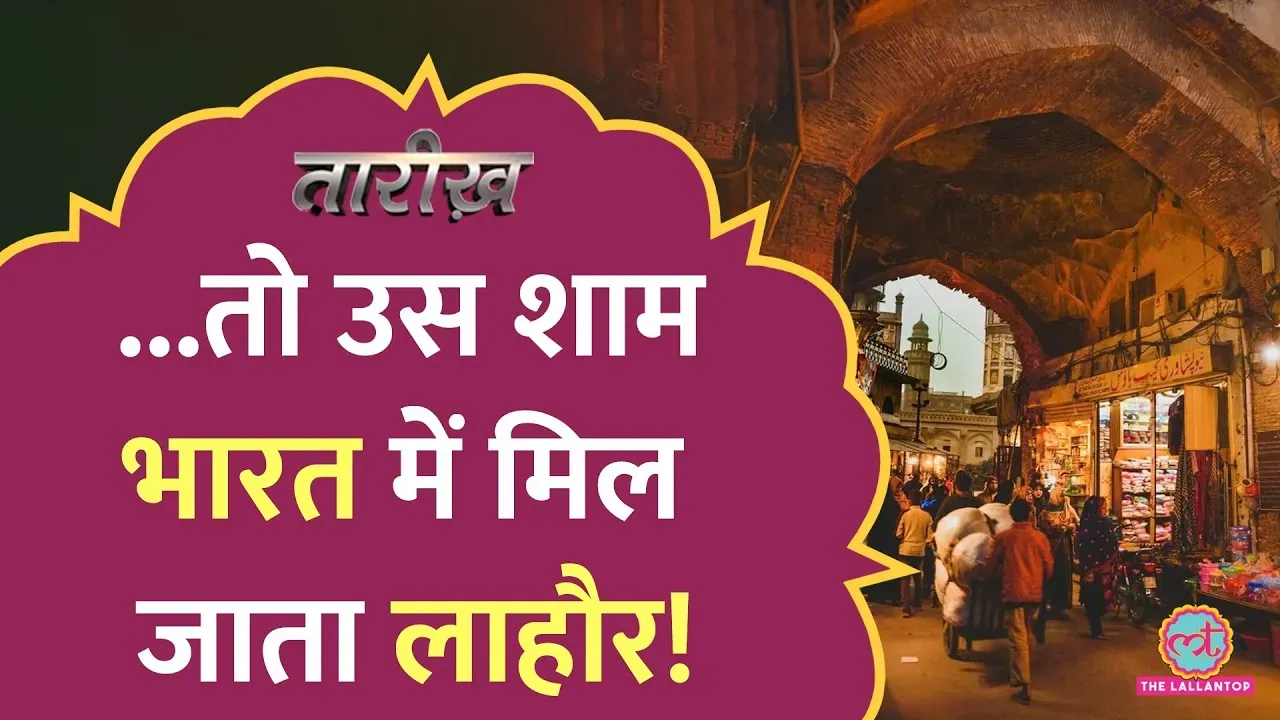

.webp)


