
जॉली एलएलबी के जज सुंदर लाल त्रिपाठी तो याद हैं न? सिविल केस बनाम क्रिमिनल केस जज और मजिस्ट्रेट में अंतर जानेंगे. उससे पहले बता दें कि दो तरह के मामले होते हैं. सिविल मामले और क्रिमिनल मामले. सिविल मामले यानि दीवानी मामले ऐसे मामले होते हैं जिसमें अधिकार और क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है. ये अधिकार जमीन-जायदाद का हो सकता है. पद संबंधी हो सकता है, या फिर धार्मिक या इसी तरह का कोई और भी हो सकता है.
उदाहरण के रूप में देखें, जैसे किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है. आप कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि आपकी जमीन से कब्जा हटाया जाए. जितने टाइम तक आपकी जमीन पर उस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा था, उसका मुआवजा दिलाया जाए. इसमें आपने अधिकार की मांग की. आपकी जमीन पर आपका कब्जा हो. दूसरा मुआवजे भी मिले. ये हो गया सिविल मामला.
इनके अलावा कॉपीराइट के मामले, पेटेंट वाले मामले, ट्रेडमार्क के मामले भी सिविल केसों के कुछ उदाहरण हैं. एक और जरूरी बात ये कि सिविल मामले में आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं.
 प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटोदूसरे होते हैं क्रिमिनल मामले. हिन्दी में इन्हें दांडिक मामले या फौजदारी मामले भी कह सकते हैं. ये ऐसे मामले होते हैं जिनमें दंड की मांग की जाती है. ऊपर वाले उदाहरण से ही समझते हैं.
यहां आप सिर्फ अपनी जमीन पर फिर से कब्जे और मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं. आप मांग करते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपकी जमीन पर कब्जा किया है, उसे सजा मिले, दंड मिले. उसे जेल में डाला जाए. इसकी सुनवाई क्रिमिनल केस के तहत होगी. लेकिन जरूरी बात ये है कि क्रिमिनल मामले में आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते. पहले FIR दर्ज करानी होती है. उसके बाद ही मामले की सुनवाई होती है.
कुछ मामले दोनों प्रकृति के होते हैं. ये पीड़ित की मांग पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के मामले के तहत याचिका दायर करता है. मजिस्ट्रेट और जज में क्या अंतर है? मजिस्ट्रेट और जज में पदक्रम (Hierarchy) का अंतर होता है. मजिस्ट्रेट फांसी या उम्रकैद की सजा नहीं देते. मजिस्ट्रेट के लेवल में भी कई स्तर होते हैं. इनमें जो सबसे ऊपर का पद होता है, वो होता है सीजेएम यानी चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट. महानगरों में इसे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं. एक जिले में एक सीजेएम होता है. लेकिन सीजेएम के बराबर के रैंक के अधिकारियों को कहते हैं सब-जज (Subordinate judge). इनका पद सब-जज होता है, लेकिन ये मजिस्ट्रेट ही होते हैं. सब-जज सिविल मामले देखते हैं. जबकि सीजेएम क्रिमिनल मामले देखते हैं. सब-जज छुट्टी के दौरान CJM का काम संभाल सकता है.
मजिस्ट्रेट की लोअर यूनिट होती है मुंसिफ मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट. हाईकोर्ट अथॉरिटी के पास ये अधिकार होता है कि वह किसको मुंसिफ मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट का चार्ज दे. सिविल केस देखते हैं. मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मामले देखते हैं. मुंसिफ की अपर यूनिट सब-जज होते हैं जबकि मजिस्ट्रेट के ऊपर होते हैं सीजेएम. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुंसिफ ही प्रमोट होकर सब-जज बनेंगे. तीन साल क्रिमिनल, तीन साल सिविल मामले देखने का क्रम चलता रहता है.
 सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीरसीजेएम के ऊपर जज होते हैं. जज की रैंक में आते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और एडीजे यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज. इस लेवल पर जब जज सिविल मामले देखते हैं, तो उन्हें कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज. लेकिन यही जज जब क्रिमिनल मामले देखते हैं तो उन्हें कहते हैं सेशन जज. जज एक ही होता है, जो दोनों तरह के मामलों की सुनवाई करता है. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद किसी भी जिले के मजिस्ट्रेट के पद का सर्वोच्च पद होता है. जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियंत्रित करता है. कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु दंड नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं दे सकता और ऐसा दंड नहीं दे सकता जो 7 साल से ज्यादा की कारावास की अवधि का है.
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी: मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किसी भी मामले को प्रारंभिक रूप से सुनता है. कोई भी मामला प्रारंभिक रूप से प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास ही जाता है. यह कोर्ट भारतीय न्यायपालिका का अत्यंत अहम अंग है. यदि इनकी कोर्ट में किसी आरोपी पर दोष सिद्ध होता है तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आरोपी को उस अपराध के अंतर्गत अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है. 10 हजार तक का जुर्माना लगा सकता है या दोनों को एक साथ भी दे सकता है. कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 3 वर्ष से अधिक का कारावास और 10 हजार से ज्यादा का जुर्माना नहीं लगा सकता.
मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी: मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी पद से न्यायपालिका के पदों का क्रम शुरू होता है. इसे न्यायपालिका का प्रारंभिक चरण भी कहा जा सकता है. कोई भी सिविल से जुड़ा मामला सबसे पहले इसी न्यायालय में आता है. आपराधिक मामलों में द्वित्तीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायायल एक साल से अधिक अवधि के कारावास और ₹5000 तक का जुर्माना या इन दोनों को एक साथ किसी भी सिद्ध दोषी को दे सकता है.
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट: भारत के महानगरों के लिए महानगर मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) जैसे पद रखे गए हैं. इन पदों में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (Chief Metropolitan Magistrate) और महानगर मजिस्ट्रेट को रखा गया है. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को वही सब शक्तियां प्राप्त होती है जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है. महानगर मजिस्ट्रेट को वही सब शक्तियां प्राप्त होती हैं जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती हैं.
कार्यपालक मजिस्ट्रेट: राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में जितने वह उचित समझे उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है. जजों की कैटेगरी सत्र न्यायाधीश (Session Judge): सीआरपी की धारा 9 में सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) की स्थापना की बात की गई है. राज्य सरकार सत्र न्यायालय की स्थापना करती है जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है. उच्च न्यायालय अतिरिक्त और साथ ही सहायक सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है. सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकते हैं. लेकिन मौत की सजा दी जाती है तो इस सजा की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि अनिवार्य है.
अतिरिक्त / सहायक सत्र न्यायाधीश ( additional Session judge): ये किसी विशेष राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं. वे सेशन जज की अनुपस्थिति के मामले में हत्या, चोरी, डकैती, पिक-पॉकेटिंग और ऐसे अन्य मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकते हैं. एक सहायक सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक के कारावास की सजा को छोड़कर अन्य सजा को पारित कर सकता है.
हाईकोर्ट के जज: जिला न्यायलयों से ऊपर होता है हाईकोर्ट. हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट की अनुशंसा पर सुप्रीम कोर्ट करता है. इस पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भी भूमिका होती है.
सुप्रीम कोर्ट के जज: भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अधिनियम संख्या 124 के दूसरे सेक्शन के तहत होती है. यह पद भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा न्यायिक पद है. संविधान में 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है. सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है. कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर.
कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है. कॉलेजियम वकीलों या जजों के नाम की सिफारिस केंद्र सरकार को भेजती है. कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार भेजने पर सरकार के लिए मानना जरूरी होता है.














.webp)
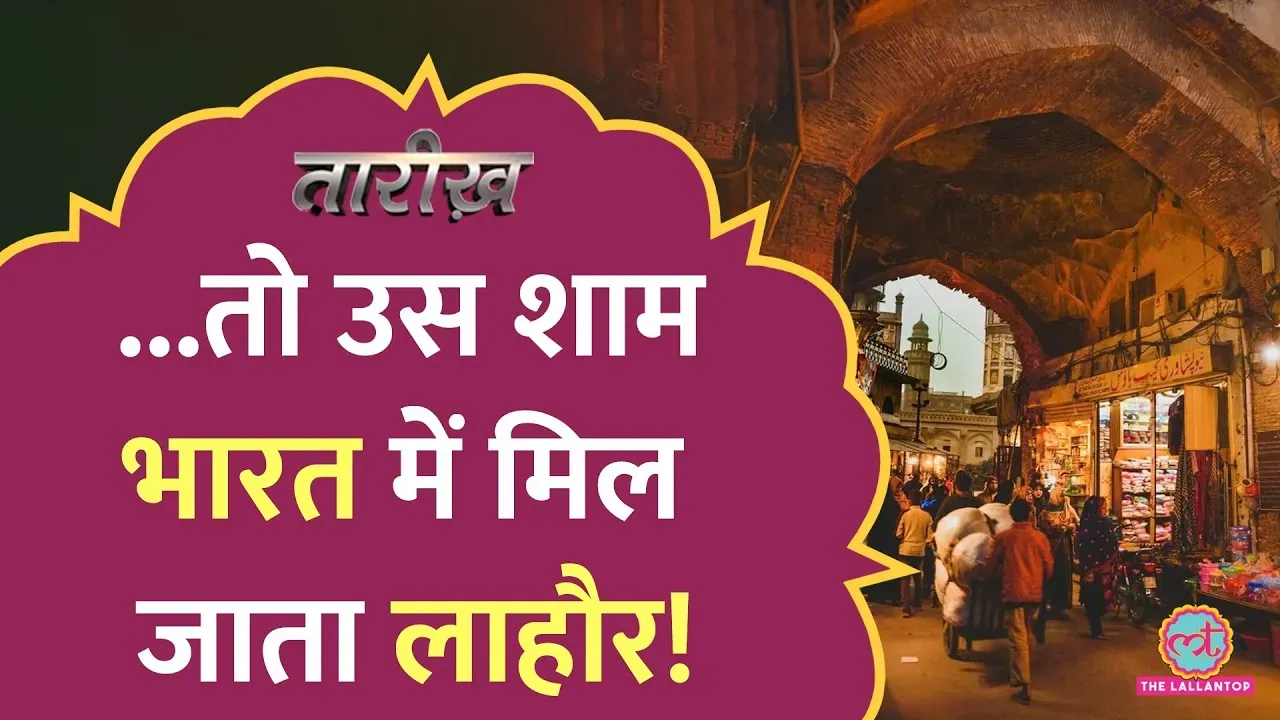
.webp)


