कुछ साल पहले विद्या बालन की एक फिल्म आई थी. 'बेग़म जान'. पार्टीशन के वक़्त एक तवायफ की अपना कोठा बचाने की जद्दोजहद की दास्तान थी ये फिल्म. फिल्म तो ख़ैर फ्लॉप हो गई थी लेकिन हम आपको भारत की उन चुनिंदा तवायफों से परिचित कराना चाहते हैं, जिनका नाम इतिहास बड़े ही आदर के साथ लेता है.चौंक गए न! तवायफ और आदर इन शब्दों को एक साथ पढ़ने की आदत नहीं है न? ये सामान्यीकरण बॉलीवुड की देन है. तवायफों को वेश्या के रूप में चित्रित कर-करके हिंदी सिनेमा ने उनको एक खांचे में महदूद करके रख दिया है. जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है. आज तवायफ लफ्ज़ के साथ जो इमेज चस्पां है, उसे देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कभी तवायफों को बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता था. शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में उनको महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्ज़त मिलती थी. तहज़ीब की तो उन्हें पाठशाला समझा जाता था और बड़े-बड़े नवाबों, सरदारों के साहबज़ादों को तहज़ीब के गुर सीखने के लिए उनके पास भेजा जाता था. यह उस ज़माने की बातें हैं, जब औरतों का पढ़ना-लिखना तो दूर घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ होता था. उस दौर में तवायफों की ज़िंदगी खुदमुख्तारी की मिसाल हुआ करती थी. उनके पास सारे सामाजिक अधिकार हुआ करते थे. यहां तक कि वे चाहें तो शादी करके घर भी बसा सकती थीं. आर्थिक रूप से भी वो काफी समृद्ध हुआ करती थीं. ऐतिहासिक दस्तावेज़ बताते हैं कि उन्नीसवीं सदी के अंत में लखनऊ की तवायफें राजकीय ख़ज़ाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थीं. इस पेशे को गरिमा और संगीत को एक समृद्ध विरासत सौंपने वाली कुछ चुनिंदा तवायफों पर नज़र डालते हैं.
1. गौहर जान 2 नवंबर 1902. ये वो तारीख़ है, जिस दिन भारतीय संगीत को एक नई दशा-दिशा मिली. इस दिन पहला भारतीय गीत रिकॉर्ड हुआ डिस्क पर. राग जोगिया में ‘ख़याल’ गाया गया. गाने वाली थीं बनारस और कलकत्ते की मशहूर तवायफ गौहर जान. इस एक घटना ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया. रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री के भारत में प्रवेश से गौहर जान बहुत जल्द घर-घर सुनी जाने लगीं.
आर्मेनियाई दंपति की संतान गौहर जान का असली नाम एंजलिना योवर्ड था. उनके पिता का नाम विलियम योवर्ड और मां का नाम विक्टोरिया था. दुर्भाग्य से उनके माता-पिता की शादी चल नहीं पाई और 1879 में, जब एंजलिना सिर्फ 6 साल की थीं, उनका तलाक़ हो गया. इसके बाद विक्टोरिया ने कलकत्ता में रहने वाले मलक जान नाम के शख्स से शादी कर ली. उसी ने एंजलिना को नया नाम दिया. गौहर जान.गौहर की मां खुद भी बहुत उम्दा नृत्यांगना थीं. जल्द ही गौहर ने भी ये हुनर सीख लिया. उन्होंने रामपुर के उस्ताद वज़ीर ख़ान और कलकत्ता के प्यारे साहिब से गायन की तालीम हासिल की. जल्द ही वो ध्रुपद, ख़याल, ठुमरी और बंगाली कीर्तन में पारंगत हो गईं. उनकी शोहरत फैलने लगी.

उनके सन्दर्भ में एक ऐतिहासिक तथ्य काबिलेगौर है कि उस्ताद मौजुद्दीन खां ने स्वयं बनारस से कलकत्ता जाकर गौहर को ठुमरी सिखाई थी. गौहर जान 19वीं शताब्दी के शुरुआत की सबसे महंगी गायिका थीं, जो महफिलें सजाती थीं. उनके बारे में मशहूर था कि सोने की एक सौ एक गिन्नी लेने के बाद ही वह किसी महफिल में गाने के लिए हामी भरती थीं. प्रतिभा के साथ ही गौहर में एक दुर्लभ व्यावहारिकता भी थी. इसी की वजह से गायन व रिकॉर्डिंग उद्योग के शुरुआती दिनों में वह एक बेहद धनवान महिला बनीं. वो अंग्रेज़ अफसरों से भी ठसक से मिलती-जुलती थीं और उनके पहनावे और ज़ेवरात तत्कालीन रानियों को मात देते थे. उन्होंने अपनी कमाई का निवेश ज़ायदाद खरीदने में किया, जिसके पीछे कहीं न कहीं बचपन के बेसहारा दिनों में भोगी गरीबी की यादें रही होंगी. गौहर की काफी सारी कोठियां कलकत्ता में थीं.गौहर जान की आवाज़ में एक ठुमरी: https://www.youtube.com/watch?v=SWuuHdf0ssg दबंग होते हुए भी स्त्री-सुलभ नर्मदिली उनके दिल में बनी रही और अपनी जवानी में अपने नाकारा भाइयों और परिजनों पर वो ख़ूब पैसा लुटाती रहीं. अधेड़ उम्र में अपनी उम्र से आधे एक पठान से शादी तो कर ली, लेकिन वो चली नहीं. बात कोर्ट-कचहरी तक पहुंची और गौहर की जायदाद वकीलों की भेंट चढ़ गई. कहते हैं कि अपने आख़िरी दिनों में ये महान गायिका बेहद तनहा और चिड़चिड़ी हो गई थीं. उन्हें दक्षिण भारत में हिजरत करनी पड़ी, जहां गुमनामी की हालत में उनकी मौत हुई.
2. बेग़म हज़रत महल इन्हें 'अवध की बेग़म' भी कहा जाता था. इनका असली नाम मुहम्मदी ख़ानम था. फैज़ाबाद में पैदाइश हुई. पेशे से तवायफ़ हज़रत महल को खवासिन के तौर पर शाही हरम में शामिल किया गया. आगे चल के अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने उनसे शादी कर ली. उसी के बाद उन्हें हज़रत महल नाम दिया गया.

1856 में जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्ज़ा कर लिया तो वाजिद अली शाह कलकत्ता भाग गए. नवाब की फरारी के बाद हज़रत महल ने कमान संभाली. 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के नाक में दम करने वालों की लिस्ट में बेग़म का नाम प्रमुखता से था. उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादरा को अवध का राजा घोषित किया. नाना साहेब के साथ मिलकर अंग्रेजों से खूब लोहा लिया.जब विद्रोह नाकाम हुआ, तो उन्हें अवध छोड़ के भागना पड़ा. नेपाल में शरण ली. नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर ने पहले तो उन्हें शरण देने से मना किया लेकिन बाद में मान गए. 1879 में, गुमनामी की हालत में उनकी मौत हो गई. काठमांडू की जामा मस्ज़िद में एक बेनामी कब्र में उन्हें दफनाया गया.
3. जद्दनबाई उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में जद्दनबाई एक ऐसा नाम था, जिसका ज़िक्र संगीत के कदरदानों में बेहद अदब से लिया जाता था. इनका एक परिचय ये भी है कि ये फिल्म एक्ट्रेस नर्गिस की मां और संजय दत्त की नानी थीं. गायिका, म्यूजिक कम्पोज़र, अभिनेत्री और फिल्म मेकर जैसे अलग-अलग मुहाज़ पर इन्होंने खुद को साबित किया. वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला संगीत निर्देशक थीं.
 जद्दनबाई का जन्म 1892 में हुआ. उन्होंने अपनी शुरुआती ट्रेनिंग कलकत्ता के भैया साहब गणपत से ली. अभी वो सीख ही रही थीं कि उनके उस्ताद की मौत हो गई. आगे की ट्रेनिंग उस्ताद मोईनुद्दीन ख़ान के पास हुई. जल्द ही ग़ज़ल गायिकी में उन्होंने अपना एक स्थान बनाना शुरू किया. कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी ने उनके रिकॉर्ड्स मार्केट में उतारकर उन्हें बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर चढ़ा दिया. वो अलग-अलग रेडियो स्टेशन के लिए भी गाया करती थीं. साथ ही रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, कश्मीर, इंदौर, जोधपुर जैसी रियासतें उन्हें अपने यहां महफ़िल सजाने की दावत भी दिया करती थी.
जद्दनबाई का जन्म 1892 में हुआ. उन्होंने अपनी शुरुआती ट्रेनिंग कलकत्ता के भैया साहब गणपत से ली. अभी वो सीख ही रही थीं कि उनके उस्ताद की मौत हो गई. आगे की ट्रेनिंग उस्ताद मोईनुद्दीन ख़ान के पास हुई. जल्द ही ग़ज़ल गायिकी में उन्होंने अपना एक स्थान बनाना शुरू किया. कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी ने उनके रिकॉर्ड्स मार्केट में उतारकर उन्हें बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर चढ़ा दिया. वो अलग-अलग रेडियो स्टेशन के लिए भी गाया करती थीं. साथ ही रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, कश्मीर, इंदौर, जोधपुर जैसी रियासतें उन्हें अपने यहां महफ़िल सजाने की दावत भी दिया करती थी.
जद्दनबाई की अंग्रेजों से भी ठनी रही. अपनी समकालीन गायिकाओं में सबसे ज़्यादा अंग्रेजों के छापे जद्दनबाई के यहां ही पड़े. उन्हें शक था कि वो क्रांतिकारियों को पनाह देती हैं. कहा जाता है कि अंग्रेजों के दबाव की वजह से ही उन्हें दालमंडी की गलियां छोड़नी पड़ी.ग़ालिब की ग़ज़ल जद्दनबाई की आवाज़ में: https://www.youtube.com/watch?v=kiGN2HACtKc जद्दनबाई एक मामले में बड़ी प्रगतिशील साबित हुईं. बदलते समय की नब्ज़ पहचान कर उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अलग, आसान और असरदार करियर चुना. न सिर्फ चुना, बल्कि उसकी दशा-दिशा निर्धारित की. नर्गिस को उन्होंने अपनी गाने-बजाने की दुनिया से अलग रखा और अंग्रेज़ी की तालीम दिलवाई. मंटो, पृथ्वीराज कपूर, महबूब ख़ान जैसे आला दर्जे के लोगों के साथ उसकी सोहबत सुनिश्चित की. नर्गिस के फ़िल्मी करियर को उन्होंने बेहद सावधानी से आगे बढ़ाया. 1935 में प्रदर्शित फिल्म ‘तलाश-ए-हक’ में उन्होंने संगीत भी दिया. इस फिल्म में कोठे पर फिल्माए गए कुछ गीतों में उन्होंने अभिनय भी किया.
4. ज़ोहरा बाई ज़ोहरा बाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत के पिलर्स में से एक माना जाता है. उनके संगीत का प्रभाव उनके बाद के फनकारों पर साफ़ देखा जा सकता है. तवायफों की गौरवशाली विरासत में उनका नाम गौहर जान के साथ बड़े ही आदर से लिया जाता है. अपनी 'मर्दाना' आवाज़ के लिए मशहूर ज़ोहराबाई आगरा घराने से ताल्लुक रखती थीं. उन्हें उस्ताद शेर खान जैसे संगीतज्ञों से तालीम हासिल हुई थी.
 ज़ोहराबाई की ख़ासियत थी कि उनकी एक से ज़्यादा विधाओं पर पकड़ थी. जिस रवानी से वो ‘ख़याल’ में डूबती-उतरती थीं, उतनी ही सहजता से वो ठुमरी या ग़ज़ल भी पेश किया करती थीं. आगरा घराने का एक बेहद बड़ा नाम फैयाज़ ख़ान उन्हीं की गायिकी से प्रभावित थे. बड़े ग़ुलाम अली ख़ान भी ज़ोहराबाई का ज़िक्र बड़े ही भक्तिभाव से किया करते. रिकॉर्ड पर उनकी कोई 78 रचनाएं उपलब्ध हैं. 1994 में उनके 18 मशहूर गानों को ग्रामोफोन से ऑडियो टेप पर ट्रांसफर किया गया. 2003 में उसकी सीडी भी बनाई गई. ज़ोहराबाई की आवाज़ में ‘पिया को ढूंढन जाऊं सखी रे’ सुनना जन्नती अहसास है. https://www.youtube.com/watch?v=3dQTDwGBJW8
ज़ोहराबाई की ख़ासियत थी कि उनकी एक से ज़्यादा विधाओं पर पकड़ थी. जिस रवानी से वो ‘ख़याल’ में डूबती-उतरती थीं, उतनी ही सहजता से वो ठुमरी या ग़ज़ल भी पेश किया करती थीं. आगरा घराने का एक बेहद बड़ा नाम फैयाज़ ख़ान उन्हीं की गायिकी से प्रभावित थे. बड़े ग़ुलाम अली ख़ान भी ज़ोहराबाई का ज़िक्र बड़े ही भक्तिभाव से किया करते. रिकॉर्ड पर उनकी कोई 78 रचनाएं उपलब्ध हैं. 1994 में उनके 18 मशहूर गानों को ग्रामोफोन से ऑडियो टेप पर ट्रांसफर किया गया. 2003 में उसकी सीडी भी बनाई गई. ज़ोहराबाई की आवाज़ में ‘पिया को ढूंढन जाऊं सखी रे’ सुनना जन्नती अहसास है. https://www.youtube.com/watch?v=3dQTDwGBJW8 5. रसूलन बाई बनारस घराने की इस महान फनकार का जन्म 1902 में एक बेहद गरीब घराने में हुआ था. अगर उनके पास कोई दौलत थी, तो वो थी अपनी मां से हासिल संगीत की विरासत. पांच साल की उम्र से ही उन्हें उस्ताद शमू ख़ान से तालीम हासिल होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से उनके गायन की नींव बेहद मजबूत हुई. बाद में उन्हें सारंगी वादक आशिक खान और उस्ताद नज्जू ख़ान के पास भेजा गया. रसूलन बाई वो कलाकार हैं, जिनका ज़िक्र उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ान बेहद आदर से किया करते थे. उन्हें ईश्वरीय आवाज़ कहा करते थे.
 रसूलन बाई ठुमरी गाती थी या ठुमरी उनके ही गले से उतरना चाहती थी, ये सोचने का अपना-अपना कायदा है. आज़ादी के अचानक बाद देश भर में हिंदू–हिंदू, मुसलमान–मुसलमान होने लगा था. शौहर सुलेमान पाकिस्तान चले गए लेकिन रसूलन के ज़मीर को ये गंवारा न हुआ. वो भारत में ही रहीं. https://www.youtube.com/watch?v=ZgNuyJdzDI0
रसूलन बाई ठुमरी गाती थी या ठुमरी उनके ही गले से उतरना चाहती थी, ये सोचने का अपना-अपना कायदा है. आज़ादी के अचानक बाद देश भर में हिंदू–हिंदू, मुसलमान–मुसलमान होने लगा था. शौहर सुलेमान पाकिस्तान चले गए लेकिन रसूलन के ज़मीर को ये गंवारा न हुआ. वो भारत में ही रहीं. https://www.youtube.com/watch?v=ZgNuyJdzDI0
ऊपर जो लिंक है वो रसूलन बाई की एक यादगार ठुमरी है, ‘लागत करेजवा में चोट, फूल गेंदवा ना मारो’. घायल हृदय का वास्ता देकर, इज़हार–ए–मुहब्बत के नाज़ुक एहसास की उम्मीद जताने वाली इस ठुमरी का एक हर्फ कालांतर में बदल दिया गया. ‘फूल गेंदवा ना मारो, लागत जोबनवां में चोट’. लफ़्ज़ में ये बदलाव उन हालात पर सांकेतिक कटाक्ष है, जिनके तहत रसूलन बाई को ग़ुरबत की ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ी. आज़ादी के बाद बनारस में हिंदुओं का सांस्कृतिक बोध कुछ ज्यादा सबल हुआ. लोगों ने पहले तवायफों के मोहल्ले से गुज़रने से इनकार किया और जल्द ही तवायफों के वहां रहने पर ऐतराज़ उठाना शुरू कर दिया. मुफलिसी कुछ ऐसी तारी हुई कि तौबा!ठुमरी, लोकगीत गाने वाली मामूली गायिकाओं की खबर तो इतिहास क्या देगा, ठुमरी साम्राज्ञी रसूलन बाई ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इलाहाबाद के फुटपाथ पर कुछ–कुछ बेचा करती थीं, अपने अधूरे अरमान बांचा करती थीं, ये भी किसको पता है! उसी रेडियो स्टेशन के बाहर जहां से उनके गीत गाहे-बगाहे ब्रॉडकास्ट हुआ करते थे. एक किस्सा पढ़कर तो कलेजे में हूक उठती है. इलाहाबाद रेडियो स्टेशन में लगी कलाकारों की तस्वीर के साथ लिखे नामों में अपना नाम ‘रसूलन बाई’ देखकर उन्होंने कहा था, “बाकी सब बाई देवी बन गई, एक मैं ही बाई रह गई.” तारीफ और इज्ज़त से उठने वाली नजरों की कायल रह चुकी रसूलन बदलते दौर की बेशर्मी और संगदिली से बुरी तरह आहत हुईं. फूल की चोट से घायल होने वाले हृदय को पत्थर की चोट झेलनी है, ये न तो रसूलन ने सोचा होगा, न ठुमरी के कद्रदानों ने.
ये भी पढ़ें:












.webp)
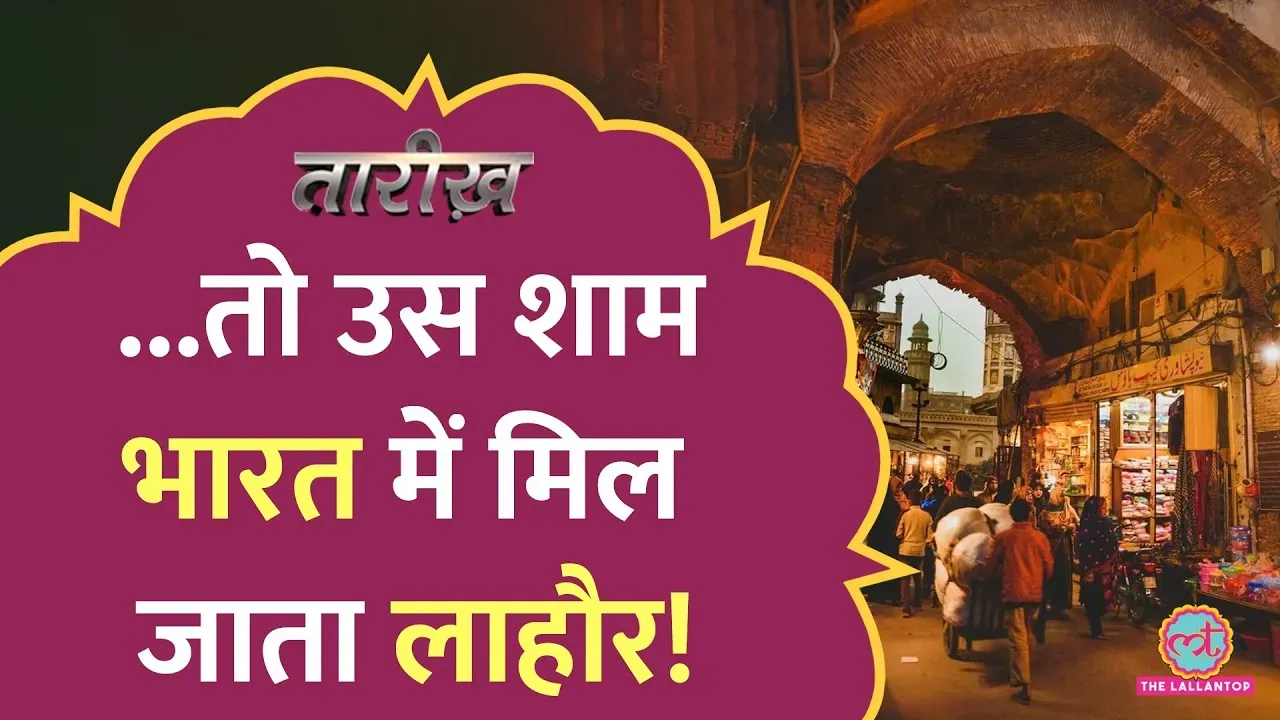

.webp)



.webp)
