क्या सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की पूरी व्यवस्था को ख़त्म करने की भूमिका लिख दी है?
EWS फैसला: क्या आरक्षण के अंत की भूमिका लिखी जा चुकी है?
'आरक्षण अनंत काल तक नहीं चल सकता' कहकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दलित और पिछड़े समुदाय को चिंता में डाल दिया है.

ये सवाल तभी से पूछा जा रहा है जब से सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने अनारक्षित जातियों के ग़रीबों (EWS) को दस प्रतिशत आरक्षण देते हुए आरक्षण की पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए. कहा जा रहा है कि ये फैसला दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को समाज में मान दिलाने के लिए आज़ादी के बाद से बनाई गई पूरी व्यवस्था को ज़मींदोज़ कर देगा. इस मुद्दे पर सोशल मीडिया और अख़बारों में भारी विवाद चल रहा है. यहाँ तक कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ आंदोलन छेड़ने का आह्वान भी किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के पांच में से तीन जजों ने 7 नवंबर को फ़ैसला सुनाया कि मोदी सरकार ने संविधान संशोधन के ज़रिए कथित सवर्ण जातियों के ग़रीबों को दस प्रतिशत आरक्षण देने की जो व्यवस्था 2019 में शुरू की थी उसे जारी रखा जाएगा. लेकिन जस्टिस एस. रवींद्र भट ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि ये फ़ैसला संविधान के मूल ढांचे के ख़िलाफ़ है. अब रिटायर हो चुके भारत के मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित ने जस्टिस भट के फ़ैसले से सहमति जताई थी. अनारक्षित जातियों को आरक्षण देकर सुप्रीम कोर्ट अपने ही उस पुराने फ़ैसले के ख़िलाफ़ चला गया है जिसमें आरक्षण को 50 प्रतिशत से कम रखने की व्यवस्था की गई थी.

एतराज़ इस बात पर भी जताया जा रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के दायरे से पिछड़ी जातियों, दलितों और आदिवासियों (OBC, SC, ST) को बाहर क्यों रखा गया है. इस व्यवस्था के तहत सभी जातियों के ग़रीबों की बजाए सिर्फ़ अनारक्षित जातियों के ग़रीबों को ही आरक्षण दिया जाएगा. क़ानून के कुछ जानकारों का मत है कि संविधान के मुताबिक़ किसी भी समूह को फ़ायदों के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता है. दलित एक्टिविस्ट और पूर्व सांसद प्रकाश आंबेडकर ने कहा है,
“इस फ़ैसले से संविधान के मूल ढांचे को चोट ही नहीं पहुंची है नष्ट भी हो गया है.”
प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला करके आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को तोड़ दिया है इसलिए अब मराठा, गूजर, पाटीदार और जाट जैसी जातियां सड़कों पर उतर आएंगी और पिछड़ी जातियों के लिए 52 प्रतिशत आरक्षण की मांग करेंगी. उन्होंने कहा है, “हम उम्मीद करते हैं कि एक जैसी समझ रखने वाले लोग इस जजमेंट के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे ताकि आने वाले दिनों में अफरा-तफरी से बचा जा सके.”
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों ने अपने फ़ैसले में जो कुछ लिखा उससे दलित संगठनों में आशंका फैल गई है कि ये आरक्षण को ख़त्म करने की भूमिका है. फ़ैसला करने वालों में एक न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी ने लिखा, "आज़ादी के 75 वर्ष बाद हमें समाज के व्यापक कल्याण को देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से नज़र डालनी चाहिए." उन्होंने आगे लिखा,
"संसद में अनुसूचित जाति, जनजाति का प्रतिनिधित्व कुछ समय के लिए ही होना था. एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व ख़त्म हो गया. इसी तरह (बाक़ी आरक्षण के लिए भी) एक समय सीमा तय की जानी चाहिए."

जस्टिस जे बी पारदीवाला ने भी कथित उच्च जातियों के लिए आरक्षण जारी रखने के फ़ैसले में लिखा, "बाबासाहेब अंबेडकर ने सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए सिर्फ़ दस बरस के लिए आरक्षण का विचार दिया था. लेकिन ये पिछले सात दशक से चल रहा है. आरक्षण अनंत काल तक नहीं चलना चाहिए ताकि ये स्वार्थ साधने का ज़रिया न बन जाए."
मोहन भागवत आरक्षण के पक्ष में या खिलाफ़?ऐसा नहीं है कि इन न्यायाधीशों ने अचानक कोई नई बात कह दी हो. आरक्षण पर होने वाली किसी भी चर्चा में ये बार बार कहा जाता है कि ये व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं चल सकती, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए. अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़ी जातियों (OBC)को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की तो पूरे उत्तर भारत में उबाल आ गया था. स्कूल-कॉलेजों में कथित अगड़ी जातियों के छात्र-छात्राएँ सड़क पर उतर आए और कई लोगों ने विरोध में आत्मदाह तक कर लिया.
हिंदुत्ववादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पांचजन्य और ऑर्गनाइज़र को दिए एक इंटरव्यू में आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही और ये काम एक "ग़ैर राजनीतिक समिति" को सौंपने का सुझाव दिया था. इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और बाद में मोहन भागवत ने कहा था कि जब तक जातिगत भेदभाव मौजूद है तब तक जातिगत आरक्षण की व्यवस्था चलनी चाहिए. लेकिन 2018 में उन्होंने आरक्षण की खुलकर वकालत की और कहा कि "आरक्षण कब तक चलना चाहिए इसका फ़ैसला वही कर सकते हैं जिनके लिए ये व्यवस्था की गई है."

लेकिन आरक्षण के प्रश्न पर संघ का द्वंद्व बार बार सामने आता रहा है. मोहन भागवत के एक और बयान से 2019 में फिर विवाद छिड़ गया. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आरएसएस की ओर से आयोजित एक 'ज्ञान उत्सव' में मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण समर्थक और आरक्षण के विरोधियों के बीच सौहार्द्र के माहौल में बातचीत होनी चाहिए. "इससे बिना क़ानून और बिना नियमों के एक मिनट में (समस्या का) समाधान किया जा सकता है." उन्होंने कहा कि संघ इसकी कोशिश कर रहा है.
इस संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था पर जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला की टिप्पणी और अर्थपूर्ण हो जाती है.
सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि 103वां संशोधन संविधान सम्मत है या नहीं. लेकिन उन्होंने आरक्षण की पूरी व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लगा दिया. इस कारण उन समुदायों की चिंता वाजिब है जो हज़ारों बरसों से जाति व्यवस्था की सबसे निचली पायदान पर रह रहे हैं. क़ानून के कई जानकारों को भी शक है कि EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फ़ैसले से कई बुनियादी बदलाव हो जाएंगे.
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर सुधीर कृष्णास्वामी ने द प्रिंट में छपे अपने एक लेख में संकेत दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से आरक्षण की व्यवस्था में बुनियादी बदलाव होने जा रहा है. उन्होंने लिखा,
“EWS के बारे में ये फ़ैसला आरक्षण की व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की शुरुआत कर देगा और समूहों के आरक्षण की बजाए व्यक्तियों के आरक्षण की तरफ़ ले जाएगा. आने वाले दशकों में आरक्षण के मुद्दे पर जातीय पहचान का महत्व निश्चित तौर पर कम होगा.”
आरक्षण में जातीय पहचान का महत्व कम होने का सीधा अर्थ है कि आने वाले बरसों में आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाएगा. अभी ऐसा नहीं हुआ है लेकिन इस फ़ैसले से ऐसा होने की आशंका बढ़ गई है. यही वजह है जिससे दलित-ओबीसी संगठन और एक्टिविस्ट सतर्क हो गए हैं.
राजनीतिक दल कहां खड़े हैं?ग़ौर करने लायक़ बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर दलित संगठन और एक्टिविस्ट तो बोल रहे हैं मगर ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने इस पर अपनी मौन सहमति दे दी है. पर इसमें अचरज कैसा? ये एक तथ्य है कि जब मोदी सरकार 103वां संविधान संशोधन विधेयक लाई तो 9 जनवरी 2019 को लोकसभा में 323 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया. महज़ तीन सांसद इसके ख़िलाफ़ थे.

ज़ाहिर है संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाली सभी पार्टियों को कथित सवर्ण वोटरों की चिंता थी इसी वजह से वो इसके पक्ष में खड़ी हो गईं. लोकसभा में तो बीजेपी बहुमत में थी मगर राज्यसभा में उसके पास बहुमत नहीं था. कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बिल को संसदीय समिति को भेजने की मांग की थी पर उसे ख़ारिज कर दिया गया और विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया. बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित ज़्यादातर पार्टियों ने कथित सवर्ण जातियों के ग़रीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फ़ैसले का समर्थन किया है. बीएसपी तो दलित-ब्राह्मण गठजोड़ के ज़रिए ही 2007 में उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती थी. कांग्रेस ने भी इस फ़ैसले का स्वागत करते हुए इसके लिए ख़ुद श्रेय लेने की कोशिश की है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मनमोहन सिंह सरकार ने 2005-6 में इसके लिए एक आयोग बनाया था, लेकिन इसे लागू करने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बरसों लगा दिए.
अगर कोई एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आई है तो वो है तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके). पार्टी के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए एक बड़ा आघात बताया है. स्टालिन ने समान विचार वाली सभी पार्टियों से अपील की है कि वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक मंच पर आएं.
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से एक पेचीदा स्थिति ये पैदा हो गई है कि कुछ राज्यों में EWS कोटा के दायरे में आने वाली जातियां सिर्फ़ चार प्रतिशत ही हैं. द हिंदू अख़बार की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ कर्नाटक में ब्राह्मण, आर्यवैश्य, नागर्ता, मुदालियार और जैन समुदाय आरक्षण के दायरे से बाहर हैं पर ये कुल जनसंख्या का सिर्फ़ चार प्रतिशत हैं. राज्य में मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, दिगंबर जैन, लिंगायत और वोक्कलिगा समुदाय 32 प्रतिशत ओबीसी कोटा के दायरे में आते हैं. ऐसे में कथित अगड़ों के ग़रीब तबकों को दस प्रतिशत आरक्षण देने में अड़चन आ सकती है.
ये सब तकनीकी पेचीदगियां अपनी जगह, मगर राजनीतिक पार्टियों के दायरे से बाहर के दलित समूह औऱ एक्टिविस्टों में सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से भारी बेचैनी है. उनकी आशंका है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने आरक्षण पर जो सवाल खड़े किए हैं उसे आधार बनाकर आने वाले दिनों में आरक्षण-विरोधी भौकाल पैदा किया जा सकता है.
वीडियो: क्या इस मुद्दे पर हो सकता है मोदी सरकार Vs चीफ जस्टिस चंद्रचूड़?











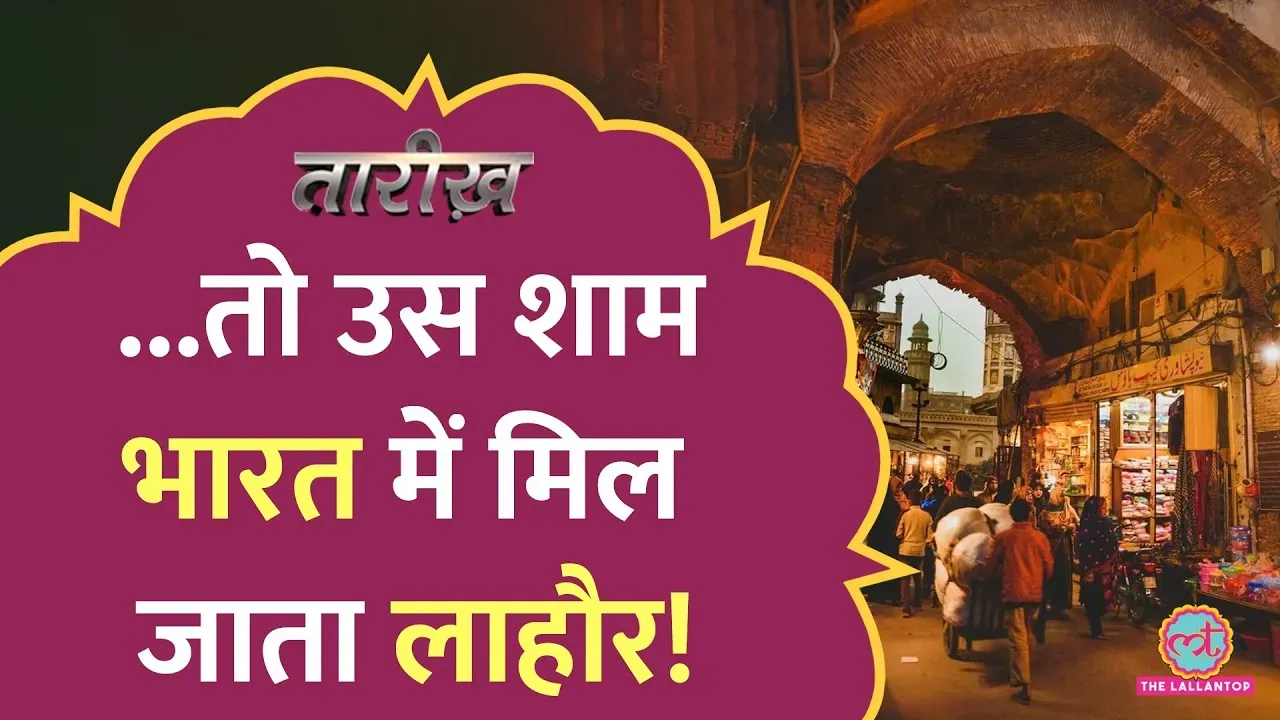





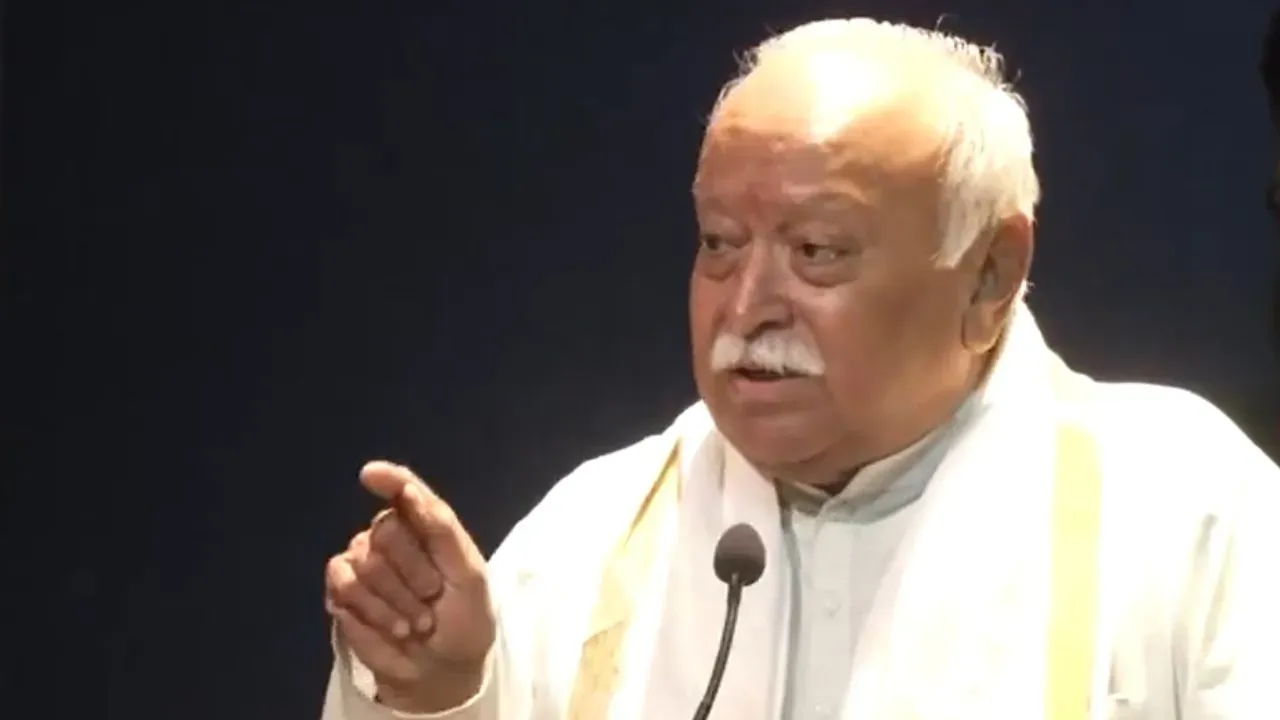
.webp)

