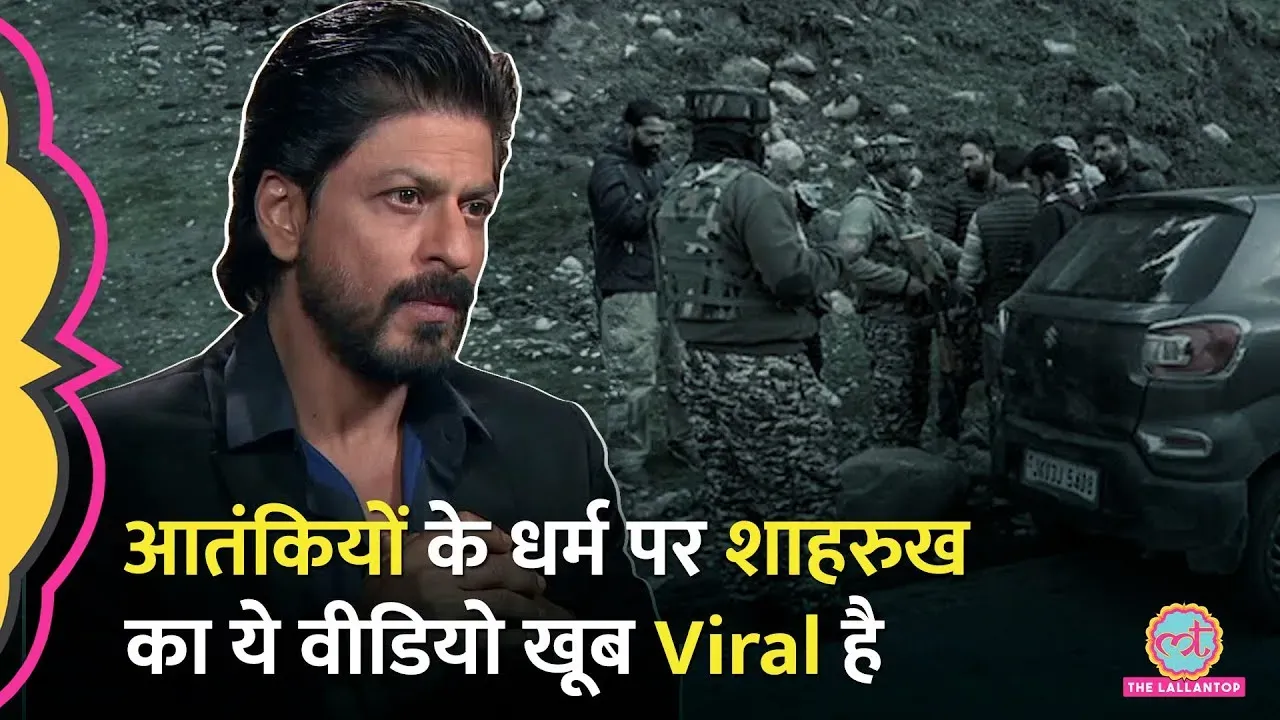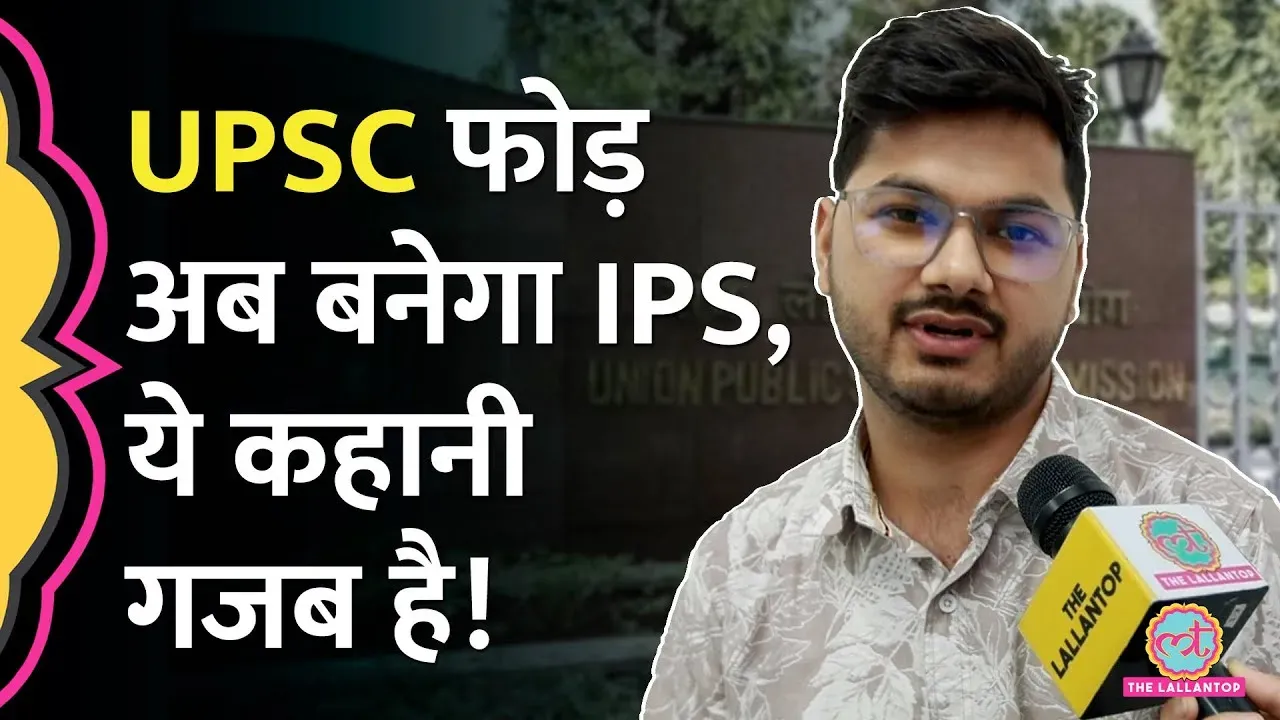शिवानी जन्मीं थीं 17 अक्टूबर 1923 को. विजयादशमी का दिन था. राजकोट की बात है. पढ़ाई-लिखाई शांतिनिकेतन में हुई. साठ और सत्तर के टाइम में इनकी कहानियां खूब फेमस हुईं. 12 साल की उम्र में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी. और ये अंत तक कहानियां लिखती रहीं. औरतों पर लिखा और बहुत अच्छा लिखा. खूब नाम कमाया. अभी जन्मदिन का हफ्ता है. हम आपको उनका लिखा पढ़ाएंगे. हफ्ते भर. कल पढ़ाया था 'गंगा बाबू कौन' आज पढ़िए गूंगा. राजकमल प्रकाशन को थैंक्स कहिए. उन्हीं की हेल्प से आपको ये कहानियां पढ़ा पा रहे हैं.
सर्जन पंड्या को दूर से देखने पर लगता, कोई अंग्रेज चला आ रहा है. सुर्ख गालों पर सुख, सन्तोष और स्वास्थ्य की चमक थी. उनके हाथ में कुछ ऐसा यश था कि उनकी प्रतिभा का स्पर्श पाते ही, मुरझाए मरीज भी चंगे होकर बैठ जाते. उनकी फीस भी उनके व्यक्तित्व की ही भांति रोबीली थी, ऐसा-वैसा व्यक्ति तो उनकी फीस सुनकर ही पीला पड़ जाता, पर रोगी के पीले चेहरे से भी उनकी आंखों में करुणा नहीं उभरती. कभी-कभी वे अपनी विकट फीस में थोड़ा-सा अन्तर भी कर देते थे. बशर्ते, मरीजा सुन्दरी हो या मरीज किसी मौलिक बीमारी का नमूना हो. पर असंख्य रोगियों को जीवन-दान देने वाला यह अनोखा मसीहा अपनी ही पत्नी का इलाज नहीं कर सका था.
एक ही पुत्री को जन्म देकर उसकी पत्नी सौर में ही पगला गई थी और सर्जन उसे ठीक नहीं कर पाए थे. सोलह वर्ष से वह आगरा के पागलखाने में पड़ी थी. बीच-बीच में सर्जन उसे देखने भी जाते थे और कुछ लोग तो कहते थे कि वह उतनी पागल नहीं थी कि उसे घर न लाया जा सके, पर सर्जन कभी लौटकर पत्नी के उन्माद का प्रसंग भी पुत्री के सामने नहीं छेड़ते और न पुत्री ही कुछ पूछती. सर्जन की कन्या का नाम था कृष्णा. रंग था गेहुंआ, पर मुखश्री अनुपम थी. सघन कृष्ण वेणी को वह ढीली-ढाली गूंथकर पीठ पर डाल देती. मां के अभाव को पिता के स्नेह ने कभी खटकने नहीं दिया था. देखरेख की लगाम तो नहीं थी, पर पिता का शासन कड़ा था. कृष्णा ने पढ़ाई के साथ संगीत और नृत्य की शिक्षा प्राप्त की. पैरों में घूंघर बांधते ही वह स्वर्ग की अप्सरा बन जाती, बड़े से बड़ा कला-मर्मज्ञ हो या नृत्य-संगीत से एकदम ही अनभिज्ञ कोई अरसिक, सब उसके नृत्य की रस- माधुरी में डूबकर रह जाते; यही उसके नृत्य की विशेषता थी.
एक बार एक नृत्योत्सव में तीन घंटे तक नाचकर दर्शकों को मन्त्रमुग्ध किया और अन्त में जब हाथ जोड़कर दर्शकों की ओर सिर झुकाया तो तालियों से हाल गूंज उठा. सर्जन की आंखों में आनन्दाश्रु छलक उठे. अन्तःकरण को अमृतवृष्टि से परिप्लावित करती उस छवि को एकटक देखते, एक और व्यक्ति की भी आंखें तरल हो गई थीं और वह था तरुण स्क्वैड्रन, लीडर वी. डीसूजा. वह कृष्णा के पड़ोसी डॉ. डीसूजा का पुत्र था. उसके पिता सर्जन के क्लिनिक में ही काम करते और सर्जरी में ही हाथ में छुरी लग जाने से टिटनेस से उनकी मृत्यु हो गई थी. पिता की मृत्यु के बाद मातृहीन डीसूजा सर्जन के साथ ही छुट्टियां बिताता. कृष्णा के आकर्षण-जाल में वह किस बुरी तरह फंस गया है यह वह उसी दिन जान पाया. स्वभाव से ही लजीले उस सौम्य गोवानी युवक पर सर्जन का अत्यन्त स्नेह था. उसके लम्बोतरे चेहरे पर सांवले रंग की चमक थी, पतली मूंछों के नीचे उसके पतले होंठों पर सदा संयम की चाबी लगी रहती. वह बड़े नम्र स्वर में बोलता और बड़े ही सलीके से कपड़े पहनता. उसके जूते ऐसे चमकते कि कोई चाहे तो अपना मुंह देख ले! सर्जन, उसके जूतों की इसी चमक पर फिदा थे. "शाब्बास बेटे, तुम्हारे जूतों की चमक देखकर हमारी तबियत खुश हो जाती है. जो शख्स अपने जूते चमकाकर रखता है उसका दिल भी हमेशा चमकता रहता है." पता नहीं, सर्जन का कथन किस अंश तक सच था, पर डीसूजा का दिल सचमुच ही एकदम साफ था. वह जितना ही कृष्णा से बचकर निकलता, वह उसे उतना ही घेर लेती. इसी बीच सर्जन को अपने निःसन्तान बूढ़े चाचा की क्रिया निबटाने पहाड़ जाना पड़ा. कुछ ही दिन पूर्व उसके चाचा का अनुनय-भरा पत्र आया था- "मैं मरणासन्न हूं, मेरी मृत्यु के बाद जैसे भी हो, मुझे पीपल-पानी कर जाना, नहीं तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी." सर्जन प्रगतिशील विचारों के होकर भी घोर सनातनी थे. अपने राजप्रासाद के गुसलखाने में लघुश्ंाका से निवृत्त होने भी जाते, तो जनेऊ कान पर चढ़ा होता. चाचा की आत्मा को तो उन्होंने भटकने से बचा लिया, पर पुत्री की आत्मा भटक गई. तेरहवीं कर लौटे तो चित्त प्रसन्न था. आत्मीय स्वजनों ने उनकी पुत्री के लिए एक हीरे-सा टुकड़ा वर ढूंढ़ दिया था. कृष्णा उन्हें लेने एअर पोर्ट पर आई- "क्यों बेटी, कान्तम्मा तुम्हें छोड़कर छुट्टी ले घर तो नहीं चली गई थी?" उन्होंने पूछा. कान्तम्मा उनकी वर्षों पुरानी बूढ़ी आया थी. "ना पापा," नम्रमुखी कन्या उन्हें कुछ पीली-सी लगी. "पापा, मेरे लिए पहाड़ की मिठाई बालसिंघौड़ी लाए या नहीं?" बच्ची की तरह मचलकर उसने पूछा. "लाया क्यों नहीं, और भी एक चीज लाया हूं अपनी दुलारी बेटी के लिए, जानती हो क्या?" सर्जन ने मुस्कराकर कहा.
"क्या पापा?"
"एक सुन्दर-सा वर, जिसे ढूंढ़ने ही शायद भगवान ने मुझे पहाड़ भेजा था." सर्जन ने कनखियों से बेटी की ओर देखा और ममता से उनका गला भर आया. थोड़े ही दिनों में उनकी बेटी पराई हो जाएगी. कृष्णा का चेहरा आश्चर्यजनक रूप से सफेद लग रहा था, वह पहले गुमसुम हो गई, फिर अचानक दृढ़ स्वर में बोली, "आपको मेरे लिए वर नहीं ढूंढ़ना होगा- मैंने वर ढूंढ़ लिया है!"
सर्जन दंग रह गए, कहती क्या है लड़की- कहां से वर ढूंढ़ लिया, यहां तो अपने समाज का एक परिवार भी नहीं था.
"क्या बात कर रही है पगली, कैसा वर?" उन्होंने स्वर को करुण बनाकर पूछा.
"हां पापा, मैं विकी से ही ब्याह करूंगी." सामान्य-सी किशोरी के कंठ की दृढ़ता में कहीं भी नम्रता की मिठास नहीं थी. सर्जन क्रोध से कांपते चुपचाप अपनी मूंछें नोचने लगे. सामान्य-सा पाइलट डीजूसा, उस पर भी ईसाई और कहां कुमाऊं के महापंडितों के खानदान की पुत्री कृष्णा! कार घर पहुंची, तो डीसूजा को बुलाने आदमी भेजा, पता लगा- डीसूजा मद्रास चला गया है. शासन की लक्ष्मण-रेखा में पुत्री को बांधकर सर्जन निश्चिन्त हो गए. बिना उनसे पूछे अब वह गुसलखाने भी नहीं जा सकती थी. सर्जन को इसी बीच जयपुर की मेडिकल सेमिनार में अध्यक्षता करने जाना पड़ा. कान्तम्मा को कड़ी हिदायतें देकर वे दो और बूढ़ी नौकरानियां तैनात कर गए, किन्तु तीन जोड़ी बूढ़ी आंखों को धोखा देने के लिए कृष्णा की एक ही जोड़ी जवान आंख काफी थीं. डीसूजा खबर पाते ही छुट्टी लेकर आ गया और दोनों फिर लुक-छिपकर मिलने लगे. "पापा के आने में केवल आठ दिन हैं विकी." एक दिन कृष्णा ने उसकी छाती पर माथा टिकाकर कहा, "तुम्हें पांच दिन बाद लम्बी टेªनिंग के लिए फ्रांस जाना है, क्यों न हम सेंट पाल के बूढ़े पादरी की खुशामद कर शादी कर लें? पापा फिर कर ही क्या लेंगे?" एक शाम, दोनों जंगल में खो गए. बच्चों की भांति, एक-दूसरे का हाथ कसकर पकड़े, सेंट पाल से लौटे. तीसरे दिन डीसूजा चला गया. सर्जन लौटे, ढाई-तीन माह तक मरीजों में फंसे रहे. एक दिन लेटे-लेटे वे अखबार पढ़ रहे थे कि पहले ही पृष्ठ पर ‘तरुण भारतीय पाइलेट की मृत्यु’ की खबर देखकर चौंक गए. डीसूजा की मृत्यु हो गई थी. वे मन-ही-मन ईश्वर को लाख-लाख धन्यवाद दे रहे थे कि एक चीख सुनकर चौंक पड़े. कृष्णा उनके पीछे खड़ी थी. उसका रोना और कोई न सुन ले, यह सोचकर सर्जन ने चट से उसे उसके कमरे में धकेलकर अन्दर से चिटकनी चढ़ा दी. पर कृष्णा सिसकती रही. "क्या तूफान मचा रखा है तुमने? कोई नादान बच्ची तो नहीं हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है." बाल बिखराए ही कृष्णा तड़पकर उठ बैठी- "मेरी शादी हो चुकी थी पापा!" "क्या बकती है?" सर्जन ने तिलमिलाकर बेटी की ओर चांटा साधा; फिर बड़ी चेष्टा से बिना मारे ही हाथ खींच लिया.
"हां पापा, तीन माह पहले सेंट पाल के पादरी ने हमारी शादी करवाई थी- विकी मेरा पति था." उसके होंठ कांपने लगे.
"चुप कर बेहूदी! तुम अभी नाबालिग हो, शादी हो ही कैसे सकती थी?" गुस्से से पैर पटककर सर्जन धड़धड़ाते पादरी के पास गए, न जाने कितने के चेक से उसका मुंह बन्द किया. लौटे तो कृष्णा को समझाते हुए कहा, "मैंने पादरी को समझा दिया है, वह सब रिकार्ड जला देगा. खिलवाड़ को कोई भी धर्म शादी नहीं कह सकता."
"पर एक बात और है पापा," सिर झुकाकर कृष्णा जमीन में गड़ गई.
"क्या?" चीखकर ही पूछा सर्जन ने.
"मैं मां बननेवाली हूं." दोनों हाथों से मुंह ढांपकर वह सिसक उठी.
नियति से जूझकर सर्जन अब धराशायी थे. रात-भर वे पिंजड़े में बन्द शेर की तरह चक्कर लगाते रहे, फिर भोर होते-होते उन्होंने कमर कस ली. दूसरे दिन वे पुत्री को लेकर यह कहकर चले गए कि सगाई की रस्म पूरी करने वे पहाड़ जा रहे हैं. मार्ग में उन्होंने बेटी को कितना समझाया, अठारह वर्ष की जिन्दगी, वह अकेली नहीं काट सकती. देहली में एक बहुत बड़े महिला आश्रम की संचालिका काशीबाई को वे जानते थे. कुछ वर्ष पूर्व उसे ब्रेस्ट कैन्सर हो गया था. उन्होंने उस विधवा सुन्दरी को कभी जीवन-दान दिया था. आज उसी का प्रतिदान मांगने जा रहे थे. सबकुछ सुनकर काशीबाई हंसकर बोली, "आप निश्चिन्त रहें सर्जन, किसी को कानों-कान खबर नहीं होने की."
भाग्य ने सर्जन पर दया करके समय से पूर्व कृष्णा को मुक्ति दे दी. सतमासी पुत्र को जन्म देकर वह चार माह बाद घर लौट आई. कुछ ही दिनों बाद उसके विवाह की तैयारियां जोर-शोर से होने लगीं. सात फेरे लगाकर सप्तपदी पूर्ण हुई तो सर्जन के दिल का पहाड़ हट गया. काशीबाई पर उन्हें पूरा भरोसा था और किसी को कानोंकान कुछ खटका भी नहीं हुआ था. धीरे-धीरे समय बीतता गया. विवाह को अब छः वर्ष पूरे हो गए थे. कृष्णा के एक पांच वर्ष का पुत्र भी था, किन्तु अभी भी उसके सौन्दर्य में वही अल्हड़-सा भोलापन था. वह नृत्य का निरन्तर अभ्यास करती थी, उसके ओडिशी और भरतनाट्यम् की ख्याति राजधानी तक पहुंची और महारानी के स्वागत-समारोह में उसे आग्रहपूर्वक आमन्त्रित किया गया. वह अपने पति और पुत्र के साथ ही आई थी, क्योंकि ठीक सातवें दिन उसके पति को वाशिंगटन दूतावास में सेक्रेटरी के पद का भार ग्रहण करने पहुंचना था. दुर्भाग्य से ठीक नृत्य-समारोह के दिन ही राजीव को तेज ज्वर हो आया. इकलौता जिद्दी लाड़ला, मां के गले में अपनी ज्वराक्रान्त तपती बांहें डालकर झूल गया- "नहीं ममी, तुम यहीं रहो." बड़ी कठिनता से एक इलेक्ट्रिकल टेªन और चाकलेट का उत्कोच देकर कृष्णा को छुट्टी मिली. उस दिन के नृत्य-प्रदर्शन ने उसके गले में कीर्ति की जयमाला डाल दी. स्वयं महारानी एलिजाबेथ ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे बधाई दी. प्रशंसा और तालियों के नशे में झूमती वह पति के साथ कार में लौट रही थी कि सर्र से महिला आश्रम के पास से कार गुजर गई. एक पल ही में उसकी सारी प्रसन्नता उड़ गई. जिस घाव की सूखी पपड़ियां तक झर गई थीं, वही आज नासूर बन गया था. घर पहुंची और बच्चे को छाती से चिपटाकर लेट गई, पर सो नहीं सकी. मां को पाकर राजीव ने प्रसन्नता से छाती में मुंह छिपा लिया.
पीपल के पेड़ के साये में घिरी आश्रम की छोटी-सी कोठरी में मूंज की झूला-सी चारपाई पर एक अभागा सो रहा था, उसके पास मुंह छिपाने को किसी की छाती नहीं थी. उसे सदा के लिए छोड़ जाने पर भी मां ने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया था. न उसे मां के लौटने का इन्तजार था, न बिछोह का दर्द. वह दिन-भर आश्रम के लावारिस बच्चों से पिटता रहता. उसकी शान्त आंखों में एक अजब उदासी थी, न वह किसी से बोलता था, न किसी से झगड़ता.
झगड़ता भी कैसे? वह बहरा था और बोलता भी क्या? बेचारा जन्म से ही गूंगा था. कृष्णा को यह सबकुछ पता नहीं था. पांच वर्षों में वह कई बार उसे देखने को व्याकुल हो उठी थी, पर उसने पापा को आश्रम में कभी पैर भी न रखने का वचन दिया था. फिर क्या पता, शायद मर ही गया हो. बेचारी कृष्णा क्या जानती थी कि ऐसे बच्चे, जिनकी मौत की मिन्नतें मांगी जाती हैं, कभी नहीं जाते. जाते हैं वे जिनकी जिन्दगी की भीख के लिए दामन फैलाए जाते हैं. सोमवार को उसे विदेश जाना था. बच्चे का बुखार उतर गया था और वह अपनी रेल से खेल रहा था. पति कहीं गए थे. कृष्णा ने अपनी कार निकाली और उसी दुकान पर पहुंची, जहां से खिलौने की रेल खरीदी थी. ठीक वैसी ही रेल खरीदी, एक बड़ा-सा भालू लिया और कई चाकलेटों से बैग भरकर आश्रम की ओर चल पड़ी. थोड़ी दूरी पर कार पार्क कर उतरी तो कलेजा धड़कने लगा. क्या पता, काशीबाई की बदली हो गई हो! साहस कर भीतर गई तो काशीबाई गेट पर ही मिल गई- "ओह तुम! वाह आओ, आओ! दफ्तर ही में बैठें." हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गई. "कहो, आज बहुत दिनों में याद किया." स्वर का तीखा व्यंग्य कृष्णा के हृदय के घाव पर नमक छिड़क गया. "आती कैसे! पापा को वचन दिया था." कहकर कृष्णा ने माथा झुका लिया.
"क्या उसे देखोगी?" बड़ी आत्मीयता से काशीबाई आगे को झुक गई.
सिर झुकाकर कृष्णा ने मौन स्वीकृति दे दी.
"देखो कृष्णा, बुलवा लेती हूं, पर जरा अपने दिल पर काबू रखना. वह अभागा गूंगा है, ये नौकरानियां साली बड़ी हरामी हैं, जरा भी शुबहा होगा, तो ब्लैकमेल करना भी जानती हैं.’’ ‘पूरनदेई!’ कहकर उसने घंटी बजाई, एक अधेड़-सी जल्लाद औरत आकर खड़ी हो गई. ‘देखो, गूंगा बाबा को ले आओ, बड़ी डाक्टरनी आई हैं. उसकी जबान देखेंगी.’ पूरनदेई चली गई तो संसार की सारी हथौड़ियां कृष्णा की कनपटी पर चलने लगीं. रूमाल निकालकर वह पसीना पोंछ रही थी कि ‘चल-चल’ कहती हुई खच्चर की तरह हांकती पूरनदेई गूंगे को ले आई. वह शायद किसी की मंगनी की कमीज पहने था, जिसकी बांहें, उसके हाथों से बहुत नीचे लटक रही थीं, या शायद कमीज की लम्बाई महज इसलिए बढ़ा दी गई थी कि जीर्ण निक्कर ने नीचे के अंगों की लाज ढांकने से एकदम ही इन्कार कर दिया था.
"तैयार क्यों नहीं किया इसे?" सकपकाकर काशीबाई ने पूरनदेई को डांटा.
"जिद्दी कैसा है यह हरामी! कितना कहा, कपड़े बदल ले, माने तब न." पूरनदेई आग्नेय दृष्टि से गूंगे को भस्म कर बाहर चली गई. कृष्णा की सजल आंखों में नन्हें राजीव का चेहरा नाच उठा, जिसके सौ-सौ नखरे उठाते हुए वह, आया और उसके पति हार-हार जाते थे. द्वार पर कुंडी चढ़ाकर काशीबाई ने इशारे से गूंगे को नजदीक बुलाया- "आओ बेटा!" "घम-घम" गूंगे ने किसी महान दार्शनिक की भांति हंसकर अपनी गूंगी दलील पेश की. जैसे कृष्णा से कह रहा हो- ‘मां, इसकी बातों में मत आना, यह बड़ी लबारी है.’ कृष्णा ने बेटे की बात समझ ली. ऐसी भाषा केवल मां ही समझ सकती है. झरझरकर उसकी आंखें बरस पड़ीं. छोटा-सा डीसूजा ही तो खड़ा था. वही संयमी दृष्टि और वैरागी मुस्कान. लपककर उसने गूंगे को खींचकर छाती से लगा लिया. कभी उसकी लटों को चूमती, कभी मैल से काली कलाइयों को. लगता था, चूम-चूमकर ही गूंगे को अपने में भर लेगी.
"अरे, बस भी कर. क्यों गूंगे का सिर फिरा रही है?" अपनी जल्लादी आंखों को और भी कठोर बनाकर काशीबाई बोली. तिलमिलाकर कृष्णा ने उसे छोड़ दिया. मुक्ति पाते ही गूंगा खिलौनों के पास खड़ा हो गया. "ले, सब तेरे हैं." कहकर काशीबाई ने उसे डिब्बे थमा दिए. गूंगी आंखें चमक उठीं, कभी इंजन को उठाता, कभी रंगीन लाल-हरे रेल के डिब्बांे को, कभी ताली बजाता और कभी गोल-गोल घूमकर नाचता- "घम घम मम मम!"
"अब तुम जाओ कृष्णा, बड़ी देर से दरवाज़ा बन्द है, मुई पूरनदेई कहीं द्वार पर ही कान लगाए खड़ी न हो. वाह, अंगूठी तो बड़ी सुन्दर है तुम्हारी!" लालची दृष्टि का सन्देश कृष्णा समझ गई. चट अंगूठी उतारकर उसने काशीबाई को पहना दी और मूक करुण दृष्टि से अपना सन्देश भी दे दिया- ‘मेरे गूंगे का ध्यान रखना.’ फिर हृदय पर पत्थर रखकर वह उठी, एक बार गूंगे को चूमा और तीर-सी बाहर छिटक गई. सोमवार को वह पति के साथ विदेश चली गई. कुछ ही महीनों में भारतीय सेक्रेटरी की नृत्य-प्रवीणा पत्नी की चर्चा पूरी एम्बेसी में थी. एक बार टेलीविजन पर उसका नृत्य हुआ और एक दिन उसे एक पत्र मिला, एक गूंगे-बहरे बच्चों की संस्था-संचालिका मदर मारिया का. "क्या वे उनके अभागे बच्चों के सम्मुख अपना मनोहारी नृत्य प्रस्तुत कर कृतार्थ करेंगी!" कृष्णा ने एकदम स्वीकृति दे दी. तीन घंटे तक वह नाचती रही. गूंगे चेहरों पर खुशी की चमक उसके लिए करोड़ों तालियों की गड़गड़ाहट से भी बढ़कर थी. नृत्य समाप्त हुआ और मदर का हाथ पकड़कर एक देवदूत-सा सुन्दर बालक आया और उसे फूलों का गुच्छा भेंट किया. "धन्यवाद बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा?" पूछते ही कृष्णा को अपनी अल्पबुद्धि पर क्रोध आया. "ओह मिसेज त्रिपाठी, यह बेचारा तो जन्म से ही गूंगा है." मदर ने कहा, "इसकी मां इसे हमारे आश्रम के द्वार पर डाल गई थी, फिर पलटकर नहीं आई- ईसू उसे क्षमा करे." मदर ने क्रास बनाया.
कृष्णा एकटक उस बच्चे के सुनहरे माथे को देखती रही. फिर टपटप कर उसके आंसू रत्नजटित वलयों को भिगोने लगे. "यह क्या मिसेज त्रिपाठी, आप रो रही हैं?" आश्चर्य से मदर ने पूछा और फिर बढ़कर उन्होंने कृष्णा के दोनों हाथों को चूम लिया. "काश, ऐसे ही प्रत्येक मानव दूसरे के दुख-दर्द के लिए रो सकता! एक विदेशी गूंगे बच्चे के लिए आपकी आंखों में आंसू देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हुई, कितनी!"
बेचारी मदर क्या जानती थी कि वे आंसू केवल उस विदेशी गूंगे बालक के लिए ही नहीं थे. वे उसके लिए भी थे जो अपनी दुबली कलाइयों से, खिड़की की सलाखों को जकड़े ही सो रहा था. उसकी छाती से एक मैला-सा कपड़े का भालू चिपका था. उसकी रेल काशीबाई ने आश्रम के खिलौने के कमरे में बन्द कर दी थी. वह कितना रोया था, पर कौन सुनता? आश्रम में, मोटरों में बैठकर, खादी की टोपी लगाए मेहमान आते, बच्चे को साफ कपड़े पहनाए जाते, मिठाई बंटती, पर गूंगा मिठाई फेंककर, अपनी रेल के लिए मचलता रहता. समुद्र की उत्तुंग लहरों को भांति, नाना तर्क-वितर्कों की लहरें उसके नन्हे-से कलेजे की कछार पर सिर पटक-पटककर व्यर्थ ही लौट जातीं. वह कितना कुछ पूछना चाहता है- मेरी रेल क्यों छीन ली? इतने मेहमान आते हैं, पर वह क्यों नहीें आती जिसने मुझे चूम-चूमकर खिलौने दिये थे? आज मेरी पीठ पर काशीबाई ने बेंत क्यों मारे? मैंने तो पूरनदेई की पीठ पर दांत ही काटे थे; पर वह जो मुझे रोज-रोज मारती है, उसे बेंत क्यों नहीं पड़े?
पर वह अभागा कुछ भी नहीं पूछ सकता. अन्धे बेजान भालू को छाती से चिपकाकर खिड़की के अंधेरे कोने में दुबक गया है, जहां थोड़ी देर तक न उसे काशीबाई ढूंढ़ सकती है, न पूरनदेई. सात समुद्र पार उसकी मां भी सिसक रही है- शायद उन्हीं लाड़भीनी सिसकियों की लोरी ने गूंगे को भी सुला दिया है. मीठी नींद में डूबा गूंगा, अपने गूंगे सपनों की दुनिया में पहुंचकर खो गया है, वहां न काशीबाई है न पूरनदेई. वहां तो बस बड़ी-सी बिजली की रेल है, सोने के पेड़ों पर खिलौने झूल रहे हैं, और वही सुन्दर-सी औरत उसे गोद में उछाल-उछालकर चूम रही है. नींद ही में गूंगा मुस्कराकर भालू को और भी कसकर छाती से लगा लेता.
शिवानी का हफ्ता में आज पढ़िए 'गंगा बाबू कौन'










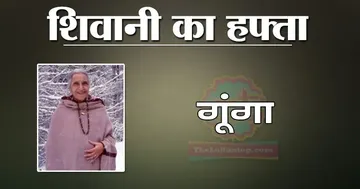



.webp)
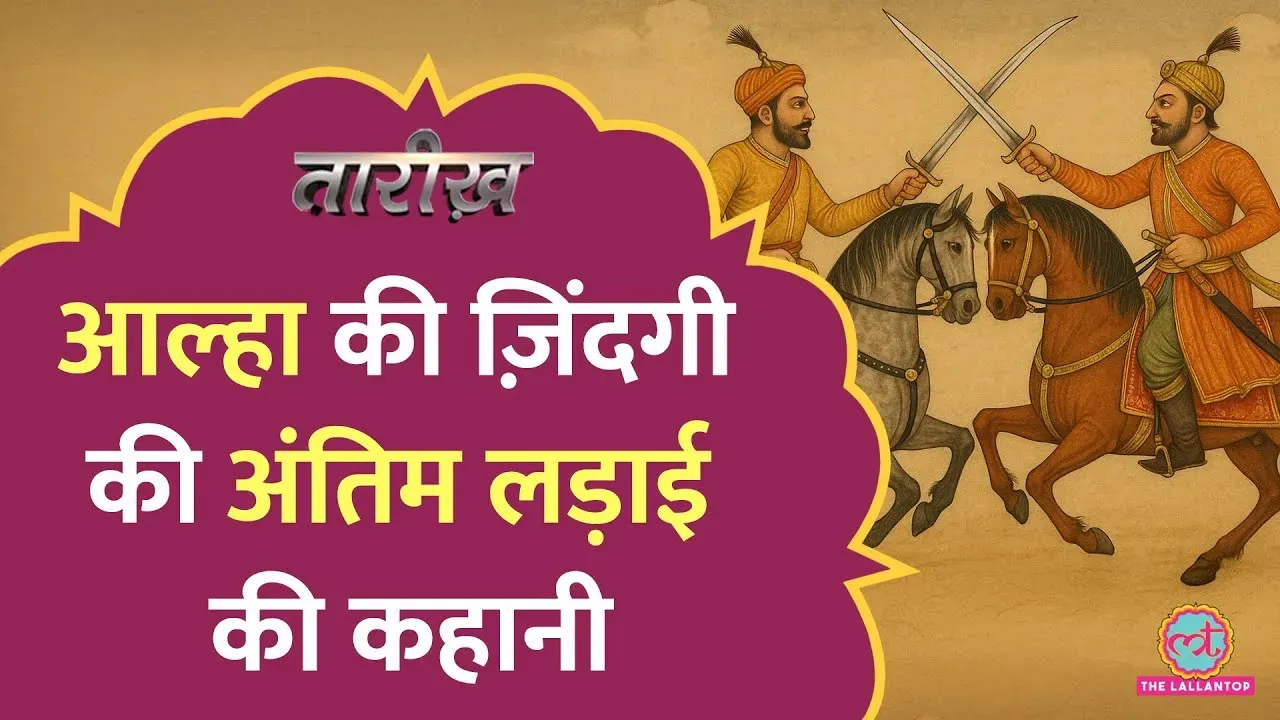
.webp)