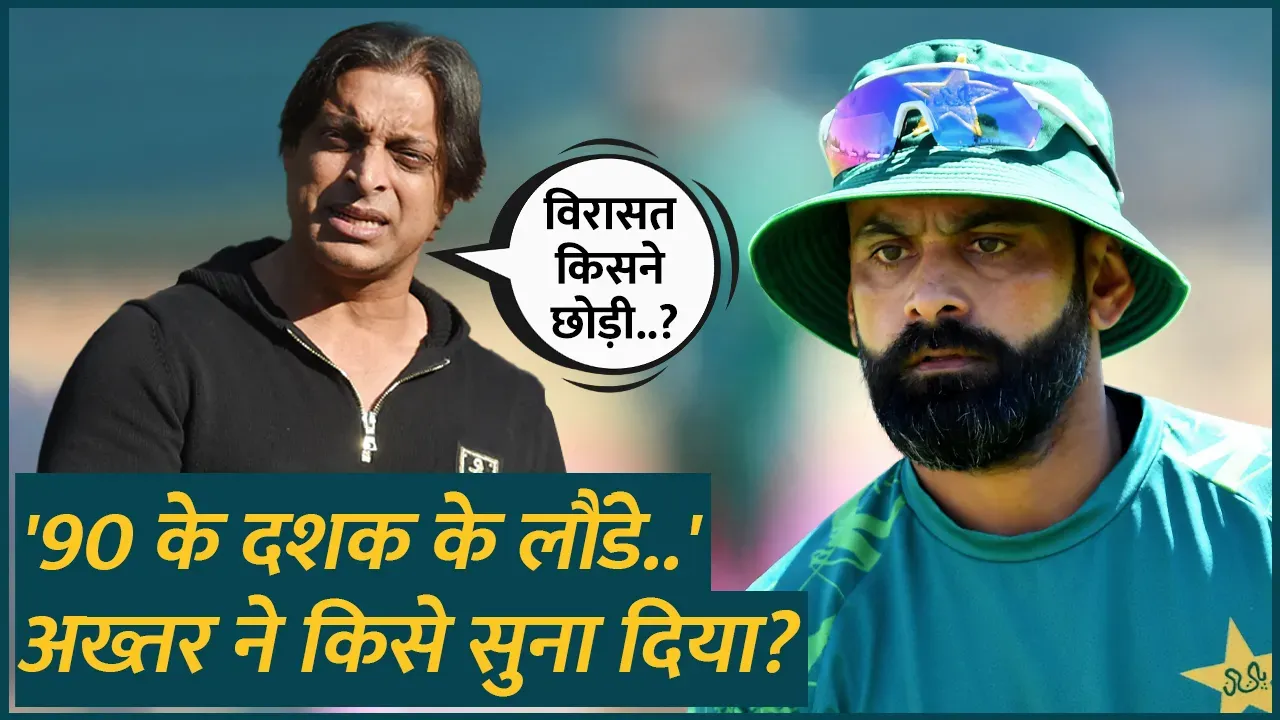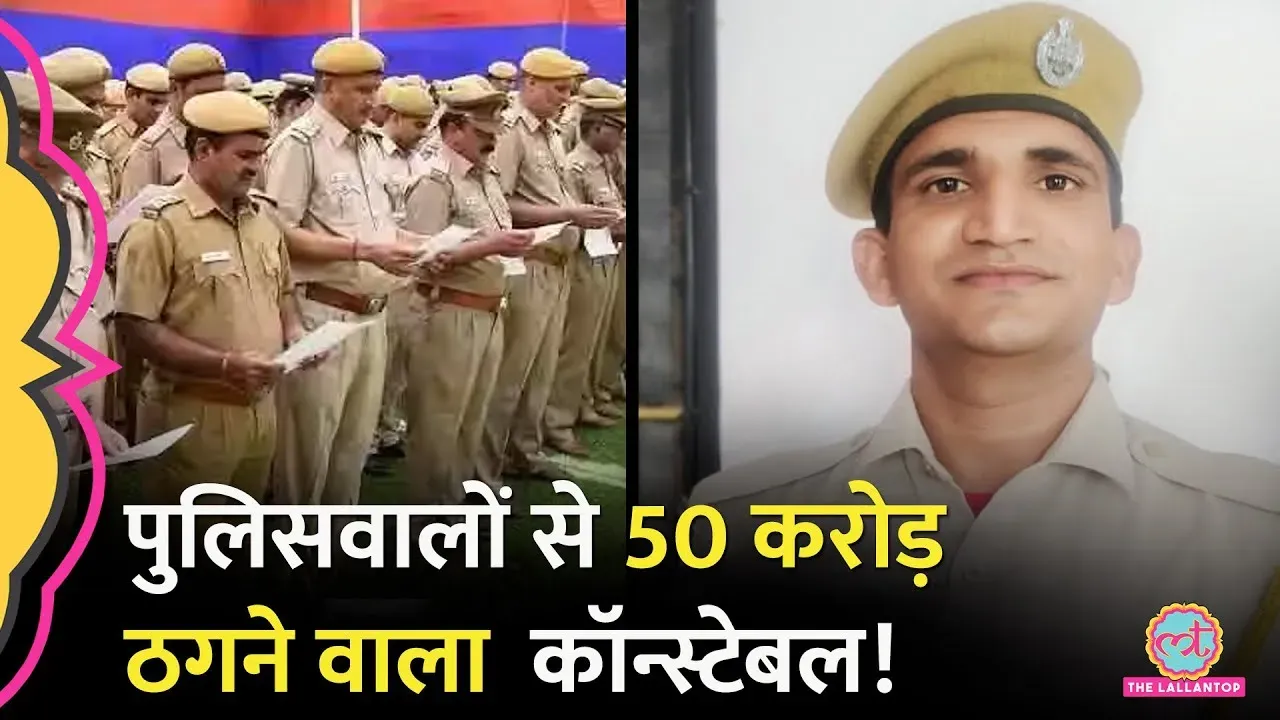डॉ. भीमराव आंबेडकर ने हिन्दू धर्म की कुरीतियों पर जो कहा, उस पर तो खूब बात होती है. लेकिन अन्य धर्मों पर उनकी राय की उतनी चर्चा नहीं होती. ये चर्चा है भी तो सिर्फ अकादमिक दायरे तक ही सिमटी हुई. लेकिन कही-सुनी से बेहतर है पढ़ी-लिखी. खासकर बात जब धर्म या जाति की हो. 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सूबेदार और अंग्रेजी के मास्टर रामजी सकपाल और भीमाबाई के घर जन्मे बच्चे को मां ने नाम दिया भीमराव. पुरखों का गांव रत्नागिरि के अम्बाडवे में पड़ता था. तो सरनेम मिला अंबाडवेकर, जो आगे चलकर आंबेडकर हुआ. खूब पढ़ाई की. एमए, पीएचडी करके वकालत सब पढ़ा. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए.
'ईसाई या मुसलमान क्रूर रहे हैं, हिंदू मतलबी', बौद्ध धर्म अपनाने वाले आंबेडकर दूसरे धर्मों पर क्या कहते थे?
आंबेडकर ने सभी धर्मों को विस्तृत तौर पर पढ़ा और समझा. आखिर में उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना?


भारत वापस लौटे तो सार्वजनिक जीवन की शुरुआत बहिष्कृत हितकारिणी सभा के गठन के साथ शुरू की. 1927 के महाड़ सत्याग्रह ने उन्हें अस्पृश्य वर्ग के हितैषी के रूप में स्थापित किया. लेकिन हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, उस दिशा में बढ़ते हैं कि आंबेडकर अलग-अलग धर्मों पर क्या मत रखते थे?
मनुस्मृति को सांकेतिक रूप से जलाने और पुरुष सूक्त की व्याख्या के विरोध को उनके हिन्दू धर्म के विरोध के सांकेतिक कृत्य के तौर पर देखा जाता है. आंबेडकर द्वारा लिखे ‘फिलॉस्फी ऑफ हिंदुइज्म’ में उनका जातिवाद जैसी कुप्रथाओं से बैर, हिन्दू धर्म के प्रति उनकी अनुख का मुख्य कारण रहा. 1935 में महाराष्ट्र के नासिक में पड़ने वाली येवला नाम की जगह पर उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है लेकिन निश्चित तौर पर मैं हिन्दू रहते नहीं मरूंगा. ‘डॉ अम्बेडकर: लाइफ एंड मिशन’ नाम की किताब में धनंजय कीर लिखते हैं
जब आंबेडकर जुलाई 1942 में 4 अन्य लोगों समेत वायसराय की अधिशाषी परिषद का हिस्सा बने, तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि ये ऐतिहासिक है क्योंकि पहली दफा कोई भारतीय अस्पृश्य हिन्दू वर्ग से उठकर अधिशाषी परिषद की सदस्यता तक पहुंचा है. इसी के बाद आंबेडकर ने बॉम्बे प्रांत की एक सभा में कहा कि दलित वर्ग को मिली अधिशाषी परिषद की एक सीट ब्राह्मणवाद के लिए घातक चोट की तरह साबित होगी.
आपने आंबेडकर के हिन्दू धर्म से अलगाव और जाति व्यवस्था के कारण विरोध के किस्से खूब सुने होगे लेकिन अन्य धर्मों के बारे में क्या ख्यालात थे, ये भी जान लेते हैं.
हिंदू vs मुस्लिममाना जाता है कि आंबेडकर भारतीय मूल वाले धर्म (माने बौद्ध, जैन और सिख धर्म) को अपनाने को लेकर जितना निश्चित थे उतना एकेश्वरवादी सिद्धांत वाले धर्मों पर नहीं थे. उनका मानना था कि एकेश्वरवादी सिद्धांत भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति में फिट नहीं बैठता. अपनी किताब ‘एनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ में आंबेडकर ने लिखा..
हिंदू, मुस्लिमों की आलोचना इस स्तर पर करते हैं कि मुसलमानों ने तलवार की दम पर धर्म का प्रसार किया. कमोबेश इसी अन्वेषण पर ईसाईयत को भी कोसा जाता है. लेकिन ज़ाहिर तौर पर किसे बुरा माना जाए, ईसाई को, मुस्लिमों को या फिर हिंदुओं को, जिन्होंने अपने ही कुछ लोगों को अंधेरे में रखा. तो मुझे यह कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि ईसाई या मुसलमान क्रूर रहे हैं, लेकिन हिंदू मतलबी.
भारत के बाहर की गतिविधियों और नृजातीय एकता को भी आंबेडकर ने खुल कर चुनौती दी. आंबेडकर ने दूसरे विश्व युद्ध में तानाशाही और लोकतंत्र में से लोकतंत्र का खुला पक्ष लिया. 1942 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस के भाषण के अंत में उन्होंने अपना प्रख्यात उद्धहरण दिया था -
शिक्षित हो, आंदोलित हो और संगठित हो.
उन्होंने इसे बैटल ऑफ फ्रीडम के तौर पर लेते हुए कहा था
जब न्याय हमारे साथ है तो हम कैसे हार सकते हैं. यह लड़ाई मेरे लिए खुशी का विषय है. यह मेरे लिए पूर्णतया आत्मिक और आध्यात्मिक है. यह लड़ाई सत्ता या संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि मानव व्यक्तित्व को पुनर्स्थापित करने की है.
सभी अब्राहमिक धर्मों में से आंबेडकर इस्लाम के ज्यादा आलोचक माने जाते थे. 1940 में छपी अपनी किताब 'Pakistan or Partition of India' में आंबेडकर ने लिखा…
The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is a brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity.
इसका हिंदी में अनुवाद करें तो आंबेडकर कहते थे…..
इस्लाम के भाईचारे का तात्पर्य मानवीय सार्वभौमिक भाईचारे से नहीं है. ये सिर्फ मुस्लिमों का मुस्लिमों से भाईचारा है. बंधुत्व के भाव में फायदा सिर्फ उसी बिरादरी तक सीमित है, इसके दायरे से जो भी बाहर है उसके लिए सिर्फ शत्रुता और तिरस्कार है.
इसी पुस्तक में आगे आंबेडकर ने लिखा था कि इस्लाम के लिए हिंदू या गैर धर्म के लोग काफिर हैं, जो अगर इस तरफ आए भी तो हाशिए पर ही रहेंगे.
सिख धर्म1935 में जब आंबेडकर ने हिंदू धर्म से अलगाव की घोषणा की तो शुरुआती विकल्प के रूप में सिख धर्म को समझना आरंभ किया. जात पात तोड़क मंडल के कार्यक्रम को छोड़कर सिख मिशन की कॉन्फ्रेंस में अमृतसर पहुंचे आंबेडकर ने महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन की तुलना में सिख पंथ के उत्थान को क्रांतिकारी माना था. उनका मानना था कि राजनैतिक क्रांति से पहले हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांति उपजती है. यहां दिए अभिभाषण में उन्होंने कहा
हिन्दुओं के धर्मांतरण के नजरिये से ईसाईयत, इस्लाम और सिख पंथ में सबसे सटीक विकल्प सिख धर्म है. क्योंकि ईसाई या मुस्लिम बनने पर दलित हिन्दू संस्कृति से भी अलहदा हो जाएगा जबकि सिख धर्म मूलतः भारतीय जमीन पर पनपा धर्म है इसलिए यहां सांस्कृतिक निरंतरता बरकरार रहेगी. अगर दलित, इस्लाम स्वीकारते हैं तो मुस्लिमों की आबादी दोगुने तक जा सकती है और इस्लामी हुकूमत का खतरा फिर से मंडराएगा. इसके अलावा अगर अस्पृश्य लोग ईसाई धर्म की ओर जाएंगे तो वे जाने-अनजाने में भारत पर ब्रितानी हुकूमत को मजबूती देंगे.
लेकिन कुछ ऐसा रहा कि जल्दी ही सिख पंथ से भी उनका मोहभंग हो गया. आंबेडकर का संपर्क जब दलित सिख वर्ग, मज़भी सिख (मजहबी सिख) और रविदासी तबके से हुआ तो सिख पंथ के अंदरूनी बंटवारे से उनका ये विकल्प हमेशा के लिए खत्म हो गया. इसके बाद आंबेडकर ने जैन धर्म को समझने का प्रयास किया. बौद्ध की ही तरह जैन धर्म भी वैदिक धर्म सुधार के प्रत्युत्तर के रूप में उपजा था. इसलिए आंबेडकर का जैन धर्म के प्रति झुकाव कबीर के दोहे की तरह रहा _
कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर.
न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर.
कर्म सिद्धांत, अहिंसा और पुनर्जन्म पर लगभग दोनों ही धर्मों का एक जैसा प्वाइंट ऑफ व्यू है. आंबेडकर कहते हैं कि बुद्ध का कर्म सिद्धांत और जैन धर्म का कर्म सिद्धांत सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन जैन धर्म में कर्म सिद्धांत आत्मा पर आधारित है और बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को ही नकारता है. बुद्ध का कर्म सिद्धांत केवल कर्म पर आधारित है जिसका प्रभाव इसी जीवन पर दिखाई देगा. दूसरे शब्दों में कहे तो डॉ आंबेडकर उस कहावत को मानते दिखते हैं ‘जैसा बोओगे वैसा काटोगे’.
फिर जैन धर्म के सिकुड़ने के मुख्य कारक यानि अहिंसा के प्रति अतिवादी झुकाव को भी आंबेडकर ने प्रैक्टिकल अप्रोच से दूर पाया. बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से कर्णिका दुबे अपने शोध में लिखती हैं कि सबके बावजूद आंबेडकर धर्म को सार्वजनिक ज़िंदगी के लिए अनिवार्य मानते थे. लेकिन सभी मजहब अच्छे है, आंबेडकर इस बात को सिरे से पुरजोर तरीके से खारिज करते थे. आंबेडकर कहते थे कि
धर्म का इतिहास, क्रांति का इतिहास होता है, ये क्रांति ही दर्शन की जनक है.
ये बड़ा दिलचस्प है कि हिंदुत्व या इस्लाम की इतनी आलोचना करने के बाद भी आंबेडकर हमेशा धर्म के होने को जिन्दगी में ऑक्सीजन मानते रहे. गौरतलब है कि आंबेडकर धर्म के जीवन में होने के पक्के समर्थक थे, वे खिलाफ थे तो धर्म के कारण पहचान के संकुचित होने पर.
बौद्ध धर्मआंबेडकर का मानना था कि सभी धर्म कहीं न कहीं मोक्ष की बातें करते हैं लेकिन बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो मोक्ष की जगह मार्ग की बात करता है. उनका मानना था कि बौद्ध संघ महासागर की तरह है जिसमें मिलने के बाद गंगा या महानदी से आने वाले पानी की पहचान करना नामुमकिन हो जाता है.

अंतिम दिनों में आंबेडकर ने अपने 3 लाख 65 हज़ार समर्थकों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हिंदू धर्म त्यागकर बौद्ध धर्म के भीतर नवयान धारा को जन्म दिया. दीक्षाभूमि, नागपुर में आज भी उनकी प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाएं स्तम्भ पर दर्ज हैं.
देखा जाए तो आंबेडकर ने 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वाले व्याख्यान में हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की और करीब 20 साल तक अलग अलग धर्मों के विकल्पों को बारीकी से समझा और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जाकर 1956 में प्रज्ञा, करुणा और समता को मुख्य तीन आधार बना कर बौद्ध धर्म को अपनाया.
वीडियो: तारीख: अलग-अलग धर्मों पर क्या सोचते थे डॉ बी आर आंबेडकर?


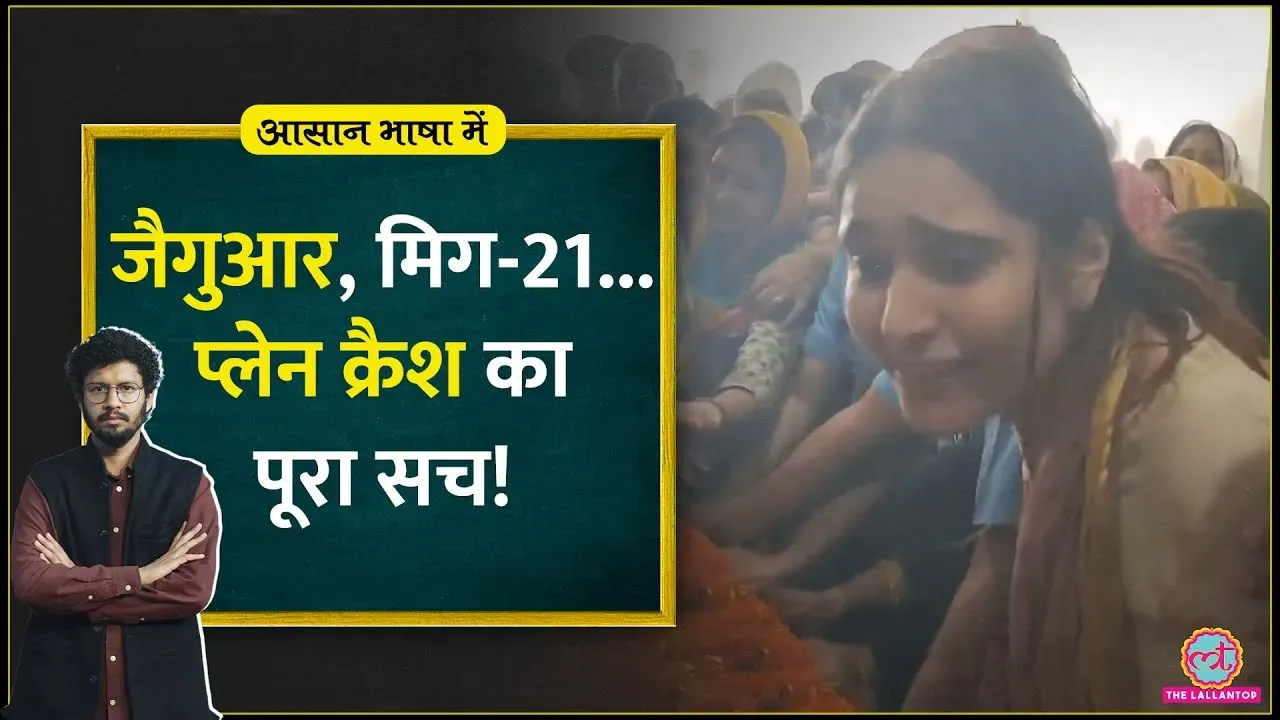
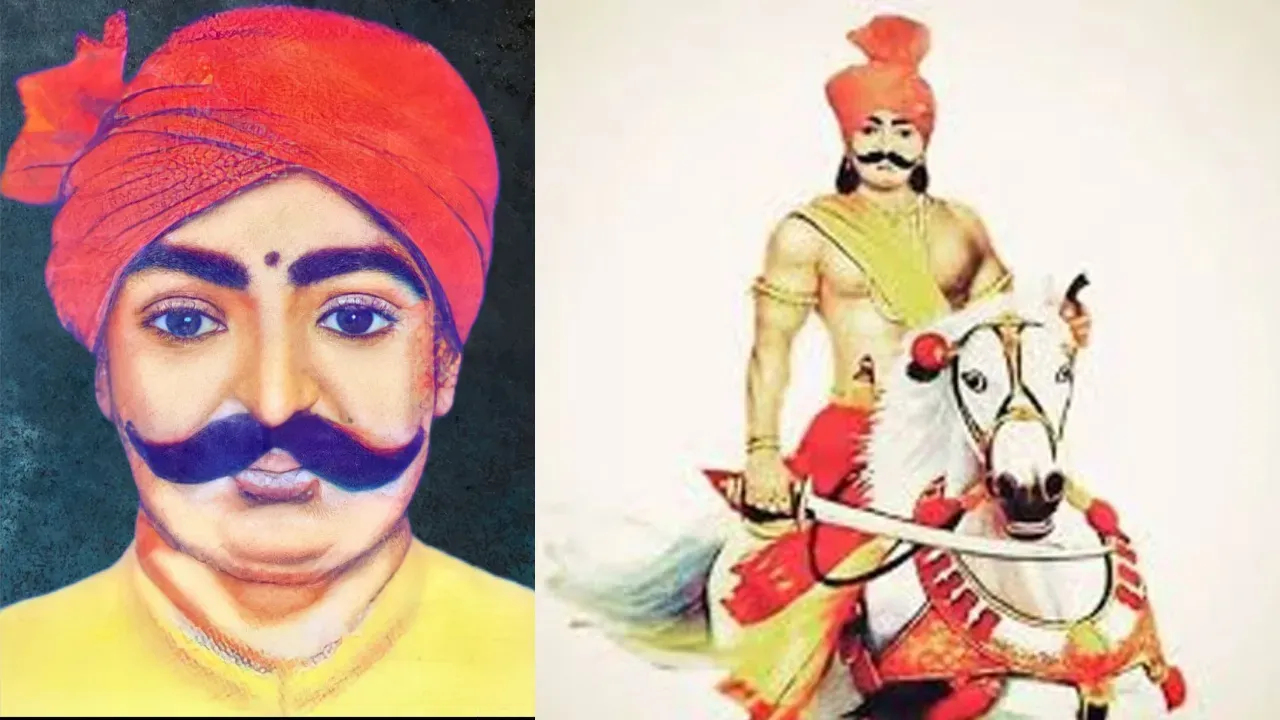

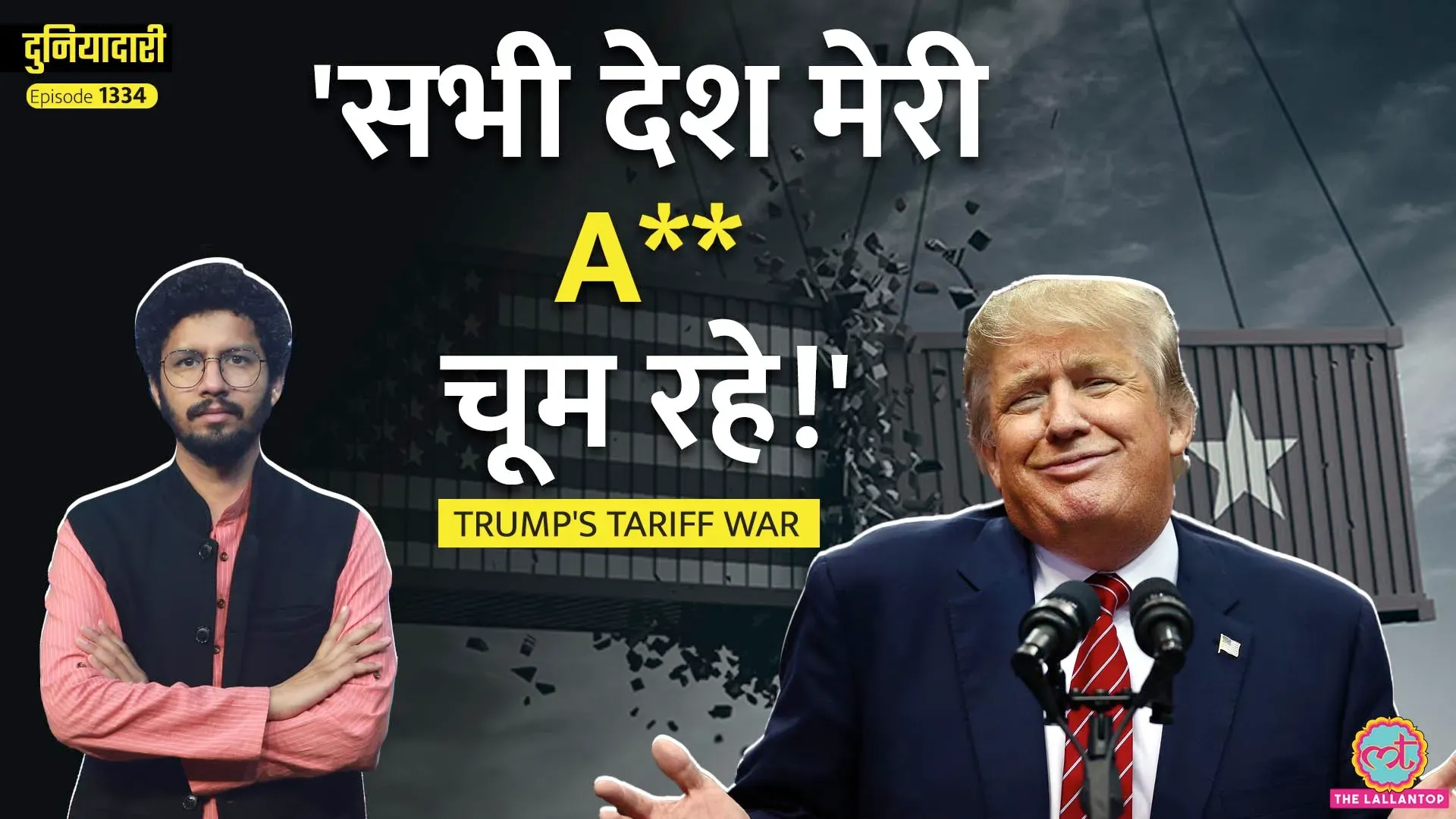


.webp)