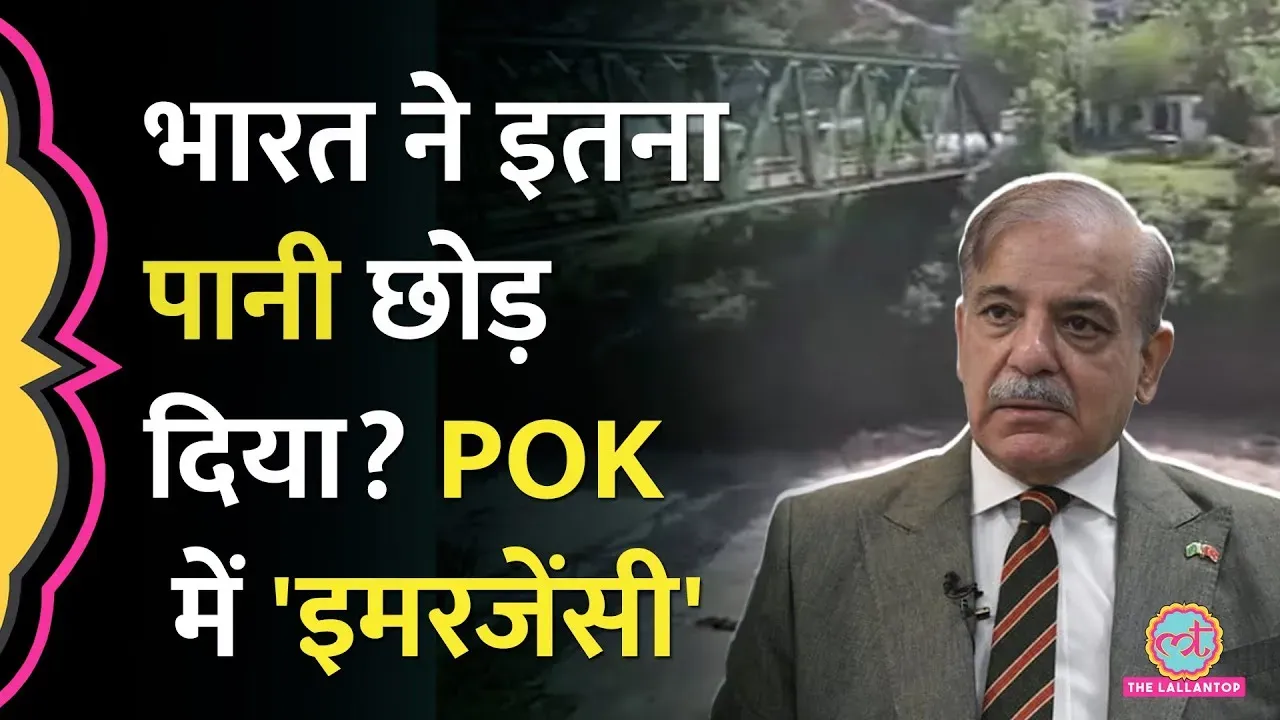कुछ लोग दहेज के इस पहलू पर ज़ोर देते हुए कहते हैं कि महिलाओं के सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकारों को मज़बूत किए बिना दहेज का बहिष्कार करना बेमानी होगा क्योंकि विवाह के बाद ससुराल में सम्पत्ति के नाम पर उनके पास यही एक बड़ा सहारा होता है.
हमारे समाज की कई कुरीतियों में से एक दहेज पर हर तरह की संभ्रांत बैठकों में आपको बातें होती दिख जाएंगी. मुमकिन है कि आधे घंटे के भीतर ही उस बैठक में आपको लगने लगे की दहेज जैसी कुप्रथा बस ख़त्म होने ही वाली है. लेकिन क्या ऐसा वाकई में हुआ? जवाब है नहीं. ऐसी बैठकें सालों से होती चली आ रही हैं और हर कोई इसकी बुराई करता दिखता है, मगर दहेज प्रथा हमारे समाज की ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता. लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों इतनी बातें होने और कुप्रथा का दर्जा मिलने के बावजूद धड़ल्ले से दहेज़ लेने और देने का काम जारी है? इस सवाल का जवाब नारीवादी लेखिका निवेदिता मेनन ने अपनी किताब
'सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट' (Seeing Like A Feminist) में देने की कोशिश की है. मूलतः किताब अंग्रेजी में है लेकिन नरेश गोस्वामी ने इस किताब का हिन्दी अनुवाद किया है और राजकमल प्रकाशन ने इसे 'नारीवादी निगाह से' नाम से छापा है. आइए पढ़ते हैं इस पुस्तक का अंश जिसमें दहेज़ जैसी कुप्रथा पर अन्य नारीवादी विद्वानों की राय के साथ निवेदिता मेनन ने अपनी बात कही है.
नारीवादी निगाह से - निवेदिता मेनन
दहेज क्या है?
अब हम एक ऐसे मुद्दे की तरफ़ बढ़ते हैं जिसे लेकर कहीं कोई मतभेद दिखाई नहीं देता—दहेज एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुराई चारों तरफ़ की जाती है. लेकिन सवाल ये है कि दहेज होता क्या है? इस प्रथा का अध्ययन करनेवाले विद्वानों का कहना है कि समय के साथ इसका स्वरूप इतना बदल चुका है और विवाह की रस्म में भेंट-उपहार देने के इतने तरीक़े पैदा हो चुके हैं कि अब उसे परिभाषित करना मुश्किल हो गया है. लेकिन एक स्थूल रूप में इसे माता-पिता द्वारा बेटियों को अपनी मृत्यु से पहले पैतृक सम्पत्ति में दिए जानेवाले उत्तराधिकार की तरह देखा जा सकता है. हम जानते हैं कि सम्पत्ति के उत्तराधिकार की दृष्टि से लड़कियों की स्थिति कमज़ोर ही रहती है. कुछ लोग दहेज के इस पहलू पर ज़ोर देते हुए कहते हैं कि महिलाओं के सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकारों को मज़बूत किए बिना दहेज का बहिष्कार करना बेमानी होगा क्योंकि विवाह के बाद ससुराल में सम्पत्ति के नाम पर उनके पास यही एक बड़ा सहारा होता है. लेकिन, कुछ अन्य लोगों का मानना यह है कि दहेज का लेन-देन दो परिवारों के पुरुषों के बीच सम्पन्न होता है जिसमें वधू के साथ आए दहेज पर उसके बजाय उसके पति और ससुराल वालों का नियंत्रण रहता है. 1980 के बाद दक्षिण एशिया में दहेज के साथ हिंसा भी जुड़ गई है.
अब दहेज दिया नहीं जाता, उसकी मांग की जाती है; अपने साथ पर्याप्त दहेज न लानेवाली महिलाओं के साथ ससुराल में मार-पीट और यातनादायी बर्ताव किया जाता है.
नारीवादी लेखिका सी.एस. लक्ष्मी दहेज को विवाह की अनिवार्य प्रकृति से जोड़कर देखती हैं. उनकी नज़र में दहेज का एक सिरा महिलाओं के अपने मातृ-परिवार से अलगाव के साथ भी जुड़ा है. लेखिका हमें एक सवाल के बारे में बताती है जो बीसवीं सदी के शुरुआती दौर में समाज-सुधार और दहेज-विरोध की मुहिम चलानेवाली प्रसिद्ध कार्यकर्ता सिस्टर सुब्बालक्ष्मी से पूछा गया था :
‘अगर दहेज न देने पर लड़कियों का विवाह ही न हो पाए?’
इस पर सिस्टर सुब्बालक्ष्मी का जवाब यह था : ‘तो फिर लड़कियों को गरिमा और हिम्मत के साथ अकेले जीने का फ़ैसला करना चाहिए.’
कुछ नारीवादी विद्वानों का मानना है कि इस दृष्टि से दहेज में निहित मसलों की पश्चिमी के पितृसत्तात्मक तंत्रों में महिलाओं की स्थिति से भी तुलना की जा सकती है. इसका मतलब है कि जेंडर-आधारित अधीनस्थता विषमलिंगी विवाह, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के मामले में महिलाओं के साथ भेदभाव तथा महिलाओं के साथ की जानेवाली व्यापक शारीरिक-संरचनात्मक हिंसा के राजनीतिक अर्थशास्त्र में गुंथी हुई है. कहने का आशय यह है कि दहेज से सम्बन्धित हिंसा कोई अनूठी चीज़ नहीं है, वह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग रूप-रंग में व्याप्त जेंडर-आधारित हिंसा का एक दक्षिण एशियाई नमूना-भर है. (बसु 2009) श्रीमति बसु का तर्क है कि दहेज निषेध अधिनियम (1984 में संशोधित) इसलिए कारगर नहीं हो पाया क्योंकि वह समाज में पैवस्त उन तौर-तरीक़ों का कुछ नहीं कर सकता जिनके ज़रिये दहेज का लेन-देन किया जाता है. यह अधिनियम तभी प्रभाव में आता है जब दहेज के मामले में शिकायत दर्ज की जाती है.
इस सम्बन्ध में यह बात भी याद रखी जानी चाहिए कि दहेज से सम्बन्धित शिकायतों में इसके औचित्य पर सवाल नहीं उठाया जाता; शिकायत केवल तब की जाती है जब कोई ‘बेतुकी’ मांग करता है या दहेज दे दिए जाने के बावजूद और ज़्यादा दहेज की मांग करता है.
इस प्रसंग में यह भी ग़ौरतलब है कि अधिनियम में दहेज लेने या देनेवाले को बराबर का दोषी माना गया है, इसलिए होता यह है कि मौत या क़ानूनी पेंचों जैसी गम्भीर परिस्थितियों के अलावा कोई भी पक्ष दहेज की शिकायत दर्ज करने से परहेज करता है. मिसाल के तौर पर, दिल्ली की एक सेशन अदालत ने 2009 में एक महिला द्वारा अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़ दायर की गई एक दहेज सम्बन्धी हिंसा की घटना पर फ़ैसला सुनाते हुए महिला के पिता को भी दहेज देने का दोषी क़रार दिया था. यही वजह है कि दहेज के मुद्दे पर काम करनेवाले कई महिला संगठन दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेने के बजाय आर्थिक निर्भरता, आवास के विकल्पों और घरेलू हिंसा जैसे उन अन्य क़ानूनी उपायों को ज़्यादा तरजीह देते हैं जो विवाह से जुड़ी समस्याओं को ज़्यादा गहराई से पकड़ते हैं. क़ानून के इन वैकल्पिक उपायों में तलाक़ की प्रक्रिया के साथ इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि अगर तलाक़ की स्थिति में दहेज का सामान नहीं लौटाया जाता तो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत इस कृत्य को आपराधिक कृत्य घोषित किया जाए. महिला संगठनों को इसके अलावा, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किए गए क्रूरतापूर्ण बर्ताव के लिए धारा 498ए तथा घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) जैसे उपाय ज़्यादा कारगर लगते हैं.
ग़ौरतलब है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत पीड़ित महिला को पति के घर में रहने का अधिकार दिया गया है.
दहेज की प्रथा मूलत: उत्तर भारत की ऊंची जातियों में प्रचलित थी, लेकिन धीरे-धीरे वह भारत के तमाम वर्गों, जातियों, क्षेत्रों और धर्मों में व्याप्त हो गई है. दहेज प्रथा के इस फैलाव को विद्वान ‘संस्कृतिकरण’ (ऊंची जातियों के रहन-सहन का अनुकरण), बढ़ते उपभोक्तावाद और बाज़ारीकरण; तथा नवें दशक में उभरी उदारवादी अर्थव्यवस्था में नकद आय के बढ़ते लेन-देन का मिला-जुला परिणाम मानते हैं. (टोमालिन 2009) मैं दहेज की जबरन मांग और इसके साथ जुड़ी हिंसा को दूसरी तरह देखती हूं. मेरा कहना है कि यह परिघटना विवाह के एक ख़ास रूप की धीरे-धीरे बढ़ती स्वीकार्यता का परिणाम है. बीसवीं सदी के आख़िर तक विवाह का यह रूप भारत में बहुत हद तक स्वाभाविक मान लिया गया था. दूसरे शब्दों में, इस समय तक विवाह और सम्पत्ति-हस्तान्तरण के पूर्व-स्थापित रूपों को पछाड़ते हुए विवाह का पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृ-स्थानिक (विरिलोकल) रूप सर्वप्रमुख और सार्वभौम बन गया. भारत के प्रत्येक समुदाय में दहेज का प्रचलन इस बात का सुबूत है कि हर समुदाय में विवाह का वही रूप स्थापित हो चुका है जिसमें शादी के बाद लड़की को पति के घर जाकर एक नए परिवेश में जीना या उससे जूझना पड़ता है; और विवाह के इस प्रकार में महिला को पत्नी के रूप में सम्पत्ति के सीमित, और बेटी के रूप में कभी कोई अधिकार नहीं दिया जाता. जब तक परिवार के इस ढांचे को प्राकृतिक और अवश्यम्भावी तथा विवाह के एक प्रकार विशेष को सबके लिए अनिवार्य माना जाता रहेगा तब तक ‘दहेज की बुराई’ से लड़ने की तमाम कोशिशें विफल होती रहेंगी. दहेज की समस्या परिवार के समकालीन स्वरूप को बदले बिना दूर नहीं की जा सकती.










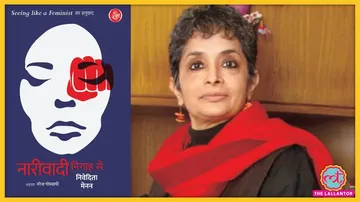




.webp)