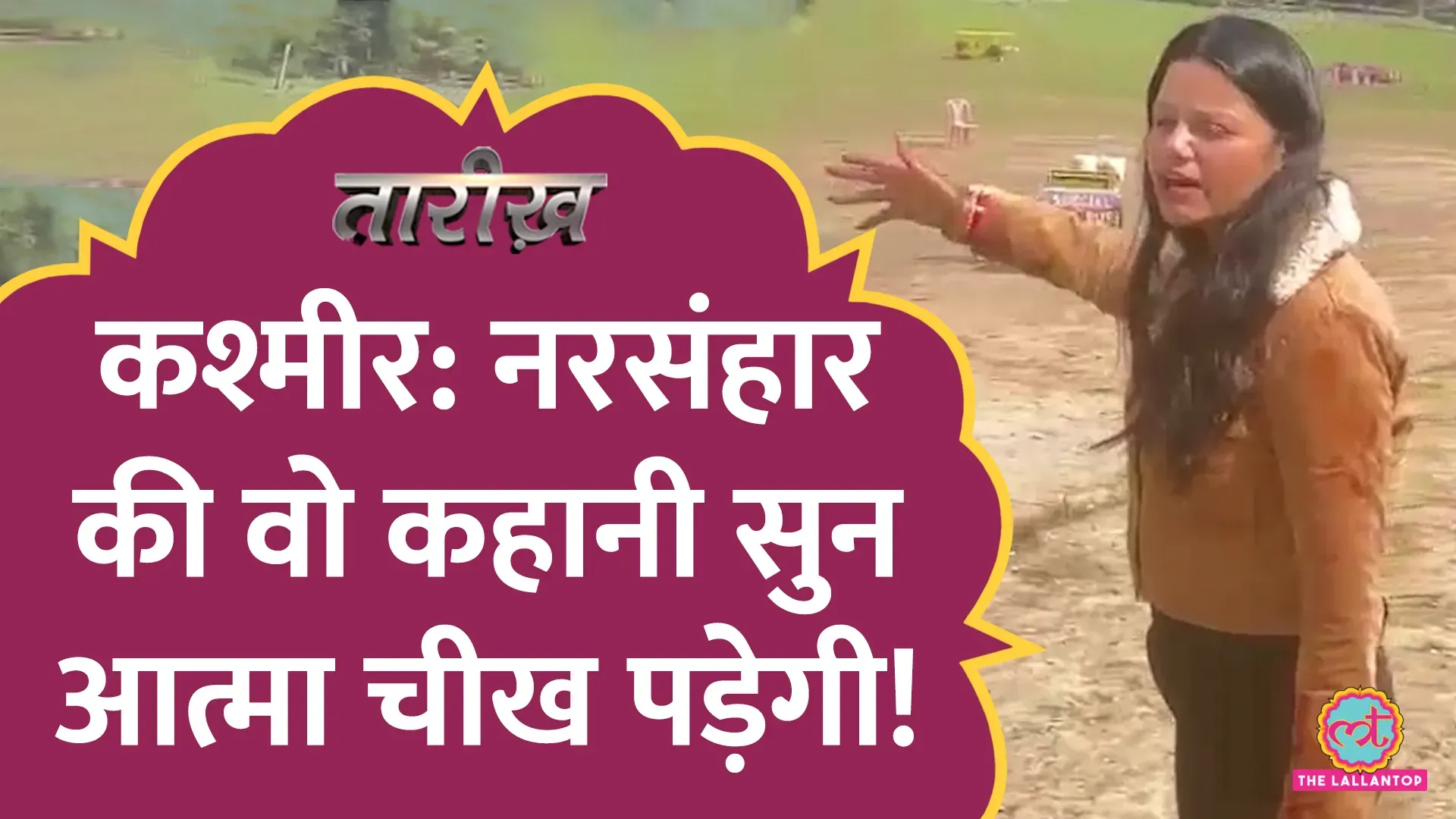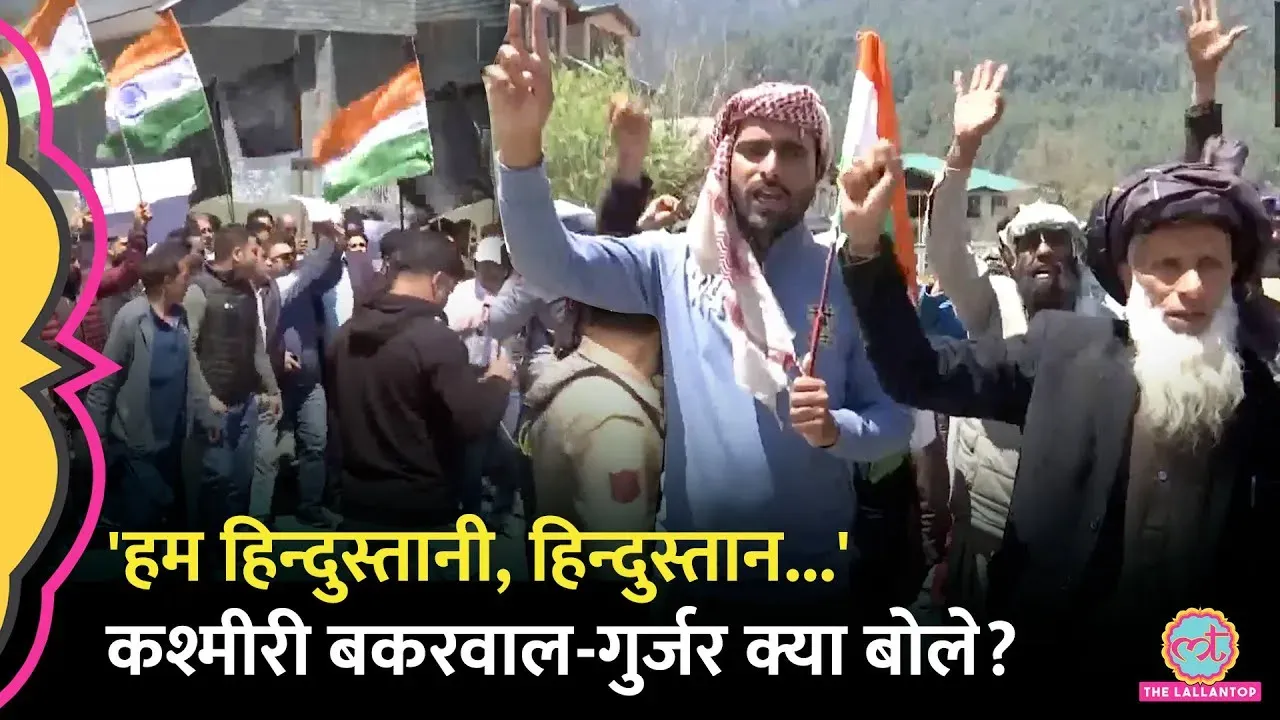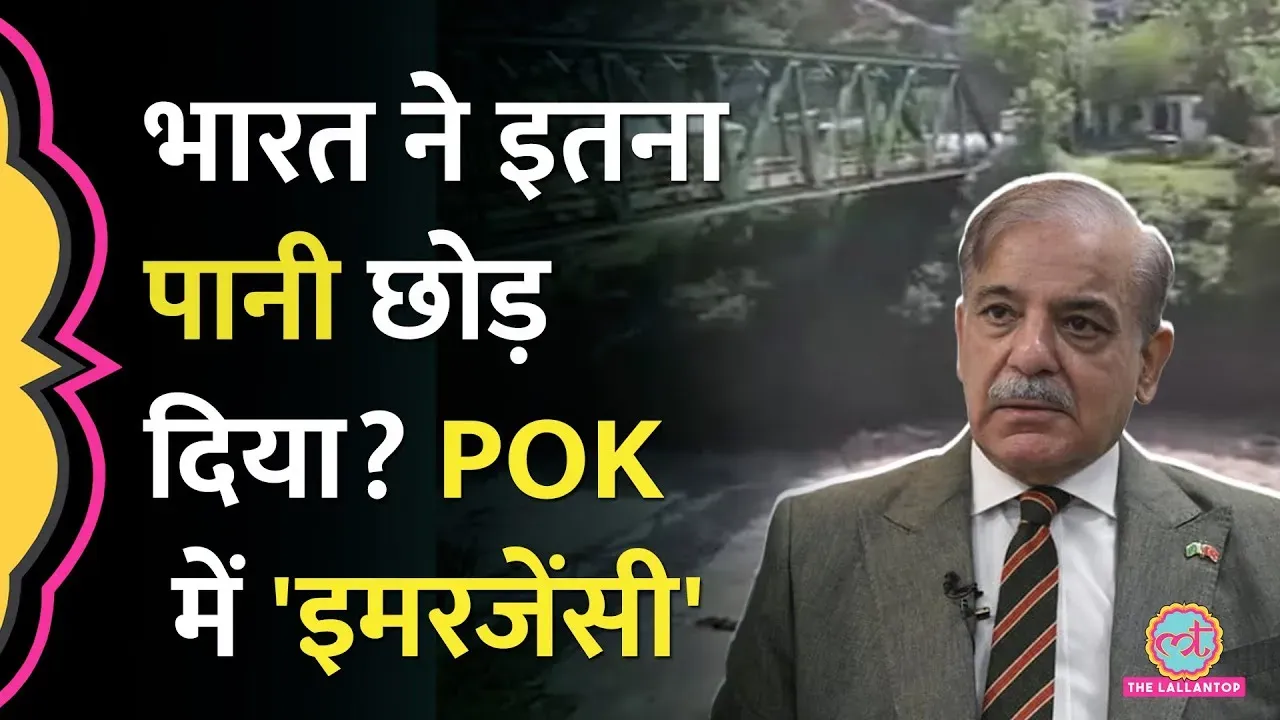हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घर या आसपास कुछ बदलाव हो जाएं तो चीजें एकदम से ध्यान खींचती हैं. यही वजह थी कि मेरे ऑफिस के रास्ते में पड़ने वाले पुलिस स्टेशन पर जब नए बोर्ड लगे तो एकाएक ध्यान उधर चला गया. माने पुलिस स्टेशन है ये तो पता था, गाहे-बगाहे देख भी लेते थे. मगर बोर्ड नया था तो उस पर लिखी जानकारियां भी पढ़ीं. और पढ़ने के बाद समझ आया कि नए बोर्ड ने एक नया कंफ्यूजन दिमाग को 'तोहफे' में दे दिया है.
कमिश्नरेट, थाना, कोतवाली, चौकी में फर्क क्या है? बहुत काम आएगा ये पुलिसिया ज्ञान
किस मामले को दर्ज कराने कहां जाना चाहिए, कहां किस लेवल के अधिकारी बैठते हैं, आज सब जानें.

वजह ये थी कि एक ही पुलिस स्टेशन को थाना भी लिखा गया था और चौकी भी. अब तक जो पढ़ा-जाना था, उसके हिसाब से तो ये दोनों अलग हुआ करते थे, फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक ही स्टेशन पर दोनों तरह के बोर्ड थे. जब दिमाग में ये बात घुसी तो उसे निकालने का एक ही तरीका था कि किसी जानकार व्यक्ति से ठीक-ठीक बात का पता कर लिया जाए. तो हमने वही किया. और जो पता चला आपको भी बता दे रहे हैं. पर उससे पहले आप वो बोर्ड तो देख लीजिए जिसकी वजह से ये सब लिखने की जिज्ञासा हुई.

ये बोर्ड देखकर जानने की इच्छा हुई कि थाना और कोतवाली में क्या अंतर होता है, चौकी और बीट इनसे कैसे अलग हैं, किस मामले को दर्ज कराने कहां जाना चाहिए, कहां किस लेवल के अधिकारी बैठते हैं और इन सभी स्टेशन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है.
इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हुए राजस्थान के भरतपुर में आईजी के पद पर तैनात राहुल प्रकाश से हमने बात की और इन सभी पुलिस स्टेशनों के बीच के अंतर और कामकाज को समझने की कोशिश की. राहुल ने कोतवाली और थाने के बीच का सबसे बड़ा फर्क बताया.
भरतपुर IG राहुल प्रकाश ने सबसे पहले ये समझाया कि जिले में पुलिस व्यवस्था चलती कैसी है. उन्होंने बताया,
सबसे ऊपर फील्ड पुलिसिंग में आता है जिला. एक डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस अधीक्षक या जिसको हम एसपी बोलते हैं यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पूरे जिले के इंचार्ज होते हैं. हेड होते हैं. ये जिले की सभी पुलिस व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं और निर्देशित करते हैं. उसके नीचे सर्किल्स होते हैं जिनमें एक डिप्टी SP रैंक के ऑफिसर बैठते हैं. उनको हम लोग पुलिस उपाधीक्षक बोलते हैं और बीच में एक एडिशनल एसपी भी होते हैं. हालांकि, आमतौर पर उनका अलग से सेक्टर नहीं होता. कहीं-कहीं सेक्टर बनता है. और इसमें जो सबसे अंतिम और इंपॉर्टेंट कड़ी है वो है पुलिस स्टेशन. इसको हम थाना बोलते हैं.
राहुल प्रकाश के मुताबिक, कोतवाली शब्द आज के समय में किसी एक थाने के लिए यूज किया जाता है. पहले शहर कोतवाल हुआ करते थे. पूरे शहर में एक ही थाना हुआ करता था, उसे कोतवाली बोलते थे. आज के टाइम में एक शहर में 4, 5, 10 और यहां तक कि बड़े शहर में आपको 40-50 थाने भी मिलेंगे. उनमें से कोई एक थाने को कई जगह परंपरागत तौर पर कोतवाली का नाम दिया जाता है. असल में कोतवाली किसी एक पुलिस यूनिट का नाम नहीं है, वो कई जगहों पर एक थाने को ही बोलते हैं. ज्यादातर वो शहर वाला थाना होता है.
चौकियां क्या होती हैं?इसके नीचे आती हैं चौकियां. इनको हम आउटपोस्ट भी बोलते हैं. राहुल प्रकाश के मुताबिक, जिस पुलिस थाना क्षेत्र में ज्यादा फैलाव होता है या कुछ अन्य महत्वपूर्ण कस्बे या जंक्शन होते हैं वहां पर अगर ऐसी जरूरत लगती है कि पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जानी चाहिए तो वहां पर एक पुलिस थाने का एक्सटेंशन होता है. ये पुलिस चौकी के रूप में स्थापित किया जाता है. यहां कुछ पुलिसकर्मी तैनात होते हैं. इसके इंचार्ज कई बार हेड कांस्टेबल रैंक के अधिकारी होते हैं. कई बार ASI रैंक अधिकारी होते हैं और कई बार सब इंस्पेक्टर (SI) रैंक अधिकारी होते हैं.
थाने और चौकी में अंतरभरतपुर पुलिस से बातचीत में थाने और चौकी का जो मूल अंतर समझ आया वो ये है कि चौकियों पर मुकदमे दर्ज नहीं होते. FIR दर्ज नहीं होती है. जबकि, थाने पर FIR दर्ज होती है. CrPC के तहत FIR दर्ज करने का अधिकार SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर को ही होता है, जो थाने का इंचार्ज होता है.
बीट क्या है?बीट के अंतर्गत बेसिकली पूरे थाने क्षेत्र को प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक-एक कांस्टेबल को जिम्मेदारी देते हुए अलग-अलग भागों में बांट दिया जाता है. उदाहरण के लिए, कोई एक मोहल्ला किसी एक कांस्टेबल की बीट होती है. दूसरे बीट की जिम्मेदारी किसी अन्य कांस्टेबल की होगी. अब उस क्षेत्र के जो भी समन आते हैं, वारंट्स आते हैं, या कोई पुलिस वेरिफिकेशन आता है, वहां की कोई जानकारी लेनी है, कोई गुप्त सूचना लेनी है, ऐसी जिम्मेदारियां उस कांस्टेबल को देते हैं जिसे वहां का बीट कांस्टेबल नियुक्त किया गया हो. ये काम किसी एक्ट के तहत नहीं होता, किसी कानून के तहत नहीं होता है. ये महज एक प्रशासनिक विभाजन है.
कमिश्नरेट प्रणाली कैसे काम करती है?कई राज्यों में शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के तहत काम करती है. हमने आईजी भरतपुर से जाना कि ये व्यवस्था क्या है और ये अन्य पुलिसिंग सिस्टम से कैसे अलग है. इस पर IG राहुल प्रकाश ने बताया कि कमिश्नरेट प्रणाली उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मुंबई और दिल्ली में होती है. उन्होंने कहा,
कमिश्नरी या पुलिस कमिश्नरेट में और नॉर्मल पुलिस में जो एक बेसिक फर्क है वो है मैजिस्टिरियल पावर का. जहां कमिश्नरेट होता है वहां पर पुलिस कमिश्नर के पास मैजिस्टिरियल पावर होती हैं. जबकि दूसरे जिलों में ये शक्तियां कलेक्टर के पास होती हैं. आपने सुना होगा कलेक्टर का पदनाम कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. उनको ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरफ तो वो कलेक्टर का काम कर रहे होते हैं, साथ ही उनके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी पावर्स होती हैं. कमिश्नरेट में वो पावर्स पुलिस के पास आ जाती हैं.
कमिश्नरेट को आमतौर पर 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में बनाया जाता है. इसका उद्देश्य होता है निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाना. क्योंकि अन्य जिलों में मैजिस्टिरियल पावर कलेक्टर के पास होते हैं और पुलिसिंग के पावर एसपी के पास होते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में दोनों को साथ में मिलकर के निर्णय लेना पड़ता है. उसमें कभी-कभी ऐसा महसूस किया जाता है कुछ लेवल पर निर्णय लेने में विलंब होने की भी संभावना होती है.

जबकि कमिश्नरेट में दोनों पावर एक ही अधिकारी के पास होती हैं, मैजिस्टिरियल और पुलिसिंग भी. जैसे धारा 144 लगाने की पावर है, धारा 151 में अरेस्ट करने के बाद व्यक्ति को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने की पावर है. मतलब जेल भेजने की अथॉरिटी से लेकर बहुत सारी चीजों में परमिशन देने तक की पावर शामिल हैं. जैसे हथियार लाइसेंस देने की पावर, धरना, रैली या जुलूस की अनुमति देने की पावर. इस तरह की अथॉरिटी आमतौर पर जिला कलेक्टर के पास होती है. पुलिस कमिश्नरेट में ये पावर पुलिस के पास आ जाती हैं.
FIR और MLC- FIR यानी फर्स्ट इनफॉरमेशन रिपोर्ट, 154 CrPC के अंतर्गत किसी भी थाने पर दर्ज होती है एसएचओ के द्वारा. किसी घटना या वारदात की जो पहली इनफॉरमेशन दर्ज की जाती है पुलिस की तरफ से, उसी को FIR कहते हैं. ये दर्ज होने के बाद ही जांच शुरू होती है.
- मेडिकल FIR होने के बाद की प्रक्रिया है. किसी दुर्घटना या वारदात में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से चोटिल होने, या मौत होने के बाद प्रभावित व्यक्ति/व्यक्तियों की मेडिकल डिटेलिंग के लिए डॉक्टर जो रिपोर्ट बनाते हैं उसको मेडिको लीगल रिपोर्ट (MLC) बोलते हैं. इस प्रक्रिया का विधिक महत्व है. MLC कोर्ट में सबमिट की जाती है. ये एक एविडेंस के तौर पर काम आता है. जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसको सजा दिलाने के प्रयास में इसका उपयोग होता है.
- IG राहुल प्रकाश ने बताया कि किसी भी स्टेट में जो पैरामिलिट्री फोर्सज होती हैं, जैसे सीआरपीएफ हैं या बीएसएफ, उसे भी पुलिस का ही हिस्सा माना जाता है. तो टॉप रैंकिंग ऑफिसर को कहते हैं डायरेक्टर जनरल (DG) और जो पुलिस को हेड करते हैं उनको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP).
- अब आप सोचेंगे DG और DGP में क्या फर्क हुआ? फर्क है विभाग का. पुलिस एक विभाग है. तो इसके हेड हो गए DGP. इसी तरह दूसरे विभाग के डीजी के साथ उस विभाग का नाम लग जाता है. जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी के लिए लिखेंगे DG (AC).
- विभाग के सबसे बड़े अधिकारी की सहायता के लिए बहुत सारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ADGP) होते हैं. ये अधिकारी DG के जस्ट नीचे के पायदान पर नियुक्त होते हैं और उनको जो भी कार्य डीजी की तरफ से दिया जाता है उसको पूरा करते हैं.

- उसके नीचे होते हैं इंस्पेक्टर जनरल (IG).
- उसके नीचे होते हैं सुपिरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP). जो किसी जिले के इंचार्ज होते हैं. इस पद का नाम अलग-अलग राज्यों में थोड़े अंतर के साथ लिया जाता है. जैसे यूपी में SSP भी बोला जाता है, लेकिन राजस्थान में हर जिले में SP पदनाम ही सुनाई देगा.
- अगर एसपी कमिश्नरेट के अंदर है तो उसको डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) बोलते हैं.
- SP के नीचे एडिशनल एसपी होता है, जो एसपी की मदद के लिए होते हैं.
- उसके नीचे डिप्टी एसपी होते हैं. ये डिप्टी सुपिरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं.
- इसी में कई बार ASP भी नाम आता है. जो असिस्टेंट सुपिरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है. जब कोई आईपीएस ऑफिसर अपने करियर के शुरुआती दिनों में DySP के तौर पर काम कर रहे होते हैं तो उनको ASP बोलते हैं. और अगर वो स्टेट पुलिस सर्विस के हैं तो उनको DSP बोलते हैं.
- इसके नीचे इंस्पेक्टर्स आते हैं जो कि पुलिस थाने के SHO होते हैं.
- उसके बाद SI. जिसको सब इंस्पेक्टर बोलते हैं. वो थाने में पदस्थ होते हैं. आमतौर पर वो अपने इंस्पेक्टर के द्वारा दिए गए कार्य को करते हैं.
- फिर आते हैं ASI होते हैं यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. जो आमतौर पर एक स्टार लगाते हैं कंधे पर. सब इंस्पेक्टर दो स्टार लगाते हैं और इंस्पेक्टर तीन स्टार लगाते हैं. इन तीनों में एक फीता लगा होता है.
- इन सबके बाद आता है हेड कांस्टेबल और उसके नीचे कांस्टेबल.
तो हमारे 'तोहफे' (पढ़ें इंट्रो) की तो अनबॉक्सिंग हो गई. उम्मीद है कि इस पिटारे से निकला ज्ञान आपके भी काम आए/आएगा.
वीडियो: पत्नी की मौत के बाद भी, UP पुलिस के जवान को नहीं मिली छुट्टी!