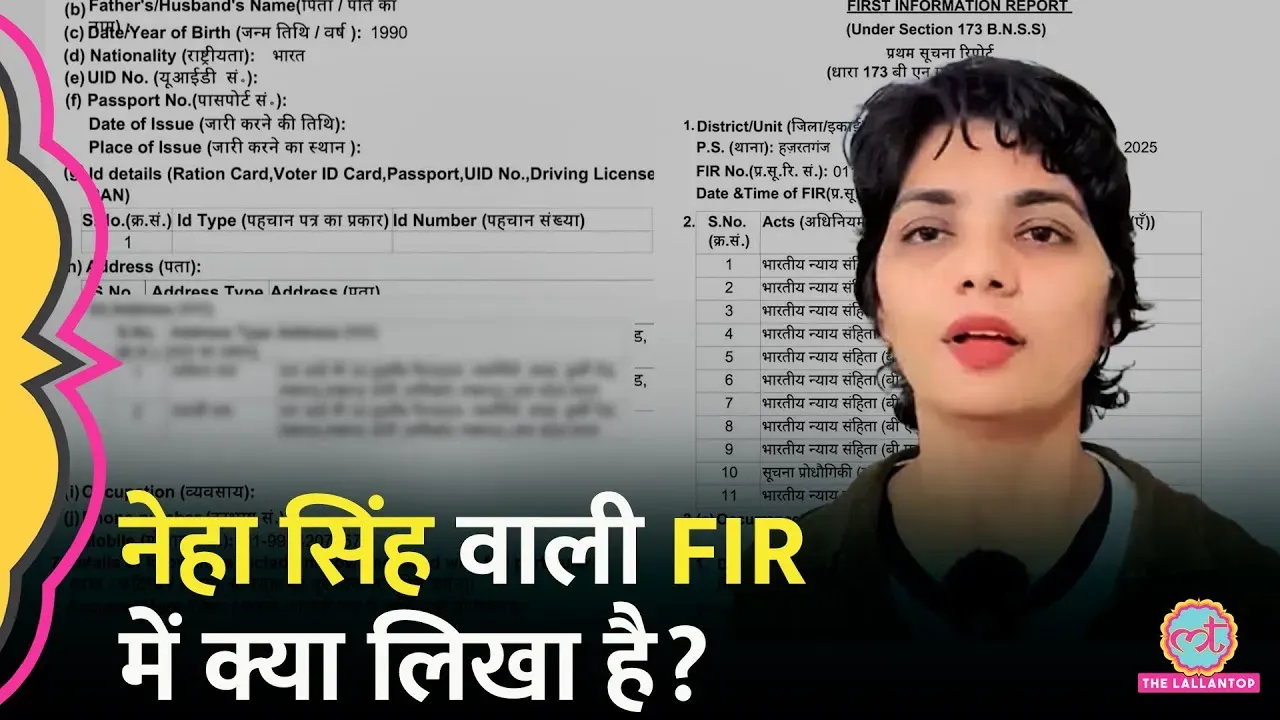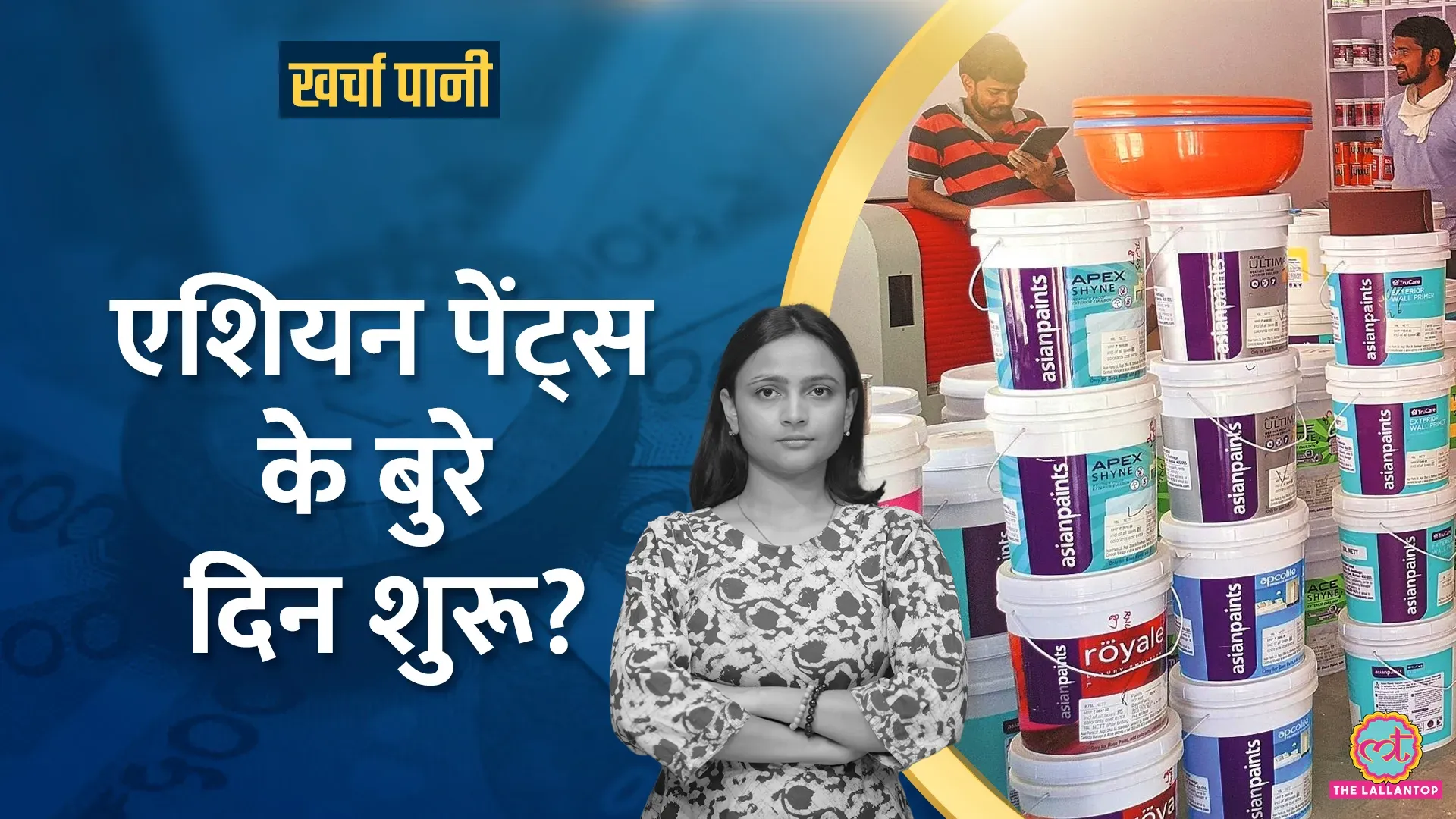अरुंधति रॉय की नई किताब आजादी एक निबंध-संग्रह है, जो अधिनायकवाद के बढ़ते वर्चस्व के दौर में दुनिया को स्वतंत्रता का अर्थ बतलाता है.
अरुंधति रॉय. 1997 में अपनी किताब 'द गॉड ऑफ़ स्माल थिंग्स' के लिए प्रतिष्ठित बुकर प्राइज जीतकर चर्चा में आयीं. उसके बाद अपने राजनीतिक विचारों और लेखों के लिए पहचानी जाने लगीं. हाल ही में इनकी एक किताब प्रकाशित हुई है, जिसका शीर्षक है- Azadi - Freedom, Fascism, Fiction (आज़ादी - फ्रीडम, फ़ासिज़्म, फ़िक्शन). यानी स्वतंत्रता, फासीवाद और कथा साहित्य. राजकमल प्रकाशन ने इसी नाम से इसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया है. हिंदी में इस पुस्तक का अनुवाद रेयाज़ुल हक़ ने किया है. ये एक निबंध-संग्रह है, जो अधिनायकवाद के बढ़ते वर्चस्व के दौर में दुनिया को स्वतंत्रता का अर्थ बतलाता है. इसमें अरुंधति ने भाषाओं की भूमिका और कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बीच नई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में विचार किया है. इस किताब का एक अंश पढ़िए.
द गॉड ऑफ़ स्माल थिंग्स के बाद
द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स के छपने के क़रीब एक साल से भी कम समय में, मार्च 1998 में भारत के इतिहास में पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाले गठबन्धन ने केन्द्र में सरकार बनाई. तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस के सदस्य थे. पद संभालने के कुछ ही हफ़्तों के भीतर उन्होंने आरएसएस का पुराना सपना पूरा करते हुए कई परमाणु परीक्षण किए. पाकिस्तान ने अपने परीक्षण करके फ़ौरन जवाब दिया. ये परमाणु परीक्षण राष्ट्रवाद की पागलनपन-भरी लफ़्फ़ाज़ियों की ओर सफ़र की शुरुआत थी, जो आज के भारत में आम बोलचाल का अन्दाज़ हो गया है. परमाणु परीक्षणों को जिस ख़ुशी के साथ लिया गया, और यह ख़ुशी ऐसे हलकों में भी मनाई जा रही थी जिनसे सबसे कम उम्मीद थी, इस सबसे मैं हैरान थी. तभी मैंने अपना पहला लेख ‘द एंड ऑफ़ इमेजिनेशन’ लिखा, जिसमें परीक्षणों की निन्दा की गई थी. मैंने कहा कि परमाणु होड़ में शामिल होकर हम अपनी कल्पना का उपनिवेशीकरण कर देंगे : ‘अगर अपने दिमाग़ में परमाणु बम लगाने का विरोध करना हिन्दूविरोधी और भारतविरोधी है तो, मैंने कहा,
"मैं इस मुल्क से अलग होती हूं. मैं ख़ुद को एक आज़ाद, ख़ानाबदोश गणतंत्र घोषित करती हूं."
आप ख़ुद यह अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाद कैसी प्रतिक्रियाएं आई होंगी. ‘द एंड ऑफ़ इमेजिनेशन’ वह पहला क़दम था, जो आगे चलकर लेखों के बीस साल लम्बे एक सफ़र में तब्दील हो गया. ये वे साल थे, जब भारत बिजली की सी रफ़्तार से बदल रहा था. हरेक लेख के लिए मैंने एक रूप, एक ज़ुबान, एक ढांचा और एक कहानी तलाशी. क्या मैं सिंचाई के बारे में उतने ही अच्छे तरीक़े से लिख सकती थी, जैसा मैं प्यार और ग़म और बचपन के बारे में लिख सकती थी? खारी हो रही मिट्टी के बारे में? पानी की निकासी के बारे में? बांध? फसलें? ढांचागत संयोजन और निजीकरण? बिजली की प्रति इकाई लागत के बारे में? उन चीज़ों के बारे में जो आम लोगों की ज़िन्दगियों को प्रभावित करती हैं? रिपोर्ताज की शक्ल में नहीं, बल्कि क़िस्सागोई की शक्ल में? इन मौज़ूंओं को साहित्य में बदलना क्या मुमकिन था? हर किसी का साहित्य— उन लोगों का भी जो पढ़ और लिख नहीं सकते थे, लेकिन जिन्होंने मुझे सोचना सिखाया था, और जिन्हें पढ़कर सुनाया जा सकता था? मैंने कोशिश की. और लेखों का आना जारी रहा, जारी रहा पांच मर्द वकीलों का आना भी (हर बार वही वकील नहीं होते, वे बदलते रहते, लेकिन लगता है कि वे झुंड में शिकार करते हैं). इसी तरह आपराधिक मामलों की आमद भी बनी रही, ज़्यादातर अदालत की अवमानना के आरोप में. उनमें से एक का अन्त जेल की एक छोटी सज़ा के रूप में हुआ, दूसरा अभी भी चल रहा है. बहसें अक्सर आक्रामक होतीं. कभी-कभी हिंसक भी. लेकिन हमेशा वे अहम रहीं. करीब-क़रीब हर लेख मेरे लिए इतनी मुश्किलें लेकर आता कि मैं ख़ुद से वादा करती कि अब मैं और लेख नहीं लिखूंगी. लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता था. ऐसे हालात बनते जिनमें ख़ुद को चुप रखने की कोशिश में मेरे सिर में ऐसा शोर उठ खड़ा होता, मेरी रगों में ऐसा दर्द उठता कि मैं हार मान लेती और लिखने बैठ जाती. पिछले साल जब मेरे प्रकाशकों ने सुझाया कि उन्हें जमा करके एक किताब बना दिया जाए, तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि माई सेडिशियस हार्ट नाम की यह किताब एक हज़ार पन्नों से भी बड़ी थी. बीस साल तक लिखते रहने, बग़ावतों के केन्द्र में सफ़र करने, ग़ैरमामूली लोगों और बेपनाह ख़ूबसूरत आम लोगों से मिलने के बाद, उपन्यास मेरे पास लौट आया. यह बात साफ़ हो गई कि मेरे भीतर जो कायनात बन रही थी, उसे सिर्फ़ एक उपन्यास ही समेट सकता है. यह कायनात उन जगहों से रची-बसी थी, जहां-जहां मैं भटकी थी, और अब यह एक दास्तान की दुनिया में ढल रही थी. मैं जानती थी कि यह उपन्यास निस्सन्देह एक जटिल, राजनीतिक और अन्तरंग होगा. मैं जानती थी कि अगर द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स घर के बारे में था, जिसमें बसे परिवार में एक टूटा हुआ दिल था, तो द मिनिस्ट्री ऑफ़ अटमोस्ट हैपीनेस की शुरुआत होगी, जब उस घर की छत उड़ चुकी होगी, जब टूटा हुआ दिल अपने टुकड़ों को जंग में तबाह घाटियों और शहरों की सड़कों के हवाले कर चुका होगा. यह एक उपन्यास होगा, लेकिन इसकी दुनिया पर नकेल कसने की सारी कोशिशें नाकाम रहेंगी. यह उन रवायतों को नकार देगी जो बताती हैं कि एक उपन्यास कैसा हो सकता है और कैसा नहीं हो सकता. यह दुनिया में मेरे हिस्से के उस ख़ूबसूरत से शहर की मानिंद होगा, जहां पढ़ने वाले एक नए मुहाजिर के रूप में पहुंचेंगे. ज़रा से डरे हुए, ज़रा सहमे हुए, लेकिन जज्बात से भरपूर. इसको जानने का अकेला रास्ता होगा इसके बीच चलना, इसमें खो जाना, इसमें रहना सीख लेना. छोटे और बड़े लोगों से मिलना सीख लेना. मजमे को प्यार करना सीख लेना. यह एक ऐसा उपन्यास होगा जो वह बातें कहेगा जिन्हें किसी भी और तरह से नहीं कहा जा सकता. ख़ासकर कश्मीर के बारे में, जहां सिर्फ़ कहानियां ही सच्चाई बयान कर सकती हैं, क्योंकि सच्चाई बताई नहीं जा सकती. भारत में अपनी जान जोख़िम में डाले बिना ईमानदारी से कश्मीर के बारे में बोलना मुमकिन नहीं है. कश्मीर और भारत, और भारत और कश्मीर की कहानी के बारे में मैं जेम्स बाल्डविन की बात से बेहतर कोई चीज़ आपको नहीं बता सकती :
"और वे मेरी बात का यक़ीन नहीं करेंगे, ठीक इसलिए कि वे जानते हैं कि मैंने जो कहा है वह सच है."
कश्मीर की कहानी इसकी मानवाधिकार रिपोर्टों का कुल जमा भर नहीं है. यह सिर्फ़ क़त्लेआमों, यातनाओं, गुमशुदगियों और सामूहिक क़ब्रों की बात भर नहीं है, या मजलूमों और उनके जालिमों-भर की बात नहीं है. कश्मीर में जो सबसे ख़ौफ़नाक चीज़ें होती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन मानी जाएं. एक लेखक के बतौर, कश्मीर में हमें इन्सानी वजूद के बड़े सबक मिलते हैं. ताक़त और कमज़ोरी के, धोखेबाज़ी, वफ़ादारी, मुहब्बत, मज़ाक़ और भरोसे के. दशकों तक एक फ़ौजी क़ब्ज़े में रहने वाले अवाम के साथ क्या होता है? जब हवा में ही ख़ौफ़ का ज़हर भरा हो तो मामले किस तरह अंजाम दिए जाते हैं? ज़ुबान का क्या होता है? उन लोगों का क्या होता है, जो इस दहशत को अमल में लाते हैं, उसे रोज़मर्रा की चीज़ बना देते हैं, उसे सही ठहराते हैं? उन लोगों का क्या होता है जो अपने नाम पर इसे जारी रहने की इजाज़त देते हैं? कश्मीर की दास्तान टुकड़ों वाली एक पहेली (जिग्सॉ पज़ल) है, जिसके टुकड़े आपस में कभी जुड़ नहीं पाते. यहां कोई आख़िरी तस्वीर नहीं मिलती.
मेरे किरदार
अजीबोग़रीब लोग मेरे पन्नों पर आए. उनमें सबसे पहले हैं एक ख़ुफ़िया अधिकारी बिप्लब दासगुप्ता. जब वे फ़र्स्ट पर्सन में बोलते हुए आए तो मैं निराश थी. मुझे लगा, मैं उनके दिमाग़ में थी, और बाद में मुझे समझ में आया कि शायद वो मेरे दिमाग़ में थे. उनकी जो बात मुझे दहशत से भर देती, वह उनकी बुराइयां नहीं थीं, बल्कि उनकी तार्किकता, उनकी होशियारी, उनका चुटीलापन, अपने को हकीर समझना और उनकी कमज़ोरियां थीं. इसके बावजूद दासगुप्ता की नफ़ासत और सूझ-बूझ से भरा राजनीतिक विश्लेषण वह नहीं देख पाता, जिसे द मिनिस्ट्री ऑफ़ अटमोस्ट हैपीनेस के एक छोटे से किरदार, एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर डी.डी. गुप्ता आसानी से देख लेते हैं. गुप्ता इराक़ से भारत लौटे हैं, जहां उन्होंने बरसों तक धमाके से बचने वाली दीवारें (ब्लास्ट वाॅल) बनाकर कमाई की थी, जिनकी तस्वीरें उन्होंने बड़े फ़ख़्र से अपने फ़ोन में जमा कर रखी थीं. इराक़ में उन्होंने जो कुछ देखा और जिया था, उससे आजिज आ चुके गुप्ता उस सब को देखते हैं, जिसे वे कभी घर समझा करते थे. उनके अपने मुल्क में जो कुछ हो रहा था, उस पर सोच-विचार करने के बाद उनका अन्दाज़ा यह था कि आने वाले बरसों में इस मुल्क में ब्लास्ट वॉल के लिए बाज़ार बढ़ जाएगा. उपन्यास अपने लेखकों को पागलपन की कगार पर पहुंचा सकते हैं. उपन्यास अपने लेखकों को पनाह भी दे सकते हैं.
एक लेखक के तौर पर मैंने द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स के किरदारों की हिफ़ाज़त की, क्योंकि वे नाजुक और ग़ैरमहफ़ूज़ थे. द मिनिस्ट्री ऑफ़ अटमोस्ट हैपीनेस के अनेक किरदार भी ज़्यादातर उनसे कहीं अधिक ग़ैरमहफ़ूज़ हैं. लेकिन वे मेरी हिफ़ाज़त करते हैं. ख़ासकर अंजुम, जो आफ़ताब के नाम से पैदा हुई थी, और आख़िरकार जो जन्नत गेस्ट हाउस की मालकिन और मैनेजर बनी. यह गेस्ट हाउस पुरानी दिल्ली की दीवारों के ठीक बाहर एक खस्ताहाल मुसलमान क़ब्रिस्तान में चलता है. अंजुम मर्दों और औरतों के बीच, जानवरों और इन्सानों के बीच, ज़िन्दगी और मौत के बीच सरहदों में नर्मी भरती है. दिन-ब-दिन बेरहम होती जाती इस दुनिया की सख़्त सरहदों की तानाशाही से बचने की जब भी मुझे ज़रूरत महसूस होती है, मैं उसके पास चली जाती हूं. 1947 में हमने औपनिवेशिक हुकूमत से आज़ादी हासिल की थी, जिसके लिए क़रीब-क़रीब सबने लड़ाई लड़ी, सिवाय उनके जो आज हम पर हुकूमत कर रहे हैं. तब से लेकर अब तक के हमारे सफ़र में हर तरह के सामाजिक आन्दोलनों, जाति-विरोधी संघर्षों, पूंजीवाद-विरोधी संघर्षों, स्त्रीवादी संघर्षों ने हमारी राह रोशन की. 1960 के दशक में इन्क़लाब की मांग थी कि अवाम को इंसाफ़ मिले, दौलत का फिर से बंटवारा हो, और शासक वर्ग काे उखाड़ फेंका जाए. 1990 का दशक आते-आते हमें अपनी ज़मीनों और गांवों से उजाड़े गए दसियों लाख लोगों की बेदख़ली के ख़िलाफ़ लड़ाइयों में समेट दिया गया. उजाड़े गए ये वे लोग थे, जो एक नए बनते भारत की चक्की में पिस गए, जहां सबसे अमीर तिरसठ लोगों के पास कुल मिलाकर जितनी दौलत है, वह 1.3 अरब लोगों के इस मुल्क के पूरे साल के बजट खर्च से भी अधिक है. अब हमें और भी पीछे धकेलकर ऐसे फ़रियादी बना दिया गया है, जो एक नागरिक के बतौर अपने अधिकार मांग रहे हैं, और उनसे मांग रहे हैं जिनका इस मुल्क को बनाने में कोई योगदान नहीं रहा है. और जब हम फ़रियादों में मसरूफ़ हैं, हम देखते हैं कि राज्य अब हमारी ख़ुशहाली के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे हट रहा है, हम देखते हैं कि पुलिस फ़िरकापरस्त हो गई है, हम देखते हैं कि न्यायपालिका धीरे-धीरे अपने फ़र्ज़ से मुंह मोड़ती जा रही है, हम देखते हैं कि मीडिया जिसका काम सुकून की नींद सोने वालों को तकलीफ़ में डालना और तकलीफ़ में घिरे लोगों को सुकून पहुंचाना था, इसका ठीक उलटा कर रहा है.













.webp)






.webp)