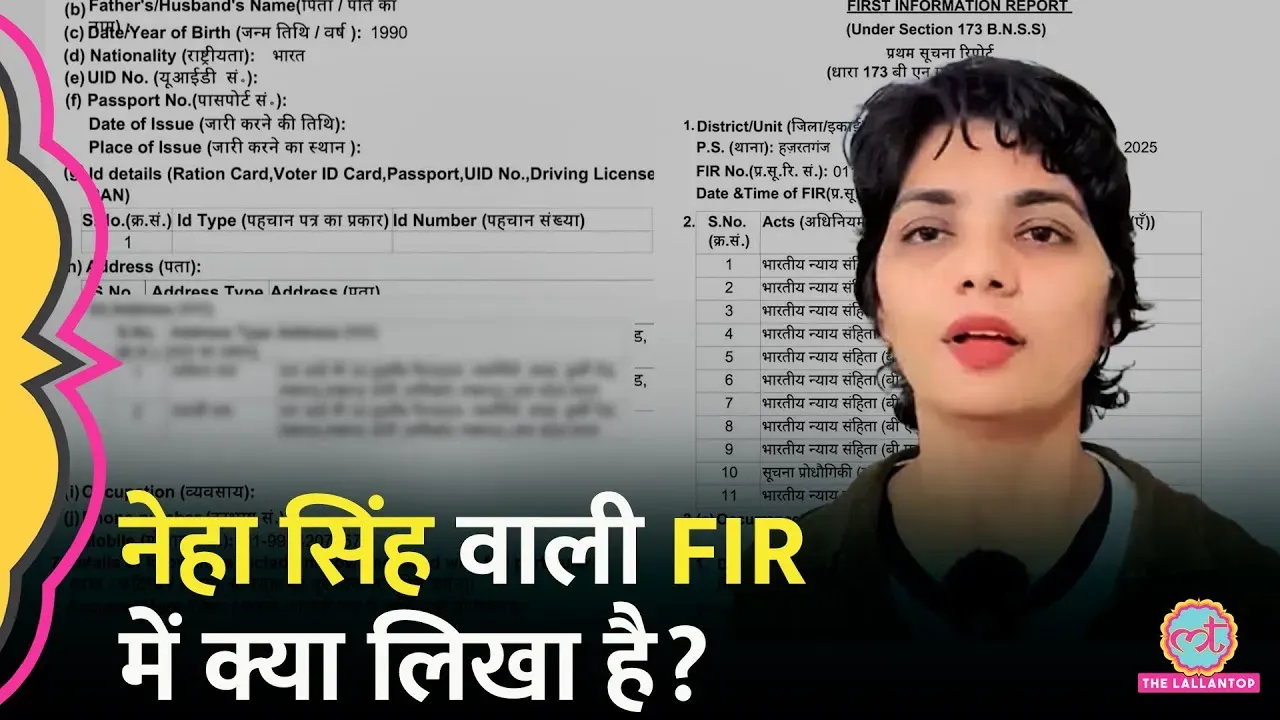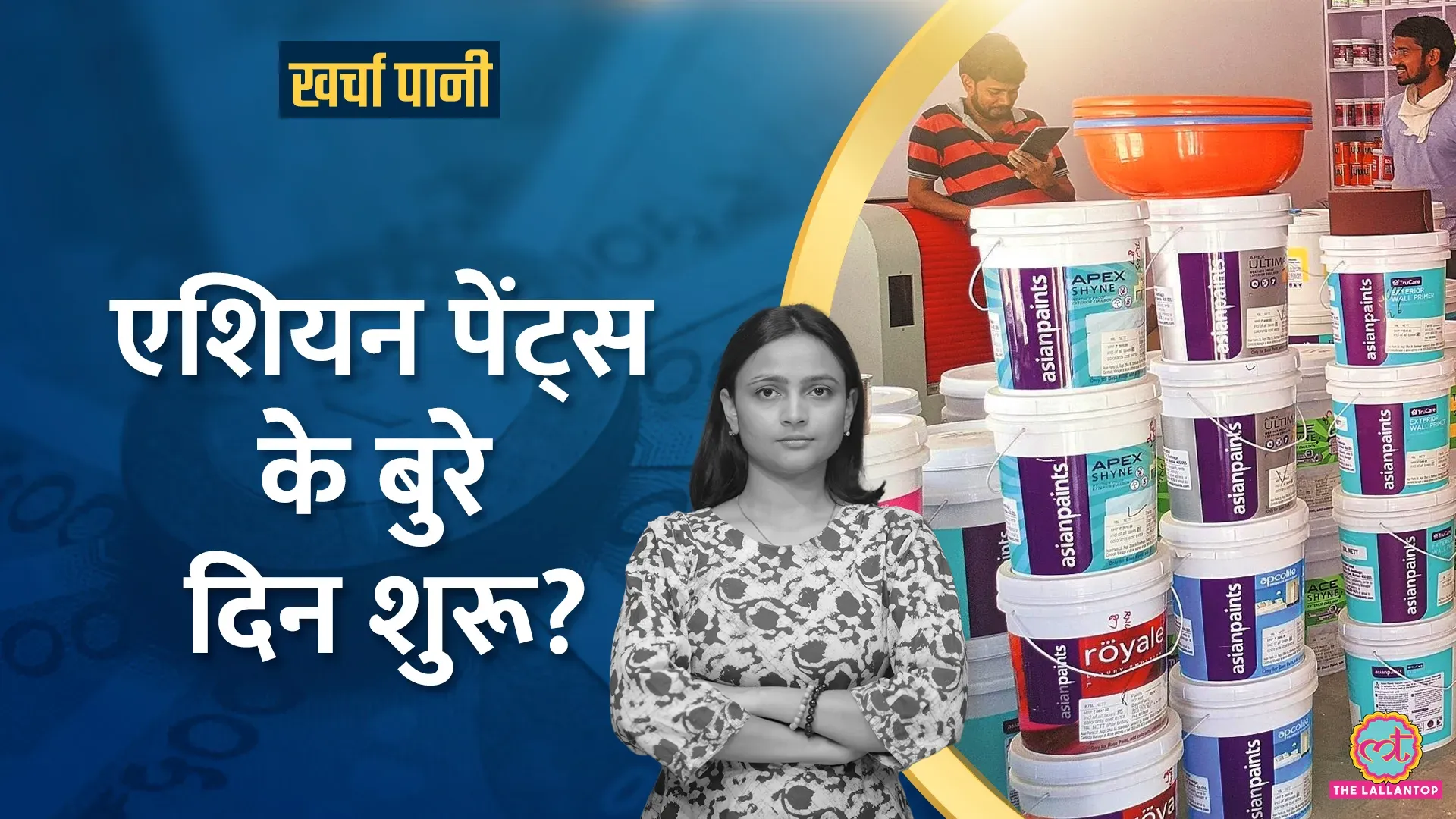हमें आर्थिक कारकों की ओर भी ध्यान देना होगा. जब लोग भूखे हों और मर रहे हों तो संस्कृति के बारे में, यहाँ तक कि ईश्वर के विषय में भी बात करना बेवकूफ़ी है.
भारत माता. कितने नारे, कितनी शहादतें, कितनी मुहब्बत गढ़ी गई 'भारत माता' के प्रति. लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 'भारत माता' का जयकारा, देशभक्ति का सबूत मांगने के काम में लाया जाता है. जब इस शब्द को लेकर इतना कोलाहल है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर ये भारत माता है कौन? इसी सवाल का जवाब देती है पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब 'कौन हैं भारत माता'. इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) की लेखनियों का संग्रह है. ये किताब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री को एक व्यक्ति, एक राजनेता और एक विचारक के रूप में मुकम्मल ढंग से जानने का अवसर देती है. इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा इस किताब के बारे में कहते हैं कि ये किताब आपको नेहरू की बौद्धिक विरासत को समझने का एक मौका देती है. इसके संपादक पुरुषोत्तम अग्रवाल अपनी किताबों के लिए कई अवार्ड जीत चुके हैं. जेएनयू से पढ़े पुरुषोत्तम अग्रवाल एनसीईआरटी की हिन्दी पाठ्य-पुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार, भारतीय भाषा केन्द्र जेएनयू के अध्यक्ष तथा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं. आइए उनकी सम्पादित पुस्तक 'कौन हैं भारत माता?' का एक अंश पढ़ते हैं.
संस्कृति क्या है?
मैं यहाँ ख़ुशी-ख़ुशी आया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा भारत के सांस्कृतिक मेल-मिलाप को बढ़ावा देने की आशा करता हूँ. यह भी मेरी इच्छा है कि भारत के न केवल अपने पड़ोसी देशों बल्कि पूरब और पश्चिम और यहाँ तक कि बाक़ी दुनिया के देशों के साथ मज़बूत सांस्कृतिक रिश्ते क़ायम हों. यहाँ पर सवाल सिर्फ़ सांस्कृतिक मेल-मिलाप चाहने या उसे बहुत अच्छा समझने-भर का नहीं है, बल्कि ये परिस्थितियों की ज़रूरत भी है. ये और ख़राब होती जाएँगी अगर इस दिशा में कोई क़दम नहीं उठाए गए तो. मैं इस बात को लेकर बहुत आशान्वित हूँ कि इंडियन काउंसिल ऑफ़ कल्चरल रिलेशन (भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद) की स्थापना से हमारे लोग और दूसरे देशों के लोगों के बीच एक बेहतर समझदारी विकसित होगी. मेरे दिमाग़ में कुछ बातों को लेकर बहुत भ्रम है और मैं उनके बारे में बिना लाग-लपेट साफ़-साफ़ कहूँगा भी. दुनिया में जो चल रहा है उसे लेकर बहुत से बुनियादी सवाल मन में उभरते हैं. राष्ट्र, व्यक्तिगत स्तर पर लोग और तमाम समुदाय एक-दूसरे को समझने का दावा करते रहते हैं और यह बहुत सहज बात भी है कि लोगों को एक-दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक-दूसरे से सीखना भी चाहिए. फिर भी, मैं जब इतिहास के पन्नों को पलटता हूँ, या, समकालीन घटनाओं को देखता हूँ, तो कभी-कभी पाता हूँ कि वे लोग जो यह एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वे ही सबसे ज़्यादा झगड़ा करते हैं. ऐसे देश एक-दूसरे के सबसे नज़दीकी पड़ोसी होते हैं. वे चाहे एशिया के हों या यूरोप के, वे सबसे ज़्यादा एक-दूसरे को ग़लत तरीक़े से उकसाते हैं, जबकि वे एक-दूसरे को ज़्यादा गहराई से समझते भी हैं. इस तरह से, एक-दूसरे को जानना ही बेहतर सहयोग या दोस्ती के लिए पर्याप्त नहीं होता. ये कोई नई बात नहीं है. यहाँ तक कि इतिहास में भी यही बात नज़र आती है. क्या इन देशों में ही कोई गड़बड़ है या इस सवाल को समझने का नज़रिया ही ग़लत है? या कि कोई और बात है जो कि उतनी कारगर नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी? हम जब भी सांस्कृतिक सम्बन्धों की बात करते हैं तो सबसे पहले यह सवाल हमारे दिल-दिमाग़ में आता है कि आख़िर ‘संस्कृति’ का वास्तविक अर्थ है क्या जिसके विषय में लोग इतनी बातें करते हैं? अपने बचपन के दिनों में, जर्मन ‘कुल्तुर’ के बारे में पढ़ी हुई बातें मुझे याद हैं, और साथ ही ये भी कि जर्मन लोग किस प्रकार दूसरों पर विजय हासिल करके और दूसरे तरीक़ों से इसे फैलाने की कोशिश करते थे. इस ‘कुल्तुर’ को फैलाने और उसका विरोध करने के लिए एक बड़ा युद्ध हुआ था. हर देश और हर व्यक्ति के पास संस्कृति को लेकर एक ख़ास नज़रिया होता है. जब कभी सांस्कृतिक सम्बन्धों की बात होती है—यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से बात होना बहुत सही है—लेकिन हक़ीक़त में होता ये है वे ख़ास नज़रिये आपस में संघर्ष पैदा कर देते हैं और दोस्ती को बढ़ावा देने की बजाय आपस में और मनमुटाव पैदा करने की वजह बन जाते हैं. यह एक बुनियादी सवाल है—संस्कृति क्या है? और मैं निश्चित रूप से आपको इसकी परिभाषा देने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मैं स्वयं अभी तक इसका जवाब नहीं पा सका हूँ. देखा जा सकता है कि प्रत्येक देश और सभी अलहदा सभ्यताएँ अपनी स्वयं की संस्कृति विकसित करती हैं, जिसकी जड़ें सैकड़ों हज़ारों वर्ष पहले की पीढ़ियों में धँसी रहती हैं. हम देखते हैं कि हर देश की एक अन्तःप्रेरणा होती है जो कि वहाँ एक सभ्यता की शुरुआत करती है. वो देश उस अन्तःप्रेरणा से संचालित होता है और वो सभ्यता एक लम्बा सफ़र तय करती है. अन्तःप्रेरणा की यह धारणा ऐसी दूसरी धारणाओं के रूबरू होती है; उनके साथ अन्त:क्रिया करती है. मेरे हिसाब से दुनिया में कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है जो पूर्णतया मौलिक, पवित्र-पावन और दूसरी संस्कृति से प्रभावित न हो. ठीक इसी तरह कोई यह भी नहीं कह सकता कि वो सौ फ़ीसदी एक ख़ास नस्ल या जाति का प्रतिनिधि है क्योंकि सैकड़ों हज़ारों साल में बहुत बदलाव और समन्वय हुआ है. इसलिए, संस्कृति कुछ हद तक मिली-जुली होने के लिए बाध्य ही है, भले ही उसमें किसी विशिष्ट राष्ट्रीय संस्कृति का मूल तत्त्व प्रबल रहे. अगर इस तरह की चीज़ें शान्तिपूर्वक चलती रहती हैं तो इसमें कोई नुक़सान नहीं है. लेकिन अक्सर इनसे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. कभी-कभी इसकी वजह से एक समुदाय को इस बात का डर सताने लगता है कि उनकी संस्कृति उन तत्त्वों से दबती जा रही है जिसे वो बाहरी लोग या बाहरी प्रभाव मानते हैं. फिर वे ख़ुद को एक खोल के भीतर छिपा लेते हैं जो उन्हें सबसे अलग-थलग कर देती है और उनके विचारों, उनकी सोच को बाहर जाने से रोकती है. यह एक बीमार मनःस्थिति है क्योंकि किसी भी मुद्दे पर और उससे भी ज़्यादा बीमारी में गतिहीनता सबसे ख़राब चीज़ है. संस्कृति में यदि कोई मूल्य है, तो उसमें एक निश्चित गहराई होनी ही चाहिए. इसका एक गतिशील व प्रवाहमान चरित्र होना ही चाहिए. आख़िरकार, संस्कृति बहुत सारे तत्त्वों पर निर्भर करती है. अगर हम उस मूल साँचे को छोड़ दें जिस पर किसी देश या वहाँ के लोगों की आन्तरिक ऊर्जा उनके शुरुआती दौर में बनी थी, तो हम पाएँगे कि किसी देश की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और दूसरे कारकों से प्रभावित होती है. अरब की संस्कृति वहाँ के भूगोल और अरब के रेगिस्तान से बहुत गहराई से प्रभावित है, क्योंकि वहाँ ऐसा ही है. स्वाभाविक रूप से, जैसा कि हमने अपने साहित्य में पढ़ा है कि प्राचीन काल में भारत की संस्कृति हिमालय के जंगलों और भारत की महान नदियों के साथ-साथ कुछ अन्य चीज़ों से प्रभावित रही है. ये यहाँ की मिट्टी से उपजा एक स्वाभाविक विकास है. संस्कृति के बहुत से आयाम होते हैं जैसे—स्थापत्य, संगीत और साहित्य. इनमें से कोई दो तत्त्व मिलकर एक सुन्दर समायोजन बनाते हैं, जैसा कि पहले भी हुआ है. लेकिन उसके किसी तत्त्व को बदलने का ऐसा प्रयास किया जाता है जिसकी जड़ें उस संस्कृति में स्वाभाविक रूप से न हों और वह संस्कृति अपनी जड़ों को छोड़ना भी न चाहे, तब निश्चित ही संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है. तब मेरी समझ से कुछ ऐसा घटता है जो कि संस्कृति के सभी विचारों से उलट होता है. ये अपने दिमाग़ को अलग-थलग कर लेना होता है और जान-बूझकर अन्य हवाओं से अपने दिलो-दिमाग़ को बचाते हुए बन्द कर लेना होता है. भारत के इतिहास के बारे में मेरा तो यह मानना है कि भारत की तरक़्क़ी और उसकी गिरावट को मापने का पैमाना यह देखकर बनाया जा सकता है कि जब भारत के लोगों का दिमाग़ बाहरी दुनिया के लिए खुला हुआ था तो उसकी तरक़्क़ी हुई थी और जब भारत ने बाहरी दुनिया से ख़ुद को काटकर रखा, तब-तब उसकी दशा में गिरावटें आईं. जितना ज़्यादा वो अपने मेें सिमटा और बन्द समाज रहा, उतना ही ज़्यादा वो ठहराव में आता गया. जीवन बुनियादी तौर पर एक गतिशील, परिवर्तनशील और विकसित होनेवाली चीज़ है. चाहे वो कोई देश हो, कोई समुदाय हो, कोई समाज हो या कि कोई व्यक्ति ही हो. जो भी तत्त्व इसकी गतिशीलता को रोकता है, वो इसे नुक़सान पहुँचाता है और नीचे गिराता है. हमारे यहाँ बड़े महान धर्म हुए हैं और उनका मानव जाति पर बहुत असर भी रहा है. फिर भी, पूरे सम्मान के साथ और बिना किसी व्यक्ति को नीचा दिखाए, मैं कहना चाहूँगा कि उन्हीं धर्मों ने लोगों के दिमाग़ को यथास्थितिवादी, कट्टर और लकीर का फ़कीर भी बनाया. और इस तरह से यह उन धर्मों का बुरा प्रभाव भी रहा है. उन्होंने जो बातें बताईं वो अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जब यह दावा किया जाने लगता है कि ये ही अन्तिम शब्द हैं तो वह समाज जड़ हो जाता है.
किसी भी मनुष्य या जाति या राष्ट्र में कहीं-न-कहीं एक निश्चित गहराई और मज़बूत जड़ें होनी ही चाहिए. जब तक उनकी जड़ें अतीत से जुड़ी रहती हैं तब तक उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ता. क्योंकि आख़िरकार उनका अतीत उनकी पीढ़ियों के अनुभव और ज्ञान का भी एक समुच्चय रहता है. ये ज़रूरी है कि वो आपके पास हो. वरना आप केवल किसी अन्य चीज़ की मुरझाई-सी नक़ल बनकर रह जाते हैं, जिसका एक व्यक्ति के रूप में या समुदाय के रूप में भी कोई अर्थ नहीं होता. दूसरी ओर कोई केवल अपनी जड़ों में ही नहीं रह सकता. आख़िरकार जड़ें भी सूख जाती हैं, अगर उन्हें बाहर से सूर्य की धूप और खुली हवा न मिले तो. केवल तभी जड़ें आपको ज़िन्दा रख सकती हैं, केवल तब ही उसकी शाखाएँ बाहर निकलेंगी और वो सरसब्ज़ होंगी. इन दोनों ज़रूरी कारकों में किस तरह सन्तुलन बनाया जाए? यह बहुत कठिन काम है, क्योंकि कुछ लोग केवल शाखाओं पर निकली पत्तियों और फूलों के बारे में ही सोच पाते हैं, और भूल जाते हैं कि यह तभी सम्भव हुआ है जब इनको जड़ों से जोड़नेवाला एक तना भी है, जो इन्हें पाल-पोस रहा है. वहीं दूसरे लोग केवल जड़ के बारे में ही सोचते रह जाते हैं कि फूल, पत्तियाँ और शाखाएँ उनसे छूट जाती हैं और केवल एक खोखला तना रहता है. तो सवाल यह है कि कोई कैसे सन्तुलन बनाए. क्या संस्कृति का मतलब मनुष्य के आन्तरिक विकास से है? निस्सन्देह, ऐसा होना ही चाहिए. क्या इसका मतलब इससे भी है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? निश्चित ही ऐसा है. क्या इसका मतलब हममें किसी दूसरे व्यक्ति को समझने की क्षमता है? मुझे लगता है कि हाँ. क्या इसका मतलब यह भी है कि हमें दूसरे लोग भी समझ सकें? मुझे लगता है कि हाँ. संस्कृति के यह सब मायने भी हैं. कोई इनसान अगर दूसरों के नज़रिये को नहीं समझ सकता तो वो एक संकुचित मानस और संस्कृति वाला कहलाएगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कुछ असाधारण मनुष्यों को छोड़ दें तो, यह नहीं सोच सकता कि उसके पास ही सारा ज्ञान और विवेक है. दूसरे के पास भी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या समुदाय, कुछ ज्ञान या विवेक या सच हो सकता है. अगर हम अपने दिमाग़ों को बन्द कर लें तो न केवल हम उससे ख़ुद को महरूम करेंगे, बल्कि हम एक ऐसे दिमाग़ी दृष्टिकोण वाले होंगे, जो कि एक सुसंस्कृत व्यक्ति के बिलकुल विपरीत होता है. एक सभ्य, सुसंस्कृत दिमाग़ वो होना चाहिए जिसकी अपनी जड़ें तो हों, साथ ही उसके दिमाग़ के दरवाज़े और खिड़कियाँ भी खुली रहें. उसमें दूसरों के दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझ सकने की क्षमता होनी चाहिए, भले ही वो उससे हमेशा सहमत न हो. सहमति-असहमति का प्रश्न तो तब उठता है जब आप उस चीज़ को समझते भी हों, वरना यह केवल एक अन्ध नकारवाद है जो कि किसी भी प्रश्न के प्रति एक सुसंस्कृत दृष्टिकोण नहीं है.
मैं यहाँ एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करना पसन्द करूँगा—विज्ञान. जीवन की समस्याओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? मेरा मानना है कि यह हर चीज़ की जाँच-परख करना है; ग़लती की गुंजाइश तक रखते हुए उनसे सीखना और परीक्षण के द्वारा सच की खोज करना है; बिना हठवादिता के चीज़ों को समझने की कोशिश करना है और अगर सन्तुष्टि हो जाए तो उस सच को स्वीकार करना और अगर कोई दूसरा तथ्य सामने आ जाए तो अपनी सोच को बदलने के लिए तत्पर रहना है; एक खुले दिल-दिमाग़ का होना है जो कि सत्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो, भले ही वो कहीं से भी आया हो. अगर यह संस्कृति है तो आज की दुनिया और देशों मेें यह कितनी दिखाई पड़ती है? निश्चित ही अगर ऐसा वास्तव में होता तो हमारे लिए बहुत-सी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना ज़्यादा आसान होता.
दुनिया के लगभग सारे देश इस विश्वास में जीते हैं कि उन्हें परमात्मा ने कुछ ख़ास आशीर्वाद दिया हुआ है और वे विशिष्ट प्रकार के चुने हुए लोग और नस्ल हैं, और दूसरे लोग चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, कहीं-न-कहीं उनसे कुछ निम्न श्रेणी के प्राणी हैं. यह ताज्जुब की बात है कि इस तरीक़े के जज़्बात सारे देशों में मौजूद हैं, चाहे वो पूरब के देश हों या पश्चिम के. पूरब के लोग अपनी धारणाओं और विचारों में गहरे धँसे हुए हैं और कुछ मामलों में श्रेष्ठता बोध के शिकार हैं. जो भी हो पिछले दो-तीन सौ सालों में उनके दिमाग़ झकझोरे गए और उन्हें अपमानित होना पड़ा है, उनका शोषण किया गया है और उनकी जड़ें भी कटी हैं. इसलिए, बावजूद इस धारणा के कि वो बहुत मामलों में काफ़ी ऊँचे थे, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें भी झकझोरा जा सकता है और उनका शोषण हुआ है. कुछ हद तक इससे उनमें एक वास्तविकता-बोध आया. सचाई से मुँह चुराने के लिए कुछ इस तरीक़े की बातें भी कही गईं कि यह तो ठीक नहीं हुआ कि हम लोग दुनियावी और तकनीकी रूप से बहुत विकसित नहीं हुए, लेकिन, आख़िरकार तो यह सब दिखावटी बातें हैं और हम लोग आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की दृष्टि में बहुत ऊँचे रहे. मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्य अन्य बातों की अपेक्षा अधिक महत्त्व के होते ही हैं, लेकिन जिस तरीक़े से सचाई से मुँह मोड़ने के लिए ये आध्यात्मिक श्रेष्ठता वाला विचार दिया जाता है वो ताज्जुब में डालनेवाला है, क्योंकि इसे भौतिक और दुनियावी हीनता की ढाल बनाया जाता है. इस बात को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता. ये एक तरह से अपनी दुर्दशा के कारणों से मुँह चुराना है. निश्चित ही राष्ट्रवाद एक बहुत दिलचस्प अवधारणा है, जो किसी देश के इतिहास के एक ख़ास दौर में ज़िन्दगी, उन्नति, ताक़त और एकता का संचार करता है, वहीं दूसरी ओर, यह एक तरह की संकीर्णता भी लाता है, क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कि उनका देश बाक़ी दुनिया से कुछ अलग है. तब राष्ट्रवाद का सन्दर्भ बदल जाता है और कोई केवल अपने संघर्षों, अपनी ख़ासियतों, अपनी असफलताओं को ही सोचता रहता है और दूसरे विचारों को उसमें जगह नहीं मिलती. नतीजा यह होता है कि वही राष्ट्रवाद जो कि लोगों की उन्नति का प्रतीक है, एक तरह से उसी उन्नति के दिमाग़ी ठहराव का प्रतीक बन जाता है. जब राष्ट्रवाद सफलता पाता है तो कभी-कभी वो अपना फैलाव आक्रामक अन्दाज़ में करने लगता है और दुनिया के लिए ख़तरा बन जाता है. आप चाहे जिस विचार के हों, आप इस निष्कर्ष पर ज़रूर पहुँचेंगे कि एक प्रकार का सन्तुलन बनाना बहुत ज़रूरी है. वरना कोई चीज़ जो अच्छी थी, एक बुराई भी बन सकती है. संस्कृति बुनियादी तौर पर अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी-कभी ग़लत नज़रिये से चीज़ों को देखने के कारण न केवल जड़ता बल्कि संघर्ष और नफ़रत को पोषित करनेवाली भी हो जाती है. आपको ये सन्तुलन कैसे मिलेगा, मुझे नहीं पता. इस समय की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के अलावा, सम्भवतः ये आज की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके पीछे मनुष्य की आन्तरिक चेतना का भयंकर संघर्ष छिपा है, ऐसी खोज की बेचैनी छुपी है जिसमें वह चेतना सफल नहीं हो पा रही है.
हमें आर्थिक कारकों की ओर भी ध्यान देना होगा. जब लोग भूखे हों और मर रहे हों तो संस्कृति के बारे में, यहाँ तक कि ईश्वर के विषय में भी बात करना बेवकूफ़ी है.
किसी भी दूसरे विषय पर बात करने से पहले सामान्य मनुष्यों के जीवन की बुनियादी ज़रूरतेें पूरी करना सबसे ज़रूरी है. यहीं पर अर्थशास्त्र की ज़रूरत पड़ती है. आज का इनसान कष्टों, भुखमरी और असमानता को बर्दाश्त करने की मनःस्थिति में नहीं है. विशेषकर जब साफ़ दिख रहा है कि बोझ बराबर नहीं उठाया जा रहा है. कुछ थोड़े से लोग मुनाफ़ा कमाते हैं, और बाक़ी बहुत सारे लोग केवल बोझ. हमें अपरिहार्य रूप से इन समस्याओं से आर्थिक और दूसरे तरीक़े से ही निपटना होेगा, लेकिन मैं यह महसूस करता हूँ कि इस सबके पीछे एक गहन मानसिक समस्या भी लोगों के दिमाग़ों में है. यह हो सकता है कि कुछ लोग इसके बारे में सजगता से सोचते हों और दूसरे अनजाने में हल्के ढंग से सोचते हों, लेकिन मनुष्य के ज़ेहन में यह संघर्ष विद्यमान है. यह बात तो पक्की है. यह मामला किस तरह से सुलझेगा, मुझे नहीं पता. एक चीज़ जो मुझे परेशान करती है वो ये है : जो लोग एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरीक़े से ज़्यादा से ज़्यादा समझते हैं, वही लोग आपस में और ज़्यादा झगड़ते भी हैं. इसका ये मतलब नहीं कि हम लोगों को एक-दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ये करना एक तरह से ख़ुद को संकुचित कर लेना होगा, जो कि आज की दुनिया के सन्दर्भ में किया ही नहीं जा सकता. इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक-दूसरे को सही तरीक़े से समझने की कोशिश करें. सही तरीक़ा ज़रूरी है. एक दोस्ताना रवैया रखना सही दृष्टिकोण है क्योंकि, यह बहुत महत्त्वपूर्ण है, एक दोस्ताना रवैये का जवाब भी दोस्ताना होता है. मुझे इसमें लेश मात्र भी सन्देह नहीं है कि मनुष्य जीवन का मूलभूत सिद्धान्त ये है कि अगर दृष्टिकोण सही है तो उसका जवाब भी सही आएगा. अगर दृष्टिकोण बुरा है तो उसका जवाब भी बुरा आने की गुंजाइश रहती है. अगर हम अपने साथ के लोगों से या देशों से भी एक दोस्ताना तरीक़े से मिलते हैं और अपने दिल और दिमाग़ को खुला रखते हुए इसके लिए तैयार रहते हैं कि जो भी हो—इसका यह मतलब नहीं कि हम मूलभूत मूल्यों, सच या अपनी बुद्धिशीलता का समर्पण कर दें—तो हम केवल समझदारी नहीं बल्कि सही तरह की समझदारी की ओर बढ़ेंगे. अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप तय करें कि संस्कृति और विवेक वास्तव में क्या है? हम ज्ञान, अनुभव और जिज्ञासा से सीखते हुए बढ़ते हैं, जब तक कि हमारे पास इन सबका इतना विशाल भंडार इकट्ठा हो जाता है कि यह जान पाना असम्भव हो जाता है कि हम वास्तव में खड़े कहाँ हैं. हम इस सबसे अभिभूत होते रहते हैं और साथ ही उसी समय कुछ न कुछ यह भी महसूस कर रहे होते हैं कि इन सारी चीज़ों को अगर मिला भी दिया जाए तो भी ज़रूरी नहीं कि यह मनुष्य जाति के विवेक में अभिवृद्धि को भी दर्शाता हो. मुझे लगता है कि शायद वो लोग जिनके पास आधुनिक जीवन और आधुनिक विज्ञान जैसी सहूलियतें नहीं थीं, वो बुनियादी तौर पर हम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान थे. मुझे नहीं मालूम है कि क्या हम आनेवाले समय में इस सारे ज्ञान, वैज्ञानिक प्रगति और मानव जाति की बेहतरी के सारे पहलुओं को सच्चे विवेक से मिला सकेंगे या नहीं? ये विभिन्न ताक़तों के बीच एक दौड़ है. मुझे एक बहुत विवेकी मनुष्य, एक प्रसिद्ध ग्रीक कवि की पंक्तियाँ याद आती हैं :
बुद्धि विवेक क्या है?
मनुष्य की कोशिशें या ईश्वरीय आशीर्वाद, इतना प्यारा, इतना महान?
बिना भयभीत हुए स्वतंत्र खड़े रहना, साँसें लेते हुए प्रतीक्षा,
नफ़रत के ख़िलाफ़ हाथ ऊँचा करना,
चिर काल तक सुन्दर चीज़ों को प्यार करना

















.webp)