15 जून 2001 को आमिर खान की फिल्म 'लगान' रिलीज़ हुई थी. इसे डायरेक्ट किया था आशुतोष गोवारिकर ने. एक्टर-डायरेक्टर-प्रोड्यूसर आशुतोष ने हिंदी सिनेमा को यादगार फिल्में दी हैं. शाहरुख खान को मोहन भार्गव के यादगार किरदार में पेश करने वाले आशुतोष का हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ा योगदान 'लगान' है. हिंदी सिनेमा के इस मास्टर पीस पर टीम लल्लनटॉप के तीन तिलंगों ने अपने-अपने ढंग से लिखा है. इसे एक एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए. गजेंद्र और मिहिर सिनेमा को हर सांस में लीलने वाले शख्स हैं. और मैं एक लोल दर्शक भर. हम तीनों को पढ़िए. अलग शैलियां हैं. नीयत बस एक. कि सिनेमा और आपका संवाद और गाढ़ा हो.
लगान और गदर, 20 साल, तीन तिलंगों की याद के चश्मे से
गजेंद्र सिंह भाटी, मिहिर पंड्या और सौरभ द्विवेदी बता रहे हैं फिल्म के पर्सनल किस्से

इस फिल्म के साथ ही सनी देओल की फिल्म 'गदर-एक प्रेम कथा' भी रिलीज़ हुई थी.
सादर- सौरभ.
पहली याद- अंत में असंभव संभव होता है - गजेन्द्र सिंह भाटी
जून 2001 में अजमेर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव एम. फारूक का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट आया था. 12वीं कक्षा का. सेकेंड डिविजन से पास हुआ था. 55.38% आए थे. फिलमें 3-4 की उम्र से ही अच्छी लगती थीं. तब सिर्फ कहानी सुनने और सम्मोहित होने के सॉफ्टवेयर ही भीतर थे. ज्यादा कुछ सोचना-समझना नहीं आता था.

गजेंद्र
तब बीकानेर में बिग सिनेमाज़ ने दो स्क्रीन वाला सिनेमैजिक मल्टीप्लेक्स नहीं बनाया था. तब सूरज टॉकीज यहां का सबसे बड़ा हॉल था. तीन-चार अन्य सिंगल स्क्रीन थे. लेकिन सूरज जीवन का पहला थियेटर था जो मैंने अंदर या बाहर से देखा. 1993 में. गांव से परिवार के साथ आया था एक दिन के लिए. अंधेरा हो रहा था. 'रूप की रानी चोरों का राजा' देखी थी. जादू हो चुका था.
इसी जून में यहां 'लगान' और 'गदर: एक प्रेम कथा' लगी थीं. सनी देओल हैंडपंप उखाड़ते हुए, पाकिस्तान बैशिंग करते हुए थियेटर की ओर बुला रहे थे. उदित नारायण की चाशनी भरी आवाज और उत्तम सिंह का ठुमकता म्यूजिक 'उड़जा काले कावां', 'मैं निकला गड्डी लेके' लाए थे. तो यही फिल्म देखनी थी. तय था. सिर्फ तीन-चार दोस्त ही थे मेरे. शायद पद्म, उमेश और रघुवेंद्र. उन्हीं के साथ.
एक-दो बार की प्लानिंग और जरा देरी के बाद देख पाए. लेकिन 'गदर' नहीं. उसका टिकट नहीं मिला. सोचा इतनी योजना बनाकर और सीट-पेटी बांधकर उड़ आए हैं तो खाली हाथ न लौटें, दुर्भाग्य है 'लगान' ही देख लें जो 'गदर' के सामने कुछ नहीं लेकिन ठीक तो होगी. बीकानेर तप रहा था. दोपहर थी. यहां पहले शो 12 बजे से शुरू होते हैं. हम शायद 3 बजे वाले में जा रहे थे. तो गए. मायूस थे, 'गदर' की टिकट नहीं मिली थी. सब खराब हो गया. जीवन बर्बाद हो गया.
सूरज टॉकीज में गए. बैठे. फिल्म चालू हुई. बींध दिया. सांसें रोक दी. समझ नहीं आया कि साढ़े तीन घंटे (तब ये सामान्य लंबाई थी) के हर एक पल में इतना जादू कैसे डल गया होगा! आज इस तथ्य को स्वीकार करने में भी आलस होता है कि 15 जून को 'गदर' भी लगी थी. पता नहीं पिछली बार 'उड़जा काले कावां' कब सुना था. 'लगान' के गाने फिर सुन रहा हूं और ठीक लग रहे हैं. अनेक बार पहले सुन चुकने के बाद भी.
सोचता हूं ये फिल्म इतनी अच्छी क्यों लगी होगी:
1. ओपनिंग क्रेडिट्स बहुत सुंदर था. वो नक्शा, रॉयल्टी, सिक्के.
2. अमिताभ बच्चन का नरेशन. उनकी आवाज कहानी शुरू करने के लिए परफेक्ट थी. हमारे मनों में एक certain भाव की प्रतिक्रिया पैदा करवाने के लिए सीमा रेखा बांधती गई. उससे बाहर हम सोच नहीं रहे थे, जा नहीं रहे थे.
3. रेत और गर्मी. बीकानेर का हूं तो ये दो डीएनए में है. जहां दिख जाएं अपनी लगती हैं. इसमें खूब थी. सब पात्रों का आने वाला पसीना बिलकुल असली था. सीन से पहले मुंह पर, कपड़ों पर छिड़का पानी नहीं था. चारों तरफ फिल्म रेत, गर्मी, पसीना था. हिरण, हाथी, कींकर, अन्य रेगिस्तानी झाड़ियां, भेड़ें, बकरियां, गायें, घोड़े, मुर्गियां भी थे.
4. नाम कितने सिंपल थे. भुवन, भूरा, कचरा, बाघा, लाखा, ईसर, गुरन, देवा, अर्जन, गोली.
5. आमिर 'सरफरोश' में बहुत पसंद आ चुके थे. यहां भी उन्होंने पूरा होमवर्क किया था. किरदार बन गए थे. भाषा सरल भी थी और फिल्मी लिहाज से नई भी थी. कहानी में उनका नेतृत्व मन शुरू से ही मंजूर कर चुका था.
6. हर पात्र में कोई ऐसी बात थी कि ये लोग याद होते जा रहे थे. रघुबीर यादव तो अभिनय में कद्दावर थे ही. मुर्गी वाले. गुस्सा बहुत होते. बेसिक से आदमी. हंसाते भी थे. गुरन (राजेश विवेक) जब भी आते फन लाते. मैच के दौरान भी उनका सामने का स्टांस लेना हो या अजब बॉलिंग. वे कुछ साधु बाबा टाइप भी थे गांव में. लंबी दाढ़ी. उनके बाद फनी था गोली (दया शंकर पांडे). बेचारगी वाला. लाखा (यशपाल यादव) विलेन था शुरू में. उसके फिर से हीरो बनने की प्रक्रिया ने बहुत सस्पेंस, डर, घबराहट, खुशी दी. जिस भी कहानी में विलेन अच्छा आदमी बनकर सही के साथ आता है वो पसंद आती ही है. कचरा (आदित्य लखिया) का हाथ मुड़ा हुआ है. वो अस्पृश्य है. भुवन सुधारवादी सा आदमी है. सबमें ईश्वर का अंश देखता है. ये भी अच्छा लगा. ईसर काका (श्रीवल्लभ व्यास), मुखिया जी (राजेंद्र गुप्ता), शंबू काका (ए. के. हंगल), राजा जी (कुलभूषण खरबंदा), भुवन की मां (सुहासिनी मुले) जैसे सभी पात्रों को निभाने वाले प्रतिष्ठित कैरेक्टर आर्टिस्ट थे. बाघा (अमीन हाजी) गजब बॉडी का धनी था. बोल नहीं सकता था. देवा (प्रदीप रावत) की एंट्री तो कहानी में जान ले आई थी. सिख पात्र जो इन सबमें ज्यादा सक्षम है. सिपाही भी था. बॉलिंग-बैटिंग दोनों में ओपनर सा. बाघा और देवा की बॉडी ऐसी थी कि लगता था जब भी अंग्रेजों से पंगा होगा ये दोनों ही हैं जो पीट सकते हैं. तब दिमाग यूं ही चलता था. ज्यादातर फिल्में आज भी वैसे ही सुचवाती है. इस्माइल (राज जुत्शी) का मुस्लिम पात्र भी वो संपूर्णता लाया जो भारत की छवि के हिसाब से अनिवार्य थी. हमारे सभी गांव ऐसे सभी विविध पात्रों से बनते हैं.
7. गौरी के रोल में ग्रेसी सिंह को लेने से ध्यान भुवन पर से नहीं हटता था. यानी ग्रेसी पर इतना नहीं जाता था. वे साइडकिक ही रहीं. तो हम दर्शक इन सब तरीकों से भी मेकर्स के चाहे गए अनुशासन से आगे बढ़ते जा रहे थे.
8. अंग्रेज एक्टर्स को हम नहीं जानते थे लेकिन एलिजाबेथ, उसका भाई कैप्टन रसेल हो या रसेल का करीबी अंग्रेज या आखिर में सिर पर कॉर्क की गेंद मारकर खून निकाल देने वाला मुच्छड़ बॉलर या फिर ब्रिटिश सेना के सीनियर और बुजुर्ग पात्र जो मैच के दौरान ग्रामीण टीम के प्रदर्शन और हेट्रिक पर निष्पक्ष भाव से प्रशंसा व हैरत बांट रहे होते हैं. ये सब पहली बार देख रहे थे लेकिन इस भाषा, छवि के साथ लाए गए कि स्थापित तुरंत होते गए मन में. इनकी आदतें, गुण, अवगुण सब करीने से रखे गए थे.
9. गाने. जावेद अख्तर ने काल्पनिक दौर की भाषा और हमारे दिमागों की सीमाओं को अच्छे से पहचानते हुए विविध गीत लिखे. बड़े ही सरल. तुरंत याद होने वाले. 'घनन घनन', 'ओ मितवा', 'राधा कैसे न जले', 'चले चलो'. सब अलग-अलग मूड वाले, अतिविशिष्ट. 'ओ री छोरी' में भुवन और एलिजाबेथ के प्रेम को दिखाते हुए अंग्रेजी गीत और डांस भी आता है और वो कहीं हमें मिसफिट नहीं लगता.
10. 'ओ पालनहारे' गीत. जब संकट पड़ा है. इंसान कुछ नहीं कर सकता. दर्शक को भी लगता है अब कुछ नहीं हो सकता. तब भगवान को याद किया जाए ये सोचना मात्र ही निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की जबरदस्त बुद्धिमानी थी. जो बाद में 'स्वदेस' में भी उन्होंने किया. धार्मिक गीत. लता मंगेशकर, उदित नारायण, साधना सरगम के इस गीत को अगले कुछ वर्षों तक मैंने सुना. लगता था असल जीवन में ये गीत कुछ मदद करेगा. ये आलम था. ये भी था कि एक 'मुस्लिम' गीतकार कितना सुंदर 'हिंदू' गीत लिख सकता है. 'राधा कैसे न जले' भी तो इन्होंने ही लिखा था.
11. फिर एक और 'मुसलमान' ने ही (हालांकि वो पहले 'हिंदू' था) 'ओ पालनहारे' का म्यूजिक दिया. हिंदी फिल्मों के सबसे प्रमुख 'हिंदू' धर्मगीतों/भजनों में से एक दो मुस्लिमों ने बनाया है ये विचार कई साल दिमाग में घूमता रहा. रहमान अगर न होते तो ये फिल्म इस जगह बिलकुल नहीं होती. हमें सम्मोहित करने वाला एक बड़ा फैक्टर ये संगीत रहा है. जिसमें कहीं भी बिजली से चलने वाले साज नहीं हैं. महसूस तो बिलकुल नहीं होते. आज जितनी भी पीरियड फिल्में आती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होते देख घृणा होने लगती है. रहमान ने इतने महीन, बेसिक बाजे यूज़ किए हैं कि झंकृत होते रहते हैं. धड़का देते हैं, फड़का देते हैं.
12. के. पी. सक्सेना के अवधी, बृज, भोजपुरी को मिलाकर लिखे गए सरलतम संवाद.
13. नितिन देसाई के झोंपड़ियों, महलों वाले ऑथेंटिक सेट.
14. दिग्गज भानु अथैया की वस्त्र सज्जा. जिन्होंने 'गांधी' (1982) में कॉस्ट्यूम बनाए थे.
15. क्रिकेट जो तब तक मेरा प्रिय खेल था. खेलता भी था. देखता भी था. ये कहानी क्रिकेट के रास्ते संघर्ष की बात करती है. दिखाती है कि कमजोर भी आततायी से जीतेगा. अंत में असंभव संभव होता है. पूरे समय हम इस लड़ाई में भुवन और गांव वालों के साथ होते हैं. क्योंकि हमें पता है वो लोग सही हैं. जब तक सृष्टि है सही और गलत के ध्रुवों के बीच ही तो मन रंजित होगा. इन्हीं दो के बीच तो जीवन चलेगा. तो ये हुआ. कहानी बड़ी मजेदार, तृप्त करने वाली और ऑथेंटिक सी थी.


सौरभ
कृष्णा टॉकीज. टेलर वाली गली का एक कोना. सामने क्राउन टेलर. पूरी गली में अकेली दुकान जो दो शटर वाली थी. लोग गर्दन उचकाकर इसकी चिट्ट दिखाते थे कमीज से. तब ब्रांड के नाम पर एक्शन के जूता ही शो ऑफ का हिस्सा होते थे. बाकी बहस इस पर होती थी कि कमीज कौन बढ़िया सिलता है. कंचन टेलर, डिलाइट या फिर क्राउन, जो सबसे ज्यादा पइसे लेता है. वैसे दावेदार एक और था. मोती. मगर उसकी अपनी दुकान नहीं थी. हावर्ड ड्राई क्लीनर वालों के यहां एक मशीन लिए बैठता था. लेकिन गांधी डिग्री कॉलेज के चिकाईबाज कहते थे कि जो कटाई मोती करता है, वो बोर्ड और पर्ची वाले टेलर क्या करेंगे. बात भटक गई, माफी चाहता हूं. कमीज काटने बैठता हूं और बीच में पाजामे का नारा नापने लगता हूं.
तो बात कृष्णा टॉकीज की. यहां हम एक ही बार गए थे. वेजीप्रो की फैक्टरी में मोहन मामा काम करते थे. ताई जी के भाई. मगर तब सबके मामा सबके मामा होते थे. कजिन शब्द जीवन में नहीं आया था. न ही शब्द और न ही भाव. कोई पूछता कि कितने भाई बहन हो तो गर्व से कहते. 9 भाई 6 बहनें. सामने वाला अजकजा जाता फिर कहता, अरे भाई सगे बताओ. हम भी अड़ जाते. सब सगे ही समझ लो.
मगर कृष्णा टॉकीज शहर की सगी नहीं रह गई थी. पाप का अंत जैसी कोई फिल्म लगी थी, जब हम इसमें पहली बार गए. फिल्म देखने नहीं. आमलेट खाने. मोहन मामा के साथ. कुछ और दोस्त थे उनके. इंग्लिश पिक्चर जैसे नाम थे उनके. नाम क्या सरनेम. रस्तोगी अंकल. और मिसेज पुंडीर के दूल्हा भी. मामा ने हमें जूता दिलाए. लौटते में आमलेट खिलवाया. प्लेट आई. सफेद. चीनी मिट्टी की. उसमें भाप छोड़ता आमलेट. साथ में छुरा कांटा. सब उसमें फंसाकर खा रहे. हम उठाते, गप्प से बीच में दबाते. फिर उठाते और मुंह खोलने के पहले आमलेट सरक कर नीचे पहुंच जाता. बड़ी देर बाद मामा की नजर गई. उन्होंने चुरा कांटे हटा दिए. आमलेट की चुक्की बना दी. जैसी बुकनू रोटी में बनती थी. और हमने निपटा दिया. डकार मारी तो पोस्टर देखा. गोविंदा था अपना. पाप का अंत कर रहा था.
फिर जैसा पहले बताया, टॉकीज का अंत होने लगा. फिर इसमें गंदी वाली पिक्चरें लगने लगीं. फूलन का हसीन बदला. चंपा चुप नहीं रहेगी जैसी. गांव से रविंद वकील के छोटे भइया देखने आते. हमने ताड़ लिया. फिलिम देख चुपचाप निकल रहे थे. झोला टांगे. पर बताते किसे. बर्रे को बताया. मेरा गांव का दोस्त. बोले. अरे भइया, बे बड़े आदमी हैं. सौकीन हैं. का कहें.
उसी कृष्णा टॉकीज की किस्मत खुली गदर से. सन्नी देओल का बड़ा सा (मतलब 8 फुट का) कटआउट बना. टेलर वाली गली के दरवाजे पर रखा गया. पूरे हाल की पुताई हुई. हल्के नीले रंग का डिस्टैंपर. कैंटीन में नए गिलास आए. लाल पेंट लगाया गया. समोसे छानने के लिए एक भट्टी एक्स्ट्रा. वो इकलौती बार था, जब हमने उस गली में नए कपड़े के रेशों वाली रासायनिक खूशबू नहीं पाई. हर तरफ भैरो गुटखा की तीखी गंध उठ रही थी. लोग लटपटाए घूम रहे थे. टिकट ब्लैक हो रहे थे. पहली बार साक्षात देखा. जैसे फिल्मों में दिखाते थे. 35-35 रुपया का बिक रहा था 20 वाला टिकट.
फिल्म कृष्णा वालों ने चार हफ्ते के लिए उठाई थी. उसी में काया पलट हो गई. सुबह साढ़े 10 वाला नीली पुताई वाली गरम फिल्मों का शो भी गदर के हिस्से आ गया. अर्चना वालों को काटो तो खून नहीं. मगर करें क्या. चार हफ्ते बाद फिल्म वापस ली. अपने यहां लगाई. मगर तब तक तो पूरा जिला देख चुका था. बस हम बचे थे.
हमने ये उरई में नहीं देखी. लखनऊ में देखी. पेपर देने गए थे एनडीए का. वहीं निपट लिए. हिंदुस्तान जिंदाबाद याद रहा. तब तक अमीशा पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल वाली लड़की सी लगती थी. तो उसे चुनरी पहन ट्रक वाले से प्यार करते देख हिंदी मीडियम अहम को सहलाहट मिल गई. और याद रहा हैंडपंप वाला सीन. लखनऊ वाले भइया बता रहे थे. अबे यहीं ला मार्टीनियर में हुई है शूटिंग इसकी. लगा कि इतिहास के काफी करीब बैठा हूं. बाहर निकले तो देखा पास के एक सिनेमा हाल में लगान लगी है. गांव देहात की फिल्म. क्रिकेट मैच दिखाया है. ऐसा ट्रेन में लोग बता रहे थे. छक्का मारता है आखिरी गेंद में. हमें लगा कि लेओ. अब बचा ही क्या.
फिर दैनिक जागरण में पढ़ा. आमिर सन्नी लक्की हैं एक दूसरे के लिए. पहले भी इनकी फिल्में साथ आईं और हिट रहीं. दिल के साथ अर्जुन आई थी शायद. और फिर घायल या दामिनी के साथ आमिर की कोई फिल्म आई थीं. सब हिट होती थीं. और अब लगान और गदर हिट हो रही थीं.
कुछ महीनों बाद उरई की अनुराधा टॉकीज में लगान देखी. और फिर देखी. और अब तक देखता हूं. फिल्म भी. इसकी मेकिंग भी. कुछ चीजें हैं, जो याद हैं.
1. क्रिकेट जो था. वो भारत के कुल नॉस्टैलजिया का हिस्सा था. चंद्रशेखर के बारे में चच्चू बताते थे. उन्हीं के शब्दों में कहूं तो लूले को कोई समझ ही नहीं पाता था और गेंद घुस जाती थी. ऐसा ही एक कैरेक्टर लगान में था. फिर सचिन तेंदुलकर जैसा भुवन था. गैंठा. तान के टांग पर छक्का मारने वाला. कपिल देव सा फास्ट बॉलर था. जट्टा दा छोरा टाइप. इसने लगान के मैच के साथ एक अलग रिश्ता बनाया. और जब आखिरी गेंद पर छक्का लगा. तो लगा कि जैसे प्रकारांतर से चेतन शर्मा की गेंद पर मारे मियांदाद के छक्के की याद धुंधली पड़ गई.
2. राधा वाला मिथक बहुत सुंदर ढंग से पिरोया गया. इतना कि आज भी पत्नी से कह देता हूं चुहल में. गोपियां आनी जानी हैं, राधा तो मन की रानी है. उसके पहले जो मंजीरे की कनख के साथ बीट बनती है. वो ताजी थी. एक गुंजाइश भरा भरोसा भी मिला था कि निपट देसी रहकर भी कोई कार्नेशियन के फूलों सी विदेशी सुंदर सुवासित मैम का प्यार पाया जा सकता है. जब कृष्ण जनम के दिन एलिजाबेथ के माथे पर टीका लगा था, तो हमें रोली से भी प्यार हो गया था.
3. भगवान पहाड़ी पर बसे थे. भगवानों को पता नहीं क्यों जनता से दूर जाकर ऊंचाई पर बसना होता है. या बदमाशी पुरोहितों की होती है. और उन तक पहुंचने के लिए हर बार लता सी अकंपित पवित्र आवाज लानी पड़ती है. और चिरौरी करनी पड़ती है. या कि शायद अहम का विसर्जन हो. कि ये गुमान न हो जाए कि अपने तईं सब कुछ ठीक किया जा सकता है. हे पालनहारे, तुम्हरे बिना हमरा कौनोई नहीं. दीनता. दंभ की मौत.
4. लगान एक एतिहासिक किस्सा भर नहीं था. भारत की आलोचना थी. पहले समाज को अपने विभाजित रूप में दिखाया. उसकी दुर्दशा दिखाई. और फिर संगठित होने का नतीजा दिखाया. लेकिन मुश्किल ये है कि फिल्म में तो हीरो अनुसूचित जाति के हीरो को गले लगा लेता है. मगर उसे देख ताली पीटने वाला समाज बाहर आते ही बाभन, ठाकुर, कुर्मी और कोरी में बंट जाता है. दोगले लोग हैं हम. खासतौर पर पढ़े लिखे सवर्ण. जो संस्कार के नाम पर अपनी झूठी श्रेष्ठता से चिपटे हैं जोंक की तरह. अपना ही खून खत्म करते.
5. और फिर फिर गदर याद आती रही. उसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई. जरूरत नहीं लगी. अभी मुल्क गदर मोड में है. जबकि इसे लगान वाली बारीक समझदारी की जरूरत है. एका की जरूरत है. चीखने वाली देशभक्ति की नहीं. हैंडपंप उखाड़ने की नहीं. ड्रामाबाजी करने की नहीं. मगर चारों तरफ देखिए. जिंदाबाद के नारे हैं. किसे जिंदा कर रहे हैं. किसे मार रहे हैं. राम जाने.


मिहिर
अौर मैं तो सुपर एक्साइटेड था. वजह, दादा ने बता दिया था कि इस फिल्म में क्रिकेट होनेवाली है. उन्हें ब्रिटिश अभिनेत्री रेचल शेली ने बता दिया था. आमिर खान का इतने जतन से छुपाकर रखा राज़ फिल्म की रिलीज़ के ठीक पहले फाश हो गया था. लेकिन क्या अौर कैसी क्रिकेट, ये मालूम नहीं था. उन दिनों हम इस खेल पर जीते-मरते थे. पर वो टाइम था कि सिनेमा में क्रिकेट ढूंढो तो कुमार गौरव की 'अॉल राउंडर' अौर देव साब की 'अव्वल नम्बर' मिलती थी. फिल्म में मैच के नाम पर हम नसीर साहब की 'चमत्कार' का क्रिकेट मैच देख खुश हो लेते थे. सच यही है कि 'लगान' से पहले तक सिनेमा की दुनिया में देश का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट एक प्रतिबंधित विषय था. 'लगान' सिनेमाई दुनिया में क्रिकेट की कहानी पर लगे अघोषित प्रतिबंध को तोड़नेवाली फिल्म साबित हुई. चार क्रिकेटीय वजहें जिन्होंने 'लगान' को खास फ़िल्म बनाया, वो थीं,
1. 'लगान' बनाते हुए ये ध्यान रखा गया था कि हिन्दुस्तानी दर्शक सिनेमा साक्षर होने के साथ ही क्रिकेट के खेल में भी बड़का एक्सपर्ट दर्शक है, अौर इसे ध्यान में रखकर फिल्म की कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न रचे जा सकते हैं. जब मैच की शुरुआत में भुवन की टीम के चमत्कारी गेंदबाज़ कचरा की गेंद नहीं घूमी, तो ये देखकर मेरी बांछें (वो जहां कहीं भी होती हों) खिल गईं थी. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि 'गेंद पुरानी होने पर स्पिन होती है' जैसी डीटेल एक बॉलीवुड फिल्म अपनी कहानी में बतौर प्लॉट ट्विस्ट इस्तेमाल कर सकती है. दर्शक की बुद्धि अौर जानकारी को इतना सम्मान देते मैंने मुम्बईया फिल्मों को कम ही देखा है. मैं एज़ ए क्रिकेट फैन
गौरवान्वित था उस क्षण.
2. लेकिन इसने सिनेमा का लॉजिक भी बचाकर रखा था. जिस दौर की कथा 'लगान' सुना रही थी, उस दौर में क्रिकेट दो पारी का अौर अोवर आठ गेंद का हुआ करता था. लेकिन फिल्म में मैच को दो पारी का कर देने से पटकथा की एकनिष्ठ गति बीच में भंग हो सकती थी. यहां बताना ज़रूरी है कि 'लगान' की पटकथा क्लासिक केस स्टडी है सिनेमा की पटकथा लेखन की कला में. इसकी शुरुआत में नायक अौर खलनायक के कैरेक्टर ग्राफ उल्टे हैं, हीरो एकदम नीचे अौर विलेन एकदम ऊपर. फिर अन्त तक ये उलटते-पलटते रहते हैं, अौर अन्त में मामला रिवर्स हो जाता है. सिनेमाई किरदारों को ग्राफ़ की शक्ल में तब्दील कर देखें तो क्लाईमैक्स तक जाते हुए यह दोनों किसी रोलरकोस्टर राइड
जैसी तरंग बनाते हैं, जो सिनेमाई पटकथा लेखन का एक क्लासिक सिद्धान्त है. अच्छा किया कि थोड़ी सिनेमाई छूट ली आशुतोष गोवारिकर!
3. लेकिन फिल्म उन दर्शकों को भी नज़र में रखती थी, जिन्हें क्रिकेट का K भी नहीं मालूम. फिल्म के प्लॉट में ही इसकी गुंजाइश थी, कि खेल से अपरिचित दर्शक सरल शब्दों में जान भी ले कि ये बला क्या है, अौर यह मूर्खता भी ना लगे. जैसे-जैसे भुवन के साथी इसे सीखेंगे, वैसे-वैसे क्रिकेट में अनपढ़ दर्शक भी खेल को जानेगा. पर मज़ेदार बात तो ये थी कि जब भुवन अौर उसके देसी साथी खेल सीख रहे हैं, तो यही फिल्म का डिवाइस टूल बन जाता है अमेरिकियों को खेल की बारीकियां सरलता से सिखाने का. जिस ज्यूरी ने वोट दिया 'लगान' को अॉस्कर की बेस्ट फॉरेन लेंग्वेज फिल्म कैटेगरी में पहले पांच में पहुंचाने के लिए, वो क्रिकेट नहीं जानती थी. उन्हें बेसिक क्रिकेट सिखाने का श्रेय 'लगान' के निर्देशक ले सकते हैं.
4. यह फिल्म क्रिकेट को सिर्फ़ एक खेल की तरह नहीं देख रही थी. पहली बार एक ऐसी कहानी हमारे सामने थी, जिसमें खिलाड़ी का खेल उसके व्यक्तित्व का परिचायक था. यह कमाल बात थी. 'गोली' जो गोफ़न शानदार फैंकता था, वो अच्छा गेंदबाज़ बना. 'भूरा' जो मुर्गियां पकड़ने में एक्सपर्ट था, वो बेहतर स्लिप फील्डर बना. यही किसी भी खेल का असली चरित्र होता है. अपने सर्वोच्च पायदान पर जाकर वो खिलाड़ी के समूचे व्यक्तित्व का प्रदर्शनकारी रूप बन जाता है. इंसान की अभिव्यक्ति क्षमता का सर्वोत्तम अौर सम्पूर्ण माध्यम. 'लगान' क्रिकेट को एज़ ए मैटाफर
इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें एक बंधनमुक्त होने की कोशिश करता इंसान, एक जकड़ा हुआ समाज अौर एक गुलाम मुल्क खुद को मुकम्मल रूप से अभिव्यक्त कर रहा था.
बाद में बड़े होकर जब फिल्म दोबारा देखी तो इस मुल्क की तमाम दरारें भी इस फिल्म की कथा में नज़र आईं. कुछ सायास, कुछ अनायास. दोनों ने ही रचना को इस सिने अध्येता के लिए अौर बड़ा अौर मुकम्मल बनाया. लेकिन वो किस्सा किसी अौर दिन.
ये भी पढ़ें :

गजेंद्र
तब बीकानेर में बिग सिनेमाज़ ने दो स्क्रीन वाला सिनेमैजिक मल्टीप्लेक्स नहीं बनाया था. तब सूरज टॉकीज यहां का सबसे बड़ा हॉल था. तीन-चार अन्य सिंगल स्क्रीन थे. लेकिन सूरज जीवन का पहला थियेटर था जो मैंने अंदर या बाहर से देखा. 1993 में. गांव से परिवार के साथ आया था एक दिन के लिए. अंधेरा हो रहा था. 'रूप की रानी चोरों का राजा' देखी थी. जादू हो चुका था.
इसी जून में यहां 'लगान' और 'गदर: एक प्रेम कथा' लगी थीं. सनी देओल हैंडपंप उखाड़ते हुए, पाकिस्तान बैशिंग करते हुए थियेटर की ओर बुला रहे थे. उदित नारायण की चाशनी भरी आवाज और उत्तम सिंह का ठुमकता म्यूजिक 'उड़जा काले कावां', 'मैं निकला गड्डी लेके' लाए थे. तो यही फिल्म देखनी थी. तय था. सिर्फ तीन-चार दोस्त ही थे मेरे. शायद पद्म, उमेश और रघुवेंद्र. उन्हीं के साथ.
एक-दो बार की प्लानिंग और जरा देरी के बाद देख पाए. लेकिन 'गदर' नहीं. उसका टिकट नहीं मिला. सोचा इतनी योजना बनाकर और सीट-पेटी बांधकर उड़ आए हैं तो खाली हाथ न लौटें, दुर्भाग्य है 'लगान' ही देख लें जो 'गदर' के सामने कुछ नहीं लेकिन ठीक तो होगी. बीकानेर तप रहा था. दोपहर थी. यहां पहले शो 12 बजे से शुरू होते हैं. हम शायद 3 बजे वाले में जा रहे थे. तो गए. मायूस थे, 'गदर' की टिकट नहीं मिली थी. सब खराब हो गया. जीवन बर्बाद हो गया.
सूरज टॉकीज में गए. बैठे. फिल्म चालू हुई. बींध दिया. सांसें रोक दी. समझ नहीं आया कि साढ़े तीन घंटे (तब ये सामान्य लंबाई थी) के हर एक पल में इतना जादू कैसे डल गया होगा! आज इस तथ्य को स्वीकार करने में भी आलस होता है कि 15 जून को 'गदर' भी लगी थी. पता नहीं पिछली बार 'उड़जा काले कावां' कब सुना था. 'लगान' के गाने फिर सुन रहा हूं और ठीक लग रहे हैं. अनेक बार पहले सुन चुकने के बाद भी.
सोचता हूं ये फिल्म इतनी अच्छी क्यों लगी होगी:
1. ओपनिंग क्रेडिट्स बहुत सुंदर था. वो नक्शा, रॉयल्टी, सिक्के.
2. अमिताभ बच्चन का नरेशन. उनकी आवाज कहानी शुरू करने के लिए परफेक्ट थी. हमारे मनों में एक certain भाव की प्रतिक्रिया पैदा करवाने के लिए सीमा रेखा बांधती गई. उससे बाहर हम सोच नहीं रहे थे, जा नहीं रहे थे.
3. रेत और गर्मी. बीकानेर का हूं तो ये दो डीएनए में है. जहां दिख जाएं अपनी लगती हैं. इसमें खूब थी. सब पात्रों का आने वाला पसीना बिलकुल असली था. सीन से पहले मुंह पर, कपड़ों पर छिड़का पानी नहीं था. चारों तरफ फिल्म रेत, गर्मी, पसीना था. हिरण, हाथी, कींकर, अन्य रेगिस्तानी झाड़ियां, भेड़ें, बकरियां, गायें, घोड़े, मुर्गियां भी थे.
4. नाम कितने सिंपल थे. भुवन, भूरा, कचरा, बाघा, लाखा, ईसर, गुरन, देवा, अर्जन, गोली.
5. आमिर 'सरफरोश' में बहुत पसंद आ चुके थे. यहां भी उन्होंने पूरा होमवर्क किया था. किरदार बन गए थे. भाषा सरल भी थी और फिल्मी लिहाज से नई भी थी. कहानी में उनका नेतृत्व मन शुरू से ही मंजूर कर चुका था.
6. हर पात्र में कोई ऐसी बात थी कि ये लोग याद होते जा रहे थे. रघुबीर यादव तो अभिनय में कद्दावर थे ही. मुर्गी वाले. गुस्सा बहुत होते. बेसिक से आदमी. हंसाते भी थे. गुरन (राजेश विवेक) जब भी आते फन लाते. मैच के दौरान भी उनका सामने का स्टांस लेना हो या अजब बॉलिंग. वे कुछ साधु बाबा टाइप भी थे गांव में. लंबी दाढ़ी. उनके बाद फनी था गोली (दया शंकर पांडे). बेचारगी वाला. लाखा (यशपाल यादव) विलेन था शुरू में. उसके फिर से हीरो बनने की प्रक्रिया ने बहुत सस्पेंस, डर, घबराहट, खुशी दी. जिस भी कहानी में विलेन अच्छा आदमी बनकर सही के साथ आता है वो पसंद आती ही है. कचरा (आदित्य लखिया) का हाथ मुड़ा हुआ है. वो अस्पृश्य है. भुवन सुधारवादी सा आदमी है. सबमें ईश्वर का अंश देखता है. ये भी अच्छा लगा. ईसर काका (श्रीवल्लभ व्यास), मुखिया जी (राजेंद्र गुप्ता), शंबू काका (ए. के. हंगल), राजा जी (कुलभूषण खरबंदा), भुवन की मां (सुहासिनी मुले) जैसे सभी पात्रों को निभाने वाले प्रतिष्ठित कैरेक्टर आर्टिस्ट थे. बाघा (अमीन हाजी) गजब बॉडी का धनी था. बोल नहीं सकता था. देवा (प्रदीप रावत) की एंट्री तो कहानी में जान ले आई थी. सिख पात्र जो इन सबमें ज्यादा सक्षम है. सिपाही भी था. बॉलिंग-बैटिंग दोनों में ओपनर सा. बाघा और देवा की बॉडी ऐसी थी कि लगता था जब भी अंग्रेजों से पंगा होगा ये दोनों ही हैं जो पीट सकते हैं. तब दिमाग यूं ही चलता था. ज्यादातर फिल्में आज भी वैसे ही सुचवाती है. इस्माइल (राज जुत्शी) का मुस्लिम पात्र भी वो संपूर्णता लाया जो भारत की छवि के हिसाब से अनिवार्य थी. हमारे सभी गांव ऐसे सभी विविध पात्रों से बनते हैं.
7. गौरी के रोल में ग्रेसी सिंह को लेने से ध्यान भुवन पर से नहीं हटता था. यानी ग्रेसी पर इतना नहीं जाता था. वे साइडकिक ही रहीं. तो हम दर्शक इन सब तरीकों से भी मेकर्स के चाहे गए अनुशासन से आगे बढ़ते जा रहे थे.
8. अंग्रेज एक्टर्स को हम नहीं जानते थे लेकिन एलिजाबेथ, उसका भाई कैप्टन रसेल हो या रसेल का करीबी अंग्रेज या आखिर में सिर पर कॉर्क की गेंद मारकर खून निकाल देने वाला मुच्छड़ बॉलर या फिर ब्रिटिश सेना के सीनियर और बुजुर्ग पात्र जो मैच के दौरान ग्रामीण टीम के प्रदर्शन और हेट्रिक पर निष्पक्ष भाव से प्रशंसा व हैरत बांट रहे होते हैं. ये सब पहली बार देख रहे थे लेकिन इस भाषा, छवि के साथ लाए गए कि स्थापित तुरंत होते गए मन में. इनकी आदतें, गुण, अवगुण सब करीने से रखे गए थे.
9. गाने. जावेद अख्तर ने काल्पनिक दौर की भाषा और हमारे दिमागों की सीमाओं को अच्छे से पहचानते हुए विविध गीत लिखे. बड़े ही सरल. तुरंत याद होने वाले. 'घनन घनन', 'ओ मितवा', 'राधा कैसे न जले', 'चले चलो'. सब अलग-अलग मूड वाले, अतिविशिष्ट. 'ओ री छोरी' में भुवन और एलिजाबेथ के प्रेम को दिखाते हुए अंग्रेजी गीत और डांस भी आता है और वो कहीं हमें मिसफिट नहीं लगता.
10. 'ओ पालनहारे' गीत. जब संकट पड़ा है. इंसान कुछ नहीं कर सकता. दर्शक को भी लगता है अब कुछ नहीं हो सकता. तब भगवान को याद किया जाए ये सोचना मात्र ही निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की जबरदस्त बुद्धिमानी थी. जो बाद में 'स्वदेस' में भी उन्होंने किया. धार्मिक गीत. लता मंगेशकर, उदित नारायण, साधना सरगम के इस गीत को अगले कुछ वर्षों तक मैंने सुना. लगता था असल जीवन में ये गीत कुछ मदद करेगा. ये आलम था. ये भी था कि एक 'मुस्लिम' गीतकार कितना सुंदर 'हिंदू' गीत लिख सकता है. 'राधा कैसे न जले' भी तो इन्होंने ही लिखा था.
11. फिर एक और 'मुसलमान' ने ही (हालांकि वो पहले 'हिंदू' था) 'ओ पालनहारे' का म्यूजिक दिया. हिंदी फिल्मों के सबसे प्रमुख 'हिंदू' धर्मगीतों/भजनों में से एक दो मुस्लिमों ने बनाया है ये विचार कई साल दिमाग में घूमता रहा. रहमान अगर न होते तो ये फिल्म इस जगह बिलकुल नहीं होती. हमें सम्मोहित करने वाला एक बड़ा फैक्टर ये संगीत रहा है. जिसमें कहीं भी बिजली से चलने वाले साज नहीं हैं. महसूस तो बिलकुल नहीं होते. आज जितनी भी पीरियड फिल्में आती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होते देख घृणा होने लगती है. रहमान ने इतने महीन, बेसिक बाजे यूज़ किए हैं कि झंकृत होते रहते हैं. धड़का देते हैं, फड़का देते हैं.
12. के. पी. सक्सेना के अवधी, बृज, भोजपुरी को मिलाकर लिखे गए सरलतम संवाद.
13. नितिन देसाई के झोंपड़ियों, महलों वाले ऑथेंटिक सेट.
14. दिग्गज भानु अथैया की वस्त्र सज्जा. जिन्होंने 'गांधी' (1982) में कॉस्ट्यूम बनाए थे.
15. क्रिकेट जो तब तक मेरा प्रिय खेल था. खेलता भी था. देखता भी था. ये कहानी क्रिकेट के रास्ते संघर्ष की बात करती है. दिखाती है कि कमजोर भी आततायी से जीतेगा. अंत में असंभव संभव होता है. पूरे समय हम इस लड़ाई में भुवन और गांव वालों के साथ होते हैं. क्योंकि हमें पता है वो लोग सही हैं. जब तक सृष्टि है सही और गलत के ध्रुवों के बीच ही तो मन रंजित होगा. इन्हीं दो के बीच तो जीवन चलेगा. तो ये हुआ. कहानी बड़ी मजेदार, तृप्त करने वाली और ऑथेंटिक सी थी.

दूसरी याद- मुल्क गदर मोड में है. जबकि जरूरत लगान वाली समझ की है− सौरभ द्विवेदी
हम दुनिया के सबसे ढेरम पिल्लार शहर उरई में रहते थे. यहां की सबसे चमकदार टॉकीज थी अर्चना. तो वहीं पर आई साल की सबसे बड़ी फिल्म. गदर. सन्नी देओल वाली. मगर तभी पता चला कि फिल्म के चक्कर में कहीं कहीं मार हो गई. शायद लखनऊ या कानपुर में सांप्रदायिक तनाव हो गया था. अर्चना वाले का मूत रुक गया. और किस्मत चमक गई कृष्णा टाकीज की.
सौरभ
कृष्णा टॉकीज. टेलर वाली गली का एक कोना. सामने क्राउन टेलर. पूरी गली में अकेली दुकान जो दो शटर वाली थी. लोग गर्दन उचकाकर इसकी चिट्ट दिखाते थे कमीज से. तब ब्रांड के नाम पर एक्शन के जूता ही शो ऑफ का हिस्सा होते थे. बाकी बहस इस पर होती थी कि कमीज कौन बढ़िया सिलता है. कंचन टेलर, डिलाइट या फिर क्राउन, जो सबसे ज्यादा पइसे लेता है. वैसे दावेदार एक और था. मोती. मगर उसकी अपनी दुकान नहीं थी. हावर्ड ड्राई क्लीनर वालों के यहां एक मशीन लिए बैठता था. लेकिन गांधी डिग्री कॉलेज के चिकाईबाज कहते थे कि जो कटाई मोती करता है, वो बोर्ड और पर्ची वाले टेलर क्या करेंगे. बात भटक गई, माफी चाहता हूं. कमीज काटने बैठता हूं और बीच में पाजामे का नारा नापने लगता हूं.
तो बात कृष्णा टॉकीज की. यहां हम एक ही बार गए थे. वेजीप्रो की फैक्टरी में मोहन मामा काम करते थे. ताई जी के भाई. मगर तब सबके मामा सबके मामा होते थे. कजिन शब्द जीवन में नहीं आया था. न ही शब्द और न ही भाव. कोई पूछता कि कितने भाई बहन हो तो गर्व से कहते. 9 भाई 6 बहनें. सामने वाला अजकजा जाता फिर कहता, अरे भाई सगे बताओ. हम भी अड़ जाते. सब सगे ही समझ लो.
मगर कृष्णा टॉकीज शहर की सगी नहीं रह गई थी. पाप का अंत जैसी कोई फिल्म लगी थी, जब हम इसमें पहली बार गए. फिल्म देखने नहीं. आमलेट खाने. मोहन मामा के साथ. कुछ और दोस्त थे उनके. इंग्लिश पिक्चर जैसे नाम थे उनके. नाम क्या सरनेम. रस्तोगी अंकल. और मिसेज पुंडीर के दूल्हा भी. मामा ने हमें जूता दिलाए. लौटते में आमलेट खिलवाया. प्लेट आई. सफेद. चीनी मिट्टी की. उसमें भाप छोड़ता आमलेट. साथ में छुरा कांटा. सब उसमें फंसाकर खा रहे. हम उठाते, गप्प से बीच में दबाते. फिर उठाते और मुंह खोलने के पहले आमलेट सरक कर नीचे पहुंच जाता. बड़ी देर बाद मामा की नजर गई. उन्होंने चुरा कांटे हटा दिए. आमलेट की चुक्की बना दी. जैसी बुकनू रोटी में बनती थी. और हमने निपटा दिया. डकार मारी तो पोस्टर देखा. गोविंदा था अपना. पाप का अंत कर रहा था.
फिर जैसा पहले बताया, टॉकीज का अंत होने लगा. फिर इसमें गंदी वाली पिक्चरें लगने लगीं. फूलन का हसीन बदला. चंपा चुप नहीं रहेगी जैसी. गांव से रविंद वकील के छोटे भइया देखने आते. हमने ताड़ लिया. फिलिम देख चुपचाप निकल रहे थे. झोला टांगे. पर बताते किसे. बर्रे को बताया. मेरा गांव का दोस्त. बोले. अरे भइया, बे बड़े आदमी हैं. सौकीन हैं. का कहें.
उसी कृष्णा टॉकीज की किस्मत खुली गदर से. सन्नी देओल का बड़ा सा (मतलब 8 फुट का) कटआउट बना. टेलर वाली गली के दरवाजे पर रखा गया. पूरे हाल की पुताई हुई. हल्के नीले रंग का डिस्टैंपर. कैंटीन में नए गिलास आए. लाल पेंट लगाया गया. समोसे छानने के लिए एक भट्टी एक्स्ट्रा. वो इकलौती बार था, जब हमने उस गली में नए कपड़े के रेशों वाली रासायनिक खूशबू नहीं पाई. हर तरफ भैरो गुटखा की तीखी गंध उठ रही थी. लोग लटपटाए घूम रहे थे. टिकट ब्लैक हो रहे थे. पहली बार साक्षात देखा. जैसे फिल्मों में दिखाते थे. 35-35 रुपया का बिक रहा था 20 वाला टिकट.
फिल्म कृष्णा वालों ने चार हफ्ते के लिए उठाई थी. उसी में काया पलट हो गई. सुबह साढ़े 10 वाला नीली पुताई वाली गरम फिल्मों का शो भी गदर के हिस्से आ गया. अर्चना वालों को काटो तो खून नहीं. मगर करें क्या. चार हफ्ते बाद फिल्म वापस ली. अपने यहां लगाई. मगर तब तक तो पूरा जिला देख चुका था. बस हम बचे थे.
हमने ये उरई में नहीं देखी. लखनऊ में देखी. पेपर देने गए थे एनडीए का. वहीं निपट लिए. हिंदुस्तान जिंदाबाद याद रहा. तब तक अमीशा पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल वाली लड़की सी लगती थी. तो उसे चुनरी पहन ट्रक वाले से प्यार करते देख हिंदी मीडियम अहम को सहलाहट मिल गई. और याद रहा हैंडपंप वाला सीन. लखनऊ वाले भइया बता रहे थे. अबे यहीं ला मार्टीनियर में हुई है शूटिंग इसकी. लगा कि इतिहास के काफी करीब बैठा हूं. बाहर निकले तो देखा पास के एक सिनेमा हाल में लगान लगी है. गांव देहात की फिल्म. क्रिकेट मैच दिखाया है. ऐसा ट्रेन में लोग बता रहे थे. छक्का मारता है आखिरी गेंद में. हमें लगा कि लेओ. अब बचा ही क्या.
फिर दैनिक जागरण में पढ़ा. आमिर सन्नी लक्की हैं एक दूसरे के लिए. पहले भी इनकी फिल्में साथ आईं और हिट रहीं. दिल के साथ अर्जुन आई थी शायद. और फिर घायल या दामिनी के साथ आमिर की कोई फिल्म आई थीं. सब हिट होती थीं. और अब लगान और गदर हिट हो रही थीं.
कुछ महीनों बाद उरई की अनुराधा टॉकीज में लगान देखी. और फिर देखी. और अब तक देखता हूं. फिल्म भी. इसकी मेकिंग भी. कुछ चीजें हैं, जो याद हैं.
1. क्रिकेट जो था. वो भारत के कुल नॉस्टैलजिया का हिस्सा था. चंद्रशेखर के बारे में चच्चू बताते थे. उन्हीं के शब्दों में कहूं तो लूले को कोई समझ ही नहीं पाता था और गेंद घुस जाती थी. ऐसा ही एक कैरेक्टर लगान में था. फिर सचिन तेंदुलकर जैसा भुवन था. गैंठा. तान के टांग पर छक्का मारने वाला. कपिल देव सा फास्ट बॉलर था. जट्टा दा छोरा टाइप. इसने लगान के मैच के साथ एक अलग रिश्ता बनाया. और जब आखिरी गेंद पर छक्का लगा. तो लगा कि जैसे प्रकारांतर से चेतन शर्मा की गेंद पर मारे मियांदाद के छक्के की याद धुंधली पड़ गई.
2. राधा वाला मिथक बहुत सुंदर ढंग से पिरोया गया. इतना कि आज भी पत्नी से कह देता हूं चुहल में. गोपियां आनी जानी हैं, राधा तो मन की रानी है. उसके पहले जो मंजीरे की कनख के साथ बीट बनती है. वो ताजी थी. एक गुंजाइश भरा भरोसा भी मिला था कि निपट देसी रहकर भी कोई कार्नेशियन के फूलों सी विदेशी सुंदर सुवासित मैम का प्यार पाया जा सकता है. जब कृष्ण जनम के दिन एलिजाबेथ के माथे पर टीका लगा था, तो हमें रोली से भी प्यार हो गया था.
3. भगवान पहाड़ी पर बसे थे. भगवानों को पता नहीं क्यों जनता से दूर जाकर ऊंचाई पर बसना होता है. या बदमाशी पुरोहितों की होती है. और उन तक पहुंचने के लिए हर बार लता सी अकंपित पवित्र आवाज लानी पड़ती है. और चिरौरी करनी पड़ती है. या कि शायद अहम का विसर्जन हो. कि ये गुमान न हो जाए कि अपने तईं सब कुछ ठीक किया जा सकता है. हे पालनहारे, तुम्हरे बिना हमरा कौनोई नहीं. दीनता. दंभ की मौत.
4. लगान एक एतिहासिक किस्सा भर नहीं था. भारत की आलोचना थी. पहले समाज को अपने विभाजित रूप में दिखाया. उसकी दुर्दशा दिखाई. और फिर संगठित होने का नतीजा दिखाया. लेकिन मुश्किल ये है कि फिल्म में तो हीरो अनुसूचित जाति के हीरो को गले लगा लेता है. मगर उसे देख ताली पीटने वाला समाज बाहर आते ही बाभन, ठाकुर, कुर्मी और कोरी में बंट जाता है. दोगले लोग हैं हम. खासतौर पर पढ़े लिखे सवर्ण. जो संस्कार के नाम पर अपनी झूठी श्रेष्ठता से चिपटे हैं जोंक की तरह. अपना ही खून खत्म करते.
5. और फिर फिर गदर याद आती रही. उसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई. जरूरत नहीं लगी. अभी मुल्क गदर मोड में है. जबकि इसे लगान वाली बारीक समझदारी की जरूरत है. एका की जरूरत है. चीखने वाली देशभक्ति की नहीं. हैंडपंप उखाड़ने की नहीं. ड्रामाबाजी करने की नहीं. मगर चारों तरफ देखिए. जिंदाबाद के नारे हैं. किसे जिंदा कर रहे हैं. किसे मार रहे हैं. राम जाने.

तीसरी याद- लगान में गुलाम मुल्क खुद को मुकम्मल रूप से अभिव्यक्त कर रहा था - मिहिर पंड्या
लक्ष्मीमंदिर में देखी थी 'लगान', सपरिवार. गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी के साथ हम सारे बच्चे फिल्म देखने जाया करते थे. फिल्म का मज़ा कम, साथ का मज़ा ज़्यादा होता था उन दिनों. ये वो दौर था जब हमारे शहर के सिनेमाघर घरेलू जगहें होते थे अौर वहां गेट पर तलाशी के नाम पर आपके सामान में रखा बम नहीं ढूंढा जाता था. खाने का चुगुर-मुगुर सब साथ बंधा होता था. ये वो दौर था जब हमारे घर में पिछले दिन की बासी रोटी से बनी डिश मशहूर हुई थी, नाम रखा गया था 'टूटो डिश', क्योंकि उसे देखते ही सब उस पर टूट पड़ते थे.
मिहिर
अौर मैं तो सुपर एक्साइटेड था. वजह, दादा ने बता दिया था कि इस फिल्म में क्रिकेट होनेवाली है. उन्हें ब्रिटिश अभिनेत्री रेचल शेली ने बता दिया था. आमिर खान का इतने जतन से छुपाकर रखा राज़ फिल्म की रिलीज़ के ठीक पहले फाश हो गया था. लेकिन क्या अौर कैसी क्रिकेट, ये मालूम नहीं था. उन दिनों हम इस खेल पर जीते-मरते थे. पर वो टाइम था कि सिनेमा में क्रिकेट ढूंढो तो कुमार गौरव की 'अॉल राउंडर' अौर देव साब की 'अव्वल नम्बर' मिलती थी. फिल्म में मैच के नाम पर हम नसीर साहब की 'चमत्कार' का क्रिकेट मैच देख खुश हो लेते थे. सच यही है कि 'लगान' से पहले तक सिनेमा की दुनिया में देश का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट एक प्रतिबंधित विषय था. 'लगान' सिनेमाई दुनिया में क्रिकेट की कहानी पर लगे अघोषित प्रतिबंध को तोड़नेवाली फिल्म साबित हुई. चार क्रिकेटीय वजहें जिन्होंने 'लगान' को खास फ़िल्म बनाया, वो थीं,
1. 'लगान' बनाते हुए ये ध्यान रखा गया था कि हिन्दुस्तानी दर्शक सिनेमा साक्षर होने के साथ ही क्रिकेट के खेल में भी बड़का एक्सपर्ट दर्शक है, अौर इसे ध्यान में रखकर फिल्म की कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न रचे जा सकते हैं. जब मैच की शुरुआत में भुवन की टीम के चमत्कारी गेंदबाज़ कचरा की गेंद नहीं घूमी, तो ये देखकर मेरी बांछें (वो जहां कहीं भी होती हों) खिल गईं थी. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि 'गेंद पुरानी होने पर स्पिन होती है' जैसी डीटेल एक बॉलीवुड फिल्म अपनी कहानी में बतौर प्लॉट ट्विस्ट इस्तेमाल कर सकती है. दर्शक की बुद्धि अौर जानकारी को इतना सम्मान देते मैंने मुम्बईया फिल्मों को कम ही देखा है. मैं एज़ ए क्रिकेट फैन
गौरवान्वित था उस क्षण.
2. लेकिन इसने सिनेमा का लॉजिक भी बचाकर रखा था. जिस दौर की कथा 'लगान' सुना रही थी, उस दौर में क्रिकेट दो पारी का अौर अोवर आठ गेंद का हुआ करता था. लेकिन फिल्म में मैच को दो पारी का कर देने से पटकथा की एकनिष्ठ गति बीच में भंग हो सकती थी. यहां बताना ज़रूरी है कि 'लगान' की पटकथा क्लासिक केस स्टडी है सिनेमा की पटकथा लेखन की कला में. इसकी शुरुआत में नायक अौर खलनायक के कैरेक्टर ग्राफ उल्टे हैं, हीरो एकदम नीचे अौर विलेन एकदम ऊपर. फिर अन्त तक ये उलटते-पलटते रहते हैं, अौर अन्त में मामला रिवर्स हो जाता है. सिनेमाई किरदारों को ग्राफ़ की शक्ल में तब्दील कर देखें तो क्लाईमैक्स तक जाते हुए यह दोनों किसी रोलरकोस्टर राइड
जैसी तरंग बनाते हैं, जो सिनेमाई पटकथा लेखन का एक क्लासिक सिद्धान्त है. अच्छा किया कि थोड़ी सिनेमाई छूट ली आशुतोष गोवारिकर!
3. लेकिन फिल्म उन दर्शकों को भी नज़र में रखती थी, जिन्हें क्रिकेट का K भी नहीं मालूम. फिल्म के प्लॉट में ही इसकी गुंजाइश थी, कि खेल से अपरिचित दर्शक सरल शब्दों में जान भी ले कि ये बला क्या है, अौर यह मूर्खता भी ना लगे. जैसे-जैसे भुवन के साथी इसे सीखेंगे, वैसे-वैसे क्रिकेट में अनपढ़ दर्शक भी खेल को जानेगा. पर मज़ेदार बात तो ये थी कि जब भुवन अौर उसके देसी साथी खेल सीख रहे हैं, तो यही फिल्म का डिवाइस टूल बन जाता है अमेरिकियों को खेल की बारीकियां सरलता से सिखाने का. जिस ज्यूरी ने वोट दिया 'लगान' को अॉस्कर की बेस्ट फॉरेन लेंग्वेज फिल्म कैटेगरी में पहले पांच में पहुंचाने के लिए, वो क्रिकेट नहीं जानती थी. उन्हें बेसिक क्रिकेट सिखाने का श्रेय 'लगान' के निर्देशक ले सकते हैं.
4. यह फिल्म क्रिकेट को सिर्फ़ एक खेल की तरह नहीं देख रही थी. पहली बार एक ऐसी कहानी हमारे सामने थी, जिसमें खिलाड़ी का खेल उसके व्यक्तित्व का परिचायक था. यह कमाल बात थी. 'गोली' जो गोफ़न शानदार फैंकता था, वो अच्छा गेंदबाज़ बना. 'भूरा' जो मुर्गियां पकड़ने में एक्सपर्ट था, वो बेहतर स्लिप फील्डर बना. यही किसी भी खेल का असली चरित्र होता है. अपने सर्वोच्च पायदान पर जाकर वो खिलाड़ी के समूचे व्यक्तित्व का प्रदर्शनकारी रूप बन जाता है. इंसान की अभिव्यक्ति क्षमता का सर्वोत्तम अौर सम्पूर्ण माध्यम. 'लगान' क्रिकेट को एज़ ए मैटाफर
इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें एक बंधनमुक्त होने की कोशिश करता इंसान, एक जकड़ा हुआ समाज अौर एक गुलाम मुल्क खुद को मुकम्मल रूप से अभिव्यक्त कर रहा था.
बाद में बड़े होकर जब फिल्म दोबारा देखी तो इस मुल्क की तमाम दरारें भी इस फिल्म की कथा में नज़र आईं. कुछ सायास, कुछ अनायास. दोनों ने ही रचना को इस सिने अध्येता के लिए अौर बड़ा अौर मुकम्मल बनाया. लेकिन वो किस्सा किसी अौर दिन.
ये भी पढ़ें :
लगान नहीं, उसकी मेकिंग हिम्मत देती है मुझे हमेशा














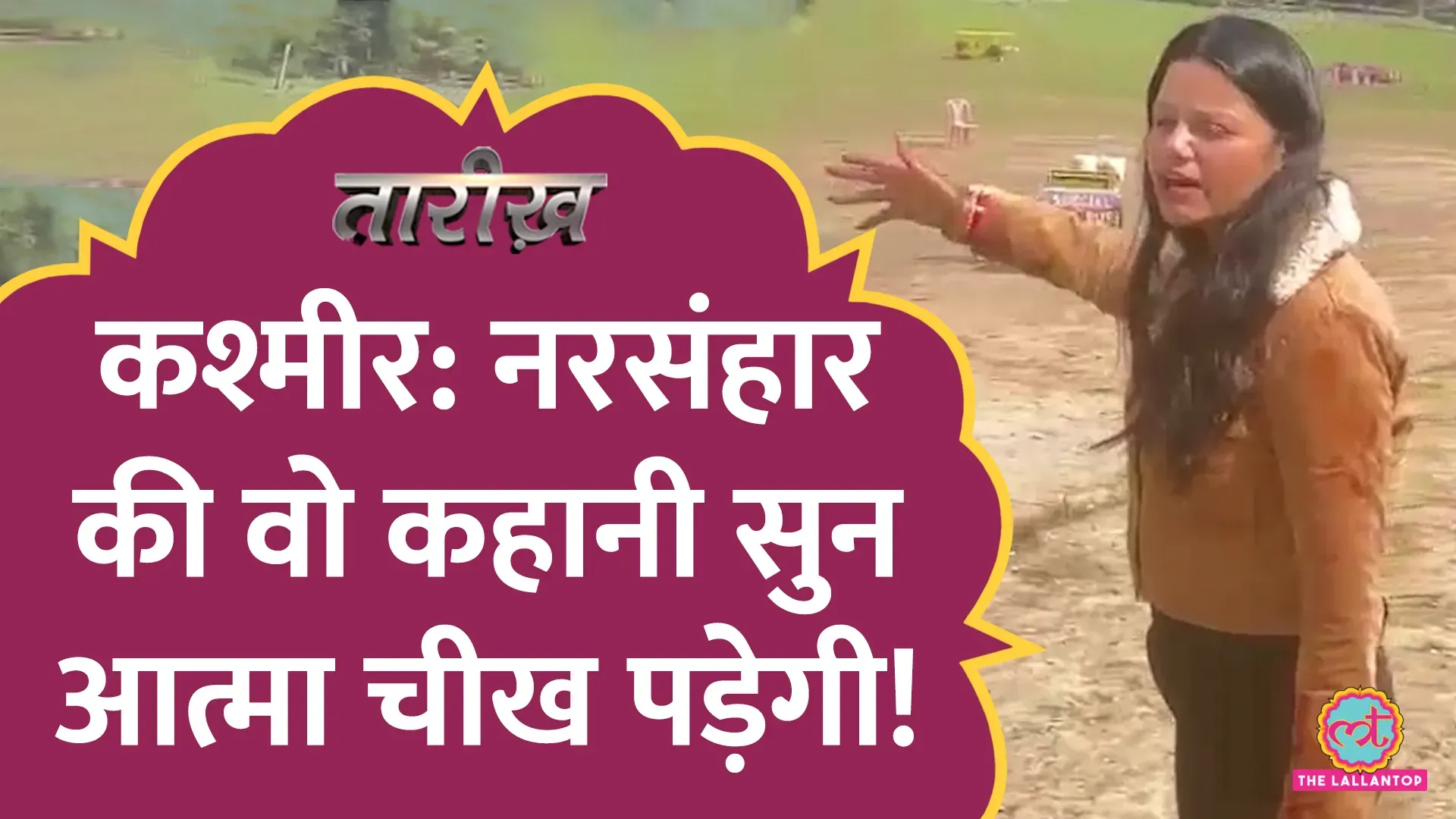
.webp)


