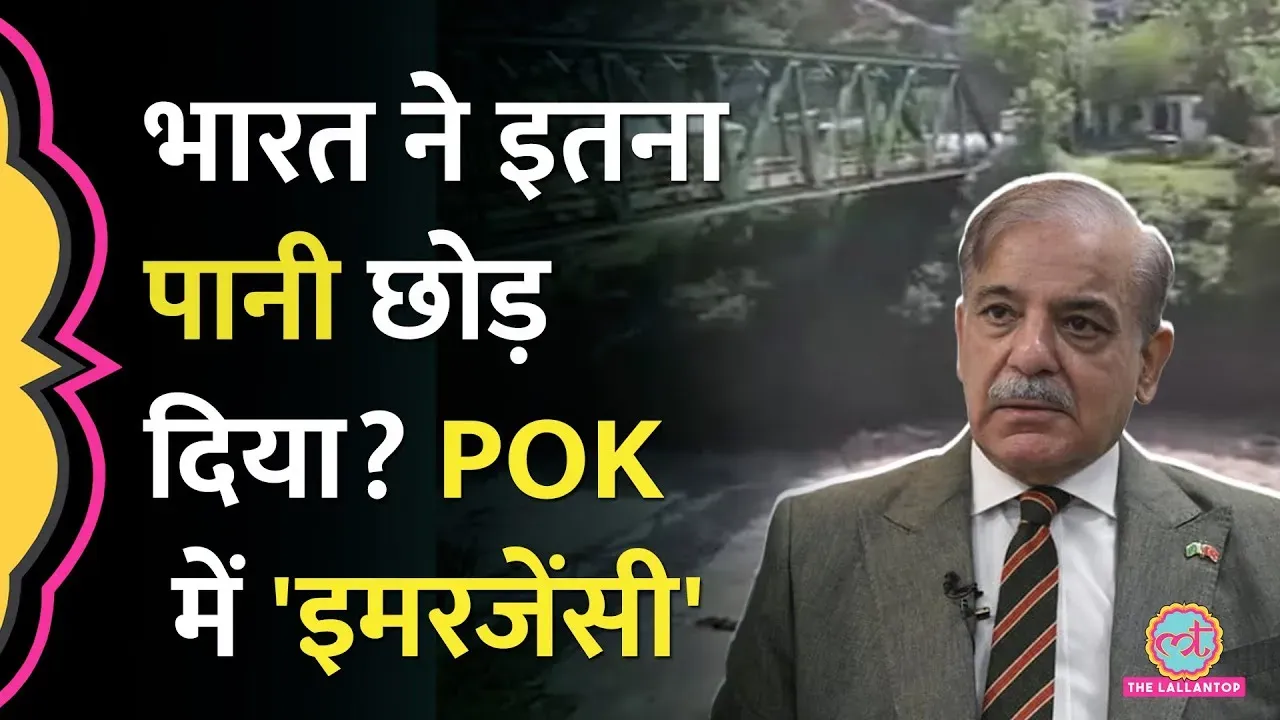एक सोलह साल का लड़का है. मुस्लिम घर में पैदा हुआ, मिशनरी स्कूल में पढ़ा, हिंदू बहुल इलाके में रहता हुआ. तीनों मज़हबों की कॉकटेल को हज़्म कर गया है और स्टीरियोटाइपिंग के चंगुल से बच निकलने के लिए बेकरार है. सालगिरह पर एक बेहद ख़ूबसूरत डायरी मिली है उसे. उसकी ज़िंदगी की पहली डायरी. पहलोटी की कोई भी चीज़ हो उसकी अहमियत का आलम ही दूसरा होता है. फिर चाहे वो प्यार हो या डायरी! लड़का पसोपेश में है कि उस ख़ूबसूरत डायरी पर पहली इबारत क्या दर्ज करे!
निदा फाजली: ग़ज़ल लिखी तो ग़ालिब, नज़्म लिखी तो फैज़ और दोहा लिखा तो कबीर याद आ गए
“घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए”
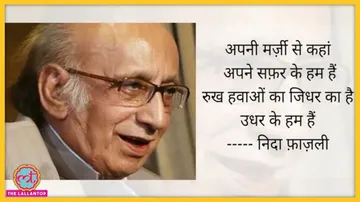
शायरी से इश्क़ शुरू ही हुआ था सो कई शायरों की किताबों से शे'र छांटे गए. ग़ालिब, मीर, इकबाल, मोहसिन नकवी, परवीन शाकिर! बहुत से शेर छांट तो लिए लेकिन किसको पहली एंट्री का शर्फ़ अता करे, इस उलझन ने उलझा रखा था. किसी पर मन ही नहीं ठहरता था. फिर एक पुराने अख़बार की कटिंग से एक ग़ज़ल बरामद हुई. उसे पढ़ने के बाद कोई डाउट न रहा कि वो पहले अल्फाज़ क्या होंगे, जो उस डायरी का और डायरी लिखने वाले की अदबी जगत से मुहब्बत का आगाज़ करेंगे.
ग़ज़लकार थे निदा फ़ाज़ली. उन्होंने पाकिस्तान से लौट कर लिखी थी ये ग़ज़ल. 16 साल की कच्ची उम्र में इस एक ग़ज़ल ने इन पंक्तियों को लिखने वाले शख्स के अंदर ये बात ठूंस दी कि धर्म, मुल्क या और किसी भी पैमाने पर इंसान-इंसान में फ़र्क करना बेवकूफ़ी है. वो क़ाबा हो या काशी हो, सब जगह इंसान ही बसते हैं. दुश्मन मुल्क में भी उतनी ही अच्छाई-बुराई है, जितनी हममें. इंसानी नफ़रत के वजूद में पनपने वाले कीड़े का डंक निकालने का काम बहुत छोटी उम्र में ही इन लफ़्ज़ों ने कर दिया था. बोल थे...
इंसान में हैवान, यहां भी है वहां भी
अल्लाह निगहबान, यहां भी है वहां भी
खूंखार दरिंदों के फ़क़त नाम अलग हैं
शहरों में बयाबान, यहां भी है वहां भी
रहमान की कुदरत हो या भगवान की मूरत
हर खेल का मैदान, यहां भी है वहां भी
हिंदू भी मजे में है, मुसलमां भी मजे में
इंसान परेशान, यहां भी है वहां भी
फास्ट फॉरवर्ड. कई सालों बाद का किस्सा. वो लड़का पुणे छोड़ कर दिल्ली आन बसा है. जॉब-वॉब करने लगा है. मसरूफ़ रहता है. निदा साहब को ढूंढ-ढूंढ कर इतना पढ़ चुका है कि लगता है उनके अशआर पर एक किताब आराम से लिख लेगा. ऐसे में ख़बर मिलती है कि उर्दू के पचास-पचास हज़ार कोस तक मशहूर जलसे ‘जश्न-ए-रेख्ता’ में निदा साहब शिरकत करेंगे. वो अपने ज़हन में 13-14 फ़रवरी 2016 की तारीख़ रजिस्टर कर लेता है. और दिन गिनने लगता है कि अपने चहेते शायर के रूबरू होने की उसकी आरज़ू पूरी होने ही वाली है. लेकिन जो चाहो वो हो जाए, तो ज़िंदगी को कोई भाव क्यों दे! महज़ पांच दिन पहले 8 फ़रवरी को ख़बर आती है कि निदा साहब की रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया है. आज एक साल हो गया उनको दुनिया छोड़े हुए. लेकिन शायद उनसे ना मिलना भी ठीक ही रहा. मिल लेता तो जिस्म से, वजूद से पहचान हो जाती. फिर उस जिस्म के मिट्टी हो जाने का मलाल ज़्यादा रहता. अब तो मेरे लिए वो हमेशा की तरह मौजूद हैं. लिख रहे होंगे कहीं ऐनक संभालते हुए. ऐसा ही कुछ..
“अब किसी से भी शिकायत न रही
जाने किस-किस से गिला था पहले”
निदा साहब का असली नाम मुक़्तदा हसन था. निदा फ़ाज़ली उनका पेन नेम है. तमाम लेखन इसी नाम से किया. निदा का मतलब है ‘आवाज़’. जो कि वो यकीनन थे. फ़ाज़िला क़श्मीर के एक इलाके का नाम है. निदा साहब के पुरखे वहीं से आए थे. इसलिए उन्होंने अपने नाम में फ़ाज़ली जोड़ा. 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली शहर में उनकी पैदाइश हुई थी. निदा साहब की शायरी की ख़ास बात ये कि उसे समझने के लिए आपका उर्दू का ज्ञाता होना ज़रूरी नहीं. साफ़ समझ में आने वाली हिंदी-उर्दू में उन्होंने इतना शानदार लिखा है कि उसके सहर से खुद को बचा ले जाना नामुमकिन है. आप उनके चार अशआर पढ़ लें और बिना इम्प्रेस हुए आगे बढ़ जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता.
“घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें
किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए”
क्या ही कमाल! दो लाइन में इबादत के शउर से लेकर इंसानियत के बुनियादी सलीके तक क्या कुछ नहीं सिखा दिया उन्होंने! ऐसा ही कमाल उन्होंने बार-बार किया. उनके बेशुमार शे'र गवाह हैं इस बात के कि उन्होंने इंसानी ज़िंदगी के हर एहसास, हर जज़्बे को ज़ुबान दी है. ना सिर्फ ज़ुबान दी, बल्कि उन्हें एक मेअयार बख्शा. कुछ ना छूटा उनसे. इस एक नज़्म को देख लीजिये. इससे आप क्या कुछ नहीं साथ ले जा सकते! एक मजबूर औरत की व्यथा, राजनीति के टुच्चेपन पर तंज और साथ ही मज़हबों के संकुचित नज़रिए पर लानत तक सब कुछ है इसमें. और वो भी बेहद आसान अल्फ़ाज़ में..
वो तवाइफ़
कई मर्दों को पहचानती है
शायद इसीलिए
दुनिया को ज़ियादा जानती है
उस के कमरे में
हर मज़हब के भगवान की
एक एक तस्वीर लटकी है
ये तस्वीरें
लीडरों की तक़रीरों की तरह
नुमाइशी नहीं
उस का दरवाज़ा
रात गए तक
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
हर मज़हब के आदमी के लिए
खुला रहता है
ख़ुदा जाने
उस के कमरे की सी कुशादगी
मस्जिद और मंदिर के आंगनों में कब पैदा होगी!
निदा साहब की शायरी में एक तरह की बग़ावत हमेशा मौजूद रही. औरतों की आज़ादी (हर तरह की. ज़हनी, जिस्मानी) से लेकर अपने मज़हब में शामिल कट्टरता तक उन्होंने हर मसले पर लिखा. औरत के किरदार को उसके शरीर से तौलने वाली हमारी महान सभ्यता को अपनी इस नज़्म से उन्होंने ज़रूर असहज कर दिया होगा.
वो किसी एक मर्द के साथ
ज़ियादा दिन नहीं रह सकती
ये उस की कमज़ोरी नहीं सच्चाई है
लेकिन
जितने दिन वो जिस के साथ रहती है
उस के साथ बेवफ़ाई नहीं करती
उसे लोग भले ही कुछ कहें मगर
किसी एक घर में
ज़िंदगी भर झूठ बोलने से
अलग अलग मकानों में
सच्चाइयां बिखेरना ज़ियादा बेहतर है
इस्लाम के नाम पर आतंक की खेती चलाने वाले लोगों को और खामोश रह कर उनकी वहशत की हिमायत करने वालों को जब उन्होंने अपने ही अंदाज़ में चेताया. तो हडकंप मच गया.
“उठ उठ के मस्ज़िदों से नमाज़ी चले गए
दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया”
इस शे'र को पढने के बाद बवाल हो गया. उनको वो महफ़िल अधूरी छोड़ के लौट जाना पड़ा. उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं. जबकि उन्होंने महज़ इस बात पर तनकीद की थी कि इस्लाम का चेहरा गलत किस्म के लोग बनते जा रहे हैं. इसे ना होने दें. निदा साहब के लिखे फ़िल्मी गीतों का भी एक आला मुकाम रहा. फिल्म आहिस्ता-आहिस्ता में इस्तेमाल हुई उनकी ग़ज़ल ‘कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता’ को कौन भूल सकता है! कोई विरला ही संगीतप्रेमी होगा जो इन लफ़्ज़ों के असर से खुद को आज़ाद रख पाता होगा.
“जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है
ज़ुबां मिली है मगर हमज़ुबां नहीं मिलता”
फिल्मों में गीत लिखने का उनका सफ़र अजीब ढंग से शुरू हुआ था. कमाल अमरोही ‘रज़िया सुल्तान’ बना रहे थे. गीतकार जांनिसार अख्तर का अचानक इंतेकाल हो गया. उसके बाद कमाल अमरोही ने जांनिसार अख्तर साहब के ही शहर ग्वालियर के बाशिंदे निदा फ़ाज़ली से राब्ता किया और उनसे इल्तेजा की कि वो फिल्म के बचे हुए दो गाने लिखें. निदा साहब ने वो गीत लिखा जो कब्बन मिर्ज़ा की आवाज़ में गाया गया और बहुत-बहुत मशहूर हुआ.
“तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा ग़म ही मेरी हयात है
मुझे तेरी दूरी का ग़म हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है”
‘तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है’, ‘होशवालों को ख़बर क्या’, ‘अजनबी कौन हो तुम’, ‘दुनिया जिसे कहते हैं’ जैसे तमाम गीत हैं जो उनकी गीतकारी के आला दस्तखत हैं. शायरी की इस आसानी पर गौर फरमाइए कि ये सहज-सुंदर होने के साथ ही मारक भी है.
“ज़िंदगी का मुक़द्दर सफ़र दर सफ़र
आखिरी सांस तक बेक़रार आदमी
हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी
फिर भी तनहाइयों का शिकार आदमी”
गीत, नज़्म और शे'र की बात से बाहर निकलें, तो उनकी उस नायाब सलाहियत पर भी गौर कर लिया जाए, जो उर्दू शायरी में बेहद दुर्लभ है. उनके कहे दोहे उनकी शायरी जितने ही मशहूर हुए. मेरे एक दोस्त का कहना है कि निदा फ़ाज़ली वो शख्स है, जिसने कबीर के दरवाज़े पर दस्तक दी थी. उनके कई दोहों को तो बाकायदा कबीर का काम समझ लिया गया. और क्यों ना समझा जाए, जब बात कहने के ढंग से लेकर बात की सच्चाई तक से फ़कीराना अंदाज़ नुमायां हो रहा हो! कुछेक पर महज़ नज़र ही फिरा लीजिये, इबादत हो जायेगी.
# सबकी पूजा एक सी, अलग-अलग है रीत
मस्ज़िद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत
# सपना झरना नींद का, जागी आंखें प्यास
पाना, खोना, खोजना सांसों का इतिहास
# चाहे गीता बांचिये, या पढिये कुरान
मेरा-तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान
# रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल
चप्पल में जो कील है, पहले उसे निकाल
# सीता रावण राम का, करें विभाजन लोग
एक ही तन में देखिये, तीनो का संजोग
# वो सूफी का कौल हो, या पंडित का ज्ञान
जितनी बीते आप पर, उतना ही सच जान
# अंदर मूरत पर चढ़े , घी, पूरी ,मिष्ठान
मंदिर के बाहर खड़ा, ईश्वर मांगे दान
निदा फ़ाज़ली की लिखी एक ग़ज़ल ‘अपनी मर्ज़ी से कहां अपने सफ़र के हम हैं’ में एक शे'र है. मूलनिवासी होने का दंभ भरते, साथ रह रहे लोगों को बाहरी बता कर धरती पर क्लेम लगाते पूरी दुनिया में फैले नफ़रत के पैरोकारों को चाहिए कि वो इस शे'र को अपने हाथ पे गुदवा लें. जब भी मन में श्रेष्ठताबोध का नाग फन उठाए, इसे पढ़ लें.
“वक़्त के साथ है मिट्टी का सफ़र सदियों से
किसको मालूम कहां के हैं, किधर के हम हैं”
निदा साहब के बारे में लिखना ना तो एक बैठक में होने वाला काम है और ना ही कोई अदना सा आर्टिकल उनकी शख्सियत के साथ न्याय कर सकता है. लिखने जैसा बहुत कुछ है लेकिन फिर कभी. थोडा लिखा है, बाकी आप लोगों के लिए छोड़ दिया है. सुनिए उन्हें और अपने-अपने ढंग से उनकी करिश्माई कलम की तर्जुमानी कीजिए. सैंकड़ों अच्छे शे'रों में से चुनना बेहद मुश्किल काम था लेकिन फिर भी आपके लिए ये कुछ चुनिंदा शे'र.
ये शहर है कि नुमाइश लगी हुई है कोई
जो आदमी भी मिला बन के इश्तिहार मिला
बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो
चार किताबें पढ़ कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे
दिन सलीक़े से उगा रात ठिकाने से रही
दोस्ती अपनी भी कुछ रोज़ ज़माने से रही
इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देगी
रात जंगल में कोई शम्अ जलाने से रही
कुछ लोग यूं ही शहर में हम से भी ख़फ़ा हैं
हर एक से अपनी भी तबीअत नहीं मिलती
हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी
जिस को भी देखना हो कई बार देखना
अजीब दौर है ये तय-शुदा नहीं कुछ भी
न चांद शब में, न सूरज सहर में रहता है
मुट्ठी भर लोगों के हाथों में लाखों की तक़दीरें हैं
जुदा-जुदा हैं धर्म इलाक़े, एक सी लेकिन ज़ंजीरें हैं
आज और कल की बात नहीं है, सदियों की तारीख़ यही है
हर आंगन में ख़्वाब हैं लेकिन चंद घरों में ताबीरें हैं
ख़ुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को
बदलते वक़्त पे कुछ अपना इख़्तियार भी रख
रोशनी की भी हिफाज़त है इबादत की तरह
बुझते सूरज से चराग़ों को जलाया जाए
दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजे रिश्ता
दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए
और ये आखिरी शे'र तो रट लीजिये, घोल के पी लीजिए, ज़हन की दीवारों पर चस्पा कर लीजिए.
“इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे
रोशनी ख़त्म न कर आगे अंधेरा होगा”
ये आर्टिकल निदा फाजली की 5वीं बरसी के मौके पर लिखा गया था.