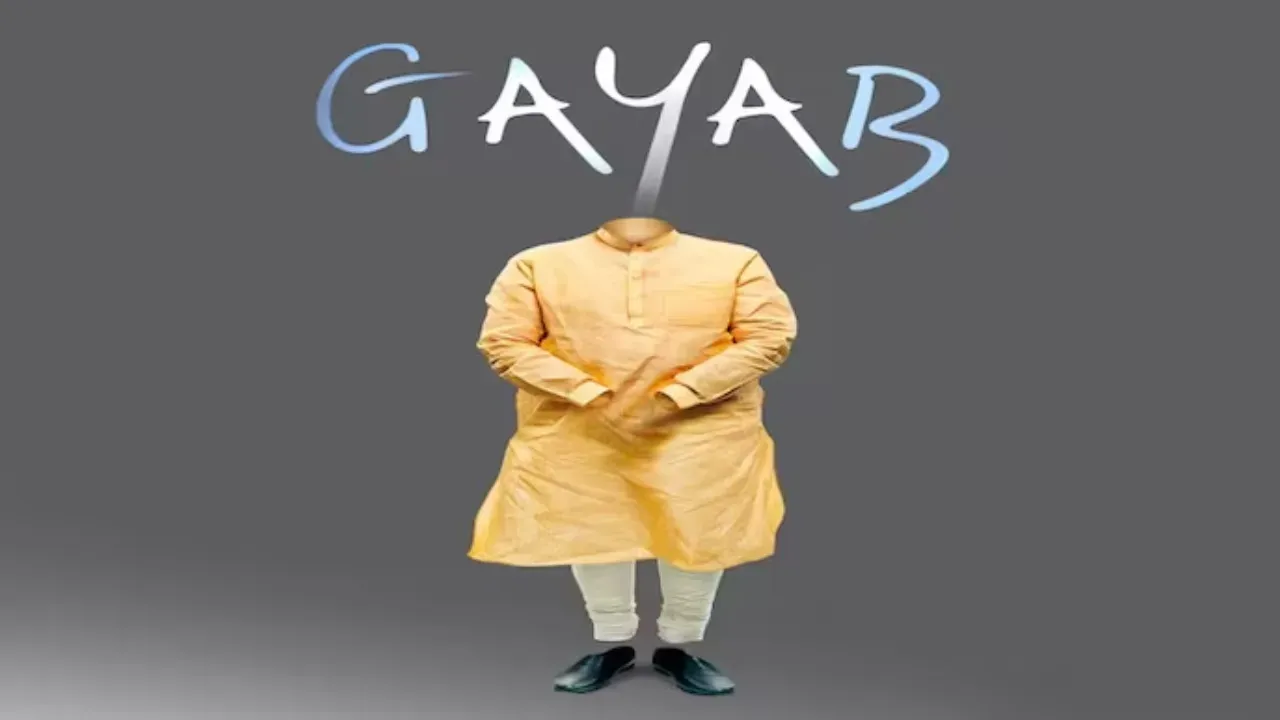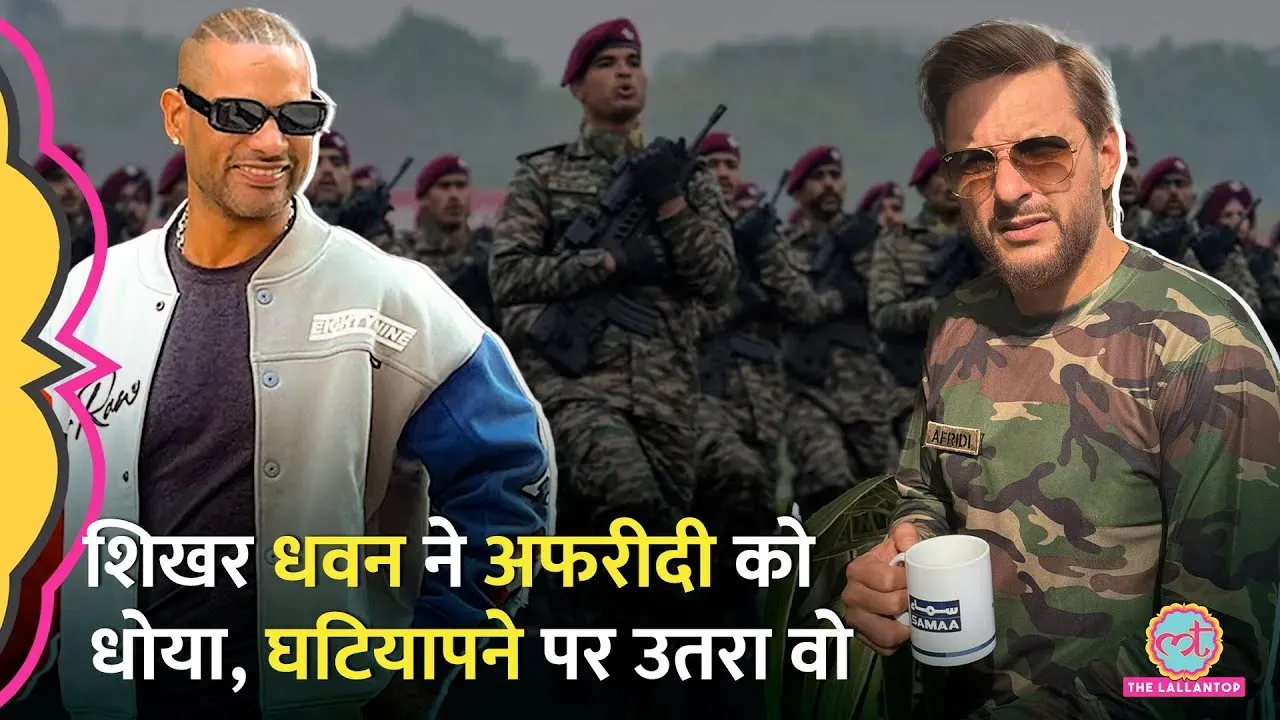Rating: 02 Stars
फुले: महात्मा, और कलाकार के अदने हाथ (Phule Movie Review)
फुले (Phule) जितना विराट कथा कैनवस मिलना किसी भी कला-निर्देशक के लिए सर्वोत्कृष्ट अवसर होगा. क्या director Anant Mahadevan और actor Pratik Gandhi इस अवसर में उतना ही क्राफ्ट और ऊर्जा लगा पाते हैं? पढ़ें इस Lallantop Review में:

"तृतीय रत्न" नाटक जोतिबा फुले की सबसे पहली रचना थी. सन् 1855 में लिखा गया मास्टरपीस. सिनेमा संसार में ऐसा कुछ देखा याद आता है सत्यजीत राय की "अशनि संकेत" (1973) में. हालांकि उस फ़िल्म में सौमित्र चटर्जी द्वारा निभाया हुआ गांव के ब्राह्मण का किरदार नेगेटिव नहीं है, वहां प्रकृति और सामाजिक ताना बाना विलेन है. फिर प्रकृति कुछ ऐसा करती है कि जाति व्यवस्था, नैतिकताएं, परंपराएं, मानव संबंध, पूरा सिस्टम सब भूख के आगे बिखरने और लोटने लगते हैं. वहीं "तृतीय रत्न" का प्रमुख पात्र भी एक ब्राह्णण जोशी है, जिसका चित्रण चरम है. "मदर इंडिया" के सुक्खी लाला से भी ज्यादा निकृष्ट और पतित इंसान का. कहानी में माली कुनबी के घर की स्त्री गर्भवती होती है. यह बात जानकर, जब उसका पति घर पर नहीं होता तो ब्राह्णण जोशी उसके दरवाजे पर आ खड़ा होता है. तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, करण की बात करके डराने लगता है. फिर उसके और स्त्री के बीच लंबा संवाद होता है. वो स्त्री फटेहाल है. खाने को अन्न नहीं लेकिन वो ब्राह्रण जोशी का पात्र बहुत ही लीचड़ व्यवहार करते हुए उस स्त्री को लूट लेता है. उसे भिखारी बना देता है. इस नाटक का एक-एक संवाद जोतिबा फुले की अंतर्वेदना, क्रोधाग्नि, प्रचंड बेलौस अभिव्यक्ति का चित्र है. फुले पर अब तक जितनी भी फ़िल्में या टेलीविज़न शो आए हैं, उनमें से कोई भी उनके भीतरी दावानल को और इस नाटक के जरूरी क्रोध को नहीं दिखा सका है.
डायरेक्टर अनंत महादेवन की नवीनतम रिलीज़ "फुले" भी नहीं.
कैसी है ये फ़िल्म?
"फुले" एक एंटरटेनिंग फ़िल्म नहीं है. जो काम गांधी के चरित्र को विराट बनाने के लिए रिचर्ड एटनबरो ने किया, या संभाजीराजे के लिए लक्ष्मण उतेकर ने किया, या आंबेडकर के लिए जब्बार पटेल ने किया, वो अनंत जोतिबा के लिए नहीं कर पाते. अधिकतम वह ये करते हैं कि हिंदी दर्शकों का परिचय फुले की कहानी से करवा जाते हैं. एक औसत और आंशिक मैसेज डिलीवर कर देते हैं. फ़िल्म जब ख़त्म होती है तो अपनी कमज़ोर स्टोरीटेलिंग के चलते आपको बहुत प्रेरित नहीं करके जाती. जब आप प्रेरित और एंटरटेन दोनों ही नहीं करते तो फिर क्या करते हैं.
कहानी शुरू होती है 1897 के पुणे में. प्लेग फैला है. बूढ़ी सावित्रीबाई (पत्रलेखा) अपनी पीठ पर एक बीमार बच्चे को दूर से लादकर ला रही हैं. आज भी कर्मठ, दूसरों की सेवा को आतुर. मेडिकल टेंट पर उसका बेटा यशवंत (दर्शील सफारी) भी इलाज कर रहा है. यहां आते आते कुछ भी समझ नहीं आता और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है. 1848 का पुणे. जोतिबा फुले माली परिवार से आते हैं. फूलों के पेशे से जुड़े हैं इसलिए परिवार के पास फुले का उपनाम है. अंग्रेजी में उच्च शिक्षा पाए और थॉमस पेन की विराट पुस्तक "राइट्स ऑफ मैन" से प्रेरित जोतिबा का एक ही ध्येय है, सामाजिक बुराइयों को दूर करना. महिला कल्याण और छुआछूत के खिलाफ लड़ना. इसीलिए वे कन्या शिक्षा के क्षेत्र में कट्टरता से काम कर रहे हैं. ब्राह्मण समाज के लोग उनका विरोध करते हैं. मार पीट होती है. जान से मारने की धमकी मिलती है. परिवार को समाज से निष्काषित करने की धमकी मिलती है. अंततः जोतिबा गांव छोड़कर चले जाते हैं पत्नी के साथ, जो कि उनकी पहली स्टूडेंट रही हैं और आगे चलकर भारत की पहली अध्यापिका बनती हैं. वे अपने दोस्त उस्मान के पास चले जाते हैं और वहां रहते हुए अलख जगाते हैं. लड़कियों के लिए स्कूलें खोलते हैं. और कहानी आगे बढ़ती है.
शुरू के काफी वक्त तक फिल्म आकृष्ट नहीं करती. कोई खंभा नहीं गाड़ पाती. बांधती नहीं. इस हिस्से को बुरा भी कह सकते हैं. ये ही स्थापित नहीं होता कि हम किसकी कहानी देख रहे हैं, और क्यों ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण है.
जोतिबा का रोल कर रहे प्रतीक गांधी में उस करिश्मे का अभाव भारी है जो किसी बायोपिक को कैरी करने के लिए एक एक्टर में होना ही चाहिए. जैसे कि उन्होंने "स्कैम 1992" करते हुए हर्षद मेहता के पात्र को करिश्माई बनाया था, डायरेक्टर हंसल मेहता और राइटर्स के योगदान से. उन्हें देख लगता है कि वो कुछ रिसीडेड से हैं, दो कदम पीछे से हटे हुए. वे जोतिबा के भीषण-विराट व्यक्तित्व में कूदकर अपने अस्तित्व को भुला दिए जाने का साहस नहीं बटोर पाते हैं या किन्हीं कारणों से उनकी इसमें रुचि नहीं होती है. जिसकी बायोपिक आप कर रहे हैं उसकी त्वचा में उतरना एक अनिवार्यता है. बल्कि अलौकिक ढंग से आपको उस पात्र में बदल जाना होगा. जैसे डेंज़ल वॉशिंगटन ने "मैल्कम एक्स" (1992) के दौरान किया. डायरेक्टर स्पाइक ली मैल्कम एक्स के भाषण का एक सीन शूट कर रहे थे. वे मॉनिटर के पीछे बैठे थे और स्क्रिप्ट पर नज़रें दौड़ाए जाते थे और डेंज़ल का कमाल परफॉर्मेंस देखते जाते थे. फिर जब भाषण पूरा हो गया तो उन्हें लगा कि अब कट बोल देना चाहिए. लेकिन डेंज़ल रुके नहीं. वे बोलते ही गए और पांच मिनट तक बोलते गए. अंत में कैमरे की फ़िल्म रील ही खत्म हो गई. फिर स्पाइक ने कट बोला. उन्होंने डेंज़ल से पूछा, "आपने शानदार किया लेकिन ये सब आया कहां से? स्क्रिप्ट के बाद आप पांच मिनट तक और कैसे बोलते रहे?" डेंज़ल ने बस इतना ही कहा, "मुझे नहीं पता." ये एक गहरी तैयारी का नतीजा था. उन्होंने मैल्कम के सारे भाषण पढ़े और सुने थे. उनके जीवन चरित्र में उतर गए थे. उनकी विचारधारा में उतर गए थे. वे इतने समर्पित हो गए थे कि मैल्कम के शब्द, सोच और भावनाएं डेंज़ल से एकाकार हो गए और वे पांच मिनट बिना स्क्रिप्ट बोलते चले गए.
विनय पाठक, प्रतीक और पत्रलेखा ने "फुले" में पिता, पुत्र, बहू के रोल किए. भाषाई बेवफ़ाई के चलते ही ये तीनों एक परिवार के लोग कभी लगते नहीं. जिस मिट्टी से जोतिबा, सावित्री और गोविंदराव आते थे वहां का कोई भाषाई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिखता. कुछ जगहों पर प्रतीक मराठी बोलते हैं लेकिन वो टोकनिज़्म लगता है. ये भी लगता है कि इससे ज्यादा शायद वो न बोल सकेंगे. गोविंदराव के रोल में विनय पाठक एक बुरी कास्टिंग हैं. जॉन अब्राहम को लेकर कभी लिखा गया कि वे काठ के एक्टर हैं, वो बात यहां विनय पर लागू होती है. जॉय सेनगुप्ता, अमित बहल के विलेनस ब्राह्रणों वाले किरदार बल्कि कहानी को अपने कालखंड में स्थापित करने का काम बेहतरी से करते हैं. सावित्रीबाई के रोल में पत्रलेखा निर्विवाद मिसफिट हैं. वे कर्मठ, प्रतिबद्ध तो दिखती हैं लेकिन उनकी प्रेज़ेंस में वो तेज नहीं है जो सावित्रीबाई जैसे विरले चरित्र को निभाने के लिए चाहिए. मराठी की कामना न भी रखें तो उनका हिंदी उच्चारण भी सामान्य नहीं है. चूंकि सावित्री का किरदार पहले सीन से लेकर अंत तक रहता है, ऐसे में पत्रलेखा एक बैड चॉयस की तरह थ्रूआउट अखरती रहती हैं. मुअज्ज़म बेग़, अनंत महादेवन की नवाचार रहित राइटिंग इन व्यवधानों से और धुंधली होती जाती है. राइटिंग में कहीं कहीं अच्छे पल आते हैं, जैसे दोपहर का वो सीन जहां फुले जा रहे हैं और उनकी परछाई सामने से आते ब्राह्णणों के एक समूह पर पड़ने जा रही होती है, तो वे नाराज होते हैं. इस संवाद में फुले कहते हैं - "एक व्यक्ति ने पेड़ से सेव गिरते देखा तो प्रश्न किया और गुरुत्वाकर्षण की खोज की. हमारे वर्ग आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूं कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है?" ये इस फ़िल्म का बेस्ट डायलॉग भी है. कुछ हद तक फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन, सेटवर्क और म्यूजिक उसे एक बुरी फ़िल्म बनने से बचाते हैं.
डायरेक्टर निलेश जळमकर की "सत्यशोधक" (2024) फुले पर बनी बेस्ट फ़िल्म है. इसमें संदीप कुलकर्णी फुले के रोल में करिश्माई लगते हैं. वे फुले के जीवन और कृतित्व के कई आयामों को सही से रेप्रज़ेंट करते हैं. फ़िल्म में एक सीन है जिसमें सावित्री जा रही हैं और उन पर ब्राह्मण समाज के लोग गोबर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं. तभी वहां फुले आते हैं. वे भीड़ की ओर मुड़कर कहते हैं - "जब तुम लोग तर्कों के साथ बहस नहीं कर सकते तो यूं हमला करते हो? अरे, तुम्हारी सावित्री ने भले ही अपने पति की जान बचाई होगी लेकिन मेरी सावित्री ये बात जानती है कि उसका पति तो बस शोषितों का उत्थान करना चाहता है. इन हाथों ने आज विचारों की लेखनी भले ही उठा ली हो लेकिन अभी भी ये हाथ लहूजी के अखाड़े के दावपेंच नहीं भूले हैं ये बात दिमाग में बैठा लेना." एक अद्भुत, एंटरटेनिंग, होलसम सीन. जिसमें एक्टिंग का प्राकट्य भी है, राइटिंग की दक्षता भी और फुले के स्ट्रगल की अंतर्रात्मा भी.
Film: Phule । Director: Anant Mahadevan । Cast: Pratik Gandhi, Patralekha, Vinay Pathak, Darsheel Safary, Joy Sengupta, Amit Behl, Sushil Pandey, Alexx O'Neil । Run Time: 129m । Watch at: Cinemas
वीडियो: गेस्ट इन द न्यूजरूम: कॉमेडी, उरी में सीरियस रोल और बॉलीवुड अवॉर्ड्स पर परेश रावल क्या बता गए?















.webp)