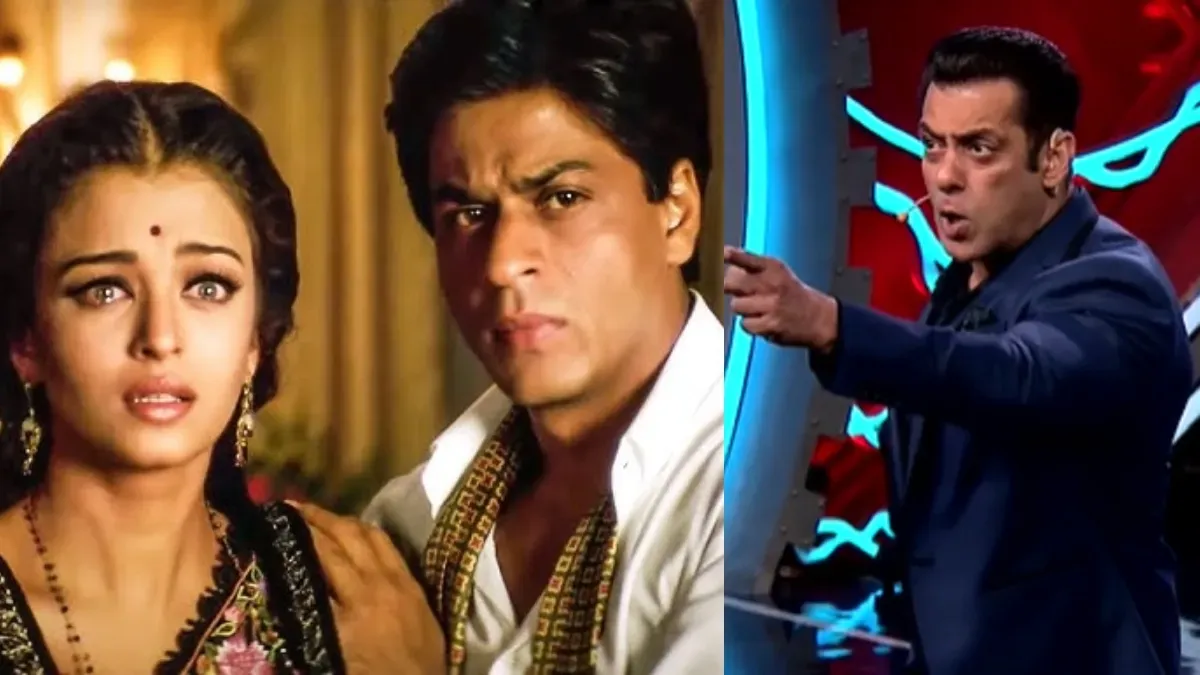फिल्म- मैदान
डायरेक्टर- अमित रविंद्रनाथ शर्मा
स्टारकास्ट- अजय देवगन, गजराज राव, प्रियमणि, इश्तियाक खान, रुद्रनील घोष, विजय मौर्या, अभिलाष थपलियाल
रेटिंग- *** (3 स्टार)
फिल्म रिव्यू- मैदान
अमित शर्मा 'मैदान' को जो बनाना चाहते थे, शायद वो ये फिल्म नहीं है. मगर 'मैदान' वो फिल्म भी नहीं है, जिसे बिना देखे नकार दिया जाना चाहिए. जीवन में कुछ चीज़ों में आपको अपना बेस्ट देकर छोड़ देना चाहिए. उसे किसी नतीजे से नहीं जोड़ना चाहिए.
.webp?width=360)
2019 में एक फिल्म बननी शुरू हुई. ये एक स्पोर्ट्स बायोपिक थी. जो देश में सबसे कम देखे जाने वाले खेल फुटबॉल के बारे में बात करती है. कहानी उस आदमी कि जिसने इंडिया की नेशनल फुटबॉल टीम को कोचिंग दी. उसकी ट्रेनिंग में टीम ने दुनियाभर में डंका बजाया. ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते. इसलिए 1950 से 1960 वाले दौर को भारतीय फुटबॉल इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है. उस करिश्माई शख्सियत का नाम था सैयद अब्दुल रहीम. और उनके ऊपर बनी फिल्म का नाम है 'मैदान'. जो पांच सालों तक मेकिंग में रहने के बाद फाइनली सिनेमाघरों में उतरी है. अपने बेसिक्स क्लीयर हो गए. अब अपन पिक्चर पर बात करते हैं.
'मैदान' देखने के दौरान मुझे दो चीज़ों ने सबसे पहले स्ट्राइक किया-
* ये फिल्म किस बारे में है?
* ये फिल्म किसके बारे में है?
एक ऐसा खेल और एक ऐसा समुदाय, जो भारत में हाशिए पर हैं. आप उन दोनों को उठाते हैं और एक पिक्चर बना देते हैं. यहां ये तर्क कमज़ोर पड़ जाता है कि आपने क्या और कैसा बनाया. हालांकि 'मैदान' में कहीं भी उस समुदाय विशेष की सामाजिक स्थिति पर बात नहीं की गई है. जो चीज़ आगे जाकर खलती भी है. मगर तब तक आप इस सोशल पॉलिटिक्स से आगे निकलकर सैयद अब्दुल रहीम के साथ हो रही पर्सनल पॉलिटिक्स पर पहुंच चुके होते हैं. इसमें कहीं भी उनका धर्म आड़े नहीं आता. मगर हमारे साथ मसला ये है कि अगर धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे, तो जाति के नाम पर लड़ेंगे. जाति की लड़ाई खत्म होगी, तो क्षेत्रवाद शुरू हो जाएगा. 'मैदान' की लड़ाई इसी क्षेत्रवाद से है.
अब कॉन्फ्लिक्ट ये है कि फुटबॉल तो कलकत्ता में सबसे ज़्यादा खेला और देखा जाता है. वहीं से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं. इसलिए उन्हें ही नेशनल टीम में जगह मिलनी चाहिए. मगर रहीम की सोच इससे अलग थी. वो देश के कोने-कोने से अच्छे खिलाड़ियों को जमा करके एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल टीम बनाना चाहते थे, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भारत को मेडल्स दिलाए. ये बात फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) के सदस्य सुभांकर को चुभ जाती है. अब यहां से सुभांकर, रहीम को दरकिनार करने की कोशिशों में लग जाते हैं. इसमें उनकी मदद करते हैं रॉय चौधरी. ये देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं. इनकी रहीम से दुश्मनी इसलिए है क्योंकि एक मौके पर रहीम इनकी अना को भी ठेस पहुंचा चुके हैं.
अब यहां से दो चीज़ें हैं, जो आपको फिल्म में देखने को मिलती हैं. रहीम कैसे भारतीय फुटबॉल टीम के कोच पद से हटाए जाते हैं? और कैसे वापस आकर भारत को टॉप पर पहुंचाते हैं. ये सब एक दम सिनेमैटिक और क्लीशे से भरपूर तरीकों से होता है. 'मैदान' सिनेमा के तौर पर आपको एक्सीपीरियंस के अलावा कुछ भी नया नहीं देती. प्रॉपर टेंप्लेट सिनेमा. मगर मैं डायरेक्टर अमित शर्मा को इसका फुल क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपनी तरफ से इस फिल्म को मास्टरपीस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. उन्होंने इस फिल्म को बनाने में अपना सबकुछ झोंक दिया है. एक तरह से देखें, तो ये उनकी 'बाहुबली' है. और हमें ये चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए.
2018 में अमित शर्मा की 'बधाई हो' रिलीज़ हुई. कोई भी और फिल्ममेकर उस सफलता को भुनाने की हरसंभव कोशिश करता है. वो कॉमर्शियल गुण वाले प्रोजेक्ट चुनता. मगर अमित ने चुनी एक स्पोर्ट्स बायोपिक. ये एक ऐसा जॉनर है, जिसकी गिनी-चुनी फिल्में ही हमारे यहां सफल हुई हैं. मुझे 'चक दे' और 'एम. एस. धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी' के अलावा कोई नाम ध्यान नहीं आता. मगर उन्होंने फिर भी वो कहानी कहने के लिए चुनी, जो उन्हें कंपेलिंग लगी. और उसे बनाने में अपने करियर के पीक पर पांच साल लगा दिए. 2019 से 2024 के बीच 'मैदान' के अलावा उन्होंने सिर्फ 'लस्ट स्टोरीज़ 2' नाम की एंथोलॉजी फिल्म का एक सेग्मेंट डायरेक्ट किया है.

'मैदान' की कहानी सबको पता थी. क्योंकि ये असल आदमी के जीवन पर आधारित फिल्म है. सारा खेल ये था कि उस कहानी को बरता कैसे जाता है. इस फिल्म की राइटिंग (स्टोरी, स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स को मिलाकर) पर 8 लोगों की टीम ने काम किया है. मगर ये इतनी मोडेस्ट फिल्म है कि आपको कहीं भी इसका भान नहीं होता. क्योंकि लेखन में ताज़गी महसूस नहीं होती. आप जब तक दर्शक को चौंकाएंगे नहीं, आप उनका भरोसा नहीं जीत पाएंगे. 'मैदान' ये नहीं कर पाती. आप कमोबेश हर ज़रूरी सीन में गेस कर लेते हैं कि 'क्या' होने वाला है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. मगर जब आप ये गेस कर ले जाते हैं कि वो सीन 'कैसे' होने वाला है, वहां बुरा लगता है.
फिल्म के विज़ुअल्स, राइटिंग की गलतियों को ढंकने की कोशिश करते हैं. फिल्म का VFX टॉप नॉच है. आपको फिल्म में दिखाए गए फुटबॉल मैचेज़ देखकर यकीन नहीं होगा कि इनको बनाने में कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद ली गई है. वो इतने रियल लगते हैं. खासकर फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों के पांव के पास से गुज़रने वाले POV शॉट्स. उस तरह के शॉट्स मैंने आज से पहले किसी फिल्म में नहीं देखे. इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि मैंने बहुत सारा सिनेमा नहीं देखा है.
बहरहाल, 'मैदान' की एक बड़ी खामियों में ये चीज़ भी शामिल रहेगी कि फिल्म की लंबाई 3 घंटे है. फर्स्ट हाफ सेट-अप में निकलता है. जिसकी छंटाई बड़े आराम से हो सकती थी. मगर सेकंड हाफ तेज़ रफ्तार में घटता है. क्योंकि अधिकतर मैच वाले सीन्स इसी हिस्से में आए हैं. ए.आर. रहमान बहुत बड़े संगीतकार हैं. कहना नहीं चाहिए. मगर इस फिल्म के लिए उनका बनाया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे इरिटेटिंग चीज़ है. हालांकि ठीक क्लाइमैक्स में वो इस चीज़ की भरपाई कर देते हैं. 'मैदान' का आखिरी का आधा घंटा, पिछले ढाई घंटे पर भारी पड़ता है.
'मैदान' में अजय देवगन ने सैयद अब्दुल रहीम का रोल किया है. अजय इस फिल्म की आत्मा हैं. वो पूरी फिल्म में संयमित नज़र आते हैं. जिसे फिल्मी भाषा में रेस्ट्रेन्ड परफॉरमेंस कहते हैं. मगर वो टिपिकल हीरो कैरेक्टर है. क्योंकि फिल्म को अजय के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता. यहीं पर मैं 'चक दे' के साथ इस फिल्म की तुलना करना चाहूंगा. शिमित अमीन ने जो चीज़ें अपने हीरो और टीम के साथ कीं, वो शायद अमित शर्मा नहीं कर पाए. 'चक दे' में आपको कबीर खान के साथ उसकी टीम के खिलाड़ियों के बारे में बताया जाता है. उनके आपसी समीकरण फिल्म का बड़ा चंक तैयार करते हैं. कबीर का धर्म फिल्म की धुरी थी. मगर 'मैदान' से वो चीज़ें नदारद हैं. हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको उसकी कमी खलती है.
गजराज राव ने रॉय चौधरी नाम के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का रोल किया है. इस किरदार की लिखावट बहुत ओवर द टॉप है. वो एक समय पर फिल्म का मेन विलन होता है. मगर फिर वही लास्ट में हृदय परिवर्तन वाला घिसा हुआ मटीरियल. वो तो गजराज राव जैसा एक्टर था, जो उस किरदार को बचा ले गया. इसलिए एक एक्टर के तौर पर जनता में आपका गुडविल होना बहुत ज़रूरी है. मगर उनका विग पूरे टाइम आपकी आंख में चुभता रहता है. रुद्रनील घोष ने FFI के सदस्य और (भावी) चेयरमैन सुभांकर का रोल किया है. उन्हें उम्मीद से ज़्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है. और उनका काम भी ठीक है.
अमित शर्मा 'मैदान' को जो बनाना चाहते थे, शायद वो ये फिल्म नहीं है. मगर 'मैदान' वो फिल्म भी नहीं है, जिसे बिना देखे नकार दिया जाना चाहिए. जीवन में कुछ चीज़ों में आपको अपना बेस्ट देकर छोड़ देना चाहिए. उसे किसी नतीजे से नहीं जोड़ना चाहिए. अमित को यही सलाह रहेगी. बाकी खूबी और खामी चीज़ों में नहीं, नज़र में होती है. इसलिए आपको सिनेमाघरों में जाकर 'मैदान' देखनी चाहिए और खुद के लिए फैसला लेना चाहिए.











.webp)