
संदीप सिंह
संदीप सिंह. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जेएनयू से पढ़ाई. स्टूडेंट पॉलिटिक्स का देश का चर्चित नाम. जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे. फिर आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी. सिनेमा, साहित्य, सामाजिक आंदोलनों पर लगातार लिखते बोलते रहे. आज आप उनका चर्चित मराठी फिल्म 'सैराट' पर लिखा आर्टिकल पढ़िए.
फिल्मों का दीवाना नागराज मंजुले
मराठी फिल्म निर्देशक नागराज पोपटराव मंजुले पर हो रही चर्चाओं का दौर थम नहीं रहा है. हिन्दी, अंगरेजी सहित अन्य कई भारतीय भाषाओं में उनकी फिल्म पर लगातार लेख निकल रहे हैं. उनकी हालिया फिल्म सैराट(wild) जाति, लिंग और प्रेम के उलझे, असहज प्रश्नों को तीखे ढंग से उठाने के बावजूद 100 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंचने वाली पहली मराठी फिल्म है. यद्यपि सिनेमा के पारखी मंजुले की बहुप्रशंसित, बहुपुरस्कृत पहली फीचर फिल्म ‘फंड्री’ से ही उनके मुरीद बन चुके हैं. पर मराठी जन-जन से लेकर बाकी हिंदुस्तान में मंजुले अब एक पहचान हैं. संभवतः काफी लोग यह न जानते हों कि नागराज शोलापुर के एक गरीब दलित परिवार से आते हैं. और करीब 80-90 साल पहले तक इनका कुनबा घुमंतू कबीलों की तरह रहता था. नागराज की सिनेमा की विधा में किसी भी तरह की विधिवत शिक्षा नहीं है. सिवाय इसके कि अपनी किशोरावस्था में दीवानगी की हद तक फिल्में देखने के शौक़ीन वे दिन में नियम से दो फिल्में देखा करते थे. अहमदनगर जिले के एक कॉलेज से जन-संचार में एमए के पाठ्यक्रम के तहत पंद्रह मिनट की फिल्म ‘पिसतुलिया’ उनकी पहली लघु फिल्म थी. जिसे 2010 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. पिसतुलिया एक दलित बच्चे की कहानी है जो स्कूल जाना चाहता है. स्कूल की ड्रेस पहनना चाहता है. पर गरीब माता-पिता को लगता है कि पढ़ाई-लिखाई से क्या होगा? बेहतर है वह काम में हाथ बटाये.
जमाने की आंख में झांकता मंजुले का सिनेमा
‘फंड्री’ में एक अत्यंत गरीब, दलित परिवार का दुबला-पतला गहरे रंग का लड़का ‘जब्या’, ऊंची जाति की गोरी रंग की एक लड़की को बहुत पसंद करता है जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती है. वह उसे अपनी ओर आकर्षित करने की तरकीबें सोचता/करता है. उसके सामने अच्छे कपड़ों में आना चाहता है. और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि उससे छुपाता रहता है. वैसे लड़की को इसकी भनक भी नहीं है. फिल्म कभी नहीं बताती कि जब्या की चाहत का क्या हुआ. क्या होता अगर जब्या गोरा होता और लड़की थोड़ा दबे रंग की होती? क्या होता अगर वह लड़की भी जब्या को पसंद करती? क्या होता अगर जब्या के सपनों की जादुई चिड़िया सचमुच उसकी चाहत को उसके करीब ला देती? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आप सैराट देख सकते हैं. कुछ लोग सैराट को उनकी पिछली फिल्म फंड्री (सुअर) का सिक्वेल कह रहे हैं. जिसका काला-कलूटा दलित किशोर जब्या/जामवंत सैराट में आकर प्रशांत/परश्या हो जाता है.
अलबत्ता सैराट, फंड्री का सिक्वेल नहीं है. फंड्री एक डार्क फिल्म थी. जो जवान हो रहे एक दलित किशोर की मासूम हसरतों, दोस्ती और आत्म-छवि को तोड़-मरोड़कर रख देने वाली सामाजिक सच्चाइयों और ‘नियति के साथ साक्षात्कार’ करती राष्ट्रनिर्माण की परियोजनाओं की परतें सहज ढंग से खोलती जाती है. फंड्री का कैमरा 14 साल के दलित किशोर की आंख और हसरतों भरा दिल है. जहां राष्ट्रगान की कीमत एक सुअर से तय होती है. और मरा हुआ सुअर जब्या के टूटे हुए मनोजगत के साथ-साथ राष्ट्र के महापुरुषों के सामने ‘विडंबनात्मक यथार्थ’ बनकर पसर जाता है.
एक विलक्षण सिनेमैटिक-सबवर्जन
सैराट मुख्यधारा के सिनेमा के रास्तों और तिकड़मों का इस्तेमाल करती हुई इस समाज का एक और सच हमारे सामने रखती है. नागराज की ताकत यह है कि वे सिनेमा के ‘इडियम’ और ‘लोकप्रिय’ होने की अहमियत जानते हैं. उनकी विलक्षणता इस बात में है कि वे मुख्यधारा के सिनेमा के तरीकों का इस्तेमाल करते तो हैं पर कहानी अपनी कहते हैं. एक ऐसे वक़्त में जब सामजिक अस्मिताएं ज्यादा से ज्यादा संकीर्ण और कठोर हो रही हैं, सैराट का सफलतम मराठी फिल्म हो जाना आशा की किरण जैसा है. दूसरी तरह से कहा जाय तो सैराट ‘सिनेमैटिक सबवर्जन’ का एक मॉडल है. दिलचस्प है कि इस फिल्म में बहुत कम आभासीपन है और न ही इसे अलग से आकर्षक बनाकर पेश किया गया है. पर यह उतनी ही रोचक है जितनी हमारे समाज की बारीक सच्चाईयों को उजागर करने में सक्षम. ‘बम्बईया सिनेमा’ अगर हमारे आस-पास बिखरे सच को नष्ट करता है या ओझल करता है तो मंजुले की सैराट ‘बम्बईया सिनेमा’ के सच को नष्ट कर एक नए सिनेमा की रचना करती है, सफल बने रहने की जिद पर कायम रहते हुए.सैराट उन चुनिंदा फिल्मों में से है जब हम कमोबेश खुद को ही सिनेमा में देख लेते हैं. हां, इस फिल्म के कर्णप्रिय, मादक, उत्सवी संगीत की कल्पना और रचना करने के लिए अजय-अतुल और मंजुले बधाई के पात्र हैं. और इसपर अलग से लिखे जाने की जरूरत है कि कैसे देशज धुनों, पदों और रूपकों के प्रयोग और संगीत के आधुनिकतम यंत्रों और तकनीकों की इस मिलावट ने फिलहाल पूरे महाराष्ट्र को झुमाकर रख दिया है. मंजुले ने साबित कर दिया कि जाति, लिंग और उत्पीड़न के विषय सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज के लिए नहीं है. कल्पना कीजिये कि आप एक ऐसी फिल्म देख रहे हैं जहां आप मनमोहन देसाई, आदित्य चोपड़ा, करन जोहर, माजिद मजीदी, अडूर गोपालकृष्णन और आनंद पटवर्धन को एक साथ देख लेते हैं. सैराट आपको गुदगुदाती है, हंसाती है, रुलाती है और कभी तो आपका सीट से उछल जाने का मन करता है. रेडिफडॉटकॉम पर ज्योति पुनवानी अपने लेख में तीन परिवारों का ज़िक्र करती हैं जिन्होंने सैराट देखने के बाद अंतर्जातीय प्रेम-विवाह के चलते घर से बहिष्कृत अपने बच्चों को वापस बुलाया और अपनाया.
स्कूल, कविता, प्यार और दोस्ती – सिनेमा की नई दुनिया
नागराज की विशेषता यह भी है वे सिनेमा की दुनिया से बाहर निकाल दिए गए दृश्यों और रूपकों को पुनर्स्थापित करते हैं. कमोबेश उनकी हर फिल्म में स्कूल का केन्द्रीय महत्व है. यही वह जगह है जहां दोस्तियां परवान चढ़ती हैं. चाहत नए-नए रंगों में सामने आती हैं. जीवन में पहली बार कविता आती है और दुनिया अपने रहस्य खोलती है. किशोरावस्था में स्कूल/कॉलेज वे जगहें होती हैं जहां हम जीवन से एक नया साक्षात्कार करते हैं. मंजुले की फिल्मों में स्कूल ही वह जगह है जहां मध्यकालीन निर्गुण कवि चोखामेला (फंड्री) या दलित कविता के हस्ताक्षर नामदेव ढसाल की कविताएं सहज रूप से चली आती हैं. वो बचपन अभागे होते हैं जिन्हें कविता लिखने या सोचने का मौका नहीं मिलता. नागराज बताते हैं कि कितना भी जटिल जीवन हो कविता साथ देती है. उनकी दोनों फिल्मों के युवा नायक कविता लिखते हैं.आजकल का बम्बईया सिनेमा दोस्ती के नाम पर दो प्रतिस्पर्धी चरित्रों का निर्माण करता है जो औरत या ताकत के लिए एक दूसरे से जोर आजमाइश करते रहते हैं. पर हम जानते हैं कि जीवन दोस्तियों का ही दूसरा नाम है. जहां दोस्त के लिए निःस्वार्थ भाव से कोशिशें की जाती हैं. कुर्बानियां दी जाती हैं. खासकर किशोरावस्था की दोस्तियां बगैर छल-कपट के सच्चे मानवीय और सरल मूल्यों का निर्माण करती हैं. फंड्री की मूक दोस्ती सैराट में आकर मुखर हो जाती है. सैराट को उसके मामूली लोगों की बेपनाह दोस्तियों के लिए भी याद किया जाएगा.
भारत जैसे देश में ज्यादातर युवाओं को पहली बार स्कूलों/कॉलेजों में ही पता चलता है कि वे किसी को चाहने लगे हैं. अमूमन ये चाहतें अनकही रह जाती हैं जिनकी टीस आगे चलकर किस्सों, कहानियों में निकलती है. सैराट आपको अपने बचपन और किशोरावस्था में लेकर जाती हैं, यह आपके मन की सबसे नरम जगह छू लेती है और आप छपाक से प्यार की बावड़ी में बावले से कूद जाते हैं. जिस निर्देशक को जीवन की कोमलताओं का इतना अहसास है जाहिर वहां प्यार की चिट्ठियां मासूमियत का प्रतीक एक छोटा बच्चा ही लेकर जायेगा.
सिनेमा का सेट और शैली में प्रयोग
सैराट में शायद ही कोई फ्रेम है जहां कृत्रिम सेट का प्रयोग किया गया हो. सारी जगहें वास्तविक और हमारे आसपास की ही हैं. पर यह मंजुले की सिनेमाई दृष्टि का ही कमाल है कि सैराट में आई बावड़ी, नदी और डैम अब एक पर्यटक स्थल बन चुके हैं. भारत के ग्रामीण परिवेश में हो रहे बदलावों को यह फिल्म पकड़ती है और बनी-बनाई टकसाली छवियों को तोड़ती है. मंजुले यह दिखाने से नहीं चूकते कि जमाना कुछ न कुछ बदला है और उनकी फिल्मों के दलित चरित्र पाटिल (ऊंची जाति) की बावड़ी में जमकर नहाते हैं. फंड्री का अंतर्मुखी ‘जब्या’ सैराट में गांव का धोनी माना जाने वाला ‘परश्या’ बन जाता है जो किसी से दबता नहीं है, उसकी कविताएं कॉलेज के नोटिसबोर्ड पर लगती हैं. और वह क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों में गिना जाता है. जब पूरी तरह से सजा-धजा परश्या अपने दोस्त को घड़ी और पर्स थमा बावड़ी में कूदने के बाद आर्ची की फटकार पर निकल रहा होता है. तब आप कैमरे के मूवमेंट पर गौर कीजिये. कैसे परश्या निचली सीढ़ी से ऊपर आता है. एक पल के लिए वह टशन में खड़ी आर्ची पर भारी पड़ जाता है. यह बहुत प्रतीकात्मक है. चाहे क्रिकेट की कमेंट्री हो या पुरस्कार वितरण में मुख्य अथिति के रूप में विराजमान एक भगवा साधु हो, स्कूटी चलाती आर्ची के पीछे बच्चे को लेकर बैठा परश्या हो या सड़क किनारे भगवा झंडा लिए कार्यकर्ता युवा ‘प्रेमियों/जिहादियों’ की पिटाई कर रहे हों- मंजुले की नजर से कुछ छूटता नहीं है. कुछेक मौकों पर लगता है कि फिल्म खिंच रही है पर तुरंत समझ में आ जाता है कि ऐसा संपादन की समस्या के चलते नहीं हो रहा है. जीवन की सांसारिकता का आख्यान रचने के लिए ‘डिटेलिंग’ में जाना ही पड़ता है. और इसी के माध्यम से निर्देशक आपको सफलतापूर्वक अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है.सैराट निचली जाति के परश्या और एक सवर्ण जमींदार की बेटी आर्ची के प्यार की कहानी है. जाहिर है यह प्यार किसी को बर्दाश्त नहीं. सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाले एक अविस्मरणीय ‘रोमांटिक स्पेल’ के बाद प्यार की डोर से बंध चुके इस जोड़े को जमींदार परिवार की हिंसा का सामना करना पड़ता है. जान बचाने के लिए वे दूसरे शहर भागते हैं. जहां उन्हें एक अप्रत्याशित और नेक मदद मिलती है. शक-शुबहे के भीतर तक चीर देने वाले एक दौर के बाद अपने प्रेम की पुनर्खोज कर वे शादी कर लेते हैं. और अब उन्हें एक बच्चा भी है. लगता है कि ‘हैप्पी इंडिंग’ होने वाली है कि अचानक सालों बाद आर्ची का परिवार उन्हें खोजकर ख़त्म कर देता है. पर उनका बच्चा बच जाता है क्योंकि नरसंहार के समय एक पड़ोसी महिला उसे घुमाने ले गयी होती है. फिल्म के अंत में लहू में डूबे अपने मां-बाप के मृत शरीरों के आतंक में वह बच्चा रोते हुए बाहर की तरफ भागता है. सीमेंट की फर्श पर बच्चे के खून सने पैरों के निशान छूटते जाते हैं. एक लहूलुहान भविष्य की ओर इशारा करते हुए.
सिनेमा का क्राफ्ट
सैराट के माध्यम से नागराज ने यह साबित कर दिया है कि वे ‘सिनेमा के क्राफ्ट’ के अनोखे कीमियागर हैं. उनकी ख़ास बात यह है कि विराट बिम्बों की रचना करते वक़्त बारीक और उपेक्षित सच्चाइयां उसकी नजर से फिसल नहीं जातीं. फिल्म का पहला हिस्सा संगीत और रंगों से भरा हुआ है और दूसरे हिस्से में यह कम होने लगता है. फिल्म के अंतिम भाग में सारे कृत्रिम उपादान धुंधले और हलके होते जाते हैं. कोई संगीत नहीं, कोई बड़ा दृश्य नहीं. अंत में सब कुछ हट जाता है, बचता है सिर्फ सन्नाटा, बच्चे का दारुण रूदन और हमारे इर्द-गिर्द का कोरस. मंजुले की शैली विराट से सूक्ष्म की तरफ जाने की है. और गहरी संवेदनशीलता, ‘पोएटिक इनसाइट’ और असाधारण ‘डिटेलिंग’ से वे इस यात्रा को इतना रोचक बना देते हैं कि लगभग तीन घंटे की लम्बी फिल्म कब ख़त्म हुई यह दर्शक को तब पता चलता है जब फिल्म का अंत उसको भीतर तक झकझोर देता है. दर्शक को थोड़ा-थोड़ा अंदाजा रहता है कि फिल्म कहां ख़त्म होगी, पर फिल्म का अंत उसके लिए एक ‘शॉक’ की तरह आता है. एक मंटोई पटाक्षेप! जहां आपके अंतर्मन में कांच की कोई चादर टूट जाती है. जिसकी कसक और गहरी उदासी लिए आप थिएटर से बाहर निकलते हैं.सैराट में (फंड्री की तरह) पेशेवर कलाकार न के बराबर हैं. और फिल्म के सारे अहम किरदार ऐसे कलाकारों द्वारा किये गए हैं जिनका सैराट से जुड़ने से पहले एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं रहा है. इन सबमें 15 साल की रिंकू राजगुरु द्वारा अभिनीत आर्ची का किरदार सबसे अहम है. सैराट की आर्ची एक दबंग जमींदार और राजनेता की बेटी और उभरते हुए दबंग भाई की बहन है. जाहिर है उसमें भी यह ठसक है. वह बुलेट चलाती है, घुड़सवारी करती है और स्कूल के छोकरों को जब-तब ‘इंग्लिश’ में समझाने की धमकी देती रहती है. जीवन और आत्मविश्वास से भरी थोडा दबे रंग की आर्ची उन रेयर महिला चरित्रों में गिनी जायेगी जिन्हें हिंदुस्तान के सिनेमा में कभी फिल्माया जायेगा. मुखर और हर मौके पर हावी रहने वाली आर्ची प्यार में पड़ने के बाद सामन्ती ठसक त्याग देती है. ‘जो आंख से न टपका तो लहू क्या है?’
को सच साबित करता हुआ उसका चरित्र ही दरअसल फिल्म की जान है. वही अपने प्यार की रक्षा में गोली चलाती है, थानेदार से भिड़ जाती है और ट्रैक्टर चलाकर भरी दोपहर में परश्या के घर पहुंच जाती है. अब उसके लिए जाति का बंधन नहीं रहा. साफ़ तौर से असहज दिख रही परश्या की मां से वह पीने के लिए पानी मांगती है और बाजार में सबके सामने उसका पैर छूती है. आर्ची का चरित्र मुक्तिदायक है. मंजुले ने उसके चरित्र के विकास को पूरी तन्मयता से पकड़ा है. ऐश्वर्य और सामन्ती माहौल में पली-बढ़ी आर्ची, निचली जाति के गरीब लड़के के प्यार में पड़ी आर्ची, एक अजनबी शहर की झुग्गी-झोपड़ी में गटर के ऊपर बने अपने टीन के कमरे और बिना दरवाजे वाले बाथरूम से गुजरते हुए बॉटलिंग प्लांट में मजदूर की नौकरी तक कैसे बदलती है, सीखती है, मंजुले ने इसे रिंकू राजगुरु के कलाकार से निकलवाने में सफलता पायी है.












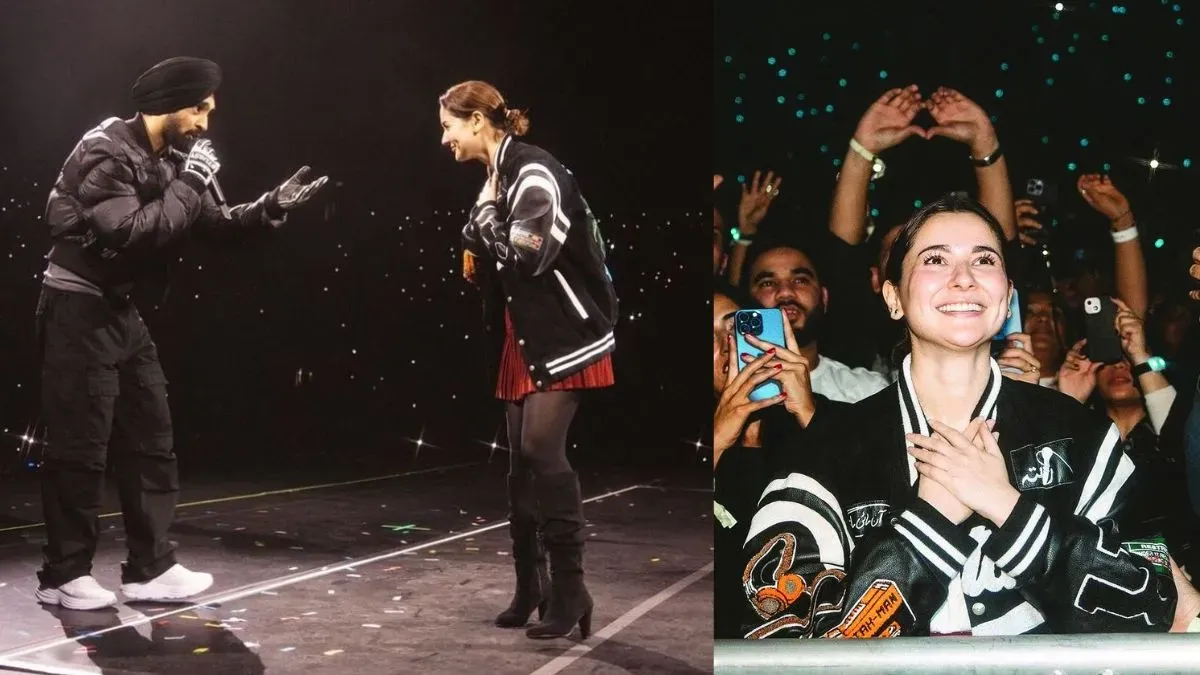
.webp)


.webp)


