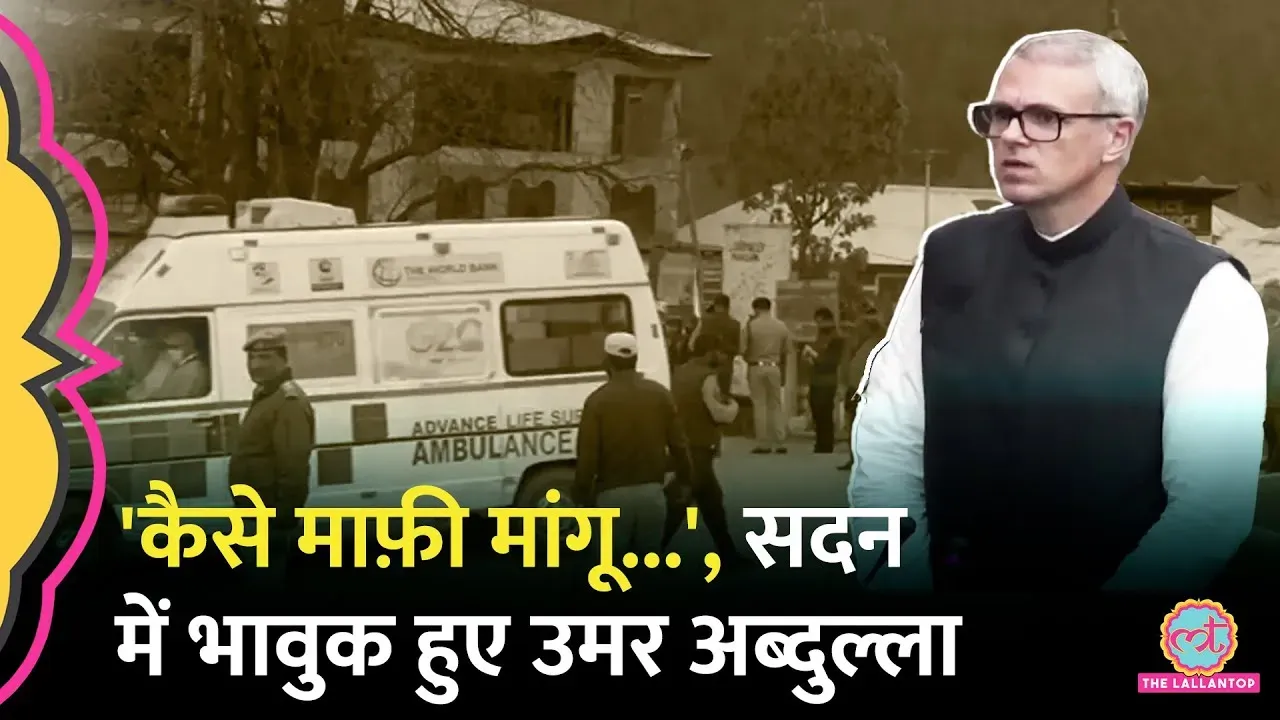रेटिंग - 3.5 स्टार
भक्षक : भारत की अच्छी जर्नलिज़्म मूवीज़ में से एक (फ़िल्म रिव्यू)
Bhumi Pednekar और Sanjay Mishra की मुख्य भूमिकाओं वाली crime thriller movie Bhakshak कैसी है? Netflix पर स्ट्रीम हो रही director Pulkit की इस हिंदी फ़िल्म का विस्तृत और detailed movie review यहां पढ़ें.

एक एंटरटेनिंग और ग्रिपिंग सिनेमा बनने से पहले “भक्षक” चाहती है कि वह एक ज़रूरी फ़िल्म बने. वह इसमें कामयाब भी रहती है. वह ऐसे भयावह मामले पर लोगों की संवेदना जगाने की कोशिश करती है जो लोगों के लिए अख़बार की तीन-चार कॉलम की खबर मात्र होती है. वह संवेदना, जिसे जगाने से फ़िल्में अब परहेज करने लगी हैं. हालांकि कहीं कहीं फ़िल्म रेटोरिकल, शब्दाडंबरपूर्ण होती है. कला-प्रयोगों से दूरी बनाती है. लेकिन जैसे कि पहले कहा, यह फ़िल्म इन सब रास्तों पर नहीं चलने निकली. वह बस एक ज़रूरी कहानी दिखलाना चाहती है. वह आज के जर्नलिज़्म का ज़मीर जगाने की कोशिश भी करती है. कहीं कहीं वो एक छोटी सी “स्पॉटलाइट” भी हो जाती है - डायरेक्टर टॉम मकार्थी की ऑस्कर विनिंग मूवी जो जर्नलिज़्म पर बनी बेस्ट फिल्मों में से है.
हाल ही में एक फ़िल्म आई थी “सिर्फ एक बंदा काफी है”. सीधी और इफेक्टिव स्टोरीटेलिंग थी. मनोज बाजपेयी ने इसमें जोधपुर स्थित ऐसे वकील का रोल किया था जो एक ताकतवर धर्मगुरू पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक नाबालिग लड़की का केस लेता है. “भक्षक” उसी धारा की फ़िल्म है. ये वैशाली और भास्कर के पात्रों पर केंद्रित है, जिन्हें भूमि पेडनेकर और संजय मिश्रा ने प्ले किया है. वे पटना में दो लोगों की टीम वाला अपना संघर्षरत न्यूज़ चैनल चलाते हैं – “कोशिश न्यूज़”. जो बड़ा चतुर नामकरण है. बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़्ड कॉरपोरेट मीडिया घरों की पत्रकारिता के बीच यह छोटा सा स्थानीय समाचार चैनल पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए जर्नलिज़्म कर रहा है. "कोशिश" कर रहा है. तभी इन्हें मुनव्वरपुर नाम की जगह पर एक बालिका गृह में बच्चियों के साथ यौन शोषण और हिंसा की बात पता चलती है. इस बालिका गृह का संचालक (आदित्य श्रीवास्तव) बहुत ताकतवर है. राज्य सरकार में शीर्ष तक पहुंच है. क्या वैशाली और भास्कर शून्य संसाधनों और सपोर्ट के कुछ कर पाएंगे? इन बच्चियों को बचा पाएंगे? यह आगे हम देखते हैं.
दुनिया की सर्वकालिक उत्कृष्ट क्राइम थ्रिलर फ़िल्मों में से एक डेविड फिंचर की “सेवन” में सीरियल किलर जॉन डो का एक नृशंस किरदार होता है. वह कहता है – “लोग आपकी बात सुनें इसके लिए अब यह काफी नहीं रह गया है कि आप उनके कंधे पर हाथ रखकर आग्रह करें. अब तो आपको उन्हें बड़े से हथौड़े से ठोकना होगा. तब जाकर वे आपको नोटिस करेंगे. तब जाकर वे गंभीरता से आपकी ओर पूरा ध्यान देंगे."
फ़िल्म के नैरेटिव में मोटे तौर पर दो तरह से आगे बढ़ा जा सकता है.
एक, या तो आप दर्शक को हथौड़े से मारो यानी उसके मन-मस्तिष्क पर चोट करने वाला तरीका अपनाओ. इसके लिए क्या किया जाता है? सिनेमैटोग्राफर कैमरे के पैंतरे दिखाता है. हिचकॉक की “साइको” इसका एक शास्त्रीय उदाहरण है. फिर थ्रिलर का ज़ॉनर आंशिक रूप से हॉरर होता है. स्क्रीनप्ले इंट्रीग से भरा रखा जाता है. कथानक को खोजकर्ता के सिरे से धीरे धीरे उघाड़ना शुरू किया जाता है. दर्शक भी उसके साथ साथ ही जानता जाता है कि क्या हुआ था, कितना भयावह था, परत-दर-परत. बैकग्राउंड स्कोर इस भयावहता में सहयोग करता है. आप विलेन का उद्घाटन अंत से पहले नहीं करते हैं.
दूसरा तरीका होता है सीधा-सहज. कि कुछ छुपाना, भटकाना, रहस्य रखना नहीं है. सीधी कहानी सुनाएं. दर्शक को पकड़कर उससे कहें कि गौर करो, ध्यान दो. यह तरीका एकदम प्राथमिक दर्शक के लिए होता है. सिनेमा का बेसिक तरीका. ताकि दर्शक को ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े. सारा काम फ़िल्म ही करे. “भक्षक” इसी वृत्ति की फ़िल्म है. इसी शैली में निर्मित है. चूंकि उसकी कहानी, भारत के कुछ असली नृशंस अपराधों से प्रेरित है, ऐसे में इसी को जॉन डो वाला स्लेजहैमर मानकर आगे बढ़ा जाता है.
इस एक “भक्षक” में मुझे दो फ़िल्में नज़र आती हैं. एक - जो स्थानीय पत्रकारों के बारे में है, कि वे अपना काम कैसे करते हैं, खतरे मोल लेते हुए. दूसरी है - एक नृशंस अपराधी के बारे में, जो छोटी बच्चियों के साथ ऐसे क्राइम करता है जो सोचे नहीं जा सकते.
मैं “भक्षक” को दो पत्रकारों की कहानी के रूप में ज़्यादा याद रखूंगा. यह खासी इंट्रेस्टिंग है. हाल में आई प्यारी और विरली फ़िल्म “कटहल” में एक ऐसा ही स्थानीय पत्रकार का करिश्माई पात्र दिखा था, जिसे राजपाल यादव ने प्ले किया था. जब पुलिस आकर कहती है – “अनुज जी, आपको, देश को बदनाम करने की साजिश के आरोप में अरेस्ट करने आए हैं”. तो वह ज़ोर से हंसता है और ख़ुशी ख़ुशी हथकड़ियां डलवाता है और विजयी मुद्रा में अपने मुहल्ले से निकलता है. सत्ता द्वारा गिरफ्तार किया जाना उसके लिए बैज ऑफ ऑनर होता है. अब संजय मिश्रा, भूमि पेडनेकर के पात्र उसी क्रम में आए हैं. हाल के वक्त में जर्नलिज़्म पर आधारित ये बेस्ट प्रस्तुतियां हैं, पात्र हैं. यह हमारी अपनी “स्पॉटलाइट” हैं. वो “स्पॉटलाइट” जिसमें पत्रकारों ने पादरियों द्वारा किए जाने वाले यौन दुष्कर्म के मुश्किल केस को रिपोर्ट किया था.
“भक्षक” के शुरुआती सीन्स में से एक है, जहां वैशाली और भास्कर बैठकर बात कर रहे हैं. अपने एक कमरे के स्टूडियो में. धूल जमी है हर तरफ. ख़ासकर, कैमरा पर. हैडफोन का तार खराब है तो लैंप का वायर लगाया है. फिर भी एक तरफ से आवाज़ नहीं आती. कपड़े एकदम स्थानीय, सस्ते और ऑथेंटिक. भास्कर के रोल में संजय मिश्रा इस फ़िल्म की बेस्ट चीजों में हैं. इस सीन में वे हाथ में कागज़ की प्लेट में नाश्ता लिए, जैसे निवाले लेते हुए बात करते हैं, वो आनंद देता है. बहुत ही नेचुरल एक्टिंग. उन्हें लगातार देखते रहने का मन करता है. एक सीन में वे एक कॉलेज के बाहर सेल्फी मोड में युवाओं की बेरोज़गारी की वीडियो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं. फ्रेम में खड़े युवक कौतुक से हंस रहे होते हैं. इसी रिपोर्ट को बाद में वैशाली यानी भूमि के आलोचक, निंदक ननदोई, जिन्हें वो स्थानीय बोली में मेहमानजी कहकर संबोधित करती हैं, वे घर के बेड पर लेटे लेटे देखते हुए हंस रहे होते हैं. जैसे कॉमेडी सर्कस देख रहे हों. सामने खड़े वैशाली और भास्कर सीरियस हो जाते हैं. कि ये इतने गंभीर विषय पर हंस क्यों रहे हैं. कि उनका जर्नलिज़्म कोई मज़ाक नहीं है. ननदोई भास्कर को चिढ़ाते हुए कहते हैं – “क्या जी. युवाओं की बेरोज़गारी के बारे में बहुत चिंता है. अपने बारे में क्या विचार है. ऐसी न्यूज़ दिखाइएगा तो कौन देखेगा आपका चैनल”. ये आज के जर्नलिज़्म के सामने खड़े द्वंद्व पर भी एक टिप्पणी है. कि दर्शक क्या देखेगा अब इसी से ख़बरें चुनी जाती हैं, अपने महत्व से नहीं.
वैशाली एक पारंपरिक गृहिणी भी है और इंडिपेंडेट जर्नलिस्ट भी. पति अरविंद (रिंकू शर्मा) अपनी लाल वैन उसे यूज़ करने देता है. ख़ुद उसकी पिंक स्कूटी लेकर ऑफिस जाता है, जिस पर लाल अक्षरों में पत्रकार छपा होता है. वैसे वो सपोर्टिव है, लेकिन उसे उसकी स्मॉलटाइम पत्रकारिता अखरती भी है. उसके भाई भाभी हर मौके पर वैशाली से कहते रहते हैं कि शादी को 6 साल हो गए बच्चा कर लो, नहीं तो उमर निकल जाएगी. भूमि ख़ुद को जैसे कैरी करती हैं, वे फिज़िकली वैशाली ही बन जाती हैं. उनका आंचलिक लहजा भी दुरुस्त है. एक सीन कमाल का है जहां अरविंद वैशाली पर चिढ़ता है कि “आने में देर क्यों हो गई, मैं भूखा हूं”. और वैशाली उन बालिका गृह की बच्चियों के लिए कुछ न कर पाने को लेकर इतनी परेशान है कि फट पड़ती है – “अगर तुम्हे भूख लगी है और तुमने खाना नहीं खाया तो इसमें मेरी गलती है क्या! एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल लेकर सीटी मारनी है. बस यही करना है. नहीं कर सकते हो? बच्चे हो क्या? अगर भूख लगी है तो उसे मिटाना भी सीख लो". स्त्री-पुरुष वैवाहिक संबंधों में, सदियों पहले से तय रोल्स के रिवर्सल की तरफ ये संवाद एक ज़ोर का धक्का लगाता है. चाहे चंद जगहों पर भूमि फ्रस्ट्रेशन को लाउडनेस से अभिव्यक्त करती हैं, जो अच्छे से लैंड नहीं करता, लेकिन कुल मिलाकर उनका पात्र एक स्ट्रॉन्ग और ज़रूरी फीमेल कैरेक्टर बनकर उभरता है.
इन दोनों के अलावा एक और पात्र है जो उल्लेखनीय है. नाम - गुप्ताजी. इसे प्ले किया है दुर्गेश कुमार (पंचायत) ने. वह एक विसलब्लोअर सा है.न्यूज़ माइनर है. ख़बरें सूंघता. खोदता है. उसकी पर्सनैलिटी कमाल की है. दिखता जितना सादा है, उतना है नहीं. उसकी हर बात डीप है. दीवार पर लिखा होता है – “यहां कुत्ता थूक रहा है”. और वह वहीं थूकता है. आप सोचते हैं, यह क्या बात हुई. लेकिन वह मूलतः एक क्लासिक जर्नलिस्ट ही है. एंटी-इस्टैबलिशमेंट वाला. जहां उसे नियम दिखाओगे वो तोड़ेगा. दीवार पर न लिखा होता तो शायद वह न थूकता. पर लिखा है तो यह उसका विरोध हो सकता है. तभी वह आम आदमी के विपरीत ख़बरों को सूंघ पाता है, घटनाओं को देख पाता है.
इसके अलावा वह वैशाली और भास्कर का कृष्ण भी है, जामवंत भी. वही है जो बालिका गृह वाली न्यूज़ वैशाली को लाकर देता है. वैशाली को उस ख़बर में न्यूज़ सेंस नहीं दिखता तो वह ताना देते हुए कहता है, “तभी तो यहां हैं आप, नहीं तो नेशनल लेवल की पत्रकार होतीं. मैं आपको सरकार की कॉलर पकड़ा रहा हूं और आप समझ ही नहीं रहीं”. एक सीन है जहां वैशाली यानी भूमि उसे कहती है कि बंसी साहू जैसा खतरनाक आदमी इस मामले में शामिल है ये बात आपको पहले बतानी थी, वो मेरे पति तक पहुंच गया है. सरकार का पूरा समर्थन है उसे. भास्कर भी कहता है कि वो रिपोर्ट दबा देगा क्योंकि सबके भेद खुल जाएंगे. तो गुप्ता कहता है – “तो पत्रकार काहे हैं आप, खोलिए भेद सबका”. भास्कर क्रोध में कहता है कि “आपके कहने पर भेद खोल दें और दुश्मनी ले लें सरकार से?” तो गुप्ता लाचारगी का ताना देते कहता है – “अरे रेरे... लिट्टी चोखा बेचिये ना. किराना दुकान खोलिए. पत्रकारिता में काहे घुसे”. एक और ऐसा संवाद जिसका प्रिंट, पत्रकार अपनी डेस्क पर लगा सकते हैं.
डायरेक्टर पुलकित और ज्योत्सना नाथ का यह लेखन एक ऐसी रेखा पर चलता है, जहां वह इम्प्रेस भी ख़ूब करता है और कहीं कहीं रेटोरिकल भी होता है. जैसे कि फ़िल्म का अंतिम मोनोलॉग. वह एक तरह से देखें तो एक पत्रकार का भावुक आक्रोश है. लोगों में संवेदना जगाने के लिखा गया. लेकिन क्या जॉम्बी हो चुके समाज में, दर्शकों पर ऐसा जेनेरिक संबोधन काम करता है? फ़िल्म का अंतिम वाक्य है – “क्या आप अब भी खुद को इंसान मानते हैं या फिर भक्षक बन चुके हैं”. इस लाइन को सुनकर भीतर कोई विस्फोट नहीं हो पाता.
एक सीन आता है जिसमें बालिका गृह के ऊपर के माले में सरकार का ही अधिकारी एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने के बाद शराब पी रहा होता है. पीछे गाना चल रहा होता है – “ये तेरी आंखें झुकी झुकी”. ऐसा लगता है कि गानों के अंबार में बीच इसे बहुत सोच समझकर चुना गया है. 1996 में रिलीज हुई विक्रम भट्ट की जिस फ़िल्म का ये गाना है उसका नाम था – “फ़रेब”. ये रूपक बन जाता है इस पूरी फ़िल्म में, इन रक्षकों को लेकर. जो इन बच्चियों के साथ, और अपने दायित्व के साथ घोर फ़रेब करते हैं. रक्षक से भक्षक बन जाते हैं. इतने भयावह कि ये सब बातें लिखते हुए भी असहजता होती है.
फ़िल्म के अन्य विभागों की बात करें तो कुमार सौरभ का कैमरावर्क पर्याप्तता के ब्रीफ पर चलता है. डायरेक्टर के विज़न को साकार करने के लिए जितना चाहिए बस उतना ही डिलीवर करता है. फ्रेम्स की लाइटिंग हमेशा नेचुरल बनी रहती है. ऐसा ही ज़ुबिन शेख की एडिटिंग के साथ है. वे फ़िल्म को यूं प्रवाहित करते हैं कि सबसे बुनियादी दर्शक तक बात पहुंच जाए. प्रोडक्शन और आर्ट वर्क फ़िल्म को ऑथेंटिक बनाने में बहुत सहयोग करता है. भूमि, संजय, बालिका गृह की बच्चियों के कपड़ों को लें. चाय के साथ बंसी साहू (आदित्य श्रीवास्तव) पार्लेजी ही खाता है. पूरी फ़िल्म में हर घर-दफ्तर में क्रॉकरी को लें, चाय के कपों को लें, जो फैंसी नहीं होते और छोटे शहरों में अपने इस्तेमाल से मेल खाते हैं. बालिका गृह में नियोन डिस्को लाइट्स तले शराब, सिगरेट पीकर नाचते सब भक्षकों वाले सीन में परदे के पीछे खड़ी सुधा को लें जिसकी स्टील की थाली में बर्फ और पानी की बोतल होती है. उस बोतल पर ढक्कन दूसरी बोतल का लगा होता है. और वह बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखता है. इतनी बारीकी न भी होती तो चलता, लेकिन यह फ़िल्म में बरते गए कमिटमेंट को दिखलाता है.
ये सब फ़िल्म के प्रशंसनीय हिस्से हैं. कुछ इससे इतर फुटनोट्स भी हैं.
एक तो फ़िल्म के अंग्रेजी सबटाइटल में भक्षक के लिए एनिमल शब्द का इस्तेमाल किया गया है. ठीक है. भक्षक वह होता है जो devour करता है, भक्षण करता है. लेकिन वह जानवर ही नहीं होता है. भक्षण कोई भी कर सकता है. दूसरी बात, भक्षक जब आता है तो अपने साथ अपना विलोम भी लाता है - रक्षक. एनिमल शब्द के साथ ये मायने नहीं आ पाते.
दूसरा, फ़िल्म का इंट्रो सीन, जिसमें एक हत्या दिखाई जाती है, अबरप्ट है. वह सीन रैंडम सा बन जाता है. आपको उस घटना की भयावहता के चरम तक ले जाने वाला आधार नहीं दे पाता. बीजीएम भी इस भयावहता को कैप्चर नहीं करता.
तीसरा, विलेन बंसी साहू का इंट्रोडक्टरी सीन. वह बहुत जल्दी रिवील हो जाता है. उसे सामने भी जैसे लाया जाता है वह लेखन जेनेरिक है. जिससे उसकी पर्सनैलिटी घटती है, डायल्यूट होती है. वह एक आम गुंडा सा लगने लगता है और उसके अपराधों की भयावहता भी घट जाती है. इसी फॉर्मेट में कई उदाहरण हैं जहां चरम अपराधों के विलेन को शुरू से ही रिवील करके भी खूब असर गढ़ा गया है. जैसे कि एंथोलॉजी सीरीज़ "डामर - मॉन्सटरः द जेफरी डामर स्टोरी." अमेरिका के सबसे दुर्दांत सीरियल किलर्स में से एक की इस कहानी में डामर को शुरू से ही दिखा दिया जाता है, बल्कि ख़ूब दिखाया जाता है. फिर भी आप इंट्रीग से भरे रहते हैं, टंगे रहते हैं. क्योंकि उसकी निर्मिति ही वैसी है. वह कम बोलता है. धीरे धीरे नाटकीय ढंग से बोलता है. इम्प्रोवाइज़ करता है. खुलकर बोस्ड नहीं करता. बकवास नहीं करता. वह सीधे जवाब टालता है. बुद्धि लगाता है. उधेड़बुन दिखलाता है. बंसी साहू एक ट्रडिशनल विलेन बनकर रह जाता है. वह बुरा है, बोस्ट करता है, घृणित है, गंदा है. बस. कुछ छुपा नहीं है. सब उघड़ा है.
यही कारण है कि एक जर्नलिज़्म मूवी के तौर पर “भक्षक” ज़्यादा लुभाती है.
यह बात यहीं तक.
अस्तु!
Film: Bhakshak । Director: Pulkit । Cast: Bhumi Pednekar, Sanjay Mishra, Aditya Shrivastava, Sai Tamhankar, Durgesh Kumar, Surya Sharma, Chittaranjan Tripathy, Tanisha Mehta, Satyakam Anand । Run Time: 2h 15m । Rating: A - Adult (Child Abuse, Sexual violence refrences, tobacco use)