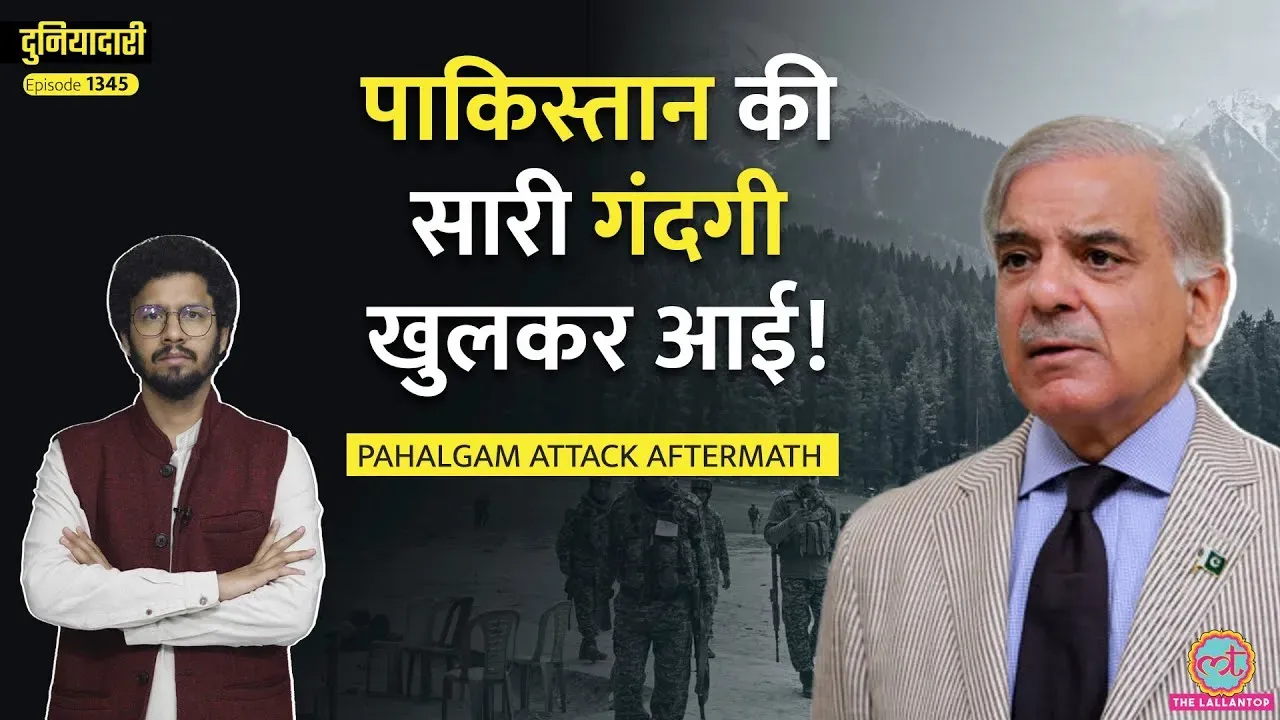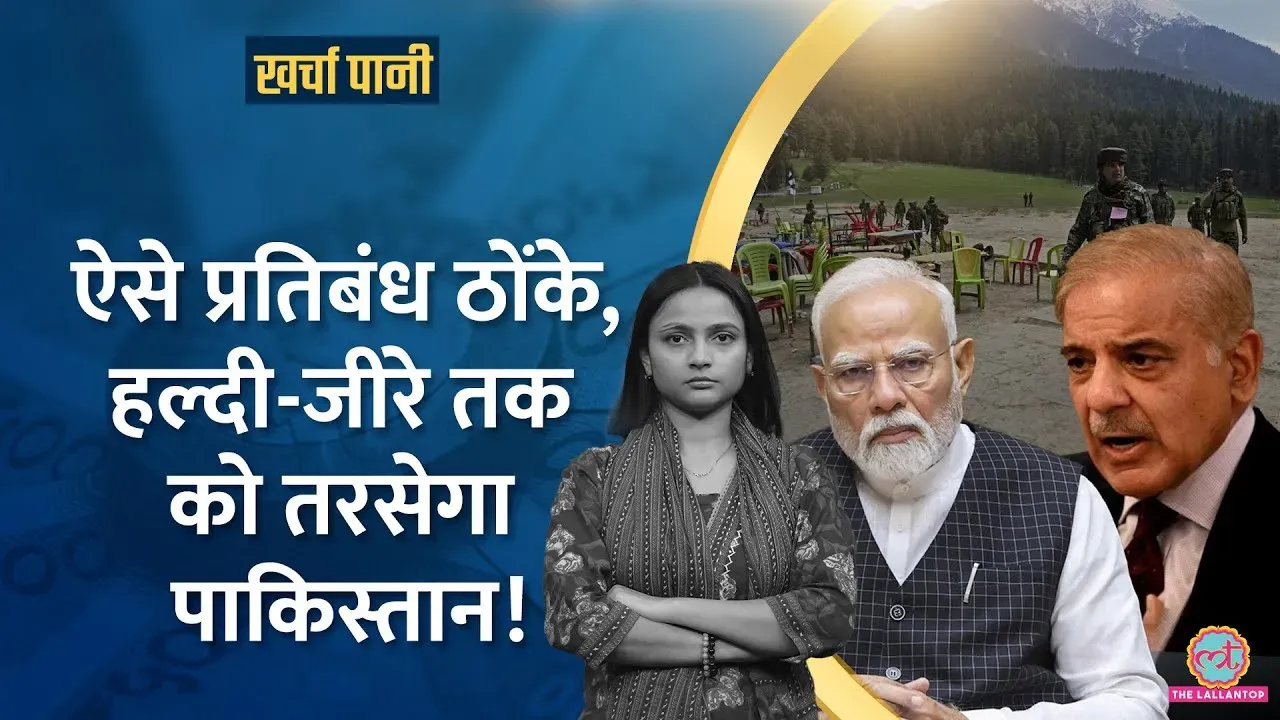उनकी फ़िल्में ऐसी हैं कि देखकर अचंभित होंगे. 'सीरियस सिनेमा', 'वर्ल्ड सिनेमा', 'आर्ट फिल्म', 'इटैलियन-फ्रेंच सिनेमा' और 'रीजनल सिनेमा' जैसे मुहावरे सुनकर बहुत से दर्शक घबराने लगते हैं और इस ओर कभी आते ही नहीं. लेकिन राय की मूवीज़ को लेकर भी ये सोचते हैं तो गलतफहमी है.बहुत से सिने-प्रेमी सोचते हैं कि वर्ल्ड सिनेमा देखना है. लेकिन कहां से शुरू करें? उन्हें.. सत्यजीत राय से शुरू करना चाहिए.
आप 2021 में भले ही रहते हैं लेकिन उनकी फिल्में आपको outsmart करती हैं. वे कभी पुरानी नहीं पड़तीं. 2007 में आई वेस एंडरसन की 'द दार्जीलिंग लिमिटेड' की मुख्य धुन सुनते हुए क्या आपको लगता है कि म्यूजि़क पुराना है? बल्कि उसकी कई धुनें बार-बार सुनने का मन करता है. वेस राय के संगीत के दीवाने थे और उनकी फिल्मों में से म्यूजिक लेकर अपनी इस मूवी में यूज़ किया. राय के म्यूजिक ने इस फिल्म को देखने का अनुभव ही बदलकर रख दिया था.
जिन्हें ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में घुसने से भय लगता है, वे राय की 'अपु ट्रिलजी' देखकर उसे अपने दिमाग़ से बाहर नहीं निकाल सकेंगे. जिन्हें ब्रिटिश सीरीज 'शरलॉक' (होम्स) ने प्रभावित किया है, उन्हें राय की 'जोई बाबा फेलूनाथ' देखनी चाहिए. जिन्हें लगता है कि इतिहास के हार्डकोर इवेंट्स पर भारत में मुकम्मल फिल्में नहीं बनीं, उन्हें 'अशनी संकेत' देखनी चाहिए जो बंगाल के 1943 के अकाल पर बेस्ड थी जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे. जिन्हें लगता है फेमिनिज़्म पर अच्छा सिनेमा अब आने लगा है उन्हें राय की 'महानगर' देखनी चाहिए. सूची बहुत लंबी है.
2 मई 1921 को सत्यजीत राय जन्मे थे और 23 अप्रैल, 1992 को उनका निधन हुआ था. उन्हें इन किस्सों और बातों में याद कर रहे हैं.
#1: उन्होंने 1947 में कलकत्ता फ़िल्म सोसायटी बनाई थी. वे और कुछ अन्य फ़िल्मी दीवाने मिलकर वर्ल्ड सिनेमा और बंगाली फ़िल्मों पर आलोचनात्मक चर्चा करते थे. जिसका विरोध भी झेलते थे. बंगाली फ़िल्म इंडस्ट्री में उनके बारे बातें होती थीं कि ये तो विनाशकारी यंगस्टर्स का एक ग्रुप है जो अपनी बैठकों में बंगाली फ़िल्मों की बुराई करता है. एक बार किसी सोसायटी मेंबर के कमरे वे बैठे थे और चर्चा चल रही थी, तभी मकान मालिक आया और ये कहते हुए उसने सबको बाहर निकाल दिया कि वो फ़िल्मी लोग हैं और उसके घर की पवित्रता ख़राब कर रहे हैं. बाद में यही सत्यजीत राय फ़िल्मी दुनिया में बंगाल की और भारत की सबसे बड़ी पहचान बने.
#2: 'द गॉडफादर' सीरीज और 'अपोकलिप्स नाओ' जैसी एपिक फ़िल्मों के डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला सत्यजीत राय के बड़े प्रशंसक थे. उनकी फ़िल्मों को कोपोला ने स्टडी किया था. उनका कहना था - "हम भारतीय सिनेमा को राय की फ़िल्मों के ज़रिए ही जानते हैं. उनकी बेस्ट फ़िल्म 'देवी' थी. वो एक सिनेमैटिक माइलस्टोन थी."

'द गॉडफादर' (1972) के सेट पर कोपोला, ब्रांडो और पचीनो; राय की फिल्म 'देवी' (1960) का पोस्टर.
#3: जब कोपोला की फ़िल्म 'द गॉडफादर' (1972) रिलीज हुई थी तो कलकत्ता से राय ने उन्हें अमेरिका फोन किया था. फ़िल्म की तारीफ करते हुए उन्होंने कोपोला से कहा कि अल पचीनो इस मूवी में उनकी खोज हैं और इसमें मार्लन ब्रांडो का काम ऐसा है जिसे कोई छू नहीं सकता.
#4: उन्होंने कहीं से भी फ़िल्में बनाने की ट्रेनिंग नहीं ली थी. आत्म-प्रशिक्षित थे. राय बताते थे कि उन्होंने अमेरिकन फ़िल्में देखकर ये क्राफ्ट सीखा.
#5: सत्यजीत राय हॉलीवुड फ़िल्म को देखकर बता देते थे कि उसे किस स्टूडियो ने बनाया है - जैसे, कौन सी एमजीएम स्टूडियो की है, कौन सी पैरामाउंट की है, कौन सी वॉर्नर की है या कौन सी 20थ सेंचुरी फॉक्स की प्रोडक्शन है. वे हर बड़े स्टूडियो के उन विशिष्ट गुणों को पहचान लेते थे जो उन फ़िल्मों में रखे जाते थे. ये पहचान करने में उन्हें बहुत मज़ा आता था. बाद में इसी से वे डायरेक्टर्स की छाप पहचानने लगे. कि जॉन फोर्ड से विलियम वाइलर अलग कैसे हैं, या फिर फ्रैंक कापरा से जॉर्ज स्टीवन्स अलग कैसे हैं? यहीं पर आते आते फ़िल्मों में उनकी दिलचस्पी ने एक गंभीर मोड़ लिया. उन्हें समझ में आया कि कैसे स्टूडियो, स्टार्स या कहानी से भी ज्यादा एक फ़िल्म को सबसे विशिष्ट पहचान उसका डायरेक्टर देता है. और वे डायरेक्टर बने.
#6: अप्रैल 1950 में सत्यजीत राय अपनी पत्नी के साथ इग्लैंड गए. उन्हें उनकी विज्ञापन कंपनी ने छह महीने के लिए हैड ऑफिस भेजा था. कंपनी प्रबंधन से सोचा था कि जब राय लौटेंगे तो फुल टाइम एडमैन बनकर और फिर पूरा मन लगाकर उनके चाय और बिस्कुट वाले विज्ञापन बनाएंगे. लेकिन इस यात्रा ने राय को हमेशा के लिए बदल दिया. लंदन पहुंचने के तीन दिन के अंदर उन्होंने विट्टोरियो डी सीका की महान फ़िल्म 'बाइसिकिल थीव्ज़' (1948) देखी. एड एजेंसी में नौकरी करते हुए पहली फ़िल्म 'पाथेर पांचाली' बनाने का विचार उनके दिमाग़ में कुछ वक्त से चल रहा था. लेकिन विट्टोरियो की फ़िल्म देखने के बाद वे जान चुके थे कि जब भी अपनी फ़िल्म बनाएंगे तो उसमें ऐसी ही नेचुरल लोकेशंस और अज्ञात एक्टर्स होंगे. लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने 99 फ़िल्में देखीं. 'बाइसाइकिल थीव्ज़' और नव-यथार्थवादी (Neo-realist) सिनेमा से सीखे सबक उनके ज़ेहन में घूमते रहे. जब वे भारत लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने 'पाथेर पांचाली' का पहला ट्रीटमेंट लिख लिया था.

'बाइसाइकिल थीव्ज़' के दोनों केंद्रीय पात्र - साइकिल चोरी हो जाने से कष्ट में आए पिता-पुत्र.
#7: उनसे एक बार पूछा गया कि हिंदी फ़िल्मों में कौन एक्टर पसंद है, तो राय ने दो नाम लिए थे - नसीरुद्दीन शाह और नाना पाटेकर.
#8: 'पाथेर पांचाली' (1955) भारत की महानतम फ़िल्मों में बहुत ऊपर आती है. इसे राय ने अपनी पहली फ़िल्म का सब्जेक्ट बनाया उसके पीछे का किस्सा ये है कि राय visualizer और illustrator के काम तो करते ही थे, वे बुक कवर भी डिजाइन करते थे. जब वे सिग्नेट प्रेस के साथ काम कर रहे थे तो एक बार उन्हें 'आम अंतीर भेपू' शीर्षक वाली किताब का कवर डिजाइन करना था. ये बुक दरअसल बिभूतिभूषण बंधोपाध्याय के नॉवेल 'पाथेर पांचाली' का बच्चों के निकाला गया संस्करण थी. राय ने इसका कवर बनाया और किताब में चित्र बनाए. तब वे इसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुए और अपनी फ़िल्म का विषय बनाया.
#9: वेस एंडरसन उन फ़िल्ममेकर्स में हैं जिनकी मूवीज़ दुनिया भर के फ़िल्म फेस्टिवल्स में लोग तलाशते फिरते हैं. जैसे उनकी ताज़ा फ़िल्म 'आइल ऑफ डॉग्स.' वे राय की फ़िल्मों के बड़े मुरीद हैं. कितने बड़े? ये जानने के लिए उनकी 2007 में आई फ़िल्म 'द दार्जीलिंग लिमिटेड' देखें. उसमें उन्होंने सत्यजीत राय के कंपोज किए कई साउंडट्रैक यूज़ किए. एक साउंडट्रैक तो फ़िल्म में हर समय बजता था. उन्होंने राय की फ़िल्म 'जलसाघर', 'तीन कन्या', 'पाथेर पांचाली', 'देवी', 'अपराजितो', 'अपूर संसार', 'जोई बाबा फेलूनाथ', 'चारुलता' और 'कंचनजंघा' की धुनें अपनी फ़िल्म में बरतीं. सत्यजीत राय ने मर्चेंट आइवरी की फ़िल्म 'शेक्सपीयर वाला' और बंगाली फ़िल्म 'बक्सा बादल' में भी म्यूजिक दिया था जिसे वेस एंडरसन ने यूज़ किया. राय द्वारा संगीतबद्ध ये साउंडट्रैक हैरान करने की हद तक बेहतरीन हैं. बार-बार सुनने लायक.
#10: 'अप्पू ट्रिलजी' जैसी विश्व प्रसिद्ध फ़िल्में बना लेने के बाद भी राय अपनी मां, पत्नी, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ किराए के घर में ही रहते थे.
#11: अपनी सब फ़िल्मों के डायलॉग वे ख़ुद लिखते थे. राय ने बताया था कि जब वो संवाद लिख रहे होते थे तो उसी के समानांतर वही लाइन्स पात्रों के मुंह से अपने कानों में सुन रहे होते थे. वो अपने हर पात्र के अलग एक्सेंट, अलग मुहावरे और शारीरिकता को इमैजिन करते थे, और उनकी आवाज़ इन संवादों के साथ सुनते थे. इसी वजह से उनके एक्टर्स डायलॉग बोलते हुए बहुत आसानी महसूस करते थे.
#12: 'गांधी' (1982) जैसी बड़ी और ऑस्कर विनिंग फ़िल्म बनाने वाले सर रिचर्ड एटनबरो का एक दूसरा इंडिया कनेक्शन भी था. ये फ़िल्म बनाने से पांच-छह साल पहले भी वे इंडिया आए थे और उन्होंने एक फ़िल्म में एक्टिंग की थी. फ़िल्म थी सत्यजीत राय की 'शतरंज के खिलाड़ी' (1977) जिसमें रिचर्ड ने जनरल जेम्स आउट्रम का रोल किया था. शूटिंग के दौरान वे राय को मनिकदा कहकर पुकारते थे. जब वे भारत से गए तो उनसे बहुत अधिक प्रभावित होकर. सर रिचर्ड ने बाद में कहा था, "मनिकदा के बारे में जो अद्वितीय बात है, वो ये कि वे फ़िल्ममेकिंग के इतने सारे काम ख़ुद करते थे जो हमेशा अलग-अलग लोग करते हैं. वो स्क्रीनप्ले लिखते हैं. वो ही म्यूज़िक कंपोज़ करते हैं. वो फ़िल्म को डायरेक्ट करते हैं. वो कैमरा ऑपरेट करते हैं. सेट में लाइटिंग कैसी होगी इसमें करीब आधी भूमिका उनकी होती है. वो अपनी फ़िल्म ख़ुद एडिट करते हैं. करीब-करीब वैसे ही जैसे चैपलिन (चार्ल्स) करते थे. अपनी फ़िल्मों में डीटेलिंग को लेकर उनकी दीवानगी इतनी ज़्यादा है कि स्क्रीन पर आपको अंत में जो भी नज़र आता है उसमें 90 परसेंट उन्हीं का डाला हुआ होता है."

एटनबरो ने जब 'जुरासिक पार्क' (1993) में अभिनय किया; 'शतरंज के खिलाड़ी' में संजीव कुमार और सईद ज़ाफरी.
#13: पहली स्क्रिप्ट जो राय ने पढ़ी, वो थी रेने क्लैयर की ब्रिटिश फ़िल्म 'द घोस्ट गोज़ वेस्ट' (1935) की. ये उन्होंने सेकेंड हैंड खरीदी थी और इसे अपनी कीमती चीज़ मानते थे. इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उन्हें आइडिया आया और उन्होंने खाली वक्त में स्क्रीनप्ले लिखने शुरू किए.
#14: उनकी फ़िल्म 'अशनी संकेत' (1973) में एक पात्र था - जोदू/जादू. उस पात्र का चेहरा एक तरफ से जला हुआ था. महिलाएं देखती तो डर जातीं. ये फ़िल्म बंगाल के भीषण अकाल पर आधारित थी. लोग जब भूख से मर रहे होते हैं तो जोदू के पास चावल होते हैं. वो चुटकी नाम की एक विवाहित महिला से सौदा करने की कोशिश करता है. वो चावल देगा, लेकिन बदले में उसे उसके साथ सोना होगा. पहले वो नहीं मानती. लेकिन बाद में भूख उसे तोड़ देती है और वो जाती है. अब किस्सा ये है कि इस फ़िल्म को जब भारत के एक जाने-माने प्लास्टिक सर्जन मुरारी मोहन मुखर्जी ने देखा तो वे जोदू को लेकर भावुक हुए. उन्होंने मन बनाया कि वे इस आदमी की सर्जरी करके इसका चेहरा सही करेंगे ताकि लोग इससे डरे नहीं और सम्मान से जीवन जी सके. उन्होंने फ़िल्म में लीड रोल करने वाले सौमित्र चैटर्जी को फोन किया और कहा कि उन्हें जोदू से मिलना है और सर्जरी करके उसका चेहरा सही करना है. इस पर सौमित्र हंसने लगे. उन्होंने बताया कि आपने जोदू के चेहरे पर जो देखा वो जलने के निशान नहीं थे बल्कि ये सत्यजीत राय का कमाल था. उन्होंने उसका मेकअप ऐसा करवाया कि वो असली जला हुआ चेहरा बन गया. राय की फ़िल्मों में डीटेलिंग इतनी जबरदस्त होती थी.

'अशनि संकेत' में जोदू; और चुटकी. दोनों की परिस्थितियां - त्रासद.
#15: उन्होंने जवाहर लाल नेहरू की 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' और जिम कॉर्बेट की 'मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं' जैसी किताबों के कवर डिजाइन किए थे.
#16: कभी भी उन्होंने कलकत्ता से बाहर रहकर काम नहीं किया. बहुत अच्छी अंग्रेजी, बोलने-जानने, वेस्टर्न पॉप कल्चर का बहुत अच्छा ज्ञान होने के बावजूद उन्हें विदेश जाकर रहना पसंद नहीं था. राय का कहना था - "मेरी जड़ें यहां (बंगाल) बहुत अधिक गहराई में हैं. मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर काम करके बहुत खुश रह पाऊंगा. भारत के दूसरे हिस्सों में शायद ऐसा कर पाऊं. भाषा में भी देखूं तो मैंने हिंदी फ़िल्में बनाई हैं लेकिन मैं तब बहुत आत्मविश्वास महसूस करता हूं जब एक बंगाली फ़िल्म बना रहा होता हूं." उन्होंने कहा था - "मैं कलकत्ता के अलावा कहीं और रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता. बॉम्बे रहने और काम करने के बारे कल्पना ही नहीं कर सकता. वहां मैं अपनी तमाम रचनात्मक ऊर्जा खो दूंगा. एकदम निरर्थक इंसान बन जाऊंगा."
#17: उनकी लंबाई 6 फुट 5 इंच थी. इसकी वजह से उनके कॉलेज में एक प्रोफेसर उन्हें 'लॉम्बो छात्रो' (लंबा छात्र) कहकर बुलाते थे.
#18: राय की जीवनी "सत्यजीत रायः द इनर आई" (1989) की तैयारी करते हुए ब्रिटिश लेखक एंड्रयू रॉबिनसन ने उनके साथ वक्त बिताया था. इंटरव्यू लिए थे. उस बीच एक बार उन्होंने पूछा था, "क्या आपने कभी चाहा था कि अमीर हो जाएं?" इस पर राय का जवाब था - "मुझे लगता है मैं अमीर हूं. फ़िल्मों की नहीं, बल्कि अपनी राइटिंग की बदौलत मुझे पैसे की चिंताएं नहीं हैं. मैं निश्चित रूप से बंबई के एक्टर्स जितना धनी नहीं हूं लेकिन मैं आराम से जी सकता हूं. मुझे बस इतना ही चाहिए. मैं वो किताबें और रिकॉर्ड खरीद सकता हूं जो चाहता हूं."
#19: जिस 'अपु ट्रिलजी' (पाथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर संसार) को देखकर सैकड़ों आकांक्षी फ़िल्ममेकर्स की जिंदगी बदल गई. जिसे देखकर पश्चिम में लोगों का नजरिया भारत के प्रति बदला. जो दुनिया की सर्वकालिक महान फ़िल्मों में गिनी जाती है. उसी 'अपु ट्रिलजी' को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कारों में नहीं भेजा गया. बोला गया कि इसमें भारत की गरीबी दिखाई गई है इसलिए.

बेस्ट तरीका ये है कि जब तक पहली फिल्म न देखें, दूसरी और तीसरी के बारे में कुछ न पढ़ें, कुछ न देखें. इससे कहानी का अनुभव चरम में होगा.
#20: सत्यजीत राय की फ़िल्मों को 32 नेशनल अवॉर्ड मिले थे. जिनमें 6 बार उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवॉर्ड दिया गया था.
#21: कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेज़ीडेंसी कॉलेज में राय ने पढ़ाई की थी. वहां उनके इंग्लिश के प्रोफेसर थे सुबोध चंद्र सेनगुप्ता जो बड़ा सम्मानित नाम थे. वे राय से बहुत नाराज़ थे जब उन्होंने ब्रिटिश एड एजेंसी डी.जे. कीमर में इलस्ट्रेटर की जॉब पकड़ ली. 8 रुपये महीना पर. बात ये थी कि राय अंग्रेजी में जबरदस्त थे. उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप भी की थी. प्रो. सेनगुप्ता सोचते थे कि राय आगे चलकर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के शिक्षक बनेंगे और इस भाषा में अध्यापन क्षेत्र में योगदान देंगे. पर राय दूसरे पेशे में चले गए. लेकिन जल्द ही सेनगुप्ता की नाराज़गी ख़त्म हो गई. 1955 में सत्यजीत राय की डेब्यू फ़िल्म 'पाथेर पांचाली' रिलीज हुई और उसकी चर्चा चारों तरफ हो गई. प्रो. सेनगुप्ता को खुशी थी कि राय ने उनके मन के विपरीत जाकर आखिर सही किया.
#22: अमेरिका के बड़े फ़िल्ममेकर मार्टिन स्कॉरसेज़ी ने सत्यजीत राय को 20वीं सदी के शीर्ष-10 डायरेक्टर्स में गिना था. उनका कहना था कि जब भी उन्हें खुद को प्रेरित करना होता है और दोबारा एनर्जी पाना चाहते हैं तो वे राय की फ़िल्में देखते हैं. जब स्कॉरसेज़ी 14 साल के थे तब टीवी पर अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ उन्होंने 'पाथेर पांचाली' देखी थी और दंग रह गए थे. उनका कहना था - "मैं कामगार लोगों के परिवार से आता हूं और मेरे घर में किताबें वगैरह नहीं होती थीं. ऐसे में मुझे भारतीय संस्कृति से परिचय करवाने वाली फ़िल्म यही थी. और सिसिलियन अमेरिकी परिवार से आने के बावजूद मैंने पाया कि इस फ़िल्म में दिख रहे भारतीय परिवार से ख़ुद को रिलेट कर पा रहा हूं."

'पाथेर पांचाली' में स्कॉरसेज़ी का ये फेवरेट सीन है जिसमें दुर्गा और अपु को रेल की आवाज़ सुनाई देती है और वे कास के फूलों के खेत में से दौड़ते हुए जाते हैं.
#23: उनकी 1962 में रिलीज हुई फ़िल्म 'अभिजान' में वहीदा रहमान ने गुलाबी का रोल किया था. ये फ़िल्म वहीदा ने तब चुनी जब वे 'प्यासा', 'काग़ज के फूल' और 'चौदहवीं का चांद' जैसी फ़िल्मों से बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थीं. इसमें उनकी कास्टिंग यूं हुई, कि सत्यजीत राय ने किसी के ज़रिए वहीदा के घर पत्र भिजवाया जिसमें लिखा था, "मेरे लीडिंग मैन सौमित्र चैटर्जी और मेरी यूनिट का मानना है कि मेरी अगली फ़िल्म की हीरोइन गुलाबी के रोल में आप सबसे उपयुक्त हैं. अगर आप ये रोल करने को हां कहती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी." वहीदा बहुत खुश हुईं कि सत्यजीत राय जैसे फ़िल्मकार ने उन्हें इस रोल में सोचा. कुछ दिन बाद वहीदा ने राय को फोन किया जो सामने से बोले, "वहीदा, आप हिंदी फ़िल्मों में बहुत सारा पैसा कमाती हो. मैं छोटे बजट वाली छोटी फ़िल्में बनाता हूं." इस पर वहीदा ने जवाब दिया, "साब, मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? मेरे लिए ये गर्व की बात है. आपने अपने साथ काम करने की बात करके मुझे इतना सम्मान दिया है. पैसे की कोई समस्या नहीं है. आप आगे से इसका ज़िक्र नहीं करना."
#24: वे अकेले भारतीय हैं जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर दिया गया था. जबकि उनकी कोई फ़िल्म कभी किसी ऑस्कर में नॉमिनेट भी नहीं हुई थी. 1992 में उन्हें ये स्पेशल ऑस्कर अवॉर्ड दिया गया था. वे बीमार थे और कलकत्ता के बेल व्यू क्लिनिक में भर्ती थे. वहां जा नहीं सकते थे इसलिए एकेडमी अवॉर्ड्स के सदस्य कलकत्ता आए, उन्हें अवॉर्ड दिया और एक वीडियो मैसेज लेकर गए जिसे ऑस्कर सैरेमनी में चलाया गया जिसे पूरी दुनिया ने देखा.
#25: चार रोमन टाइपफेस उनके नाम पर पेटेंट हैं - राय रोमन, राय बिज़ार, राय डेफनिस और हॉलिडे स्क्रिप्ट. इनमें से पहले दो टाइपफेस ने 1971 में एक इंटरनेशनल मुकाबला जीता था.

वो चार राय टाइपफेस.
#26: अमेरिका के दिग्गज फ़िल्ममेकर बिली वाइल्डर की 1944 में आई फ़िल्म 'डबल इनडेम्निटी' ने सत्यजीत राय को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने बिली को 12 पन्नों का पत्र लिखकर भेज दिया. लेकिन बिली ने कभी उसका जवाब नहीं दिया. करीब 40-45 साल बाद राय के घर अमेरिका से एक एयरमेल आया. ये बिली वाइल्डर ने भेजा था. उन्होंने राय से बहुत विनम्रता से माफी मांगी थी कि वे उनके पत्र का जवाब नहीं दे पाए. ये यूं हो पाया कि राय को जब ऑस्कर मिला तो उन्होंने अपनी स्पीच में बिली को लिखे पत्र का ज़िक्र किया था कि उन्हें कभी जवाब नहीं आया. राय की स्पीच के बाद हॉलीवुड के दिग्गजों ने खड़े होकर तालियां बजाई. बिली को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुरंत राय को पत्र लिख भेजा और उनकी बेहतर स्वास्थ्य की कामना की.
#27: 1992 में भारत का माहौल सांप्रदायिक हो चुका था. आज भी देश उस समस्या के चरम मोड़ पर खड़ा है. उनके प्रशंसक शायद ही जानते हैं कि राय इस विषय पर फ़िल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे. उन्होंने कहा था - "संभव हुआ तो मैं ऐसी फ़िल्म बनाना चाहूंगा जो इस समस्या (सांप्रदायिकता) को उजागर कर दे."
#28: उनकी फ़िल्म 'महानगर' भारत से बाहर एक फेस्ट में दिखाई जा रही थी. वहां एक फ़िल्म क्रिटिक ने देखा कि आखिरी सीन में कलकत्ता बाज़ार के आसमान की तरफ पैन होता हुआ कैमरा फुटपाथ पर लगी स्ट्रीटलाइट पर टिक जाता है. इसका सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा है, दूसरा नहीं. फिल्म का ये आखिरी सीन है जहां पति-पत्नी के दोनों केंद्रीय पात्र वहां से जा रहे हैं. दोनों अपनी नौकरी खो चुके हैं और सिर्फ उम्मीद है कि इस शहर में उन्हें कोई न कोई दूसरी जॉब मिल ही जाएगी. उस फ़िल्म आलोचक ने इस बात की बड़ी तारीफ की कि कैसे स्ट्रीटलाइट में एक जला और एक बुझा बल्ब, उम्मीद और निराशा के विरोधाभासी इमोशंस को दिखा रहा है. जब सत्यजीत राय से इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहते थे. कलकत्ता की लाइट्स में बल्ब कई बार ऐसे ही आधे जले - आधे बुझे होते हैं जिसका श्रेय नगर निगम को जाता है. ये सिर्फ संयोग की बात थी कि कैमरा ने इस अर्थपूर्ण रूपक को कैप्चर किया.

'महानगर' का वो दृश्य जिसमें स्ट्रीटलाइट का एक बल्ब चालू है; पोस्टर में आरती के रोल में माधबी मुखर्जी.
#29: कमल हसन की फ़िल्में राय ने नहीं देखी थी लेकिन वे उनको जानते थे और उनसे बातें करना पसंद करते थे. उनका कहना था कि कमल बुद्धिमान आदमी हैं.
#30: सत्यजीत राय 23 अप्रैल 1992 को गुज़र गए थे. इससे कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े अलंकरण 'भारत रत्न' से सम्मानित किया था.
#31: वे अमिताभ बच्चन की प्रशंसा करते थे लेकिन उनके साथ फ़िल्म बनाने की बात जमती नहीं थी. राय का कहना था - "मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं लेकिन मैं बंगाली फ़िल्में ही बनाता हूं." जब उनसे पूछा गया कि अमिताभ बंगाली भी बोलते हैं तो राय ने कहा था कि थोड़ी-बहुत बंगाली से काम नहीं चलेगा. और अगर वो गैर-बंगाली किरदार भी निभाना चाहें तो उन्हें टूटी-फूटी बंगाली बोलनी होगी. राय बोले - "दुर्भाग्य से हम दो, अलग-अलग दुनिया में रहते हैं. वो हिंदी सिनेमा के विश्व में और मैं बंगाली सिनेमा के एक छोटे से संसार में." बच्चन परिवार से राय का एक गहरा कनेक्शन ये था कि उन्होंने जया बच्चन को फ़िल्मों में प्रवेश दिया था. जब जया सिर्फ 14-15 साल की थी तब उन्होंने राय की फ़िल्म 'महानगर' (1963) में काम किया था.

तीन दिग्गज: 1977 में भारत यात्रा के दौरान ताज महल घूमते इटैलियन फिल्ममेकर मिकेलएंजेलो एंटोनियोनी, अकीरा कुरोसावा और सत्यजीत राय.
#32: जापान मूल के अकीरा कुरोसावा महान फ़िल्मकार थे. उनके बिना दुनिया के सिनेमा की कल्पना नहीं की जा सकती. किस-किस बड़े फ़िल्मकार ने कुरोसावा से नहीं सीखा. उनकी फ़िल्म 'राशोमॉन' 1952 में कलकत्ता पहुंची तो सत्यजीत राय ने भी देखी. तीन दिन लगातार देखी. वे इससे बहुत प्रभावित हुए. कुछ दशकों के बाद इन्ही कुरोसावा ने राय के बारे में कहा था - "मानव प्रजाति के लिए एक शांत लेकिन बहुत गहरा प्रेम, समझ और अवलोकन उनकी फ़िल्मों की चारित्रिक विशेषता रही है जिसने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया है. मुझे लगता है कि वो मूवी इंडस्ट्री के विराट व्यक्तित्व हैं. उनकी फ़िल्में न देखे होना वैसा ही है जैसे बिना चांद और सूरज को देखे इस दुनिया में जीना है."
Also Read:
वो गंदा, बदबूदार, शराबी डायरेक्टर जिसके ये 16 विचार जानने को लाइन लगाएंगे लोग
सत्यजीत राय अपनी हॉलीवुड फिल्म क्यों नहीं बना पाए और उनके साथ क्या धोखा हुआ!
'संजू' के टीज़र पर 10 बातें : क्या राजकुमार हीरानी की ये फ़िल्म निराश करेगी?
‘ओमेर्टा’ की 15 बातें: हंसल मेहता की ये फिल्म देखकर लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे
'भावेश जोशी सुपरहीरो' का टीज़र आ गया हैः इस साल की मस्ट वॉच फिल्मों में है
इस फिल्म को बनाने के दौरान मौत शाहरुख ख़ान को छूकर निकली थी!
बलराज साहनी की 4 फेवरेट फिल्में : खुद उन्हीं के शब्दों में
'डनकर्क': वो वॉर मूवी जिसमें आम लोग युद्ध से बचाकर अपने सैनिकों को घर लाते हैं










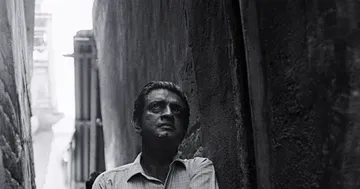



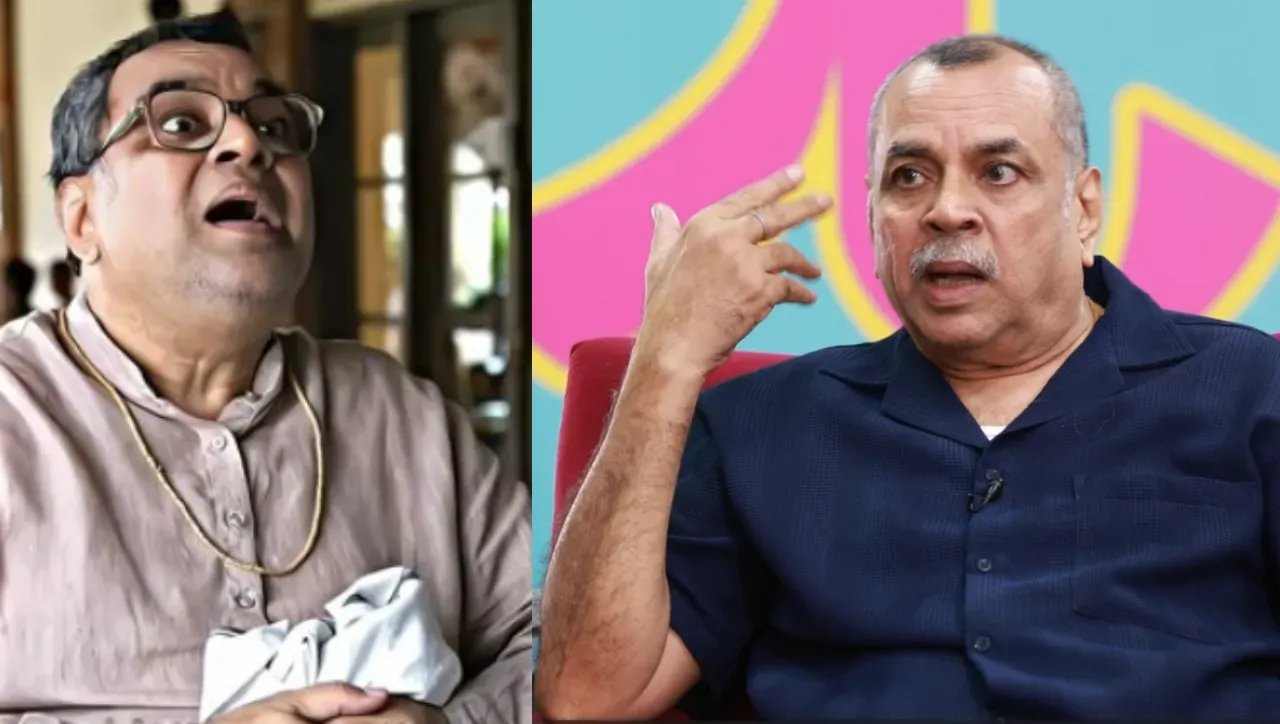
.webp)